राजस्थानी चित्रकला
राजस्थानी चित्रकला भारतीय चित्रकला के अन्तर्गत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और भारतीय कला के इतिहास में भी इसका अपना विशिष्ट स्थान है। कुछ विद्वान इसे राजपूत चित्रकला और कुछ विद्वान इसे राजस्थानी चित्रकला कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला को केवल राजपूत शैली या हिन्दू शैली की संज्ञा देना उचित नहीं है वरन् यह अनेक शैलियों का समन्वित रूप है।
राजस्थानी चित्रकला का विकास-
राजस्थान में प्रागैतिहासिक
काल से चित्रकारी होती रही है जिसके साक्ष्य चम्बल नदी घाटी क्षेत्र में
तथा क्षेत्रों की पहाड़ियों, शैलाश्रयों में चित्रांकन के रूप में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पायुगीन
कालीबंगा तथा ताम्रयुगीन आहड़ पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त मृदपात्रों
पर की गई चित्रकला उल्लेखनीय हैं।

राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों की विशेषताएँ
प्राचीनकाल में पोथियाँ
लेखन के साथ चित्रित भी की जाती थीं। यह कार्य भोजपत्रों एवं ताड़पत्रों
पर किया जाता था। इनमें पत्रों में छेदकर ग्रन्थित करने के कारण इन्हें ग्रन्थ
कहा जाता है। इस प्रकार के अनेक ग्रन्थ आज भी जैन भण्डारों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित
हैं। जैसलमेर के भण्डारों में 1060 ई. के दो ग्रन्थ 'ओधनियुक्ति वृत्ति'
तथा 'दश वैकालिका सूत्रचूर्णि' उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार 'सावगपड़िकमण सुत्त
चुन्नी' तथा 'सुपासनाहचरित्रम'
भी महत्त्वपूर्ण चित्रित ग्रन्थ हैं।
राजस्थानी चित्रकला
की विभिन्न शैलियाँ
17वीं तथा 18वीं शताब्दी में राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अलवर, नाथद्वारा आदि चित्र शैलियों का विकास हुआ। राजस्थान के विभिन्न राज्यों में चित्रशैली का विकास कुछ स्थायी विशेषताओं के साथ हुआ। अतः विभिन्न राज्यों में विकसित चित्र शैली का नामकरण भी उन राज्यों के नाम के आधार पर ही किया गया।
राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों का विवेचन
निम्नलिखित है-
मेवाड़ चित्रकला शैली
अरबों के आक्रमण
के परिणामस्वरूप गुजरात के कलाकार भागकर सबसे पहले मेवाड़ में आए।
गुजरात के चित्रकार अजन्ता परम्परा शैली में प्रशिक्षित थे, अत: उन्होंने अजन्ता शैली
के साथ स्थानीय शैली का सामंजस्य करके चित्रकला को एक नवीन रूप दिया जिसे हम मेवाड़
शैली कहते हैं। मेवाड़ शैली में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रन्थ 'श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि' है जिसे 1260 ई. में चित्रित किया गया था। इसी प्रकार 1423 ई.
में चित्रित 'सुपासनाहचरित्रम'
तत्कालीन मेवाड़ शैली का उदाहरण है।
16वीं शताब्दी में मेवाड़ शैली में परिवर्तन आने लगा। अब चेहरों में सुघड़ता
तथा रंगों में विविधता आ गई और आकृतियाँ भावना-प्रधान होने लगी। इन चित्रों
में पेड़-पौधों का चित्रण अलंकरण के लिए किया गया। प्रतापगढ़ में रचित 'चौर पंचशिखा' मेवाड़ की इस परिवर्तित शैली का
उत्कृष्ट नमूना है।
17वीं शताब्दी के आरम्भ तक मेवाड़ की अपनी एक शैली बन चुकी थी। महाराणा
अमरसिंह ने चावण्ड में रागमाला का सेट बनवाया। 1615
की मेवाड़-मुगल सन्धि के बाद मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने
लगा। 1640 ई. के आसपास बने नायिका भेद के चित्र इस
समय के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। महाराणा जगतसिंह के शासनकाल (1628-1652 ई.) में मेवाड़ शैली का अत्यधिक विकास हुआ। इस युग में राधा-कृष्ण
चित्रों के केन्द्र-बिन्दु थे। इस समय 'भागवत पुराण'
की अनेक प्रतियाँ चित्रित हुई जिनमें साहेबदीन द्वारा
चित्रित 'पुराण भागवत' उल्लेखनीय
है। 1649 ई. में मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण को
चित्रित किया।
महाराणा जगतसिंह के समय में भी मेवाड़ चित्रशैली का पर्याप्त
विकास हुआ तथा महाराणा राजसिंह (1652-1680 ई.) और महाराणा जयसिंह (1680-1698 ई.) के समय में मेवाड़ चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हो गई। इस
शैली में मुगल सजावट अधिक बढ़ती चली गई। इस काल में 'रागमाला',
'बारहमासा', 'कादम्बरी',
'मालती माधव', 'पृथ्वीराज री वेल' आदि
ग्रन्थ चित्रित किए गए। इन चित्रों में तत्कालीन समाज की झाँकी दिखाई देती है
परन्तु उनमें शृंगारिकता का पुट भी है। इस काल की चित्रकला पर मुगल
चित्रकला का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता दिखाई देता है
18वीं शताब्दी में व्यक्ति-चित्र, दरबार के दृश्य,
अन्तःपुर की झाँकियाँ, शिकार के दृश्य आदि
चित्रकला के विषय बन गए। भित्ति-चित्रों की प्रधानता भी बढ़ी। मेवाड़ के महाराणाओं
के पुराने महलों तथा सामन्तों की हवेलियों में भित्ति-चित्रों के श्रेष्ठ नमूने
मिलते हैं।
मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताएँ-
1. रंगों का प्रयोग-
मेवाड़ शैली के
चित्रों में लाल, पीले, नीले आदि गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है।
इनमें हिंगुल रंग विशिष्ट है। रात्रि के दृश्यों को दिखाने के लिए
गहरे नीले रंग या धुएँ के रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है। लाल रंग की
पृष्ठभूमि से नीले, पीले, हरे और काले
रंग की रूपाकृतियाँ उभारी गई हैं। कहीं-कहीं स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है, जो मुगल प्रभाव को प्रकट करता है।
2. पुरुष आकृतियाँ-
पुरुष आकृतियों
में नुकीली नाक, गोल तथा अण्डाकार चेहरे मछली जैसी आँखें, ठोड़ी तथा
गर्दन के बीच का भाग अधिक पुष्ट चित्रित किया गया है। पुरुष आकृतियाँ लम्बी तथा
पतले शरीर की चित्रित हैं। स्त्रियाँ आकार में कुछ छोटी बनाई गई हैं। अजन्ता
परम्परा के प्रभाव के कारण हस्त-मुद्राएँ तथा अंग-भंगिमाएँ सुन्दर हैं।
3. वेशभूषा-
पुरुषों की
वेशभूषा में गोल घेरदार जामा दिखाया गया है। कमर में रंगीन पट्टियों से
अलंकृत लम्बे पटके दिखाए गए हैं। स्त्रियों की वेशभूषा में फूल व बूटों से
सुसज्जित छींट के लहंगे, कसी हुई चोलियाँ, पारदर्शक चिपकी ओढ़नी आदि दिखाई गई
हैं। चित्रों में स्त्रियों को कर्णफूल, गले में हार,
हाथों में चूड़ियाँ, भुजबन्द से लटकते हुए
फुंदे व चोटियों से गुंथे मोती तथा फूलमालाएँ आदि पहने हुए चित्रित किया गया है।
4. विषय-
मेवाड़ में नायक
व नायिका के रूप में विभिन्न क्रियाएँ करते हुए कृष्ण और राधा
चित्रकारों के प्रमुख विषय बन गए। बिहारी सतसई, पंचतंत्र की कहानियाँ, पृथ्वीराज रासो, नल दमयन्ती और मीरा की जीवनी आदि से सम्बन्धित चित्र बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति चित्र, दरबार के दृश्य,
हरम की झाँकियाँ, सवारी और शिकार के दृश्य आदि
मेवाड़ चित्रकला के विषय बन गए।
5. प्राकृतिक उपमानों से
अलंकृत-
मेवाड़ चित्रकला
की एक प्रमुख विशेषता उसका प्राकृतिक उपमानों से अलंकृत करना भी रहा है।
6. प्रकृति का चित्रण-
मेवाड़ के
चित्रों में प्रकृति का संतुलित चित्रण किया गया है। पशु-पक्षियों का भी चित्रण
किया गया है। पक्षियों में चकोर, हंस, मयूर तथा पशुओं में हाथी,
घोड़े, हिरण व शेर आदि विशेष रूप से चित्रित हैं।
7. भित्ति चित्र-
मेवाड़ चित्रकला
में भित्ति चित्र की भी परम्परा रही है। उदयपुर के राजप्रासादों के चित्र, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप तथा मुगल बेगमों के चित्र अपनी मौलिकता के साथ चित्रित
हैं।
मारवाड़ चित्रकला शैली
मारवाड़ की
स्वतन्त्र शैली का प्रादुर्भाव राव मालदेव (1537-1562 ई.) के समय में हुआ। जोधपुर दुर्ग
में चोखेला व महलों की छतों पर राम-रावण युद्ध के चित्र चित्रित किये गये
हैं जिनसे मालदेव की सामरिक रुचि की अभिव्यक्ति होती है। मोटा राजा उदयसिंह
(1583-1595 ई.) के समय में मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का
काफी प्रभाव पड़ा। 1610 ई. में चित्रित 'भागवत पुराण' में मुगल शैली के प्रभाव का बोध
होता है, जिसमें कृष्ण-अर्जुन को बहुवादी आकृतियाँ स्थानीय
शैली की हैं जबकि उनकी वेशभूषा मुगलों जैसी है। गोपिकाओं के चित्रण में
उनकी वेशभूषा मारवाड़ी है, जबकि उनके आभूषण मुगलों के समान
हैं।
1623 ई. में चित्रित 'कल्याणी रागिनी' के चित्र में नायक नायिका को आलिंगनबद्ध किये शयन-कक्ष की ओर ले जा रहा
है। चित्र का चित्रण मारवाड़ी शैली में किया गया है, परन्तु
शयन-कक्ष में रखा लोटा मुगल कला का प्रभाव दर्शाता है। महाराजा सूरसिंह (1595-1620 ई.) के समय में ढोला-मारु के चित्रों में भी मुगल शैली का प्रभाव
अधिक दिखाई देता है।
17वीं शताब्दी के चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव था। महाराजा जसवन्तसिंह
(1638-1678) को मुगल चित्रकला में अधिक अभिरुचि थी। जसवन्तसिंह
के बने चित्रों में आभूषणों की बनावट, वेशभूषा, बाग-बगीचों की सजावट, हुक्का आदि मुगल शैली के
अनुरूप हैं। अजीत सिंह के शासनकाल (1708-1724 ई.) में
भी मारवाड़ शैली मुगल शैली से प्रभावित थी। जोधपुर के चित्रकार मुगल चित्रकारों की
भाँति अन्तःपुर, तुर्की स्नानागार आदि के चित्र बनाने लगे। 18वीं शताब्दी के अन्त में महाराजा विजयसिंह के काल में भक्तिरस तथा
शृंगार रस के चित्र अधिक मिलते हैं। इस समय ग्रन्थ चित्रण का कार्य अधिक हुआ। महाराजा
मानसिंह के शासनकाल में चित्रकला की खूब उन्नति हुई तथा काफी वृत्त चित्र बनाए
गए।
मारवाड़ चित्र शैली की विशेषताएँ-
1. वेशभूषा-
मुगल चित्रकला
से प्रभावित होने के कारण चित्रित शासकों व उनके सामन्तों की वेशभूषा मुगलों
के समान है। पुरुष वेशभूषा में सफेद जामों की अधिकता, रंग-बिरंगो पगडिया यादि उल्लेखनीय
हैं । स्त्री पोशाक में लहंगों के नीचे के भाग काफी चौड़े तक फैले हुए हैं।
2. आकृतियाँ-
मारवाड़ी
चित्रों को आकृति भावपूर्ण हैं तथा उनके चेहरे सुदृढ़ हैं। गोल मुहँ, तिरछी आँखों वाले नारी चेहरे चित्रित
किए गए हैं। पौरुषयुक्त गोल मुहँ वाले पुरुष चेहरे चित्रित किए गए हैं।
3. विषय-
मारवाड़
चित्रशैली के विषय विभिन्न हैं। उनमें प्रेम-कथाओं के चित्रण जैसे डोला-मारु
तथा सोहनी-महिवाल के चित्रण, केशव तथा मतिराम को साहित्यिक कृतियों पर आधारित चित्र,
विभिन्न प्रस्तुओं का चित्रण, धार्मिक विषय से
सम्बन्धित चित्रण आदि उल्लेखनीय हैं।
मारवाड़
चित्रकला के अन्तर्गत कृष्णलीला, पशु-युद्ध, विवाह-उत्सव, शिकार
के दृश्य, दरबार, शाहो शोभा-यात्रा के दृश्य, रागमाला, गीत-गोविन्द
के चित्र आदि उल्लेखनीय हैं।
4. रंग-
मारवाड़ शैली के
चित्रों में लाल, पोले, काले, नीले और सुनहरे
रंगों जैसे चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें लाल और पीले रंगों का अधिक
प्रयोग किया गया है। 18वीं शताब्दी के चित्रों में सुनहरी
रंग का प्रयोग भी किया गया है, जो मुगल प्रभाव का प्रतीक है।
5. स्थानीय शैली-
स्त्रियों के
चित्रण में मारवाड़ी चित्र शैली स्थानीय रही है। उनके परिधान तथा आभूषण स्थानीय
रहे हैं।
6. पुरुषों और स्त्रियों
का चित्रण-
मारवाड़ी शैली
के चित्रों में पुरुषों का लम्बा कद, संजीदा आँखें, दाढ़ो, घनी मूंछ, गठीले बदन और आभूषणों से अलंकृत दिखाया
गया है। स्त्रियों का लम्बा कद, तलवार से तीखे नयन, पतली कमर और लम्बी भुजा दिखाई गई हैं।
7. अजन्ता शैली से
प्रभावित-
मारवाड़
चित्रशैली अजन्ता परम्परा से भी प्रभावित है।
किशनगढ़ चित्रकला शैली
किशनगढ़ के शासक
रूपसिंह, मानसिंह,
राजसिंह, सावन्तसिंह आदि चित्रकला के
संरक्षक थे। उनके शासनकाल में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। सावन्तसिंह के
शासनकाल (1748-1764 ई.) में किशनगढ़ चित्रकला अपनी समृद्धि
की चरम सीमा पर पहुँच गई। सावन्तसिंह नागरीदास के नाम से भी प्रसिद्ध था।
सावन्तसिंह स्वयं एक उच्च कोटि का चित्रकार था। वह अपनी प्रेमिका बनी-ठनी में राधा
का रूप देखता था। निहालचन्द नागरीदास के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था।
निहालचन्द तथा नागरीदास ने जो राधा-कृष्ण के चित्र बनाये, उनमें बनी-ठनी को हो राधा के रूप में चित्रित किया।
निहालचन्द के
द्वारा किया गया राधा का चित्रण राजस्थानी कला की एक बड़ी उपलब्धि है। राधा के
चित्रण में उसको सुन्दर वेशभूषा, नुकीली नाक, संजन के समान नेत्र, उभरा हुआ कोणीय चेहरा, पतले होंठ, तीखी ठोड़ी, लम्बी गर्दन आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय
हैं। 19/ शताब्दी के उत्तरार्द्ध में निहालचन्द द्वारा बनाया
गया कृष्ण-लीला का चित्र एक मौलिक एवं सुन्दर रचना है, जिसमें
पेड़, फूलों और पानी के श्रेष्ठ रंगों का प्रयोग किया गया
है। डॉ. जी. एन. शर्मा का कथन है कि कला, प्रेम और
भक्ति का सर्वांगीण सामंजस्य हमें किशनगढ़ शैली में देखने को मिलता है।
निहालचन्द और सावन्तसिंह द्वारा प्रारम्भ की गई
किशनगढ़ शैली की उन्नत परम्परा बाद में भी चलती रही जिसे हम पिछवाई पर देख
सकते हैं। निहालचन्द के बाद अमरचन्द, सीताराम, मेघराज, कल्याणदास,
नानगराम, सूरतराम, रामनाथ
आदि चित्रकारों ने किशनगढ़ चित्रकला के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
किशनगढ़ चित्रकला की विशेषताएँ-
1. विषय-
किशनगढ़ चित्रकला के चित्रों में विषयों की
विविधता मिलती है। इस शैली के चित्रों के विषय आखेट दृश्य, दरवार, व्यक्ति
चित्र, राधा और कृष्ण, कृष्ण-लीला,
नायक-नायिका भेद, राग-रागनियाँ, वैभव, विलास, पशु-पक्षी,
प्रकृति चित्रण आदि रहे हैं।
2. प्रकृति चित्रण-
प्रकृति चित्रण
में कमल से भरे तालाब, पक्षियों की पंक्तियाँ, फूलों से परिपूर्ण बगीचे,
आकाश में छिटकते हुए तारे एवं चन्द्रमा, आम्रकुंज,
बाग-बगीचों में विचरण करते राधा-कृष्ण, यमुना
में नौका-विहार आदि उल्लेखनीय हैं।
3. चित्र-
परिकोणात्मक
प्रभाव-इस शैली के चित्रों में त्रि-परिकोणात्मक प्रभाव दिखाई देता है।
पशु-पक्षियों का विचरण, मयूर, हरे और लाल तोते, हिरण
के जोड़े बड़ी सुन्दरता से चित्रित किए गए हैं।
4. नारी-सौन्दर्य-
नारी-सौन्दर्य
का प्रदर्शन इस शैली को प्रमुख विशेषता है। नारी-चित्रण में लम्बा कद, लम्बा चेहरा, नुकीली नाक, पतले होंठ, खंजन
आकार के नेत्र, पतली कमर आदि दिखाए गए हैं।
5. वेशभूषा-
स्त्रियों को
लहंगा, चोली तथा
पारदर्शी चुनरी पहने हुए चित्रित किया गया है। अलंकरण के लिए आभूषणों का अत्यधिक
प्रयोग किया गया है। मोतियों का भव्य चित्रण किशनगढ़ शैली की एक अन्य विशेषता है।
पुरुषों को लम्बा जामा, पाजामा या धोती, सिर पर पगड़ी तथा कमर में पटका धारण किए हुए दिखाया गया है।
6. रंग-
इस शैली के
चित्रों में अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों को दृष्टि से प्रायः हरा, नीला, गुलाबी,
भूरा, सफेद सुनहरा, पीला
तथा नारंगी रंग अधिक काम में लिए गए हैं।
7. शैली की विशिष्टता-
इस शैली के
चित्रों में रंगों की सुयोजना, वस्त्रों की सज्जा, परिधानों और मोती-हीरों के
चित्रण का अनुपम सौन्दर्य दर्शित है। मोतियों का भव्य चित्रण इस शैली की एक अन्य
विशेषता है।
बीकानेर चित्रकला शैली
बीकानेर के शासक
रायसिंह के शासनकाल (1574-1612) में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। उसके समय से बीकानेर की चित्रकला पर मुगल
शैली का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इस समय भागवत पुराण, रसिकप्रिया और रागरागिनी के चित्र बनाए गए। बीकानेर के महाराजा
अनूपसिंह के शासनकाल (1669-1698 ई.) में बीकानेर
चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। इस समय धार्मिक एवं पौराणिक चित्र, रागमाला, बारहमासा, दरबार के
चित्र बनाए गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अनेक
मुस्लिम चित्रकार बीकानेर में आकर बस गए। उनके द्वारा बनाए गए चित्र मारवाड़ी शैली
तथा मुगल शैली से ही प्रभावित थे।
18वीं शताब्दी में बीकानेर शैली पर जोधपुर शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता
है। बीकानेर दुर्ग के महलों के भीतरी भागों की दीवारों पर शिकार के दृश्य, हरम के दृश्य, पुराण आदि का चित्रण इसका श्रेष्ठ
उदाहरण है। पंजाब की सीमा से सटा होने के कारण बीकानेर की चित्रकला पंजाब की
चित्रकला से भी प्रभावित हो गई।
बीकानेर चित्रकला की विशेषताएँ-
1. विषय-
इस शैली में
भागवत गीता, पौराणिक कथाओं, कृष्णलीला, शिकार, दरबार के दृश्य, रसिकप्रिया, रागमाला आदि से सम्बन्धित चित्रों का निर्माण
किया गया।
2. आकृतियाँ-
नारी चित्रण में
बड़ी आँखें, पतली कमर, उभरा वक्षस्थल, लम्बी चोटी आदि दिखाए गए हैं। छोटी ऊँची कसी हुई
चोली, रंगीन घेरावदार घाघरा, सुनहरी ओढ़ना ओढ़े स्त्रियों को दशार्या गया है।
3. मुगलकला का प्रभाव-
मुगलकला की
भाँति बीकानेर के चित्रों का रेखांकन बारीक है।
4. चित्रों का प्रौढ़ रूप-
बीकानेर शैली के
चित्रों का प्रौढ़ रूप अनूपमहल तथा फूलमहल की सज्जा में, चन्द्रमहल तथा
सुजानमहल के दरवाजों की चित्रकारी में और रागमाला तथा बारहमासा के दृष्टान्त
चित्रों में दिखाई देता है।
5. दक्षिण का प्रभाव-
बीकानेर की
चित्रकला दक्षिण भारत की चित्रकला से भी प्रभावित है।
जयपुर चित्रकला शैली
जयपुर चित्रकला
पर मुगल शैली का काफी प्रभाव पड़ा। आमेर के महलों में सजावट तथा अलंकरण आदि मुगल
शैली के अनुरूप हैं, परन्तु चित्रों के विषय हिन्दू धर्म से
सम्बन्धित हैं। 17वीं शताब्दी के शुरू में बने 'रसिक प्रिया के
चित्र तथा 17वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में बने चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता
है। 17वीं शताब्दी के अन्त तथा 18वीं शताब्दी के शुरू में बने ‘कृष्ण लीला', 'गोवर्द्धन धारण', 'गोवर्द्धन पूजा', 'रागमाला', 'बारहमासा' आदि के चित्रों
में भी मुगल शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन चित्रों में स्थानीय मौलिकता
होते हुए भी रंगों का संयोजन मुगल शैली के आधार पर हुआ है।
सवाई जयसिंह के
शासनकाल में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। इस समय अनेक सचित्र ग्रन्थों की रचना
हुई जिनमें 'बिहारी सतसई' का चित्रण उल्लेखनीय है। साहिबराम तथा मुहम्मद
शाह उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस काल के चित्रों में हिन्दू शैली का
प्रभाव दिखाई देता है। यह शैली जयपुर के महलों के भित्ति-चित्रों में देखी जा सकती
है।
सवाई ईश्वरी
सिंह के समय में व्यक्ति चित्र, शिकार के चित्र, हाथियों की लड़ाइयों के चित्र तथा राजकीय
सवारियों के चित्र खूब बनाए गए। ये चित्र काल्पनिक न होकर चित्रकार द्वारा अपनी
आँखों से देखी घटनाओं के आधार पर बनाए गए थे। सवाई माधोसिंह के शासनकाल में भी
चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था।
सिसोदिया रानी का उद्यान भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के पोथीखाना
में सुरक्षित असावरी रागिनी' के चित्र में शबरी की वेशभूषा य आभूषण आदि में
जयपुर शैली की प्राचीनता देखी जा सकती है।
सवाई प्रतापसिंह
के शासनकाल (1778-1803) में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। स्वयं
प्रतापसिंह एक उच्चकोटि का संगीतज्ञ एवं चित्रकार था। उसने 'कृष्ण लीला', 'नायिका भेद' एवं रागों से
सम्बन्धित चित्र बनाए। चित्रों में हरे, गुलायी, भूरे तथा पीले रंग का प्रयोग किया गया। उसके समय
में पुष्टि मार्ग से सम्बन्धित अनेक चित्रों का निर्माण किया गया जिनमें
गोवर्द्धन-धारण व गोवर्द्धन-पूजा के चित्र उल्लेखनीय हैं।
19वीं शताब्दी के मध्य में जयपुर शैली की चित्र
परम्परा अवनत होती दिखाई देती है। धीरे-धीरे जयपुर की चित्रकला का यूरोपीयकरण होने
लगा। सवाई रामसिंह के काल में 1850 ई. के आसपास बने देवी सरस्वती के चित्र में
हिन्दू देवी को मुगलों के समान दिखाया गया है, परन्तु उसे कुर्सी पर बिठाकर उसको यूरोपीय शैली
से प्रभावित दिखाया गया है।
जयपुर चित्रकला की विशेषताएँ-
1. व्यक्ति चित्र-
जयपुर शैली में
व्यक्ति चित्रों को विशेष स्थान प्राप्त है। राजाओं के चित्र अधिकांश विशाल आकृति
के मिलते हैं। इस शैली में कृष्ण से सम्बन्धित चित्र भी बनाए गए हैं।
2. संयोजन-
इस शैली में
संयोजन अलंकारिक व सन्तुलित है। चित्रों में एक चश्म चेहरे अधिकतर बनाए गए हैं।
मुद्राएँ आकर्षक व भावपूर्ण हैं।
3. वेशभूषा-
स्त्रियों को
घेरदार घाघरा, पायजामा तथा छोटी ओढ़नी पहने हुए चित्रित किया गया है। इस प्रकार स्त्रियों की
वेशभूषा पर मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अलंकरण में प्रयुक्त आभूषणों पर भी मुगल
प्रभाव दिखाई देता है।
4. रंग-
जयपुर शैली के
चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले, सफेद रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है।
5. प्राकृतिक
वातावरण-
इस शैली के
चित्रों में प्राकृतिक वातावरण अलंकारिक है।
6. आकार-
इस शैली के
अधिकांश चित्रों का आकार सामान्यत: विशाल है।
7. विषय-
कृष्णलीला, गोवर्द्धन धारण, गोवर्धन पूजा, रागमाला, बारहमासा, सवारी और शिकार
के दृश्य, भागवत पुराण, प्रकृति चित्रण, हाथियों की लड़ाई आदि से सम्बन्धित अनेक चित्र
बनाए गए। नायिका भेद के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। पशु-पक्षियों का चित्रण यथार्थ
और सुन्दर है। इस शैली में स्त्री-पुरुष, व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों पर चित्र बनाए गए।
8. भित्ति चित्र-
जयपुर के
राजप्रासादों एवं प्रमुख हवेलियों में भित्तिचित्र देखे जा सकते हैं। राजा मानसिंह
के काल के भित्तिचित्रों में बारामासा, रागमाला, भागवत पुराण को चित्रित किया गया है।
9. मुखाकृति-
जयपुर शैली में
मुखाकृति चित्रण भी काफी लोकप्रिय रहा है। सवाई जयसिंह तथा प्रतापसिंह के चित्र
उल्लेखनीय हैं।
बूंदी चित्रकला शैली
प्रारम्भ में
बूंदी चित्रकला शैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ा। बूदी के शासक सुर्जन हाड़ा (1554-1585) के शासनकाल में
बूंदी की चित्रकला पर मुगल चित्रकला का काफी प्रभाव पड़ा। बूँदी के शासक रत्नसिंह
के शासनकाल (1607-1631 ई.) में भी बूंदी शैली का पर्याप्त विकास हुआ। उसके समय
में बने चित्र 'रागमाला' तथा 'रागिनी भैरव' में मेवाड़ी, मुगल व दक्षिण शैलियों का समन्वय दिखाई देता है।
शत्रुसाल ने भी चित्रकला के विकास में योगदान दिया। अब बूँदी चित्रकला पर मुगल
प्रभाव और बढ़ गया तथा 1692 ई. के बसन्त रागिनी के चित्र में
राजा और रानी बगीचे में खड़े नये चाँद को देख रहे हैं। इसमें वृक्षों, फूलों, पानी के कुण्ड, तालाबों आदि का
चित्रण चित्र को रोमांटिक बनाने के लिए हुआ है। इसमें रंगों का संयोजन मुगल शैली
से उन्नत है।
महाराव
उम्मेदसिंह के शासनकाल (1734-1771 ई.) में बूंदी
की चित्रकला अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंच गई। इस काल के बने चित्रों में
अधिकतर विभिन्न ऋतुओं का चित्रण किया गया है। उदाहरणार्थ वर्षा ऋतु दिखाने के लिए
चित्र में काले बादल, नाचते मोर, झूमते हाथो, बहते हुए झरने आदि का अंकन हुआ है। ग्रीष्म ऋतु
के चित्रों में प्रेमी-प्रेमिका को फव्वारे के पास बैठा दिखाया गया है। इस काल में
नायक-नायिका भेद के चित्र भी कुशलता से बनाए गए हैं। इस काल में बना 'राधा और कृष्ण
का मिलन' चित्र भावात्मक सौन्दर्य-चित्रण का उत्कृष्ट
नमूना है।
महाराव विशनसिंह (1773-1821 ई.) के समय में शेरों के शिकार के चित्र अधिकता
से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों पर फुदकते बन्दरों का चित्रण भी सुन्दर और
सजीव है। महाराव रामसिंह (1821-1862 ई.) के काल में वैष्णव धर्म से सम्बन्धित चित्र
अधिक मिलते है।
बूंदी शैली की विशेषताएँ-
1. मानव आकृतियाँ-
नारी चित्रांकन
में कोमलता तथा सुन्दरता के भाव दिखाई देते हैं। स्त्रियों की लम्बी आकृति, पतली कमर, तीखी नाक, पतली ठोड़ी, बादाम के सामान
नेत्र, गोलाकार मुख आदि उल्लेखनीय हैं। पुरुष आकृतियाँ सुडौल बनाई गई हैं।
2. रंग-
बूंदी शैली के
चित्रों में सोने तथा चाँदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। चित्रों में
अधिकतर नीले, लाल, पीले तथा हरे रंगों का प्रयोग किया गया है।
3. भू-दृश्य-
इस शैली की
मुख्य विशेषता भू-दृश्य है। चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकतर वनस्पति से ढके हुए
टीले दिखाए गए हैं। चित्रों के ऊपरी भाग में वृक्षों की पंक्तियाँ बनाना तथा नीचे
पानी, कमल, बतखें आदि चित्रित करना भी बूंदी शैली की विशेषता है।
आकाश का चित्रण
भी आकर्षक है। चित्रों में कदली, आम व पीपल के वृक्षों के साथ-साथ फूल-पत्तियों
की बेलों एवं पशु-पक्षियों को चित्रित करना परम्परा-सी हो गई थी। हरे-भरे पहाड़, घनी वनस्पति, चिड़िया, कमल, पानी में तैरती बत्तखें, मछलियाँ आदि भी
चित्रित किए गए हैं।
4. स्थापत्य का
प्रदर्शन-
बूंदी शैली के
चित्रों में स्थापत्य का प्रदर्शन मुगल शैली के अनुरूप है। गुम्बदों से युक्त भवन, चबूतरे तथा
बरामदे मुगल शैली के प्रतीक हैं। पृष्ठभूमि में चौकोर बने भवन भी दिखाये गये हैं।
5. स्त्रियों की
वेशभूषा-
स्त्रियों की
वेशभूषा में लहंगा, चोली तथा ओढ़नी, पटका आदि प्रमुख वस्त्रों के रूप में दिखाए गए
हैं। स्त्रियाँ लाल तथा पीले वस्त्र अधिक पहने हुई दिखाई गई हैं। स्त्रियों को नाक, कान, गले व हाथ में
कई आभूषण पहिनाकर चित्रकार ने चित्रों को सुन्दर व सजीव बना दिया है।
6. पुरुषों की
वेषभूषा-
पुरुषों की
वेशभूषा में पारदर्शी घेरदार जामा, चौड़ा पटका आदि पहनावे में मुगल शैली का प्रभाव
स्पष्ट दिखाई देता है। अटपटी पगड़ी बूंदी शैली की अपनी विशेषता है।
7. अलंकरण-
चित्रों में
अलंकरणों को प्रमुखता दी गई है। पशु-पक्षियों को सुन्दर ढंग से चित्रित किया गया
है। हाथी का चित्रण बड़ा सुन्दर एवं सजीव है।
8. विषय-
बूंदी चित्रकला
के विषयों में शिकार, सवारी, रासलीला, स्नान करती हुई नायिका, उत्सव, प्रकृति के
विभिन्न स्वरूपों का चित्रण, घने जंगलों में विचरण करते हुए शेर, हाथी, हिरण, आकाश में उड़ते
हुए पक्षी, पेड़ों पर फुदकते बन्दर आदि रहे हैं। श्रावण-भादो में नाचते हुए मोर बूंदी की
चित्रकला परम्परा में अनुपम एवं आकर्षक बन पड़े हैं। राग-रागणियाँ, नायक-नायिका
भेद, बारहमासा, ऋतुएँ, कृष्णलीला के भेद आदि भी चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं।
9. दृश्य चित्र-
बूंदी शैली के
दृश्यं चित्र अधिक यथार्थ बन पड़े हैं। रंग-विन्यास की दृष्टि से सुन्दर गहरे
रंगों से चित्रों को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। नारियों के चित्र बड़े
सुन्दर हैं। बूंदी चित्रकला की यह एक विशेषता रही है कि चेहरे लाल-भूरे रंग में
दिखाये गए।
कोटा चित्रकला शैली
कोटा की चित्र
शैली में बूंदी शैली और मुगल शैली का सामंजस्य होते हुए भी कोटा में एक नवीन शैली
का प्रादुर्भाव हुआ। कोटा के शासक रामसिंह तथा अर्जुनसिंह के काल
में कोटा चित्र शैली में मौलिकता आने लग गई थी, फिर भी उस पर बूंदी शैली का प्रभाव यथावत् वना
रहा। महाराव उम्मेदसिंह के शासनकाल (1771-1820 ई.) में कोटा चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच
गई थी। इस समय के अधिकांश चित्रों में महाराव उम्मेदसिंह को शिकार करते हुए
दिखाया गया है।
कुछ चित्रों में
कोटा के शासकों को श्रीनाथजी की पूजा करते दिखाया गया है। मथुराधीश के मन्दिर में
श्रीनाथजी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले कपड़ों पर भी सुन्दर चित्र बनाए गए, जिन्हें 'पिछवाई के चित्र' कहा जाता है। महाराव रामसिंह द्वितीय के
शासनकाल (1828-1866 ई.) के चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है।
कोटा चित्रकला शैली की विशेषताएँ-
1. विषय-
कोटा चित्रकला
के विषयों में शिकार के दृश्य, दरबार के दृश्य, धार्मिक कथाओं के दृश्य, भित्ति चित्र
आदि उल्लेखनीय हैं।
2. मानव आकृतियाँ-
स्त्रियों का
ललाट काफी चौड़ा, आँखें बड़ी-बड़ी, खंजर के समान आँखें, नाक छोटी, ठुड्डी गोल, वक्षस्थल काफी
ऊँचा और कमर अत्यधिक पतली दिखाई गई है। आभूषण भी बहुलता से दिखाए गए हैं।
3. रंग-
इस शैली के
चित्रों में नीले, हरे, काले, लाल आदि रंगों का प्रयोग किया गया।
4. भित्ति चित्र-
कोटा शैली में
भित्ति चित्रों का निर्माण भी किया गया। कोटा के भित्ति चित्रों में हाथियों की
लड़ाई, स्वस्तिक, मंगलकलश, तोते और मोर के चित्र उल्लेखनीय है। चित्रों के किनारे लाल, काले और सुनहरी
रंगों से बनाए गए हैं। राजमहलों, हवेलियों आदि में बने हुए भित्ति चित्र काफी
आकर्षक हैं।
नाथद्वारा चित्रकला शैली
नाथद्वारा वल्लभ
सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध केन्द्र है। अत: यहाँ के चित्रकारों ने ईश्वर रूप की
लीलाओं को चित्रित करना आरम्भ किया। श्रीनाथजी की छवि, गुसाइयों के
दैनिक जीवन तथा उनकी श्रीनाथजी की पूजा करते हुए दिखाना, कृष्ण-लीला आदि
चित्रों के विषय थे। बाल-लीला के पद, बाल-गोपाल का हँसना, हिंडोले में
झूलना, यशोदा से माखन माँगना आदि प्रसंगों का रोचक चित्रण किया गया।
इस शैली में
राग-रागिनियों के जमघट तथा ऋतु वर्णन और प्रेम-कथाओं के चित्रण का अभाव है। इस
शैली में तो बलदाऊ की जोड़ी, नन्द की गायों का कालिन्दी के तट-प्रस्थान, ग्वालों का
कृष्ण के साथ माखन के लिए जाना, गोपियों से छेड़छाड़, माखन चोरी आदि
बाल-लीला के प्रसंग अधिकता से चित्रित कियेग गए हैं। परन्तु इनमें राजस्थान तथा
अन्य उत्तरी भागों की शैलयों का समावेश हुआ, जिससे एक नई नाथद्वारा शैली का
प्रादुर्भाव हुआ।
नाथद्वारा शैली के चित्रों में सबसे महत्त्वपूर्ण
है-पिछवाई। श्रीनाथजी की प्रतिमा के पीछे दीवारों को सजाने के लिए कपड़ों
पर मन्दिर के आकार के अनुसार चित्र बनाए जाते हैं। यह नाथद्वारा शैली
की अपनी मौलिकता है।
अलवर चित्रकला शैली
अलवर शैली में मुगल
प्रभाव की अधिकता दिखाई देती है। इस शैली के चित्रों में मुगलकालीन
चित्रों जैसा बारीक काम, परदों पर धुएँ के समान छाया तथा रेखाओं की
सुदृढ़ता दर्शनीय है। अलवर शैली में गणिकाओं के चित्र अत्यन्त आकर्षक बनाए जाते
हैं। हाशियों में बेलबूटों का प्रयोग करने में यहाँ के चित्रकार निपुण थे। अलवर के
लघु चित्रों में हरे व नीले रंग का अधिकता से प्रयोग किया गया है।
आशा है कि हमारे
द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो
इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।




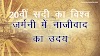









0 Comments