वियना कांग्रेस के सिद्धान्त,
प्रादेशिक व्यवस्था
मेटरनिख के विशेष
संदर्भ में वियना कांग्रेस के सिद्धान्त व प्रादेशिक व्यवस्था
नेपोलियन के पतन से यूरोप में अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गई थीं। इन समस्याओं की पृष्ठभूमि में वियना कांग्रेस का सम्मेलन सितम्बर 1814 ई. में प्रारम्भ हुआ। किन्तु एल्बा से नेपोलियन के पुनः आगमन के कारण सम्मेलन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो गई। मित्र राष्ट्र अपने पारस्परिक मतभेद भुलाकर यूरोप की शान्ति भंग करने वाले नेपोलियन के विरुद्ध एक हो गये।
वाटरलू के युद्ध में 18 जून
1815 को नेपोलियन का अन्तिम रूप से पतन हुआ तथा दूसरी ओर युद्ध से
कुछ ही दिन पूर्व 9 जून, 1815 को कांग्रेस
ने अपने निर्णयों प हस्ताक्षर कर दिये। वियना कांग्रेस के इन निर्णयों से
ही 19वीं शताब्दी की यूरोपीय राज्य व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। वियना
सम्मेलन में टर्की को छोड़कर यूरोप के सभी देशों के
प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। आस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख
को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मेटरनिख एक असाधारण व्यक्ति था।
1848 ई. तक मेटरनिख न केवल आस्ट्रिया का कर्णधार ही बना रहा वरन् वह
यूरोपीय राजनीति के रंगमंच पर भी छाया रहा। वियना कांग्रेस के सभी
महत्त्वपूर्ण निर्णय उसको नीति से ही प्रभावित थे।
 |
| वियना कांग्रेस मेटरनिख के संदर्भ में |
वियना कांग्रेस की प्रमुख
समस्याएँ
वियना कांग्रेस
के सामने निम्न प्रमुख समस्याएँ थीं-
1. यूरोप का
मानचित्र अस्त-व्यस्त होना-
फ्रांस की
क्रान्ति एवं नेपोलियन के युद्धों के परिणामस्वरूप यूरोप का राजनीतिक नवशा
अस्त-व्यस्त हो गया था। अनेक छोटे-बड़े राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, इंग्लैण्ड के
प्रधानमंत्री पिट का कथन था,"यूरोप के
मानचित्र को बन्द कर दो। अगले दस वर्ष तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।" अतः अब
वियना कांग्रेस के समक्ष यह समस्या थी कि इन पुराने राज्यों एवं राजवंशों की
पुनर्स्थापना किस प्रकार की जाय तथा उसका स्वरूप क्या हो।
2. फ्रांस की उचित
व्यवस्था करना-
30 मई, 1814 की पेरिस की प्रथम
सन्धि द्वारा फ्रांस की प्राकृतिक सीमाओं एवं वुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की जा
चुकी थी, किन्तु फ्रांस के सम्बन्ध
एक ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक था जिससे कि वह भविष्य में यूरोप की शान्ति भंग न कर
सके।
3. यूरोप में
क्रान्ति की भावना का दमन करना-
यूरोप के देशों
में क्रान्ति की भावना तीव्र हो रही थीं। यद्यपि फ्रांस की क्रान्ति समाप्त हो
चुकी थी, फिर भी समानता, स्वतन्त्रता एवं
राष्ट्रीयता के सिद्धान्त लगभग सारे यूरोप में फैल चुके थे। इटली, जर्मनी, आस्ट्रिया, रूस व स्पेन में जनता
लोकतंत्र शासन स्थापित करना चाहती थी। सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनीतिज्ञ घोर
प्रतिक्रियावादी थे। इसलिए क्रान्तिकारी एवं प्रतिक्रियावादी परस्पर विरोधी
सिद्धान्तों के संघर्ष का फैसला करना सम्मेलन की मुख्य समस्या थी।
4. चर्च की समस्या-
नेपोलियन ने चर्च
को एक साधारण संस्था बना दिया था तथा उसकी सम्पत्ति राज्य ने हस्तगत कर ली थी।
धार्मिक आदालतें भी बन्द कर दी गई थीं। अतः प्राचीन निरंकुश शासन व्यवस्था की
पुनर्स्थापना के साथ ही पोप की शक्ति की पुनर्स्थापना करने का प्रश्न भी वियना
कांग्रेस के लिए समस्या बन गया था।
5. अन्य समस्याएँ-
(i) विजयी राष्ट्रों की
आकांक्षाओं को पूरा करना।
(ii) जर्मनी की नवीन व्यवस्था
करना।
(ii) पॉलैण्ड की पुनर्स्थापना
करना।
(iv) नेपोलियन के मित्र
सेक्सनी तथा हॉलैण्ड, बेल्जियम और
फिनलैण्ड के भाग्य का निर्णय करना।
(v) इटली की नई व्यवस्था
करना।
(vi) डेनमार्क को मित्र
राष्ट्रों के विरोध का दण्ड देना।
(vii) स्वीडन को उसकी सहायता
का पुरस्कार देना।
(viii) युद्ध से त्रस्त यूरोप
में स्थायी शान्ति की स्थापना करना आदि विचारणीय समस्याएँ थीं।
वियना कांग्रेस की कार्य-प्रणाली
वियना सम्मेलन की कोई निश्चित
कार्य-प्रणाली नहीं थी। न तो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते थे और न ही मतदान
की व्यवस्था थी। प्रारम्भ में चार बड़े राज्य-रूस, आस्ट्रिया, प्रशा व
इंग्लैण्ड अपने स्वार्थों की सिद्धि हेतु अपनी इच्छानुसार सम्मेलन को
संचालित करते रहे। तैलेरा ने छोटे राज्यों की ओर से बड़े राज्यों के निर्णय
लेने के अधिकार को चुनौती दी। फलतः आठ राज्यों की समिति बना दी गई। इस समिति में
रूस, आस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और स्वीडन के
प्रतिनिधि थे। नैतिकता के सिद्धान्त ताक पर रख दिये गये। विचारों के आदान-प्रदान
का कोई महत्त्व नहीं था। बड़े राज्यों की साम्राज्य लिप्सा के कारण कांग्रेस के
भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। कांग्रेस के आधारभूत सिद्धान्त-वियना सम्मेलन
में तीन मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकार किये गये, जो निम्नलिखित थे-
(1) वैधता का
सिद्धान्त-
यह सिद्धान्त
तैलेरा द्वारा प्रतिपादित एवं मैटरनिख द्वारा समर्थित था। इस सिद्धान्त का
अर्थ था कि जो शासक नेपोलियन द्वारा गद्दी से हटाये गये थे, उन्हें वापस राज्याधिकार
मिलना चाहिए। इसी सिद्धान्त के आधार पर फ्रांस के शासक लुई 18वें को
मान्यता प्राप्त हुई।
(2) शक्ति सन्तुलन
का सिद्धान्त-
यह सिद्धान्त इंग्लैण्ड
के विदेश मंत्री कैसर ले की नीति का प्रमुख अंग था। इसके मूल में यह धारणा
थी कि यूरोप को प्रादेशिक व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि यूरोप का कोई भी राष्ट्र
इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरे राज्यों के लिए खतरा बन जाय। इस सिद्धान्त को
ध्यान में रखते हुए फ्रांस के चारों ओर बेल्जियम, हॉलैण्ड, प्रशा तथा
सार्डिनिया के शक्तिशाली राज्य स्थापित किये गये। जर्मनी का पुनर्गठन किया गया
ताकि भविष्य में शान्ति भंग न हो सके।
(3) पुरस्कार एवं
क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त-
जिन राज्यों ने नेपोलियन
की शक्ति को समाप्त करने में मित्र राष्ट्रों को सहयोग दिया था उन्हें पुरस्कार
एवं जिन राज्यों ने नेपोलियन को सहयोग दिया उन्हें दण्डित किया जाय, इस सिद्धान्त के अनुसार
भी निर्णय लिये गये। इस आधार पर फ्रांस की सीमा का पुनर्निर्धारण करते समय रूस, आस्ट्रिया व प्रशा को
नेपोलियन के साम्राज्य के हिस्से दिये गये।
वियना कांग्रेस की प्रादेशिक
व्यवस्था अथवा निर्णय
वियना कांग्रेस
ने अपने निर्णय में ऐसी व्यवस्था की जिससे यूरोप के मानचित्र में भारी
परिवर्तन हुआ। ये प्रादेशिक व्यवस्था निम्नलिखित थी-
(1) फ्रांस- फ्रांस की क्रान्ति और
नेपोलियन के काल में जितने प्रदेश फ्रांस ने अपने राज्य में मिला लिये थे, वे सभी प्रदेश उससे छीन
लिये गये। फ्रांस की सीमा के चारों ओर शक्तिशाली राज्य स्थापित किये गये ताकि
फ्रांस भविष्य में कभी यूरोप की शान्ति भंग न कर सके। बुओं वंश के लुई 18वें को
फ्रांस का शासक बनाया गया।
(2) आस्ट्रिया- आस्ट्रिया से बेल्जियम
का प्रदेश ले लिया गया और इसके बदले उसे इटली में वेनेशिया, लोम्बार्डी और इरीटिया के
प्रदेश दिये गये। उसे डालमेशिया और कट्टोरा का बन्दरगाह भी प्राप्त हुआ। इसके
अतिरिक्त उसे बवेरिया से टीरोल व साल्जबर्ग प्राप्त हुआ तथा पौलेण्ड में पूर्वी
गेलेसिया प्राप्त हुआ। नव-निर्मित जर्मन संघ का मुखिया आस्ट्रिया को बनाया गया।
(3) प्रशा- प्रशा को राइन नदी का
पश्चिमी प्रदेश दिया गया। प्रशा ने सैक्सनी के आधे हिस्से को हस्तगत कर लिया। इसके
साथ ही उसे बर्ग की डची तथा वेस्टफेलिया को डची का कुछ भाग प्राप्त हुआ। पोलैण्ड
और पौमेरेनिया का कुछ प्रदेश भी प्रशा को सौंपा गया। इन भू-भागों को प्राप्त होने
से प्रशा यूरोप के प्रथम श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित हो गया।
(4) जर्मनी के अन्य राज्य- जर्मनी में 39 राज्यों
का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। इसकी एक केन्द्रीय राष्ट्र सभा बनायी गई जिसका
अध्यक्ष आस्ट्रिया को बनाया गया। प्रत्येक राज्य के आन्तरिक मामलों में पूर्ण
स्वतंत्रता प्रदान की गई, किन्तु राज्यों
को आपस में युद्ध करने तथा बाह्य शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने पर प्रतिबन्ध लगा
दिया गया।
(5) इटली- इटली के राज्य
सार्डिनिया के साथ पीडमाण्ट, जिनोआ तथा सेवाय
को मिलाकर फ्रांस की सीमा पर एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया गया। बुओं वंश के शासक
फटनेण्ड सप्तम को वैधता के सिद्धान्त के आधार पर सिसली और नेपल्स का राज्य दिया
गया। पोप के प्रदेश पुन: पोप के अधीन कर दिये गये।
(6) हॉलैण्ड- उत्तर में फ्रांस पर
नियंत्रण रखने के लिए हॉलैण्ड को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। इसके लिए बेल्जियम
को हॉलैण्ड के साथ मिलाकर लक्जम बर्ग का क्षेत्र भी उसमें शामिल कर दिया गया। यहाँ
ओरेन्ज राज वंश को पुनः स्थापित किया गया।
(7) स्वीडन- स्वीडन से फिनलैण्ड का
प्रदेश लेकर रूस को दे दिया गया तथा पश्चिमी पामेरिया का प्रदेश प्रशा को सुपुर्द
किया गया। इस प्रकार स्वीडन और डेनमार्क दोनों को कमजोर बना दिया गया।
(8) पौलेण्ड- पौलेण्ड को रूस, आस्ट्रिया और प्रशा में
तीन भागों में विभाजित कर बाँट दिया गया। पौलेण्ड का मुख्य भाग एवं वारसा का राज्य
रूस को, पोसन, थार्न तथा डान्टिसग के
प्रदेश प्रशा को तथा दक्षिणी गेलेशिया आस्ट्रिया को दिया गया।
(१) स्विट्जरलैण्ड- स्विट्जरलैण्ड में
फ्रांस के तीन तिरिक्त केण्टन जोड़कर 22 केण्टनों का एक परिसंघ बनाया गया, जिससे उसका राज्य विस्तार
हुआ। उसकी तटस्थता तथा स्वतन्त्रता का दायित्व यूरोप के बड़े राज्यों ने अपने ऊपर
ले लिया।
(10) रूस- रूस के जार ने सम्पूर्ण
डची ऑप बारसा की माँग की किन्तु अन्त में समझौता हो गया। पौलेण्ड में स्थित पोसेना
के गैलेशिया के भाग को छोड़कर शेष डची ऑफ वारसा रूस के अधीन कर दिया गया। इसके
अतिरिक्त फिनलैण्ड व बेसारबिया पर भी रूस को अधिकार करने दिया गया। इस व्यवस्था से
रूस को काफी लाभ हुआ तथा यूरोप में उसका प्रभाव काफी बढ़ गया।
(11) स्पेन तथा पुर्तगाल- स्पेन से ट्रिनिडाड लेकर
इंग्लैण्ड को दे दिया गया। स्पेन में फर्डीनेण्ड सप्तम को पुनः शासक बना दिया गया।
पुर्तगाल में जॉन चतुर्थ का शासन पुनः स्थापित कर दिया गया।
(12) ब्रिटेन- इंग्लैण्ड को वियना
सम्मेलन से अनेक नवीन उपनिवेश प्राप्त हुए। फ्रांस से माल्टा, साण्डालूसिया, टोबेगो तथा मॉरीशस के
क्षेत्र लेकर इंग्लैण्ड को दिये गये। स्पेन से ट्रिनिडाड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार
हॉलैण्ड से लंका तथा कैप ऑफ गुडहोप भी प्राप्त हुआ। डेनमार्क से हेलीगोलैण्ड तथा
आयोनिन द्वीप समूह का संरक्षण प्राप्त हुआ। वियना सम्मेलन में प्राप्त द्वीपों से
भूमध्यसागर, एड्रियाटिक सागर तथा
एल्चा के समुद्री तटों में इंग्लैण्ड की सामुद्रिक शक्ति सुरक्षित हो गयी।
(13) वियना कांग्रेस के अन्य निर्णय-
(1) दास व्यापार
के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। इसे अनैतिक एवं अमानवीय घोषित किया गया।
(2)
अन्तर्राष्ट्रीय विधान बनाने का प्रयत्न किया गया।
(3) संयुक्त व्यवस्था
के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई।
निष्कर्ष-
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वियना
सम्मेलन 'नैतिक व्यवस्था का
पुनर्निर्माण तथा राजनीतिक शक्ति के न्यायोचित पुनर्विभाजन पर आधारित स्थायी
शान्ति आदि महान आदर्शों एवं पवित्र उद्देश्यों की घोषणाओं के साथ प्रारम्भ हुआ
था। यूरोप की जनता को इस सम्मेलन से बड़ी आशाएँ थी, किन्तु कांग्रेस के निर्णयों से सभी को निराशा हुई और इसकी
तीव्र आलोचना की गई।
सम्मेलन के सचिव गेज
ने तो यहाँ तक कह डाला कि, "कांग्रेस के बड़े-बड़े
सुन्दर शब्दों का केवल यही उद्देश्य है कि सर्वसाधारण की उत्तेजनाओं को शान्त किया
जाए तथा सम्मेलन को शान एवं प्रतिष्ठा दिलायी जाय, किन्तु कांग्रेस का वास्तविक उद्देश्य यह था कि विजयी
राष्ट्र पराजित राष्ट्रों की लूट-खसोट को आपस में बाँट ले।" वस्तुत: यह
सम्मेलन शक्तिशाली देशों का एक सेना झमेला था जहाँ बड़े राष्ट्रों को अपने
स्वार्थों का ध्यान था। अपनी स्वार्थसिद्धि के सामने उन्होंने जनसाधारण के हितों
और अधिकारों को त्याग दिया। शक्तिशाली देशों ने छोटे देशों की उपेक्षा की तथा
निर्णय लेते समय उचित-अनुचित तथा न्याय-अन्याय का कोई ध्यान नहीं रखा।
वियना कांग्रेस में कई दोषों के होने के
बावजूद यह महत्त्वपूर्ण था। जैसा कि कैटलबी ने लिखा है कि, "इस सम्मेलन में राजनीति, संयम एवं दूरदर्शिता से
काम लिया गया तथा इससे एक ऐसा आधार तैयार किया गया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव
रखी गई।" ग्राण्ट और टेम्परले के शब्दों में, "वियना के शान्ति
संस्थापकों को अत्यन्त प्रतिक्रियावादी और अनुदार कहकर उनकी आलोचना करना एक
परम्परा बन गई है। यह सत्य है कि वे प्राचीन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे और
अधिकांश रूप में नवीन विचारों से अछूते थे। किन्तु वे प्राचीन शासन के निकृष्ट रूप
के नहीं बल्कि उत्कृष्ट रूप के प्रतिनिधि थे तथा उनकी व्यवस्था से यूरोप
अगले 40 वर्षों तक युद्धों से बचा रहा।"
आशा हैं कि हमारे
द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो
इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।










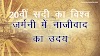




0 Comments