व्याकरण
शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाने वाला ग्रंथ ही व्याकरण कहलाता है अर्थात व्याकरण को हम भाषा के शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण शुद्ध प्रयोग करने वाला एक ग्रंथ की संज्ञा दे सकते हैं। जिसमें हिन्दी के सभी व्यंजनों को शुद्ध व सही क्रम में लिखा होता है।
व्याकरण का अर्थ है भली भांति समझना
अर्थात हिंदी के व्यंजनों को भली भांति से समझना और उनका शुद्ध उच्चारण व शुद्ध
लेखन करना।
व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद - वि+आ+करण
हिन्दी व्याकरण को हम अपनी सुविधा के
हिसाब से तीन भागों में बांट सकते हैं।
(1) वर्ण विचार, (2)
शब्द विचार, (3) वाक्य विचार।
यह छोटे से बड़े रूप में इसी
क्रम में व्यवस्थित है वर्ण, शब्द, व वाक्य। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण की सबसे छोटी
इकाई वर्ण है तथा सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वर्ण से शब्द और
शब्द से वाक्य बनने का क्रम है।
 |
| वर्ण विचार |
वर्ण विचार
वर्णो का शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन शुद्ध प्रयोग करना ही वर्ण
विचार कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण
कहलाती है। अकेले वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण ध्वनि से उत्पन्न
होता है।
अर्थ के आधार पर सबसे छोटी
इकाई शब्द है और अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वाक्य है।
ध्वनि-
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है।
अक्षर- मुख
के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं होता अर्थात् हवा के एक ही
प्रवाह में बोले जाने वाले ध्वनि या अक्षर कहलाती है।
शब्द-
वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे- कलम, कमल।
वर्णमाला- वर्णो
का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है।
वाक्य-
शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते
हैं और पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं तो उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे कृष्ण गाय
चराता है, राधा गाना गाती है।
वाक्यांश- जब
दो या दो से अधिक शब्द मिलते है, परंतु पूर्ण अर्थ का बोध नहीं करा पाते, वाक्यांश कहलाते हैं, जैसे- जिसके जैसा कोई दूसरा न
हो।
पद- जब
किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध
स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद
कहलाता है, जैसे महेश फुटबॉल खेलता है।
जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द
होता है लेकिन जब उसे शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद
कहलाता है।
वर्ण के प्रकार
वर्ण दो प्रकार के होते हैं।
(1) स्वर,
(2) व्यंजन।
स्वर
स्वर स्वतंत्र होते हैं इन्हें
बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर
वर्ण कहलाते हैं।
विशेष- प्रत्येक वर्ण को अक्षर कहा जा सकता है, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते हैं।
स्वर 11 होते हैं जो निम्न है-
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
विशेष- अं अः आयोगवाह ध्वनि कहलाती है।
आयोगवाह ध्वनियाँ वह होती है, जो
किसी के साथ (व्यंजनों के साथ) जुड़कर वहन नहीं होती।
अं
अनुस्वार है।
अः
विसर्ग है।
ऋ
संस्कृत का तत्सम रूप है।
स्वर के प्रकार-
- मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर-
- ओष्ठाकृति के आधार पर-
- जीभ (जिह्वा) की क्रियाशीलता के आधार पर-
- मुखाकृति के आधार पर (तालू की स्थिति के आधार पर)-
- नासिका के आधार पर-
-
जाति के आधार
पर-
मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर-
मात्रा या उच्चारण में लगने
वाले समय के आधार पर हम स्वरों को तीन भागों में विभक्त करते हैं।
1. ह्रस्व स्वर, 2. दीर्घ स्वर व 3.
प्लूत स्वर।
1. ह्रस्व स्वर (लघु, छोटा, एकमात्रिक)-
वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा
का समय लगता है,
यह ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते है। यह चार
है- अ इ उ ऋ
2. दीर्घ स्वर (गुरु, बड़ा, द्वी मात्रिक)-
वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है अर्थात
दो मात्रा का समय लगता है,
दीर्घ स्वर कहलाते है। यह सात
हैं- आ ई ऊ ए ऐ ओ औ।
3. प्लूत स्वर-
वे स्वर, जो लंबे समय तक लगातार बोल दिए जाए
तो वह स्वर प्लूत स्वर बन जाता है, जैसे- गायन से पहले कलाकार का कई स्वरों
का निकालना आदि।
ओष्ठाकृति के आधार पर-
1. वृताकार
स्वर-
वे स्वर जिनका
उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार
स्वर कहते हैं। इन्हें वृत्त मुखी स्वर भी कहा जाता है, ये चार
होते हैं, उ ऊ ओ औ।
2. अवृताकार
स्वर-
वे स्वर जिनके
उच्चारण में होंठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर फैल जाते
हैं। अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ इ ई ऋ ए ऐ।
जिह्वा (जीभ) की क्रियाशीलता के आधार पर-
जीभ की क्रियाशीलता के
आधार पर हम स्वरों को तीन भागों में बांट सकते हैं।
1. अग्र
स्वर-
जिन स्वरों को बोलने
या उच्चारण के समय जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता है, अग्र
स्वर कहलाते है। यह पांच होते हैं, इ ई ए ऐ ऋ।
2. मध्य
स्वर-
वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य
भाग क्रियाशील रहे, मध्य स्वर कहलाते हैं, यह एक है, अ।
3. पश्च
स्वर्ग-
वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च
भाग क्रियाशील रहे पश्च स्वर कहलाते है, यह पांच होते हैं, आ
उ ऊ ओ औ।
मुखाकृति के आधार पर-
मुखाकृति के आधार पर
स्वर चार प्रकार के होते हैं।
1. संवृत
स्वर-
वे स्वर जिनके
उच्चारण में मुख वृत के समान बंद सा रहता है अर्थात सबसे कम
खुलता है, संवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे- इ ई उ ऊ ऋ।
2. अर्द्धसंवृत
स्वर-
वे स्वर जिनके
उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, अर्द्धसंवृत
स्वर कहलाते हैं जैसे ए ओ।
3. विवृत
स्वर-
विवृत स्वर का अर्थ खुला
हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है अर्थात
सबसे ज्यादा खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे- आ।
4. अर्द्धविवृत
स्वर-
वे स्वर जिनके
उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्द्धसंवृत
स्वरों की तुलना में ज्यादा खुला सा रहता है अर्द्धविवृत
स्वर कहलाते हैं, जैसे- अ ऐ ओ।
नासिका के आधार पर-
1. निरनुनासिक
स्वर-
वे स्वर जिनके
उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता अर्थात सिर्फ मुख
से उच्चारित होने वाली ध्वनिया निरनुनासिक कहलाती है, जैसे सभी
स्वर।
2. अनुनासिक
स्वर-
वे स्वर जिनके
उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है अर्थात मुख के साथ साथ नासिका
से भी उच्चारित होने वाली ध्वनिया अनुनासिक कहलाती है, जैसे- अँ आँ इँ ईँ
उँ ऊँ एँ ऐँ ओँ औँ आदि।
जाति के आधार पर-
जाति के आधार पर हम
स्वरों को दो भागों में बांट सकते हैं।
1. सजातीय
स्वर-
एक ही जाति
के स्वर को सजातीय स्वर कहते हैं अर्थात यह एक ही जाति के वर्णो
से मिलकर बने होते हैं, जैसे- अ+अ=आ इ+इ=ई
उ+उ=ऊ।
2. विजातीय
स्वर-
अलग अलग जाति
के स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं अर्थात यह अलग अलग जाति के
वर्णो से मिलकर बनते हैं, जैसे-
अ आ / इ ई = ए
अ आ / ए ऐ = ऐ
अ आ / ओ औ = औ।
मात्रा-
मात्रा स्वर का ही रूप है जो
व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं, मात्रा स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। मात्राओं की
संख्या 11 होती है जो दृश्य रूप में 10 होती है। अ स्वर की कोई
मात्रा नहीं होती, कोई संकेत के रूप में नहीं है, इसलिए अ एक उदासीन
स्वर है।
ह्रस्व
(लघु) स्वर
वे स्वर जिन पर एक
मात्रा हो या एक मात्रा वाले स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं,
अ इ उ ऐ।
दीर्घ
स्वर
वे स्वर जिन पर दो
मात्राएँ हो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं,
आ ई ऊ ऐ ओ औ।
व्यंजन
वे वर्ण जो स्वतंत्र
रूप से उच्चारित नहीं होते और उन्हें उच्चारण करने के लिए अन्य स्वर
की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्वर के सहयोग से उच्चारित
होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती है।
व्यंजनों की संख्या
33 होती है।
क ख ग घ ड
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह
व्यंजनों के प्रकार-
- अध्ययन के
आधार पर-
- घोष कंपन के
आधार पर-
- प्राणवायु के
आधार पर-
- उच्चारण के
आधार पर-
- उच्चारण
स्थान के आधार पर-
अध्ययन के आधार पर-
अध्ययन के आधार पर
व्यंजनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है।
1. स्पृशी
व्यंजन-
जिस व्यंजन के
उच्चारण के समय हमारी जीभ मुख्य के किसी अवयव को छूती अर्थात
स्पर्श करती है तो उन्हें सपृशी व्यंजन रहते हैं, इनकी संख्या 25
होती है, जो क से म तक सभी व्यंजन आते हैं।
क ख ग घ ड़
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म।
2. अंतस्थ
व्यंजन-
वह व्यंजन जिनका
उच्चारण अंदर ही अंदर होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते
हैं अर्थात जिन्हें बोलने में मुख्य के अंदर ही अंदर उच्चारण किया जाए यह
वर्ण चार है- य र ल व।
3. उष्ण
व्यंजन-
वह व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ मुख के
किसी अवयव के पास तो जाती है पर उसे स्पर्श नहीं करती
ओर हवा संघर्ष से बाहर निकलती है और गर्म हो जाती है तो ऐसी
उच्चारित वर्ण उष्ण व्यंजन कहलाते हैं, जो निम्न है- श ष स ह।
घोष या कंपन के आधार
पर-
कंपन के आधार पर
व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है।
1. अघोष
व्यंजन-
वे व्यंजन जिनको
उच्चारण करते समय मुख के किसी अवयव में कंपन नहीं होता या न
के बराबर कंपन होता है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं, यह 13 है-
क ख
च छ
ट ठ
त थ
प फ
श ष स।
2. सघोष
व्यंजन-
ऐसे व्यंजन जिनको
उच्चारण करते समय मुख के किसी अवयव में कंपन होता है सघोष
व्यंजन कहलाते हैं, यह 31 है-
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
ग घ ङ
ज झ ञ
ड ढ ण
द ध न
ब भ म
य र ल व ह।
प्राणवायु के आधार पर-
प्राणवायु के आधार
पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते है।
1. अल्पप्राण
व्यंजन-
ऐसे व्यंजन जिनके
उच्चारण में वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती हैं, वे वर्ण अल्प
प्राण व्यंजन कहलाते हैं यह 30 है-
क ग ङ
च ज ञ
ट ड ण
त द न
प ब म
य र ल व
अ आ इ ई ऋ ए ऐ ओ औ।
2. महाप्राण
व्यंजन-
वे वर्ण जिनके
उच्चारण में वायु मुख से ज्यादा बाहर निकलती है। वे महा
प्राण व्यंजन कहलाते हैं, जो निम्न है-
ख घ
छ झ
ठ ढ
थ ध
फ भ
य र ल व।
उच्चारण के आधार पर-
उच्चारण के आधार पर
व्यंजनों को आठ भागों में बांटा गया है।
1. स्पर्शी
व्यंजन-
वह व्यंजन जिनके
उच्चारण के समय जीभ का मुख के किसी अवयव के साथ स्पर्श हो स्पर्श
व्यजन कहलाते है यह 16 है,
क ख ग घ
ट ठ ड ढ
त थ द ध
प फ ब भ।
2. संघर्षी
व्यंजन-
वह व्यंजन जिनके
उच्चारण से हवा को संघर्ष करके मुख से बाहर आना पड़े संघर्षी
व्यंजन कहलाते हैं,
श ष स ह
क़ ख़ ग़ ज़ फ़ फारसी भाषा के।
3. स्पर्शी
व संघर्षी व्यजन-
वे व्यजन जिनको
उच्चारण में जीभ का स्पर्श हो और हवा संघर्ष करती बाहर निकले
स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं,
च छ ज झ।
4. नासिक्य
व्यंजन-
वे व्यंजन जिनके
उच्चारण में हवा नासिका द्वार से मुख की अपेक्षा ज्यादा बाहर
निकले नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, पाँचों वर्गो के पंचम अक्षर है,
ङ ञ ण न म।
5. संघर्ष
हीन-
वे व्यंजन जिनके
उच्चारण में जीभ तथा हवा को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्ष
हीन व्यंजन कहलाते है,
य व।
नोट य व व्यंजनों को
अर्द स्वर भी कहते हैं।
6. प्रकंपित
या लुंठित व्यंजन-
वे व्यंजन जिनके
उच्चारण में जीभ तालू के साथ रगड़ खाती है अर्थात कंपन करती
है, मुडती है, परम्पित य़ा लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। यह एक है,
र।
7. पार्श्विक
व्यंजन-
जिस व्यंजन के
उच्चारण में प्राणवायु जीभ के दोनों किनारों से बाहर निकले पार्श्विक
व्यंजन कहलाते है, यह एक है, ल।
8. ताड़नजात
व्यंजन-
ऐसे व्यंजन जिनके
उच्चारण में जीभ बाहर की तरफ फेंकी जाए या मुड़कर एकदम नीचे
पढ़ें ताडनजात व्यंजन कहलाते है, जो दो है,
ड़ ढ़।
विशेष- ताडनजात वर्णो को आधा या स्वर रहित नहीं कर
सकते।
उच्चारण स्थान के आधार पर-
हम उच्चारण स्थान के
आधार पर व्यंजनों को दस भागों में बांट सकते हैं।
1. कंठय
व्यंजन-
वह व्यंजन जिनके
उच्चारण में जीभ कंठ से स्पर्श करती है,
जैसे- क ख ग घ ङ अ आ ः।
2. तालव्य
व्यंजन-
वह व्यंजन जिनके
उच्चारण में जीभ तालू को स्पर्श करे तालव्य व्यंजन कहलाते
हैं,
च छ ज झ ञ इ ई य श।
3. मूर्धन्य
व्यंजन-
जिन वर्णों के
उच्चारण में जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है, मुर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं,
ट ठ ड ढ ण ऋ र ष।
4. दंन्तय
व्यंजन-
वे व्यंजन जिनके
उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, दंत्य व्यंजन कहलाते हैं,
त थ द ध न ल स।
5. ओष्ठय
व्यंजन-
वे व्यंजन जिनका
उच्चारण होठों की सहायता से किया जाऐ ओष्ठय व्यंजन कहलाते
हैं,
प फ ब भ म उ ऊ।
6. कंठतालव्य
व्यंजन-
वे व्यंजन जिनका
उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, कंठतालव्य व्यंजन कहलाते हैं,
ए ऐ
अ (कण्ठय)+ई(तालव्य)=ऐ।
7. कण्ठोष्ठय
व्यंजन-
वे व्यंजन जिनका
उच्चारण कंठ और होठों दोनों से होता है कंण्ठोष्ठय व्यंजन
कहलाते हैं,
ओ औ
अ (कण्ठय) +उ (औष्ठय)= ओ।
8. दंतोष्ठ
व्यंजन-
वे व्यंजन जिनका
उच्चारण दांत और होठ दोनों से होता है उन व्यंजनों को दंत ओष्ठ्य
व्यंजन कहलाते हैं,
व।
9. अलिजिह्वा
/ काकल्य व्यंजन-
वे व्यजन जिनका
उच्चारण करते समय जीभ बिलकुल न हिले या जीभ की स्थिरता रहे
उन व्यंजनों को अलिजिह्वा व्यंजन कहते है, ह।
10. वर्तस्य
व्यजन-
ऐसे व्यंजन जिनको
उच्चारण करते समय जीभ मसूडों से टकराए ऐसे व्यंजनों को वर्त्स्य
व्यंजन कहते हैं,
र न ल स ज।
वर्णो की संख्या गणना
स्वर 11 है- अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ।
व्यंजन 33 है- क से म।
योग 44 (मूल वर्ण)
आयोगवाह 2 है- अं अः
संयुक्ताक्षर 4 है- क्ष त्र ज्ञ श्र
ताड़नजात 2 है- ड़ ढ़।
कुल योग 52
विदेशी वर्ण 4 है- ख़ ग़ ज़ फ़।
मानक वर्ण 56
कुल 52
मूल वर्ण 44।
विशेष-
शिरोपरी रेखा वर्ण के ऊपर
खींची जाने वाली रेखा को सिरोपरी रेखा कहते हैं।
खड़ीपाई जिस डंडे के साहारे
वर्ण लिखा जाता है। खडीपाई होती है कुछ वर्णो या व्यंजन में
नहीं होती, जैसे- ड ढ छ।
अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगने वाला
बिंदु अनुस्वर कहलाता है, जैसे- खँ मँ तँ।
पंचमाक्षर वर्ण के पाँच वें
अक्षर के आगे लगने वाला बिन्दु पंचमाक्षर कहलाता है, यह केवल एक है- ड़.।
नुक्ता वर्ण के आगे लगते है।
यह केवल फारसी
अरबी भाषा मैं ही लगते है और वर्ण अरबी या फारसी भाषा का बन
जाता है।
हलंत् या हल प्रत्येक वर्ण, स्वर के सहयोग
से बोला जाता है, जब व्यंजन मे से वर्ण को अलग कर दिया जाता है तो
वह व्यंजन अधूरा हो जाता है इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन
के नीचे रेखा खींची जाती है उसे हम हलंत् कहते हैं,
क् ख् ग् घ् आदि।
आशा हैं कि हमारे
द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो
इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।





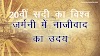









0 Comments