भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ
भारतीय संविधान की
मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
1. लिखित, निर्मित एवं विस्तृत
संविधान-
भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लम्बा संविधान है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे जो, 22 भागों में विभाजित था। वर्तमान में (104 संविधान संशोधन तक) 25 अध्याय, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 3 परिशिष्ट हैं। जबकि अमरीका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं। सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में, "भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है।"
2. नमनीयता और
अनमनीयता (लचीलेपन और कठोरता) का मिश्रण-
भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश
संविधान की भाँति लचीला है और न अमरीकी संविधान की भाँति कठोर
है। इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान में मध्य मार्ग अपनाया गया है।
 |
| भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ |
संविधान की अधिकांश धाराओं में संशोधन
के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भारतीय
संविधान एक कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से
देखें तो भारतीय संविधान के संशोधन की पद्धति उतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमरीका
या अन्य संघ राज्यों के संविधानों की संशोधन पद्धति। दूसरे, कुछ विषयों में तो
संसद साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। ये तथ्य उसे लचीला बनाती है।
इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण
है।
3. सम्पूर्ण
प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य-
संविधान की
प्रस्तावना में भारत को एक
सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का रूप
प्रदान किया गया है। इस शब्दावली की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार है-
(क) सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न- सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न के दो पहलू हैं- आन्तरिक एवं
बाह्य। आन्तरिक पहलू के अनुसार भारतीय सीमा के अन्तर्गत भारत संघ सर्वोच्च सत्ता
है और इसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। उसका आदेश अन्तिम है, जिसका क्षेत्र के
अन्तर्गत सभी लोग पालन करने के लिए बाध्य हैं। बाह्य क्षेत्र में भी भारत पूर्णतः
स्वतन्त्र तथा सार्वभौम है। वह किसी अन्य राज्य के कानूनी नियन्त्रण से पूर्णतया
स्वतन्त्र है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी अन्य राज्य की आज्ञा मानने के
लिए बाध्य नहीं है।
(ख) समाजवादी- संविधान की मूल
प्रस्तावना में यद्यपि भारत को समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया था, तथापि इस बात पर सभी
भारतीय सहमत रहे हैं कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। इस
सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए भी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना
में भारत को 'समाजवादी राज्य' घोषित किया गया है।
(ग) पंथ-निरपेक्ष राज्य- यह शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, वरन् 42वें संविधान
संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है । धर्मनिरपेक्ष राज्य से
तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है।
(घ) लोकतन्त्रात्मक- लोकतंत्र का अर्थ यह है कि शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथ में है।
भारत का शासन स्वयं जनता द्वारा अर्थात् उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा
संचालित होता है। भारत में वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचित
प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र की स्थापना की गई है।
(ङ) गणराज्य– संविधान द्वारा भारत में गणतन्त्र की
स्थापना की गई है। क्योंकि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर
भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है।
4. इकहरी नागरिकता-
साधारणतः संघात्मक
राज्य में दोहरी नागरिकता पाई जाती है पूरे संघ की नागरिकता
एवं प्रत्येक अवयवी राज्य की नागरिकता। अमेरिका और स्विट्जरलैण्ड के संविधानों में
दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। लेकिन भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता
की व्यवस्था है। इसमें राज्य की कोई पृथक् नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। भारतीय
संघ के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के नागरिक को एक ही प्रकार की नागरिकता (भारत की
नागरिकता) के अधिकार ही प्राप्त हैं।
5. द्विसदनात्मक
व्यवस्थापिका-
भारतीय संविधान के
अनुच्छेद- 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा
दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा एवं लोक सभा
होंगे। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अर्थात् संसद = राष्ट्रपति +
राज्य सभा + लोक सभा। इस प्रकार भारतीय संसद या व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक
है।
6. संघात्मक और
एकात्मक तत्त्वों का मिश्रण-
1950 में संविधान के
प्रथम अनुच्छेद के अनुसार "भारत राज्यों का एक संघ
होगा।" इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और
इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान ने शासन-शक्ति एक
स्थान पर केन्द्रित न कर, केन्द्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है और दोनों ही
अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। संविधान लिखित और बहुत अधिक सीमा तक कठोर है
तथा इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक
बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केन्द्र एवं राज्यों के
मध्य उत्पन्न संवैधानिक झगड़ों पर निर्णय देने का अधिकार दिया गया है।
भारत के संविधान के संघात्मक
होते हुए भी इसमें कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जिनसे इसका झुकाव एकात्मक
शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे- इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ, राष्ट्रपति द्वारा
राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में
परिवर्तन का अधिकार आदि।
7. मूल अधिकार-
अमरीका, आयरलैण्ड आदि के
संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी नागरिकों के मूल अधिकारों
की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को छ: मूल
अधिकार प्रदत्त हैं। ये निम्नलिखित हैं-
(1) समानता का
अधिकार,
(2) स्वतन्त्रता का अधिकार,
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार,
(4) धार्मिक स्वतन्त्रता का
अधिकार,
(5) सांस्कृतिक एवं शिक्षा
सम्बन्धी अधिकार तथा
(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये अधिकार वाद
योग्य हैं। ये अधिकार भारतीय लोकतन्त्र तथा उसकी उदार व स्वतन्त्र संस्थाओं के
अस्तित्व के मूल आधार हैं, परन्तु नागरिकों के ये मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं
हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था व हित, विदेशों से मैत्रीपूर्ण
सम्बन्ध, सार्वजनिक नैतिकता आदि आधारों पर मूल अधिकार मर्यादित किए
जा सकते हैं।
8. राज्य के
नीति-निर्देशक तत्त्व-
भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में राज्य
के नीति-निर्देशक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में नीति-निर्देशक
तत्त्व का विचार आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है और इन तत्त्वों की
प्रकृति के सम्बन्ध में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि "नीति
निर्देशक तत्त्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किन्तु तो भी ये
तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं।"
9. मूल कर्त्तव्य-
भारतीय संविधान में 42वें सांविधानिक
संशोधन द्वारा उसके भाग-4 (क) के रूप में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को
जोड़ा गया है, जो संख्या में 11 हैं। महत्त्वपूर्ण मूल कर्त्तव्य ये हैं- संविधान
का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और
राष्ट्रगान का आदर करना; राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक आदर्शों का अनुसरण
करना; भारत की प्रभुता, एकता, अखण्डता परिपुष्ट
करना और उसकी रक्षा करना; देश की रक्षा करना; भारत के सभी लोगों में
समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना; सार्वजनिक सम्पत्ति की
सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना तथा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने
का सतत प्रयास करना आदि।
10. स्वतन्त्र
न्यायपालिका-
संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान
की रक्षा व व्याख्या करने के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है।
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएँ दी गई हैं, जैसे- न्यायाधीशों
की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की
सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न हो सकना, न्यायाधीशों के आचरण
पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना आदि। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय
अनुच्छेद 32 के अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और
उत्प्रेषण आदि लेखों को जारी कर सकते हैं।
11. विश्व शान्ति
तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थक-
संविधान का अनुच्छेद 51 भारत के
अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और
सुरक्षा का इच्छुक है, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को
स्थापित करना चाहता है और किसी दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहता
है। विवादों के निपटारे के लिए शान्तिपूर्ण साधनों पर बल देता है और किसी देश के
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। भारत की विदेश नीति के आधार हैं-
शान्तिवाद, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय
संस्थाओं के पति आदर, साम्राज्यवाद और रंग-भेदभाव का विरोध।
12. निर्दिष्ट
जातियों के लिये विशेष व्यवस्थाएँ-
भारतीय संविधान में पिछड़ी जातियों के
कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनके लिए संसद, राज्य विधानमण्डलों
एवं स्थानीय संस्थाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। अनुसूचित जातियों
तथा अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अन्तर्गत
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में यह
व्यवस्था 25 जनवरी, 1960 तक के लिये थी, किन्तु संविधान में
संशोधन करके इसकी समय-सीमा को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है और अब 95वें
संवैधानिक संशोधन, 2010 के आधार पर इन प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण
की व्यवस्था को 25 जनवरी, 2020 ई. तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन जातियों के लिए
सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत की गई है तथा 8
सितम्बर, 1993 से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी 27% आरक्षण
लागू कर दिया गया है। लेकिन इन जातियों के 'सम्पन्न तबके' (क्रीमी लेयर) को इसका लाभ नहीं दिया गया है।
13. पंचायतों तथा नगरपालिकाओं
की संवैधानिक व्यवस्था-
भारत में 73वें एवं 74वें संवैधानिक
संशोधन द्वारा क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की संवैधानिक
व्यवस्था की गई है।
73वें संवैधानिक
संशोधन द्वारा सम्पूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की
गई तथा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण
की व्यवस्था की गई है तथा 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी
क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन की संवैधानिक व्यवस्था करने हेतु नगरपालिकाओं
में नियमित चुनाव कराने, तीन श्रेणियों की नगरपालिकाएँ बनाने यथा- ग्राम पंचायत से
नगर परिषद् बनाने पर नगर पंचायत, छोटे नगर क्षेत्रों के लिए
नगर परिषद् व बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम का प्रावधान किया गया।
इस प्रकार भारत
का संविधान एक ऐसा आदर्श संविधान है जिसमें सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक
दोनों पक्षों पर बल दिया गया है।
आशा हैं कि हमारे
द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो
इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।
Back To - भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था




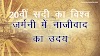










0 Comments