सर्वोच्च न्यायालय का संगठन
भारतीय संविधान के भाग-4 तथा
अनुच्छेद 124 में,
सर्वोच्च न्यायालय के
संगठन का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन इस प्रकार है-
1. न्यायाधीशों की
संख्या-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार प्रारम्भ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश निश्चित किये गये। 2008-09 में संसद ने एक विधेयक पारित कर न्यायाधीशों की संख्या 31 (मुख्य न्यायाधीश सहित) कर दी है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 31 न्यायाधीश हैं जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं।
उच्चतम न्यायालय का कार्य-स्थल नई
दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से न्यायालय की
बैठक कहीं भी बुला सकता है।
2. नियुक्ति-
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति
करता है।
(अ)
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति– सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर
नियुक्ति के बारे में 1978 से अपनायी गई सर्वमान्य परम्परा के आधार पर अब यह पूरी
तरह से निश्चित हो गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश
को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जायेगा। विधि आयोग ने भी अपनी 80वीं
रिपोर्ट में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे
में वरिष्ठता के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
(ब)
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति- संविधान का अनुच्छेद 124 इस
बात की व्यवस्था करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा
इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
करते समय राष्ट्रपति मन्त्रियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय और उच्च
न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लें जिनसे परामर्श लेना वह उचित
या आवश्यक समझता है।
(स)
न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित परम्परा- न्यायाधीशों
की नियुक्ति के बारे में यह परम्परा विकसित हुई है कि कम से कम एक न्यायाधीश
मुस्लिम होना चाहिए। दूसरी परम्परा वरिष्ठता के नियम की है, यद्यपि
इसका उल्लंघन अनेक बार किया जा चुका है।
3. परामर्श की
प्रक्रिया-
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है। 28 अक्टूबर, 1998
को लिये गये एक निर्णय के आधार पर अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार है-
 |
| सर्वोच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियाँ |
राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व 'चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह' से लिखित परामर्श प्राप्त करेंगे और इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा कि "वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह को एकमत से तथा लिखित में सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाये तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।"
सर्वोच्च न्यायालय ने
स्पष्ट कर दिया है कि "यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया
पूरी किये बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के
स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करते हैं तो सरकार ऐसी
सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है।"
4. न्यायाधीशों की
योग्यता-
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं
का होना आवश्यक है-
(i)
वह भारत का नागरिक हो।
(ii)
किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक उच्च
न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका
हो।
(iii)
वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
पद पर रह चुका हो,
या
(iv)
वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय
में वकालत कर चुका हो।
(v)
राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विख्यात विधिवेत्ता
हो।
5. कार्यकाल तथा
महाभियोग-
संविधान के अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। इस अवस्था से पूर्व
वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके
पद से केवल प्रमाणित कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसके लिए निर्धारित आयु से
पूर्व भी हटाया जा सकता है। इस तरह के महाभियोग की कार्य-विधि निश्चित करने
का अधिकार संसद को है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों
सदनों को अलग-एलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने
वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत से प्रस्ताव पारित करना होगा और वह प्रस्ताव
राष्ट्रपति को भेजा जायेगा। उसके पश्चात् राष्ट्रपति उस न्यायाधीश
की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का
प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने पक्ष के
समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जायेगा।
6. वेतन, भत्ते एवं सेवा-शर्ते-
वर्तमान समय में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन
2.50 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर दिया गया है। उनको बिना किराये का निवास
स्थान व अनेक प्रकार के भत्ते आदि दिये जायेंगे। उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके
वेतन, भत्ते आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। उनका वेतन आदि भारत की
संचित निधि पर भारित होगा। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को व्यय भत्ते, वाहन
भत्ते तथा पेंशन,
ग्रेच्युटी आदि की सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। संभवतया नये
संशोधन के तहत अब प्रतिमाह वेतन बढ़ने की कि आशंका है।
7. शपथ ग्रहण-
अनुच्छेद 124 (6) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति
के मक्ष शपथ लेते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि
सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के बारे में संविधान द्वारा
निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं -
(1) सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर किये
जायेंगे।
(2) सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर
होंगे। बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना पृथक् निर्णय दे सकता है, परन्तु
वह अन्य किसी प्रकार से बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकेगा। बहुमत का
निर्णय ही मान्य होगा।
(3) ऐसे मामले जिनमें-
(i) संविधान की व्याख्या से
सम्बन्धित विषय सम्मिलित हों,
(ii) संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हों,
(iii)
विधि के अर्थ को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, या
(iv) राष्ट्रपति द्वारा विचार का
कार्य सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया हो, उनकी
सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।
क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काफी व्यापक क्षेत्राधिकार
प्राप्त है, यथा-
1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार-
सर्वोच्च न्यायालय के
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को दो वर्गों में रखा जा सकता है-
(1)
संघ और राज्यों से सम्बन्धित- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित
वाद आते हैं-
(i) भारत सरकार तथा एक या एक से
अधिक राज्यों के विवाद;
(ii) भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद:
(iii) दो या दो से अधिक राज्यों के
बीच विवाद। जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अन्तर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का
अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो।
सर्वोच्च न्यायालय को
केवल संघ सरकार और राज्य सरकारों के पारस्परिक विवाद के सम्बन्ध में प्रारम्भिक
अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, अर्थात् उपर्युक्त प्रकार के विवाद केवल
सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किये जा सकते हैं।
(2)
मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार- मौलिक
अधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित मामले उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में
प्रस्तुत किये जाते हैं। संविधान में अनुच्छेद 32 (i) के द्वारा मौलिक
अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया
है। वह मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार
पृच्छा, उत्प्रेषण एवं परमादेश की याचिका जारी कर सकता है।
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार-
सर्वोच्च न्यायालय को
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के साथ-साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान
किया है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का
अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को
निम्नलिखित पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-
1. संवैधानिक
क्षेत्राधिकार- संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि
उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से
सम्बन्धित कानून का कोई सारमय प्रश्न अन्तर्निहित है, तो उच्च
न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा
सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर
दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है
कि वह ऐसी किसी अपील को अनुमति प्रदान कर सकता है, यदि उसको यह विश्वास
हो जाए कि उस विषय में संविधान की व्याख्या का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है।
उसके परिणामस्वरूप यह सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम संरक्षक और
व्याख्याकर्ता बन जाता है
2. फौजदारी
क्षेत्राधिकार- अनुच्छेद 134 के अनुसार फौजदारी विवादों
में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न परिस्थितियों में सर्वोच्च
न्यायालय में की जा सकती है-
(i) यदि उच्च न्यायालय ने अपील
प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदण्ड दे
दिया हो;
(ii) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ
न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मँगवाकर अभियुक्त को प्राणदण्ड दे दिया है;
(iii) अगर उच्च न्यायालय यह
प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार योग्य है तो अपील की जा सकती
है।
3. दीवानी
क्षेत्राधिकार- इस सम्बन्ध में 30वें संविधान संशोधन
द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 133 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय
से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा
सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाये कि विवाद में कानून
की व्याख्या से सम्बन्धित सारभूत प्रश्न अन्तर्निहित है और "विवाद सर्वोच्च
न्यायालय में अपील के लिए अभीष्ट है।"
4. विशेष
अपीलीय क्षेत्राधिकार- ऐसे मामले जो कि उपर्युक्त
विषयों में नहीं आते,
परन्तु फिर भी उनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
आवश्यक लगता हो,
उनमें सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार
है। सर्वोच्च न्यायालय भारत राज्य की क्षेत्र सीमा में स्थित किसी भी
न्यायालय अथवा न्यायाधीकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आज्ञाप्ति, दण्ड
या आदेश के विरुद्ध अपील सुन सकता है। परन्तु सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय
के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
सर्वोच्च न्यायालय को
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के अन्य
पदाधिकारियों के चुनाव में उत्पन्न विवादों में भी निर्णय देने का अधिकार प्राप्त
है।
5. विशेष
अदालतों से सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील की व्यवस्था- राष्ट्रपति ने 13 जुलाई, 1984 को आतंकवादी क्षेत्र' अध्यादेश
जारी कर केन्द्र सरकार को अधिकार दिया है कि वह देश (जम्मू-कश्मीर के अलावा) के
किसी भी भाग को आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र घोषित कर आतंकवादियों पर मुकदमे चलाने
के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर सकती हैं। इन अदालतों के खिलाफ अपील सीधे
सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी।
3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार-
संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को
परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार से विभूषित किया है—
(i)
अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी
राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि अथवा तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, जो
सार्वजनिक महत्त्व का है,
तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श माँग
सकता है। यद्यपि न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे
परामर्श देना ही पड़ेगा।
(ii) अनु. 143 का खण्ड (2) राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह संविधान के लागू होने के पूर्व किसी
सन्धि समझौता आदि के बारे में उठे विवादों को इस न्यायालय के पास उसकी सम्मति
जानने के लिए भेज सके। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या प्रकरण के सम्बन्ध में
राष्ट्रपति द्वारा माँगी गयी राय के सम्बन्ध में निम्न बातें स्पष्ट की-
(i) अनुच्छेद 143 (1) कानूनी तथा
सांविधानिक महत्त्व के मामले में ही लागू होता है, ऐतिहासिक व पुरातात्विक मामलों में नहीं।
(ii) न्यायालय का मत है कि वह सभी
मामलों में राष्ट्रपति को राय देने के लिए आबद्ध नहीं है।
(iii) अनु. 143 (1) के अन्तर्गत प्रकट
की गयी उच्चतम न्यायालय की राय 'न्यायिक उद्घोषणा' या न्यायिक निर्णय नहीं है।
4. सविधान की व्याख्या और सुरक्षा का अधिकार-
संविधान की व्याख्या तथा
सुरक्षा का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही प्रदान किया गया है। सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा दी गई संविधान की व्याख्या सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम मानी जाती
है तथा साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक
पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय को अपने
द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति
प्राप्त है। यदि संसद द्वारा निर्मित कानून या केन्द्रीय कार्यपालिका
द्वारा जारी किए गए आदेश संविधान के किसी अनुच्छेद की अवहेलना करते हों तो सर्वोच्च
न्यायालय ऐसे कानून या आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केन्द्र सरकार
अथवा राज्य सरकार अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर किसी कानून का निर्माण करे तो
सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को रद्द कर सकता है। संविधान देश का सर्वोपरि
कानून है, उनकी सुरक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य वैधानिक कर्त्तव्य है।
24 अप्रैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद
भारती के प्रसिद्ध अभियोग में यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान में
ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जो संविधान के मौलिक ढाँचे को नष्ट करती हो। सर्वोच्च
न्यायालय के इस निर्णय ने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया
है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय
संसद की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।
5. अभिलेख न्यायालय-
अनु. 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का
स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं-
1. इस न्यायालय के अभिलेख सब जगह तथा साक्षी रूप में
स्वीकार किये जायेंगे तथा इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनकी
प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता।
2. इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना' पर
दण्ड दिया जा सकता है,
वैसे तो यह बात प्रथम स्थिति में स्वयं ही मान्य हो जाती है, परन्तु
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमानना करने वालों को दण्ड देने की
व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गई है।
6. अभियोगों को स्थानान्तरित करने की शक्ति-
संविधान के अनुच्छेद 139 (क) के
अनुसार कुछ अभियोग जिनका सम्बन्ध एक या लगभग एक ही प्रकार के कानून के प्रश्नों से
है जो कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों के पास निर्णय के लिए पड़े हैं तो
सर्वोच्च न्यायालय अपनी पहल के आधार पर अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा
दिये अनुरोध पत्र के आधार पर या अभियोग से सम्बन्धित किसी पक्ष की ओर से
किये विनय-पत्र द्वारा तुष्ट होने पर कि ऐसे प्रश्न साधारण महत्त्व वाले
महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले उच्च न्यायालयों
से अपने पास मंगवा सकता है और उन समस्त अभियोगों का निर्णय स्वयं कर सकता
है।
7. न्यायिक सक्रियता सम्बन्धी भूमिका-
1980 के बाद से, विशेषकर 1993-2019 ई. के
वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने जनहित अभियोग
और न्यायिक सक्रियता के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका
प्राप्त कर ली है। अपनी इस भूमिका के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न
सरकारी एजेन्सियों को समय-समय पर अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिये
हैं और इस बात का प्रतिपादन किया है कि कानून सर्वोपरि है एवं सरकारी
एजेन्सी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए।
विधायिका और कार्यपालिका जब
अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे, तब न्यायपालिका को न्यायिक
सक्रियता की स्थिति अपनानी पड़ी है। न्यायिक सक्रियता ने सामान्य व्यक्तियों के
मन-मस्तिष्क में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाये रखने में योगदान
दिया है।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मौलिक क्षेत्राधिकार
को छोड़कर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ "विश्व के किसी भी
सर्वोच्च न्यायालय से अधिक हैं।" अपीलीय क्षेत्राधिकार में उसकी
शक्तियाँ अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्च
न्यायालयों के संवैधानिक,
दीवानी तथा फौजदारी निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है।
यह देश के निम्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की
विशेष आज्ञा दे सकता है। इस पर भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमरीकी
सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तिशाली नहीं। वस्तुत: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की
शक्तियाँ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के कारण मर्यादित हैं
जबकि अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ 'कानून की उचित प्रक्रिया के
कारण अमर्यादित हैं।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई
होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।
Back To - भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था




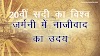










0 Comments