पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियाँ
पृथ्वीराज चौहान की जन्म-तिथि विवादास्पद है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रन्थ के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म वि. सं. 1223 के ज्येष्ठ मास की द्वादशी को हुआ था। पृथ्वीराज के सिंहासन पर बैठने की आयु 11 वर्ष की थी। प्रारम्भ में पृथ्वीराज ने अपनी माता के कुशल संरक्षण में शासन करना आरम्भ किया, अपने मन्त्रियों व पदाधिकारियों को पुराने पदों पर कायम रखा। इस समय पृथ्वीराज का मुख्यमन्त्री कदम्बवास था जो कि अत्यधिक विद्वान्, कुशल शासक व स्वामिभक्त था। पृथ्वीराज की प्रारम्भिक विजय का श्रेय इसी को जाता है। इस समय दूसरा प्रमुख व्यक्ति भुवनैमल्ल था जो कलचुरी का राजा था और पृथ्वीराज को माता ने इसे अपना सेनापति नियुक्त किया था।
डॉ. गोपीनाथ
शर्मा का कथन है कि
महत्त्वाकांक्षी पृथ्वीराज ने 1178 ई. के आस-पास ही अपने राज्य का सम्पूर्ण शासन
अपने हाथों में ले लिया था।
गद्दी पर बैठते
समय पृथ्वीराज के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं। पृथ्वीराज चौहान
को बाहरी और आन्तरिक दोनों ही शत्रुओं से लोहा लेना था। पृथ्वीराज ने सबसे
पहले अपने आन्तरिक शत्रुओं को परास्त करके चौहान राज्य को एक सूत्र में
बाँधकर केन्द्रीय शक्ति को सबल बनाने का निश्चय किया।
पृथ्वीराज चौहान की प्रारम्भिक
विजयें
नागार्जुन का दमन-
पृथ्वीराज चौहान के गद्दी पर बैठते ही
विग्रहराज चतुर्थ के छोटे पुत्र नागार्जुन ने उसके अधिकार को चुनौती दी। पृथ्वीराज
ने अपने सेनापति की देखरेख में एक विशाल सेना नागार्जुन के विरुद्ध रवाना की। इस
सेना ने नागार्जुन के प्रधान केन्द्र गुड़गाँव को चारों तरफ से घेर लिया।
नागार्जुन तो किसी तरह वहाँ से भाग निकला लेकिन उसके परिवार के सदस्यों व अनेक
सैनिकों को पकड़ कर अजमेर लाया गया। यहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उनके
सिर किले के दरवाजे पर लटका दिये गये। भविष्य में नागार्जुन का कहीं उल्लेख
नहीं मिलता।
भण्डानकों का दमन-
विग्रहराज चतुर्थ ने इन्हें
पराजित किया था। लेकिन अब ये वापिस शक्तिशाली हो गये थे और पृथ्वीराज की
अल्पवयस्कता का लाभ उठाते हुए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। डॉ. दशरथ शर्मा
का मानना है कि सम्भवतः यह जाति कन्नौज और हर्षपुर के आस-पास के क्षेत्रों में
आबाद थी और सम्भवतः बयाना भी इनके अधिकार क्षेत्र में था। नागार्जुन के दमन
के बाद पृथ्वीराज ने भण्डानकों की तरफ ध्यान दिया। 1182 ई. में उसने
भण्डानकों पर जबरदस्त आक्रमण बोला। उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया और
सैंकड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया, हजारों भण्डानक उत्तर की तरफ भाग गये। इसके बाद एक
शक्ति के रूप भण्डानकों का उल्लेख नहीं मिलता।
 |
| पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियाँ |
इन विजयों के बाद
पृथ्वीराज का उत्तराधिकार सुदृढ़ हो गया। भविष्य में किसी चौहान उम्मीदवार ने उसके
नेतृत्व को चुनौती देने का साहस नहीं किया।
पृथ्वीराज चौहान की
दिग्विजय
जैजाकमुक्ति की
विजय-
भण्डानकों की विजय के बाद पृथ्वीराज
ने चन्देलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस समय चन्देलों का राज्य काफी
विस्तृत था और महोबा उसकी राजधानी थी। परश्भर्दी देव
चन्देलों का राजा था। पृथ्वीराज रासो व कल्प काव्यों से पता चलता है कि पृथ्वीराज
ने राजधानी महाबो को घेर लिया व चन्देलों को पराजित किया, लेकिन कुछ वर्षे के बाद
ही चन्देल पुनः शक्तिशाली हो गये और पृथ्वीराज के शत्रुओं की
नामावली में गिने जाने लगे।
गुजरात पर आक्रमण-
पृथ्वीराज व गुजरात के सम्बन्ध सोमेश्वर
के शासन काल तक तो मैत्रीपूर्ण थे, लेकिन सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में यह सम्बन्ध
शत्रुतापूर्ण होने लगे। डॉ. गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संघर्ष का मूल कारण
दोनों राज्यों की विस्तारवादी नीति थी। गुजरात के चालुक्य अजमेर के चौहानों
को भी अपनी अधीनता में लाना चाहते थे जबकि पृथ्वीराज स्वयं अपनी स्वतन्त्र सत्ता
का विस्तार करना चाहता था। तत्कालीन साहित्यों व शिलालेखों के आधार पर यह कहा जा
सकता है कि 1184 ई. के आसपास दोनों के बीच किसी स्थान पर अनिर्णित युद्ध लड़ा गया, लेकिन 1187 ई. में दोनों
पक्षों के बीच पुनः मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गये।
गहड़वालों के साथ
संघर्ष-
परम्पराओं के
अनुसार पृथ्वीराज चौहान का कन्नौज के गहड़वालों के साथ भी संघर्ष
हुआ। संघर्ष का कारण संयोगिता का विवाह माना जाता है। कन्नौज नरेश जयचन्द
भी अपने समय का शक्तिशाली शासक था। उसने एक स्वतन्त्र व विशाल साम्राज्य की
स्थापना करके राजसूय यज्ञ का आयोजन भी किया था। जयचन्द ने अपनी पुत्री के विवाह के
लिये स्वयंवर का आयोजन किया। उसने अन्य सभी शासकों को तो आमन्त्रित किया लेकिन पृथ्वीराज
को नहीं बुलाया,
जबकि संयोगिता
पहले से ही पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी। पृथ्वीराज किसी तरह अपने
सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गया और संयोगिता को उठा लाया।
लेकिन अधिकांश
विद्वानों ने इस कथा को अविश्वसनीय माना है। वास्तव में पृथ्वीराज व जयचन्द
दोनों का संघर्ष विस्तारवादी नीति का परिणाम था। जयचन्द वास्तव में दिल्ली
पर अधिकार करना चाहता था जबकि पृथ्वीराज दिल्ली पर अधिकार बनाये रखने के लिये कृत
संकल्प था। इसके आलावा पृथ्वीराज को प्रारम्भिक सफलताओं ने जयचन्द
की ईर्ष्या को बढ़ाने का काम किया और जयचन्द के लिये पृथ्वीराज की
बढ़ती शक्ति को रोकना आवश्यक हो गया। फिर भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि उत्तर
भारत में अपनी शक्ति का प्रसार करने के लिये दोनों के बीच प्रत्यक्षत: कोई युद्ध
हुआ हो।
पृथ्वीराज चौहान एवं
मुहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष
तराइन का प्रथम
युद्ध (1191 ई.)-
पृथ्वीराज चौहान व गौरी
के बीच प्रथम युद्ध 1190-91 में हुआ। संघर्ष का मूल कारण नैतिक व धार्मिक
था। गौरी महत्त्वाकांक्षी शासक था और वह भारत में अपने राज्य का विस्तार
करना चाहता था। इसके लिये उसे विपुल धन सम्पदा की आवश्यकता थी और वह केवल भारत से
ही पूर्ण की जा सकती थी। भारत की राजनीतिक स्थिति भी गौरी के अनुकूल थी, एक केन्द्रीय शक्ति का
अभाव था। प्रान्तीय सरकारें शुरू हो रही थी, प्रान्तों में मतैक्य का अभाव था। ये प्रान्तीय राजवंश
हमेशा एक-दूसरे को नीचा दिखाने को तत्पर रहते थे।
कुछ इतिहासकारों
ने संघर्ष का मूल कारण धार्मिक भावनायें बताया है, लेकिन वास्तव में संघर्ष का मूल कारण दोनों की साम्राज्यवादी
नीति ही थी जिसने दोनों के बीच युद्ध को अवश्यम्भावी बना दिया था।
युद्ध का आरम्भ- मोहम्मद गौरी ने गजनी से
प्रस्थान करके पहले लाहौर और उसके बाद सरहिन्द पर भी अधिकार कर लिया। इससे चौहान
राज्य की सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने अपने
सेनापति गोविन्द राज के साथ सरहिन्द की तरफ कूच किया। मोहम्मद गौरी
भी आगे बढ़ा और तराइन के मैदान में दोनों की सेनायें आमने-सामने आ डटी।
युद्ध के आरम्भ
से ही चौहान सेना का पलड़ा भारी रहा, राजपूत सेना ने दोनों ओर से गौरी की सेना पर भीषण धावा बोला, जिससे गौरी की सेना में
भगदड़ मच गयो। पृथ्वीराज के सेनापति गोविन्द राज ने कटार का जोरदार
प्रहार करके गौरी को घायल कर दिया। एक स्वामिभक्त खिलजी सैनिक गौरी को
युद्ध-क्षेत्र से सुरक्षित निकाल ले गया। गौरी के पलायन के साथ ही उसकी सेना के
पाँव उखड़ गये। कुछ दिनों बाद ही पृथ्वीराज ने सरहिन्द पर आक्रमण किया और पुनः
अधिकार कर लिया।
तराइन का यह
युद्ध पृथ्वीराज का
चरमोत्कर्ष था,
लेकिन भागती
मुस्लिम सेना का पीछा न करना और उसके सेनापति को ससम्मान छोड़ देना, भयंकर भूल थी। दूसरी तरफ
यह युद्ध मोहम्मद गौरी के लिये भयंकर अपमानजनक था। वह इस घटना को कभी भूला
नहीं था और गजनी पहुंचते ही युद्ध की तैयारियों में जुट गया।
तराइन का दूसरा
युद्ध (1192 ई.)-
एक वर्ष तक पूरी
तैयारी करने के बाद गौरी 120,000 चुने हुये घुड़सवारों के साथ भारत में
प्रवेश किया। लाहौर व मुल्तान के रास्ते वह भारत के तराइन के मदैन में आ डटा। पृथ्वीराज
ने भी अपनी विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। एक बार तो गौरी विशाल सेना को
देखकर घबरा गया,
लेकिन उसने
गुपचुप तैयारी की और दस-दस हजार की सैनिक टुकड़ियों ने चारों तरफ से चारों दिशाओं
से आक्रमण किया। अचानक हुये इस आक्रमण से राजपूत सेना में खलबली मच गई। दिन के
तीसरे पहर तक राजपूत सेना थककर चूर हो गयी, प्रतिकूल परिस्थिति देखकर पृथ्वीराज सिरसा की तरफ
भाग गया लेकिन दुर्भाग्य से पकड़ा गया और कत्ल कर दिया गया। गोविन्दराज व
अन्य बहुत से सामन्त हजारों सैनिकों के साथ मारे गये।
तराइन का दूसरा
युद्ध निर्णायक सिद्ध
हुआ। गौरी ने पृथ्वीराज से अपनी पिछली पराजय का बदला ले लिया। गौरी
ने दिल्ली व अजमेर सहित विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यद्यपि पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने कुछ समय तक चौहानों
की शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया।
युद्ध के परिणाम-
सम्पूर्ण भारत को
इस युद्ध के घातक परिणाम भुगतने पड़े। दिल्ली व अजमेर पर से चौहानों की सत्ता का
अन्त हो गया। डॉ. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि तराइन का
दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना है। हमारे इतिहास में
पहली बार मोहम्मद गौरी ने हिन्दुस्तान के बीचों बीच तुर्की राज्य की
नींव डाली। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह रहा कि बार-बार की पराजय के बाद भी राजपूतों
ने इतिहास से कोई सबक नई सोखी और नवोदित मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर
मुकाबला करने का प्रयास नहीं किया। विजय के बाद तुर्की सैनिकों ने लूटमार और
तोड़-फोड़ का घृणित प्रदर्शन किया। हजारे हिन्दुओं को अपनी संचित सम्पत्ति से हाथ
धोना पड़ा। कलात्मक मन्दिरों व मूर्तियों को तोड़ा गया जिससे अमूल्य स्मारक नष्ट
हो गये। मन्दिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। सबसे ज्यादा आघात बौद्ध धर्म को
लगा।
आर. सी. मजूमदार लिखते हैं कि तराइन के
इस युद्ध ने केवल चौहानों को शक्ति को ही समाप्त नहीं किया बल्कि पूरे हिन्दू धर्म
का विनाश कर दिया। शासन कुमारों का साहस टूट गया और पूरा हिन्दुस्तान आतंक में
जकड़ गया।
पृथ्वीराज की पराजय
के कारण
पृथ्वीराज की पराजय का पहला कारण
तो उसकी भोग-विलासिता और शासन के प्रति अरुचि थी। संयोगिता का अपहरण उसकी
रसिकता व भोग-विलासिता का ज्वलंत उदाहरण है। पृथ्वीराज के इस कृत्य ने न
केवल जयचन्द को बल्कि अन्य शासकों को भी उसका विरोधी बना दिया था। दूसरा कारण गौरी
की तुलना में उसकी योग्यता कुछ कम थी।
डॉ. दशरथ शर्मा लिखते हैं
कि युद्ध कला में वह गौरी से कुछ कम था। जबकि गौरी एक निपुण व चालाक सेनानायक था। पराजय
का तीसरा कारण सैनिक संख्या का कम होना था। वह गौरी की तुलना में कुछ
कम सैनिक जुटा पाया। उसका एक सेनानायक स्कन्ध किसी दूसरी दिशा में गया हुआ था जो
ठीक समय तक तराइन नहीं पहुंच पाया जबकि गौरी एक विशाल सेना के साथ पहले से ही डेरा
जमाये बैठा था।
एक अन्य वास्तविक
कारण उसका गौरी की सेनाओं को नहीं समझ पाना था। यदि उसने जागरुक रहकर गौरी
की प्रत्येक क्रिया पर गिद्ध दृष्टि रखी होती तो उसे अचानक हुये आक्रमण का सामना
नहीं करना पड़ता।
पृथ्वीराज का
मूल्यांकन
चौहान वंशी
शासकों में पृथ्वीराज चौहान का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह
वीर, सुन्दर, साहसी व सैनिक प्रतिभाओं
से युक्त शासक था। वह विद्वानों व कलाकारों का आश्रयदाता था। पृथ्वीराज विजय
का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासो
के चन्दर बरदाई, बागीश्वर, जनार्दन आदि अनेक
विद्वान् उसके दरबार में आश्रय पाते थे।
अपने शासन के
प्रारम्भिक समय में ही शानदार सफलतायें प्राप्त करके उसने अपने आपको एक सफल व विजयी
सम्राट सिद्ध कर दिया था। उसने न केवल राज्य की सीमाओं का विस्तार किया बल्कि
आन्तरिक व बाहरो विद्रोहों का दमन करके शान्ति व व्यवस्था स्थापित की और अपने शासन
को दृढ़ता प्रदान की, लेकिन उसमें
कूटनीति की कमी थी। उसने अपने राजनीतिक अहंकार के चलते अनेक शासकों को अपना शत्रु
बना लिया, जबकि पहले विदेशी शत्रु
को समुचित व्यवस्था करना आवश्यक था।
डॉ. सत्यप्रकाश ने इस सम्बन्ध में ठीक
ही लिखा है कि उसने मुस्लिम आक्रमण को कभी भी गम्भीरता से नहीं लिया और न ही कभी
पड़ोसी राज्यों से सहयोग लेने का प्रयल किया। 1178 ई. में चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी
को परास्त किया और 1191 ई. में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को
परास्त किया। यदि दोनों में मतैक्य होता तो अनुमान लगाया जा सकता है कि गौरी
की क्या स्थिति होती?
वास्तविकता यह है
कि पृथ्वीराज में युवकोचित साहस व महत्त्वाकांक्षायें तो थीं लेकिन
सम्पूर्ण देश की राजनीतिक स्थिति और आवश्यकता को समझने योग्य क्षमता व परिपक्यता
उसमें नहीं थी। उसमें राजनीति और युद्ध में शत्रु को छकाने योग्य कूटनीति का अभाव
था। तराइन के पहले युद्ध में उसे सफलता मिली लेकिन शत्रु सेना का
पीछा नहीं किया और न ही आगे बढ़कर उसने पंजाब पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया।
उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सक्षम बनाने का कभी प्रयास नहीं किया। परिणाम यह
निकला कि गौरी ने उसे ही असावधान स्थिति में दबोच लिया। डॉ. दशरथ शर्मा के
अनुसार इन्हीं गलतियों की वजह से उसका सर्वनाश हुआ। उसकी गलतियों के कारण उसे
क्षमा नहीं किया जा सकता। तराइन के युद्ध के, ठीक पहले उसके लक्षण न तो एक सुयोग्य योद्धा के थे और न ही
एक सेनानायक के वरन् एक नये सिखतड़ के थे।
वस्तुतः पृथ्वीराज
चौहान अवसर के अनुकूल खरा नहीं उतर पाया। यही कारण है कि उसे उस युग का महान्
शासक कहने से पहले उसकी इन गलतियों की तरफ ध्यान स्वतः ही चला जाता है।
आशा है कि हमारे
द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो
इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।





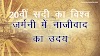








0 Comments