परिचय (Introduction):
भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी- देशी रियासतों का एकीकरण। इनमें राजस्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय था, जहाँ 24 स्वतंत्र रियासतें अलग-अलग शासकों के अधीन थीं। इन रियासतों को एक सूत्र में बाँधना न केवल प्रशासनिक चुनौती थी, बल्कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति और कूटनीतिक कौशल की भी परीक्षा थी।
"राजस्थान के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या थीं?" यह प्रश्न इतिहास के उस
अध्याय की ओर इशारा करता है जहाँ स्वार्थ, शंका, असुरक्षा और नेतृत्व की लड़ाई हावी थी। हर रियासत अपना प्रभुत्व बनाए रखना
चाहती थी और एक साझा सत्ता के अधीन आने को तैयार नहीं थी। यही कारण है कि राजस्थान
के एकीकरण की प्रक्रिया धीमी, जटिल और संघर्षपूर्ण रही।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि राजस्थान के एकीकरण में क्या-क्या
कठिनाइयाँ सामने आईं, किन राजाओं ने विरोध किया, किसने नेतृत्व किया और अंततः कैसे भारत के हृदयस्थल में एक मजबूत, एकीकृत राज्य की स्थापना
हुई।
 |
| राजस्थान के एकीकरण में बाधाएँ और प्रयास: सम्पूर्ण जानकारी |
राजस्थान के एकीकरण में बाधाएँ, कारण, समस्याएँ और समाधान (1947–1949)
भारत को स्वतन्त्रता के समय राजस्थान में छोटे-बड़े 24 राज्य थे। प्रत्येक
राज्य का पृथक राज्य हुआ करता था। ये सब मिलकर वृहत् संगठित क्षेत्र का निर्माण
करते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तक देशी राज्यों की राजनीति का संचालन
भारत सरकार का राजनीतिक विभाग करता था। इसे समाप्त कर दिया गया तथा 5 जुलाई, 1947 को सरदार वल्लभभाई
पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। रियासती सचिवालय ने
छोटे-छोटे राज्यों को संगठित कर बड़े राज्यों का निर्माण करने की योजना बनाई।
संयुक्त राज्य के निर्माण में भाषा, भौगोलिक सीमा, संस्कृति को आधार बनाया गया। एक संयुक्त राज्य में, एकसामान्य शासन विभाग, धारासभा और न्याय विभाग
की स्थापना की गई। समूहीकरण की प्रक्रिया में एक राज्य को अपने निकटवर्ती प्रान्त
में विलीन करना था।
यह भी जानें- राजस्थान के एकीकरण के चरण
भारत सरकार के रियासती विभाग ने राजस्थान के भी विभिन्न राज्यों को संगठित कर एकीकृत
राजस्थान का निर्माण करने का फैसला किया। यह कार्य पाँच चरणों में सम्पन्न किया गया।
सर्वप्रथम अलवर,
भरतपुर, धौलपुर करौली को मिलाकर 'मत्स्य संघ' का निर्माण किया गया।
दूसरे चरण में प्रथम संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा के
राज्यों को सम्मिलित किया गया। तीसरे चरण में उदयपुर राज्य को भी प्रथम चरण में
संयुक्त राजस्थान में शामिल कर लिया गया। चौथे चरण में राजस्थान के शेष राज्यों को
मिलाकर वृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर
राज्यों को भी शामिल किया गया। अन्तिम चरण में मत्स्य संघ को भी एकीकृत
राजस्थान में सम्मिलित कर लिया था। बाद में अजमेर, मेवाड़ व सिरोही राज्य को भी एकीकृत राजस्थान
में मिला दिया गया।
राजस्थान के एकीकरण की कठिनाइयाँ
1. राजस्थान के नरेशों का स्वाभिमानी होना-
हालांकि राजस्थान के समस्त नरेश ब्रिटिश हुकूमत के तो पूर्णतः गुलाम बन चुके
थे उनकी दासता में वे अपना हित समझते थे। परन्तु राजस्थान की विभिन्न रियासतों
(सिवाय टोंक के) के राजपूत नरेश स्वयं को दूसरे से प्रतिष्ठा में कम नहीं समझते
थे। डूंगरपुर,
बांसवाड़ा व
शाहपुरा जैसी छोटी रियासतों के नरेश भी अपने को महाराणा, जोधपुर नरेश व कोटा के
राव से कम नहीं समझते थे। अत: जब कभी राजस्थान को मिलाकर एक इकाई गठित करने की बात
आई तो प्रत्येक नरेश का यही प्रयास रहा कि उस इकाई में वह अपने राज्यों को
महत्त्वाकांक्षी रखे। इसके साथ ही इस इकाई में वे अपना पद भी गौरवशाली बनाये रखना
चाहते थे।
मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह ने जब अपने नेतृत्व में संघ बनाना चाहा तो
उन्होंने इसी नीति पर आचरण किया। इसी प्रकार जब जयपुर नरेश मानसिंह ने
राजस्थान की दक्षिण पूर्वी रियासतों का संघ बनाना चाहा, तो उसे भी इसी नीति पर
बनाने प्रयास किया। उनकी इस नीति ने छोटी रियासतों के नरेशों के मस्तिष्क में शंका
उत्पन्न कर दी। परन्तु जब इंग्लैण्ड की एटली सरकार ने भारत की सत्ता भारतवासियों
को सौंपने का समय (जून 1947) निर्धारित कर दिया तो रियासतों में खलबली का मचना स्वाभाविक था।
यह भी जानें- राजस्थान के एकीकरण के चरण
रियासतों के भविष्य के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया था कि भारत के
भावी संवैधानिक ढांचे में समुचित रूप से अपना भाग अदा करने के लिए छोटी-छोटी
रियासतों को आपस में मिलकर बड़ी इकाइयाँ बना लेनी चाहिए या उन्हें पड़ोस की बड़ी
रियासतों या प्रान्तों में मिल जाना चाहिए। इसी संदर्भ में सितम्बर, 1946 में अखिल भारतीय देशी
लोक परिषद् भी यह निर्णय ले चुकी थी कि राजस्थान की कोई भी रियासत अपने आप में
भारतीय संघ में शामिल होने के योग्य नहीं है। अतः राजस्थान को एक ही इकाई के रूप
में भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में छोटी रियासतें अपने
भविष्य के लिए भयातुर थीं।
मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह ने समय के बदलाव को पहचाना और समय का लाभ
उठाते हुए उन्होंने छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाने का प्रयास किया।
अपने विचार को क्रियान्वित करने की दृष्टि से उन्होंने 25 जून, 1947 को राजस्थान, गुजरात व मालवा के राजाओं
का सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में विभिन्न रियासतों के 22 राजा उपस्थित हुए। उस
सम्मेलन में महाराणा ने रियासतों के मिलने का प्रस्ताव रखा था। उपस्थित नरेशों ने
प्रस्ताव पर विचार करने का प्रयास का वायदा किया।
23 मई, 1947 को उदयपुर में दूसरा
सम्मेलन बुलाया। इसमें महाराणा के संवैधानिक सलाहकार श्री के.एस. मुंशी भी
उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने उपस्थित नरेशों को चेतावनी भी दी कि "हम लोगों ने
मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रान्तों के समकक्ष
नहीं हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो
जावेंगी।" उनकी इस चेतावनी का भी नरेशों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसका
प्रमुख कारण यही था कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़,
बाँसवाड़ा, शाहपुरा आदि रियासते यही
सोचने लगी थी कि महाराणा हमारा विलय करके हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं
और वे मेवाड़ का प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं। इसी प्रकार जब जयपुर नरेश
मानसिंह की अनुमति से उनके प्रधानमंत्री वी. टी. कृष्णाचारी ने प्रदेश के शासकों
का सम्मेलन बुलाया अलवर, भरतपुर व करौली को अपना अस्तित्व संकट में लगा। इसी प्रकार राजस्थान की अन्य छोटी
रियासतें भी पारस्परिक अविश्वास के कारण संघ में मिलने को तैयार नहीं होरही थीं।
2. नरेशों के विभिन्न दृष्टिकोण-
राजस्थान की छोटी स्यिासतों के विलय के संदर्भ में राजस्थान की रियासतों को
बड़ी इकाई के रूप में बदलने के प्रस्ताव पर राजस्थान के लगभग सभी राजा सहमत थे, परन्तु वे अपने विचारों
को अमली जामा विभिन्न स्वरूपों में पहनाना चाहते थे। मेवाड़ के महाराणा राजस्थान
की चार बड़ी रियासतों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर) का अस्तित्व रखते
हुए ऐसा संघ बनाना चाहते थे, जो एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में भावी भारतीय संघ में भूमिका निभा सके।
जबकि कोटा के महाराव भीमसिंह कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर उनका संयुक्त संघ बनाना
चाहते थे। इसी प्रकार डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मणसिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व प्रतापगढ़ को
मिलाकर एक अलग इकाई बनाना चाहते थे। जैसा कि बताया जा चुका है कि जयपुर नरेश अलवर
व करौली को लेकर अलग संघ बनाना चाहते थे। नरेशों के विभिन्न विचारों कारण राजपूतों
की 19 रियासतें आपस में एक
इकाई के रूप में परिणत नहीं हो पा रही थीं।
3. जोधपुर व बीकानेर नरेशों की अलग धारणा-
जोधपुर नरेश हनुवन्तसिंह ब्रिटिश सरकार की घोषणा के उपरान्त अपनी नई
धारणा बना रहे थे। वे भारत में न मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। उनका साथ
जैसलमेर व धौलपुर भी दे रहे थे। हनुवन्तसिंह पाकिस्तान के निर्माता मिस्टर मुहम्मद
अली जिन्ना के हाथों में पूर्णत: खेल रहे थे। परन्तु वी. पी. मेनन के ठीक समय
पर किए गए प्रयासों व लार्ड माउन्टबैटन के समझाने के कारण जोधपुर नरेश ने अपनी रियासतों
को पाकिस्तान में विलय करने का विचार त्याग दिया।
इसके साथ ही जैसलमेर राजकुमार की हिन्तुत्व की भावना ने भी उनको इस मार्ग से हटाया। जब
जोधपुर नरेश जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान के साथ समझौता करने को उद्यत हो गए तो
उन्होंने जैसलमेर के राजकुमार से पूछा कि तुम मेरे साथ पाकिस्तान में विलय पर
हस्ताक्षर करोगे या नहीं। प्रत्युत्तर में जैसलमेर राजकुमार ने कहा कि यदि हिन्दू
व मुसलमानों के मध्य कोई संकट उत्पन्न हुआ तो वह हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों का
साथ नहीं देगा। जैसलमेर के एक राजकुमार का यह कहना जोधपुर के नरेश को एक वज्रपात
के सदृश लगा। उसने पाकिस्तान में विलय होने का विचार त्याग भारतीय संघ में मिलने
का इरादा किया।
इसी प्रकार बीकानेर नरेश शार्दुलसिंह भी पहले बीकानेर रियासत को राजस्थान
संघ में विलय करने के पक्ष में नहीं थे। दिसम्बर, 1946 में वी. पी. मेनन
बीकानेर नरेश से इस संदर्भ में मिले। उन्होंने मेनन को इन्कार किया, परन्तु जब जयपुर व जोधपुर
नरेश राजस्थान में विलय के लिए राजी हो गये तब बीकानेर नरेश ने अपनी अनुमति दी। 30 मार्च, 1949 को जब वृहत् राजस्थान का
निर्माण हो गया तो बीकानेर रियासत के नरेश का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। इस
प्रकार जोधपुर व बीकानेर के रियासतों के नरेशों ने भी राजस्थान संघ के निर्माण में
कुछ विलम्ब किया।
निष्कर्ष (Conclusion):
राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया मात्र प्रशासनिक निर्णय नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक
समझदारी, धैर्य, और दूरदर्शिता का परिणाम
थी। जहाँ एक ओर रियासतों के नरेश अपनी सत्ता, प्रतिष्ठा और स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर चिंतित थे, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र
भारत की नींव एक मजबूत और संगठित राष्ट्र के रूप में रखी जा रही थी। इन दोनों
धाराओं के बीच संतुलन स्थापित करना आसान नहीं था।
राजस्थान की एकता में बाधाएँ अनेक थीं, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि रहा। अंततः सभी मतभेदों और
स्वार्थों को दरकिनार कर रियासतें एक साथ आईं और एक समृद्ध, सशक्त एवं एकीकृत
राजस्थान का उदय हुआ। यह एकीकरण ना सिर्फ प्रशासनिक सफलता थी, बल्कि यह उस भावना का
प्रतीक है जिसमें विविधता होते हुए भी एकता संभव है।
आज का राजस्थान, जो गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकास का प्रतीक है, उसी ऐतिहासिक समर्पण और एकता का फल है। यह गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।
यह भी जानें- राजस्थान के एकीकरण के चरण



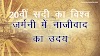











0 Comments