मन का अर्थ
मन शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। जैसे- मानस, चित्त, मनोभाव तथा मत इत्यादि। लेकिन मनोविज्ञान में मन का तात्पर्य आत्मन्, स्व या व्यक्तित्व से है। यह एक अमूर्त सम्प्रत्यय है। जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसे न तो हम देख सकते है। और न ही हम इसका स्पर्श कर सकते है। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क के विभिन्न अंगों की प्रक्रिया का नाम मन है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक सिगमण्ड फ्रायड के अनुसार मन का सिद्धान्त एक प्रकार का परिकल्पनात्मक सिद्धान्त है।
मन की परिभाषा
फ्रायड के अनुसार- ‘‘मन से तात्पर्य
व्यक्तित्व के उन कारकों से होता है जिसे हम अन्तरात्मा कहते है। तथा जो
हमारे व्यक्तित्व में संगठन पैदा करके हमारे व्यवहारों को वातावरण के साथ समायोजन
करने में मदद करता है।’’
रेबर के अनुसार- ‘‘मन का तात्पर्य परिकल्पिक
मानसिक प्रक्रियाओं एवं क्रियाओं की सम्पूर्णता से है, जो मनोवैज्ञानिक प्रदत्त
व्याख्यात्मक साधनों के रूप में काम कर सकती है।
अत: मन की हम
मात्र कल्पना कर सकते हैं। इसको न तो किसी ने देखा है और न ही हम इसकी कल्पना कर
सकते हैं।’’
मन की अवस्थाएँ
मन की अवस्थाओं से तात्पर्य इसके विभिन्न पहलुओं से है। मन
आत्मा या व्यक्तित्व के दो पक्ष होते है- जिन्हें आकारात्मक पक्ष और गत्यात्मक
पक्ष कहते हैं- मन के आकारात्मक पक्ष से तात्पर्य जहाँ संघर्षमय परिस्थिति
की गत्यात्मकता उत्पन्न होती है मन का यह पहलू वास्तव में व्यक्तित्व के गत्यात्मक
शक्तियों के बीच होने वाले संघर्षों का एक कार्यस्थल होता है। मन के गत्यात्मक
पक्ष से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिसके द्वारा मूल-प्रवृत्तियों से उत्पन्न
मानसिक संघर्षों का समाधान होता है।
 |
| मन का अर्थ, परिभाषा, अवस्थाएँ एवं विशेषताएं |
मन के आकारात्मक पक्ष
आकारात्मक पक्ष
का अध्ययन हम तीन भागों में बाँट कर करेंगे।
1. चेतन मन 2. अर्द्ध चेतन
मन 3. अचेतन मन।
1. चेतन मन-
मन का वह भाग जिसका सम्बन्ध
तुरन्त ज्ञान से होता है, या जिसका सम्बन्ध
वर्तमान से होता है। जैसे- कोई व्यक्ति लिख रहा है तो लिखने की चेतना है, पढ़ रहा है तो पढ़ने की
चेतना है। व्यक्ति जिन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के प्रति जागरूक रहता है वह
चेतन स्तर पर घटित होती है। इस स्तर पर घटित होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी
व्यक्ति को रहती है। यद्यपि चेतना में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं परन्तु इसमें
निरन्तरता होती है अर्थात् यह कभी खत्म नहीं होती है।
चेतन मन की विशेषताएँ-
यह मन का सबसे
छोटा भाग है।
चेतन मन का बाह्य जगत की
वास्तविकता के साथ सीधा सम्बन्ध होता है।
चेतन मन व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक
आदर्शों से भरा होता है।
यह अचेतन
और अर्द्धचेतन पर प्रतिबन्ध का कार्य करता है।
चेतन मन में वर्तमान विचारों एवं
घटनाओं के जीवित स्मृति चिºन होते हैं।
2. अर्द्ध चेतन मन
अर्द्धचेतन का तात्पर्य वैसे मानसिक
स्तर से होता है। जो वास्तव में में न तो पूरी तरह से चेतन हैं और ही पूरी तरह से
अचेतन। इसमें वैसी इच्छाएँ, विचार, भाव आदि होते हैं। जो
हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते हैं परन्तु प्रयास करने पर वे हमारे
चेतन मन में आ जाती है। अर्थात् यह मन का वह भाग है, जिसका सम्बन्ध ऐसी विषय सामग्री से है जिसे व्यक्ति
इच्छानुसार कभी भी याद कर सकता है। इसमें कभी-कभी व्यक्ति को किसी चीज को याद करने
के लिए थोड़ा प्रयास भी करना पड़ता है। जैसे- अलमारी में रखी किताबों में से जब
किसी किताब को ढूँढते हैं और कुछ समय के बाद किताब न मिलने पर परेशान हो जाते हं।ै
फिर कुछ सोचने पर याद आता है कि वह किताब हमने अपने मित्र को दी थी। अर्थात्
अर्द्धचेतन मन चेतन व अचेतन के बीच पुल का काम करता है।
अर्द्ध चेतन मन की विशेषताएँ
मन का वह भाग जो चेतन
से बड़ा व अचेतन से छोटा होता है।
अचेतन से चेतन में जाने
वाले विचार या भाव अर्द्धचेतन से होकर गुजरते हैं।
अर्द्धचेतन में किसी चीज को याद करने
के लिए कभी-कभी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है।
3. अचेतन मन
हमारे कुछ अनुभव
इस तरह के होते हैं जो न तो हमारी चेतना में होते हैं और न ही अर्द्धचेतना
में। ऐसे अनुभव अचेतन होते हैं। अर्थात् यह मन का वह भाग है जिसका सम्बन्ध ऐसी
विषय वस्तु से होता है जिसे व्यक्ति इच्छानुसार याद करके चेतना में लाना चाहे, तो भी नहीं ला सकता है।
अचेतन में रहने वाले विचार एवं
इच्छाओं का स्वरूप कामुक, असामाजिक, अनैतिक तथा घृणित होता
है। ऐसी इच्छाओं को दिन-प्रतिदिन के जीवन में पूरा कर पाना सम्भव नहीं है। अत: इन
इच्छाओं को चेतना से हटाकर अचेतन में दबा दिया जाता है और वहाँ पर ऐसी इच्छाएँ
समाप्त नहीं होती है। बल्कि समय-समय पर ये इच्छाएँ चेतन स्तर पर आने का प्रयास
करती रहती है।
फ्रायड ने इस सिद्धान्त की तुलना
आइसबर्ग से की है। जिसका 9/10 भाग पानी के
अन्दर और 1/10 भाग पानी के बाहर रहता
है। पानी के अन्दर वाला भाग अचेतन तथा पानी के बाहर वाला भाग चेतन होता है तथा जो
भाग पानी के ऊपरी सतह से स्पर्श करता हुआ होता है वह अर्द्धचेतन कहलाता है।
अचेतन मन की विशेषताएँ
अचेतन मन
अर्द्धचेतन व चेतन
से बड़ा होता है।
अचेतन में कामुक, अनैतिक, असामाजिक इच्छाओं की
प्रधानता होती है।
अचेतन का स्वरूप गत्यात्मक
होता है। अर्थात् अचेतन मन में जाने पर इच्छाएँ समाप्त नहीं होती है। बल्कि
सक्रिय होकर ये चेतन में लाटै आना चाहती है। परन्तु चेतन मन के रोक के कारण ये
चेतन में नहीं आ पाती है और रूप बदलकर स्वप्न व दैनिक जीवन की छोटी-मोटी गलतियों
के रूप में व्यक्त होती है और जो अचेतन के रूप को गत्यात्मक बना देती है।
अचेतन के बारे में व्यक्ति पूरी
तरह से अनभिज्ञ रहता है क्योंकि अचेतन का सम्बन्ध वास्तविकता से नहीं होता है।
अचेतन मन का छिपा हुआ भाग होता
है। यह एक बिजली के प्रवाह की भाँति होता है। जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता है
परन्तु इसके प्रभावों के आधार पर इसको समझा जा सकता है।
स्पष्ट है कि अचेतन
अनुभूतियों एवं विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन, अर्द्धचेतन अनुभूतियों एवं विचारों
से अधिक होता है। इसी कारण चेतन व अर्द्धचेतन का आकार चेतन की अपेक्षा बड़ा होता
है।
चेतन, अर्द्धचेतन तथा अचेतन मन का तुलनात्मक अध्ययन-
चेतन मन का वह भाग है जिसका
सम्बन्ध तुरन्त ज्ञान से होता है। अर्द्धचेतन मन का वह भाग है जिसका
सम्बन्ध ऐसी विषय-सामग्री से होता है, जिसे व्यक्ति इच्छानुसार कभी भी याद कर सकता है।
चेतन मन का आकार छोटा अर्द्धचेतन
मन का आकार उससे बड़ा और अचेतन मन का आकार सबसे बड़ा होता है।
चेतन मन में केवल वर्तमान अनुभव
की स्मृतियाँ रहती है। परन्तु अचेतन का सम्बन्ध पिछले अनुभव से होता है और अर्द्धचेतन
में ऐसे अनुभव से होता है जो पिछली अनुभूतियाँ (अनुभव) तो होती है। परन्तु
आवश्यकता पड़ने पर हम उनका प्रत्यावहन कर सकते हैं।
चेतन मन का विषय व्यक्त एवं
स्पष्ट होता है। अचेतन मन में विषय पूरी तरह से दमित होते हैं और अर्द्धचेतन
मन में विषय आंशिक रूप से दमित होते हैं।
मन के गत्यात्मक पक्ष
मन के गत्यात्मक
पक्ष से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न
मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य वैसे जन्मजात और
शारीरिक उत्तेजन से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित
किये जाते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ दो तरह की होती हैं- 1. जीवन मूल प्रवृत्ति 2. मृत्यु मूल प्रवृत्ति।
जीवन मूल
प्रवृत्ति में व्यक्ति सभी तरह के रचनात्मक कार्य करता है और मृत्यु मूल्य
प्रवृत्ति में व्यक्ति सभी तरह के विध्वंसात्मक कार्य करता है। सामान्य व्यक्तित्व
में इन दोनों तरह की मूल प्रवृत्तियों में सन्तुलन पाया जाता है और जब इन परस्पर
विरोधी मूल प्रवृत्तियों में संघर्ष होता है तो व्यक्ति उनका समाधान करने की कोशिश
करता है। इस तरह के समाधान के लिए मुख्य रूप से तीन प्रवृत्तियों का वर्णन किया
गया है- 1. उपाहं, 2. अहम्, 3. नैतिक मन।
1. उपाहं-
जन्म के समय शरीर
की संरचना में जो कुछ भी निहित होता है वह पूर्णत: उपाहं होता है। अर्थात्
जन्मजात और वंशानुगत है। तात्कालिक सन्तुष्टि की इच्छाएँ और विचार ही उपाहं की
प्रमुख विषय सामग्री है। वातावरण की वास्तविकता से उपाहं का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं
होता है। इसका नैतिक, तार्किकता, समय, स्थान और मूल्यों आदि से
कोई सम्बन्ध नहीं होता है।
उपाहं के कार्य- इसका मुख्य कार्य
शारीरिक इच्छाओं की सन्तुष्टि से है। यह किसी भी प्रकार के तनाव से तुरन्त छुटकारा
पाना चाहता है। तुरन्त तनाव को दूर करना ही सुखवाद नियम कहा गया है। दूसरे शब्दों
में उपाहं अपने उद्देश्यों की पूर्ति सुखवाद नियम के आधार पर करता है। सुख की
प्राप्ति और दु:ख को दूर करने के लिए उपाहं के दो मुख्य कार्य हैं-
1.सहज क्रियाएँ- ये जन्मजात और स्वयं
चलने वाली होती है। जैसे पलक झपकना, छींकना आदि। सभी व्यक्ति इन क्रियाओं को करने के बाद संतोष
का अनुभव करते हैं।
2.प्राथमिक
क्रियाएँ- तनाव को दूर
करने के लिए प्राथमिक क्रियाएँ व्यक्ति के सामने उस वस्तु की प्रतिभा बनाती है।
जैसे- एक प्यासे व्यक्ति के सामने पानी की प्रतिमा प्रस्तुत कर उसकी प्यास की सन्तुष्टि
करना। यहाँ पानी की प्रतिमा उपस्थित करना एक प्राथमिक प्रक्रिया का कार्य है।
2. अहम्-
यह मन के गत्यात्मक
पहलू का दूसरा भाग है। यह जन्म के समय बच्चे में मौजूद नहीं होता है बल्कि बाद में
विकसित होता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ-साथ वह वातावरण की वास्तविकता की ओर
बढ़ने लगता है। आयु बढ़ने के साथ-साथ वह ‘मेरा’ और ‘मुझे’ जैसे शब्दों का अर्थ
समझने लगता है। धीरे-धीरे वह समझने लगता है कि कौन सी वस्तु उसकी है और कौन सी
वस्तु दूसरों की। यह उपाहं का एक मुख्य भाग है। जो वाºय वातावरण के प्रभाव के
कारण विकसित होता है।
अहम् के कार्य- अहम का मुख्य कार्य वाºय वातावरण के खतरों से
जीवन की रक्षा करना है। यह अपने लक्ष्य को वास्तविकता के नियम के आधार पर पूरा
करता है। यह सुखवादी नियम का विरोधी नहीं है बल्कि उपयुक्त परिस्थिति के आते ही
तात्कालिक सन्तुष्टि में सहायता करता है क्योंकि यह व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष
है। अत: तुरन्त सन्तुष्टि के लिए उपयुक्त परिस्थिति को खोजने या उत्पन्न करने का
कार्य भी करता है। अहम् को व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला माना गया है। यह थोड़ा
चेतन, थोड़ा अर्द्धचेतन और
थोड़ा अचेतन होता है। इसके द्वारा इन तीनों स्तरों पर निर्णय लिया जाता है।
3. नैतिक मन-
यह मन के गत्यात्मक
पक्ष का सबसे अन्तिम भाग है और यह व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है। जैसे-जैसे बच्चा
बड़ा होता जाता है, वह अपना
तादात्म्य माता-पिता के साथ स्थापित करने लगता है और बच्चा यह सीख लेता है कि क्या
उचित है और क्या अनुचित है, क्या नैतिक है और
क्या अनैतिक। इस तरह सीखने से नैतिक मन की शुरूआत होती है।
यह आदर्शवादी
सिद्धान्त द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होता है। बचपन में सामाजीकरण के दौरान
बच्चा, माता-पिता द्वारा दिये
गये उपदेशों को अपने अहम्ं में संजोए रखता है और यही बाद में नैतिक मन
का रूप ले लेता है। यहाँ विकसित होकर एक ओर उपाहं की कामुक, आक्रामक एवं अनैतिक प्रवृत्तियों
पर रोक लगाता है तो दूसरी ओर अहं को वास्तविक एवं यथार्थ लक्ष्यों से हटाकर नैतिक
लक्ष्यों की ओर ले जाता है। नैतिक मन व्यक्ति के कामुक एवं आक्रामक प्रवृत्तियों
पर नियंत्रण दमन के माध्यम से करता है। जबकि नैतिक मन दमन का प्रयोग स्वयं नहीं
करता है बल्कि वह अहम् को दमन के प्रयोग का आदेश देकर ऐसी इच्छाओं पर नियंत्रण
करता है और यदि अहम्ं इस आदेश का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति में अनेक दोष-भाव
उत्पन्न हो जाते हैं।
नैतिक मन के
कार्य- यह सामाजिकता
तथा नैतिकता का कार्य करता है। यह अहम्ं के उन सभी कार्यों पर रोक लगाता है
जो सामाजिक और नैतिक नहीं है। नैतिक मन का अहमं के प्रति कार्य और व्यवहार
वैसा ही होता है जैसा एक बच्चे के प्रति माता-पिता का व्यवहार होता है। अत: नैतिक
मन के मुख्य कार्य है-
1. उपाहं
के अनैतिक, असामाजिक और कामुक
संवेगों पर रोक लगाना।
2. अहम् के
आवेगों को नैतिक और सामाजिक लक्ष्यों की ओर ले जाने की कोशिश करना।
3. पूर्ण सामाजिक
और आदर्श प्राणी बनाने के लिए प्राणी बनाने के लिए प्रयास करना।
उपाहं, अहम्ं और नैतिक मन में
सम्बन्ध-
उपाहं, अहम् और नैतिक मन
तीनों का ही सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व से है और ये तीनों इकाइयाँ गतिशील हैं।
उपाहं आनन्द (सुख) सिद्धान्त, अहम्ं वास्तविकता सिद्धान्त और नैतिक मन आदर्शवादी
सिद्धान्त से नियंत्रित होता है। सामान्य व्यक्तित्व में इन तीनों ही अंगों में
पर्याप्त मात्रा में मेल पाया जाता है। इन तीनों इकाइयों में जितनी ही खींचातानी
होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व
उतना ही अधिक असामाजिक हो जाता है और उसके व्यक्तित्व का विघटन उतना ही अधिक होता
है। जबकि सामान्य व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि इन तीनों में आपस में समायोजन
बना रहे। जब इन तीनों में कोई एक या दो इकाई अधिक प्रभावशील हो जाती है तो इनमें
आपस में समायोजन बिगड़ जाता है। अहम्ं व्यक्तित्व का केन्द्र होता है। यह उपाहं, नैतिक मन और वातावरण की
वास्तविकताओं के बीच समायोजन बनाकर व्यवहार करता है। इसे हम निम्न तरह से समझ सकते
हैं-
नैतिक मन
↓
पर्यावरण की वास्तविकताएँ
→ अहम ← सक्रियता या व्यवहार
↑
उपाहं
उपाहं, नैतिक मन और वातावरण की
वास्तविकताओं के मध्य अहम्ं जितना ही अधिक समायोजन करने में सक्षम होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व
उतना अधिक स्थायी होगा। उपाहं और नैतिक मन को हम इस उदाहरण द्वारा
समझ सकते हैं- एक सुनसान सड़क पर एक युवती को देखकर युवक के मन में विचार आता है
कि मैं इसे छेड़ू। इस प्रकार का विचार उपाहं है। फिर उसके मन में विचार आता
है कि यहाँ छेड़ना ठीक नहीं है। यहाँ किसी ने देख लिया तो पिटाई हो जायेगी, थोड़ी दूर आगे जहाँ इसे
कोई नहीं देखेगा वहाँ छेड़ना अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार का विचार अहमं
है। फिर उस युवक के मन में विचार आता है कि नहीं? इसे छेड़ना अच्छी बात नहीं है। यह युवती किसी की बेटी होगी
या किसी की बहन होगी। समाज में इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। इस
प्रकार का विचार नैतिक मन है।
जब व्यक्ति में उपाहं
की इच्छा तीव्र होती है तो व्यक्ति सुखवादी, स्वार्थवादी और अनियंत्रित होता है और जब व्यक्ति में अहमं
की इच्छा प्रबल होती है तो उसमें मैं की अधिकता होती है। जिस व्यक्ति में नैतिक
मन तीव्र होता है वह व्यक्ति आदर्शवादी होता है। उसमें भले-बुरे का विचार अधिक
होता है।
उपाहं, अहम्ं और नैतिक मन के बीच समानताएँ एवं विभिन्नताए
फ्रायड के अनुसार एक
स्वस्थ-सामान्य व्यक्ति में तीनों ही काफी समन्वित ढंग से कार्य करते हैं तथा
इसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। इन तीनों में कुछ समानताएँ और
भिन्नताएँ भी पायी जाती हैं जो इस प्रकार हैं-
समानताएँ
1. उपाहं, अहम्ं, नैतिक मन तीनों ही मन के
गत्यात्मक पहलू के काल्पनिक भाग है। जिन्हें अन्य वस्तुओं की भाँति दिखाया
नहीं जा सकता है।
2. किसी भी
मानसिक संघर्ष में तीनों शामिल रहते हैं। अन्तर सिर्फ मात्रा का होता है।
विभिन्नताएँ
1. उपाहं बच्चों
में जन्म से ही मौजूद रहता है। एक वर्ष के बाद बच्चों में अहं का विकास होता है और
जब बच्चा तीन-चार वर्ष का हो जाता है तब वह अपने माता-पिता के साथ सम्बन्ध
(तादात्म्य) स्थापित कर लेता है तथा उनके द्वारा कही गयी बातों को ग्रहण करने लगता
है। फलत: बच्चे में नैतिक मन का विकास होने लगता है।
2. उपाहं आनन्द
सिद्धान्त (सुखवादी), अहम्ं वास्तविकता
सिद्धान्त तथा नैतिक मन आदर्शवादी सिद्धान्त से नियंत्रित होता है।
3. उपाहं तथा
पराहं को वाºय वातावरण की वास्तविकता
से कोई मतलब नहीं होता है जबकि अहम्ं का बाह्य वातावरण की वास्तविकता से सीधा
सम्बन्ध होता है।
4. उपाहं पूरी
तरह से अचेतन होता है जबकि अहम्ं और नैतिक मन दोनों ही थोड़ा चेतन, थोड़ा अर्द्धचेतन और
थोड़ा अचेतन होते हैं।
5. अहमं एक
समायोजक के रूप में कार्य करता है जबकि उपाहं और नैतिक मन की प्रवृत्ति परस्पर
विरोधी होती है।
6. उपाहं पूरी तरह से अनैतिक होता है जबकि नैतिक मन पूरी तरह से नैतिक होता है।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।




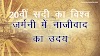










0 Comments