पुनर्जागरण का अर्थ
विश्व-इतिहास में पुनर्जागरण का
अत्यधिक महत्त्व है। यूरोप में 15वीं शताब्दी में एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी जिसके फलस्वरूप
मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, मध्य युग में प्रचलित
अन्धविश्वास दूर हुए एवं साहित्य, कला तथा विज्ञान
के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। इस महत्त्वपूर्ण घटना को पुनर्जागरण
के नाम से पुकारा जाता है।
चौदहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक यूरोप में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक उन्नति हुई, उसे 'पुनर्जागरण' के नाम से पुकारा जाता है। रोमन साम्राज्य के समय यूरोप ने सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की परन्तु रोमन साम्राज्य के पतन के साथ-साथ यूरोप की संस्कृति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस समय लोग प्राचीन यूनानी तथा रोमन संस्कृति को भूलकर अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों के शिकार बन गये। लोगों में स्वतंत्र चिंतन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था। चर्च तथा धर्म का मानव समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था। चर्च का विरोध करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाता था।
परन्तु मध्य युग
के अन्त में यूरोप में एक बौद्धिक क्रांति हुई। अब
यूरोपवासियों ने स्वतंत्र रूप से चिंतन करना शुरू किया। उनमें प्राचीन यूनान तथा
रोम के साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। अब लोग प्रचलित विश्वासों और प्रथाओं
को तर्क की कसौटी पर कसने लगे जिसके फलस्वरूप उनमें प्रचलित अंधविश्वासों के प्रति
अरुचि उत्पन्न हुई। साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों
में अत्यधिक उन्नति हुई। इस प्रकार यूरोप की सभ्यता और संस्कृति का गौरव चरम सीमा
पर जा पहुंचा। इस प्रकार प्राचीन संस्कृति की उन्नति एवं परिवर्तन को ही पुनर्जागरण
या बौद्धिक चेतना कहा जा सकता है।
 |
| पुनर्जागरण |
पं. जवाहरलाल
नेहरू का कथन है कि, “पुनर्जागरण का अर्थ विद्या का
पुनर्जन्म तथा कला, विज्ञान और
साहित्य तथा यूरोपीय भाषाओं का विकास है।"
इतिहासकार
स्वेन का कथन है कि, “पुनर्जागरण से
ऐसे सामूहिक शब्द का बोध होता है जिसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के
प्रारम्भ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश होता है।"
प्रो. ल्यूकस का कथन है कि, "चौदहवीं से
सत्रहवीं शताब्दी के बीच में यूरोप में होने वाले महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक
परिवर्तनों को 'पुनर्जागरण' कहते हैं।"
इतिहासकार
डेविस के अनुसार, "पुनर्जागरण
शब्द मानव के स्वातन्त्र्य प्रिय, साहसी विचारों को
जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बन्दी बना दिये गये थे, व्यक्त करता है।"
सीमोण्ड के अनुसार, "पुनर्जागरण
एक ऐसा आन्दोलन है, जिसके फलस्वरूप
पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकल कर वर्तमान युग के विचार तथा जीवन की
पद्धतियों को ग्रहण करने लगे हैं।"
फिशर का कथन है कि, "सर्वप्रथम इटली ने
नगरों में प्राचीन यूनानी एवं रोमन कला, साहित्य का पुनः सृजन, मानववादी आन्दोलन का प्रारम्भ, स्थापत्य कला एवं चित्रकला
का नया स्वरूप,
व्यक्तित्व एवं
व्यक्तिवादी सिद्धान्तों का विकास, नवीन दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक आलोचना, छापेखाने का आविष्कार, दर्शन शास्त्र एवं धर्मशास्त्र
का नया स्वरूप तथा विवेचन इत्यादि तत्त्वों तथा विशेषताओं को सामूहिक रूप से 'पुनर्जागरण' कहते हैं।"
एलिस और जौन के अनुसार, "पुनर्जागरण
ने मनुष्य के क्षितिज का विस्तार किया। यूरोप में पुनर्जागरण युग, मध्य युग और आधुनिक युग
के बीच पुल की तरह है। पुनर्जागरणकालीन लोगों ने मध्यकालीन यूरोप की संस्कृति
के आधार पर एक नई संस्कृति का विकास किया जिसमें उन्होंने यूनानी और रोमन
सभ्यताओं से प्राप्त प्रेरणाओं और विचारों का योगदान लिया है।"
पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएँ
1. स्वतन्त्र
चिंतन को प्रोत्साहन- पुनर्जागरण ने स्वतन्त्र चिन्तन की विचारधारा को
प्रोत्साहन दिया। अब मनुष्य परम्परागत विचारों और मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर कसने
लगा। अब मनुष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ।
2. व्यक्तित्व का
विकास- पुनर्जागरण के
परिणामस्वरूप मनुष्य को प्राचीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं धार्मिक पाखण्डों से मुक्ति मिली। इसके
फलस्वरूप मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ।
3. मानववादी
विचारधारा का विकास- पुनर्जागरण ने मानववादी विचारधारा का प्रसार किया। अब मनुष्य को यह प्रेरणा
मिली कि उसे परलोक की चिन्ता छोड़कर इस जीवन को आनन्द से बिताना चाहिये। धर्म एवं
मोक्ष के स्थान पर मानव-जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाना चाहिये।
4. देशी भाषाओं का
विकास- पुनर्जागरण के
परिणामस्वरूप देशी भाषाओं का अत्यधिक विकास हुआ। अब जन-साधारण की भाषाओं में
ग्रन्थ लिखे गए जिसके फलस्वरूप देशी भाषाओं का बहुत अधिक विकास हुआ।
5. चित्रकला के
क्षेत्र में उन्नति- पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप चित्रकला के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई।
6. वैज्ञानिक
विचारधारा का विकास- पुनर्जागरण के कारण वैज्ञानिक विचारधारा का भी विकास हुआ। अब सभी विषयों को
तर्क एवं विज्ञान की कसौटी पर कसा जाने लगा।
पुनर्जागरण के कारण
पुनर्जागरण के
प्रमुख कारण निम्नलिखित थे-
1. धर्म-युद्ध-
मुसलमानों के
चंगुल से अपने पवित्र स्थान जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईसाइयों तथा
मुसलमानों में दीर्घकाल तक युद्ध लड़े गये, जिन्हें धर्म-युद्ध कहा जाता है। इन धर्म-युद्धों के
कारण यूरोपवासियों को पूर्वी देशों की तर्क-शक्ति, प्रयोग पद्धति तथा वैज्ञानिक खोजों की पर्याप्त जानकारी
प्राप्त हुई। उन्हें प्राचीन यूनानी तथा रोमन विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने का अवसर
मिला। जिससे उन लोगों के ज्ञान-विज्ञान में वृद्धि हुई। धर्म-युद्धों के कारण
यूरोप के पूर्वी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए। यूरोप के अनेक साहसी लोगों
ने पूर्वी देशों की यात्राएँ की तथा अपनी यात्राओं के विवरण लिखे, जिन्हें पढ़ने से
यूरोपवासियों के संकीर्ण विचार समाप्त हुए तथा उनके ज्ञान-विज्ञान में वृद्धि हुई।
इन धर्म-युद्धों में ईसाइयों की पराजय हुई जिससे पोप की शक्ति तथा
प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुँचा। अब धर्म के बंधन ढीले पड़ गए और चर्च के प्रभाव
में कमी हुई।
2. पूर्व से सम्पर्क-
पूर्वी देशों के
सम्पर्क में आने से यूरोपवासी अत्यधिक प्रभावित हुए। अरब लोग
स्वतन्त्र रूप से चिंतन करते थे। उन्हें अरस्तू, प्लेटो आदि की पुस्तकों का भी
ज्ञान था। इस प्रकार अरब लोगों ने यूर पियनों का ध्यान यूनानी दर्शन, ज्ञान-विज्ञान आदि की ओर
आकर्षित किया । यूरोपियन लोगों ने अरबों तथा चीन से कुतुबनुमा, बारूद, कागज, छापेखाने आदि की जानकारी
प्राप्त की। इस प्रकार पूर्वी देशों के सम्पर्क में आने से यूरोपवासियों में
स्वतन्त्र चिंतन,
वैज्ञानिक
दृष्टिकोण आदि की भावनाएँ उत्पन्न हुईं।
3. मंगोलों का
योगदान-
13वीं शताब्दी में मंगोल
नेता कुबलई खाँ ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य थापित किया। कुबलई
खाँ ने अपने दरबार में अनेक विद्वानों, साहित्यकारों, धर्म प्रचारकों, राजदूतों आदि को संरक्षण दे रखा था। इटली का
प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो भी उसके दरबार में पहुंचा था। चीन से लौटकर
उसने अपनी यात्रा का रोचक वर्णन लिखा। इस वर्णन से यूरोपवासियों को नये-नये देशों
की खोज करने तथा अपनी संस्कृति को विकसित करने की प्रेरणा मिली। प्रसिद्ध यात्री कोलम्बस
भी कुबलई खाँ के दरबार में पहुंचा। उसने कुबलई खाँ से
प्रभावित होकर समुद्री यात्रा के लिए प्रस्थान किया। अरबों तथा मंगोलों के सम्पर्क
से यूरोपवासियों को छापाखाना, कुतुबनुमा, बारूद, कागज आदि की जानकारी हुई।
इन चीजों की जानकारी ने यूरोपवासियों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला
दिया।
4. नगरों का विकास-
व्यापार के विकास के कारण यूरोप
में नगरों का विकास हुआ। व्यापारी लोग नगरों में रहने लगे। नगरों के विकास के कारण
व्यापारी लोग धनवान बनते चले गये। इन्होंने अपने रहने के निवास स्थानों को सुन्दर
चित्रों एवं मूर्तियों से सुसज्जित करवाया। नगरों के निवासी स्वतन्त्र वातावरण को
पसन्द करते थे तथा कठोर नियमों के बन्धनों में बँधने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग
मध्ययुगीन रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इन
लोगों की प्राचीन यूनानी तथा रोमन साहित्य एवं कला में रुचि थी। अतः नगरों के
विकास के कारण स्वतन्त्र चिंतन की प्रवृत्ति का विकास हुआ तथा लोगों में प्राचीन
यूनानी एवं रोमन साहित्य तथा कला के प्रति रुचि भी बढ़ी। इससे पुनर्जागरण
को प्रोत्साहन मिला।
5. व्यापार का विकास-
धर्म-युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी
देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए। इससे व्यापार की अत्यधिक उन्नति हुई।
उस समय वेनिस, मिलान, फ्लोरेन्स आदि व्यापार के प्रसिद्ध
केन्द्र बन गए। इस व्यापारिक सम्पर्क से यूरोपवासियों के ज्ञान में वृद्धि हुई।
व्यापारिक विकास के कारण अनेक नगरों का उदय एवं विकास भी हुआ। नगरों का वातावरण
स्वतन्त्रता का था जिससे व्यापारियों में स्वतन्त्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न
हुई। इसके अतिरिक्त धन की प्रचुरता के कारण व्यापारियों को अध्ययन करने का अवसर
मिला। धनी व्यापारियों को बगदाद, काहिरा आदि से
खरीदी हुई पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला। जिससे उनके ज्ञान-विज्ञान में वृद्धि हुई।
व्यापारी लोग साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, विद्वानों, कलाकारों आदि को
उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देने लगे। इसके फलस्वरूप साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों
में महत्त्वपूर्ण उन्नति हुई।
6. सामन्तों की
शक्ति का क्षीण होना-
मध्य युग में सामन्तों का अत्यधिक
प्रभाव था। सामन्त अपने क्षेत्रों में शासकों की भाँति शासन करते थे। वे सामान्य
जनता से अनेक प्रकार के कर वसूल करते थे। ये लोग युद्धों एवं लूटमार में भी लिप्त
रहते थे। सामन्तों के कारण गृह-कलह, अशांति एवं अराजकता व्याप्त थी। सामन्त और चर्च के
धर्माधिकारी दोनों जनता का शोषण करते थे। परन्तु 14वीं शताब्दी के अन्त तक सामन्तों की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो
चुकी थी। सामन्तवाद के पतन के कारण यूरोप में सुदृढ़ एवं राष्ट्रीय राज्यों
की स्थापना हुई तथा अंशाति एवं अराजकता का वातावरण समाप्त हुआ। अब जनता के लिए
स्वतन्त्र रूप से चिंतन करना सुगम हो गया। परिणामस्वरूप साहित्य, कला, विज्ञान आदि की उन्नति के
लिए अनुकूल वातावरण बन गया।
7. शिक्षा का विकास-
मध्य युग के अन्त में शिक्षा
की काफी उन्नति हुई। यूरोप के प्रमुख नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना
हुई। इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी किसी भी विषय का अध्ययन कर सकते थे, क्योंकि ये धार्मिक
नियंत्रण से मुक्त थे। शिक्षा के विकास के कारण मनुष्य में स्वतन्त्र चिंतन, तार्किक दृष्टिकोण और
वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। अब उसे धार्मिक पाखण्डों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों
में कोई रुचि नहीं रही तथा वह प्रत्येक विषय पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने लगा।
8. भौगोलिक खोजें-
भौगोलिक खोजों ने भी पुनर्जागरण
के विकास में योगदान दिया। मार्कोपोलो, कोलम्बस, वास्कोडिगामा आदि साहसी यात्रियों ने
भारत, चीन एवं अरब देशों के
जल-मार्गों की खोज की। भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपीय व्यापार की उन्नति हुई। अब
यूरोपवासी अपने व्यापार एवं धर्म प्रचार के लिए विश्व के विभिन्न भागों में
पहुंचने लगे। जब ये लोग दूसरे देशों की सभ्यता के सम्पर्क में आए तो उनके ज्ञान
में वृद्धि और उनकी चिंतन शक्ति का विकास हुआ। अब उनकी संकीर्णता समाप्त होने लगी
और उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। उनकी वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन के ढंग
में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने पुनर्जागरण के लिए अनुकूल वातावरण
तैयार कर दिया।
9. कागज तथा
छापाखाना-
कागज एवं छापेखाने के
आविष्कार ने भी पुनर्जागरण के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। कागज और
छापेखाने का आविष्कार चीन ने किया। यूरोपवासियों को कागज और छापेखाने की जानकारी
अरबों से प्राप्त हुई। 1450 में छापेखाने
का आविष्कार जर्मनवासी गुटनबर्ग ने किया था। शीघ्र ही यूरोप के
प्रमुख नगरों में छापेखाने की स्थापना हो गई। छापेखाने के आविष्कार के कारण
पुस्तकें सस्ते मूल्यों पर मिलने लगीं। अब साधारण व्यक्ति भी पुस्तकें खरीद सकता
था तथा पढ़ सकता था। पुस्तकों, समाचार पत्रों
आदि के माध्यम से लोग बड़े लाभान्वित हुए। उनके अंधविश्वास धीरे-धीरे कम होने लगे
और उनमें स्वतन्त्र चिंतन की प्रवृत्ति विकसित हुई।
10. विज्ञान के
क्षेत्र में उन्नति-
मध्ययुग के उत्तरार्द्ध में विज्ञान
के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोजर बैकन
ने तर्क और प्रयोग पर बल दिया। उसका कहना था कि जो बात तर्क और विज्ञान की कसौटी
पर खरी उतरे, केवल उसे ही स्वीकार करना
चाहिये । कोपर निकस, बूनो, गैलीलियो आदि प्रसिद्ध
वैज्ञानिकों ने ज्योतिष एवं खगोल के क्षेत्र में अनेक नवीन आविष्कार कर प्राचीन
मान्यताओं का खण्डन किया। इन वैज्ञानिक खोजों के कारण मनुष्य में वैज्ञानिक
दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और उसका विश्वास प्राचीन रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से हटने
लगा। अब यूरोपवासियों की तर्क, विज्ञान और
प्रयोग में रुचि बढ़ने लगी।
11. मानववाद का
प्रचार-
मानववाद का शाब्दिक अर्थ है-'उन्नत ज्ञान' । मानववादी स्वतन्त्र
विचारों के व्यक्ति थे। उनका धर्म की संकुचित विचारधारा में विश्वास नहीं था। वे
यूनानी तथा रोमन साहित्य से प्रभावित थे। वे परलोक की अपेक्षा इस जीवन की अधिक
चिन्ता करते थे। वे वर्तमान जीवन को सुखी और आनन्ददायक बनाने पर जोर देते थे। उनका
कहना था कि मनुष्य को परलोक की चिन्ता छोड़कर इस जीवन को आनन्द के साथ व्यतीत करना
चाहिये। वे सत्य,
तर्क और स्वतंत्र
चिंतन का प्रचार करते थे। मानववाद के प्रसार के कारण लोगों की धर्म
शास्त्रों में रुचि कम हो गई, उनके अंधविश्वास
दूर होने लगे और उनमें स्वतन्त्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। अब लोगों में
प्राचीन यूनानी एवं रोमन साहित्य के अध्ययन में रुचि उत्पन्न हुई।
12. स्कालिस्टिक
विचारधारा-
मध्ययुग में स्कालिस्टिक
विचारधारा का प्रचार हुआ जिसने पुनर्जागरण के विकास में महत्त्वपूर्ण
योगदान दिया। इस विचारधारा का आधार अरस्तू का तर्कशास्त्र तथा सन्त
आगस्टाइन का तत्त्व ज्ञान था। इसमें तर्क तथा धर्म दोनों का समन्वय था।
इससे विद्याध्ययन तथा वाद-विवाद को प्रोत्साहन मिला। परन्तु प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोजर
बैकन ने इस विचाराधारा का विरोध किया तथा वैज्ञानिक प्रयोगों पर बल दिया।
13. कुस्तुन्तुनिया
पर तुर्कों का अधिकार-
1453
ई. में उस्मानी
तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया नगर पर अधिकार कर लिया। कुस्तुन्तुनिया
यूनानी, ज्ञान, दर्शन एवं कला का
प्रसिद्ध केन्द्र था। कुस्तुन्तुनिया के पतन के पश्चात् यहाँ रहने वाले
अनेक यूनानी विद्वान अपने ग्रन्थों के साथ इटली में शरण लेने के लिए पहुंचे। वहाँ
उन्होंने प्राचीन यूनानी एवं रोमन साहित्य दर्शन आदि का प्रचार किया। यूरोपवासी
प्राचीन यूनानी एवं रोमन साहित्य एवं दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्हें नवीन
वैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण मिला। रोम ने ही यूरोप में प्राचीन ज्ञान का
प्रकाश फैलाया था। यही कारण था कि पुनर्जागरण इटली में ही सर्वप्रथम शुरू हुआ और
धीरे-धीरे इसका प्रभाव समस्त यूरोप पर दिखाई देने लगा।
कुस्तुन्तुनिया पर तुर्कों की विजय का
एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे यूरोपवासियों को नये देशों तथा मार्गों की
खोज करने की प्रेरणा मिली। अब यूरोपवासी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए
नये जल मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े इसी संदर्भ में कोलम्बस ने अमेरिका
की तथा वास्कोडिगामा ने भारत के जल मार्गों की खोज की। इससे भी पुनर्जागरण
को प्रोत्साहन मिला।
आशा हैं कि हमारे
द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो
इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।




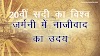









0 Comments