वैदिक सभ्यता (1500-600 ई.पू.)
सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilization) के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य (Aryan) अथवा वैदिक सभ्यता (Vedic Civilization) के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमे मुख्यत: वेदों से प्राप्त होती है, जिसमे ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल (1500-1000 ई.पू.) तथा उत्तर वैदिक काल (1000-600 ई.पू.) में बांटा गया है।
वेदों से प्राप्त समाज एवं
उनकी आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक
जीवन को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते है। प्रथम ऋग्वैदिक संस्कृति
का भाग है प्रारम्भिक वैदिक संस्कृति, जिसकों जानने का स्त्रोत ऋग्वेद है जो कि आर्यो का
प्राचीनतम ग्रंथ है। उतर वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि से होता है।
वेदों में इसके संस्थापकों को आर्य कहा गया है। वैदिक सभ्यता का
आरम्भ आर्यों के आगमन के साथ होता है।
आर्य कौन थे?
आर्य जाति द्वितीय सहस्राब्दी ईसा
पूर्व के मध्य में भारत में एक नवीन जाति या कबीले का
अस्तित्व मिलता है। कुछ विद्वान इन्हें आक्रमणकारी मानते हैं और बाहर से
आया बताते हैं। ए. एल. बाशम तथा कुछ अन्य विद्वानों का विचार है कि ये आक्रामक
थे और अपने को आर्य कहते थे। अंग्रेजी भाषा में आर्य शब्द का सामान्य अर्थ
आर्यन्स (Aryans) है, बाशम के अनुसार फारस के
प्राचीन निवासी भी इस नाम का प्रयोग करते थे और वर्तमान ईरान शब्द में तो यह शब्द
अब भी विद्यमान है।
'आर्य' शब्द संस्कृत भाषा
का है जिसका अर्थ है 'उच्च', 'उत्तम' अथवा 'श्रेष्ठ। व्यापक अर्थ में आर्य
को मनुष्य की उस जाति को कहते हैं जिसकी शरीर रचना, रंग रूप तथा प्राकृति एक
विशेष प्रकार की होती है। जैसे गोरा रंग, लम्बी नाक, ऊंचा माथा, हृष्ट-पुष्ट, लम्बे शरीर वाला इत्यादि।
वेदों में आर्य उसे कहा गया है जो ऊपर लिखे विवरण वाला तो हो तथा
इन्द्र, वरूण मित्र आदि की पूजा
करने वाला हो।
सम्भवतः अपनी उच्च जातीयता, उच्चतम कर्म और श्रेष्ठता प्रदर्षित करने हेतु इस जाति ने
अपने को 'आर्य' नाम से विभूषित किया।
अपनी विरोधी जाति को उन्होंने 'अनार्य', 'दस्यु' अथवा 'दास' कहकर सम्बोधित किया जिसकी
पुष्टि ऋग्वेद में दिए गए ‘अकर्मन’, ‘अब्रह्मन्', 'अव्रत', 'अदेवयु' जैसे शब्दों से होती है।
अपनी शारीरिक रचना तथा मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से वशीभूत होकर ही वे अनार्यों से
अपने को श्रेष्ठ समझते थे। उनके आचार-विचार विकसित और उन्नत थे। ऐसा लगता
है कि उनके भारत आगमन से पूर्व उन्हें उत्तर भारत में द्रविड़ों से संघर्ष
करना पड़ा। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप के अनेक ऋग्वैदिक वर्णन संघर्षों की
पुष्टि भी करते हैं। द्रविड़ पराजित होने के पश्चात दक्षिण की ओर चले गए। इस तरह
द्रविड़ सभ्यता तथा सिन्धु घाटी के ध्वासावशेषों पर आर्य सभ्यता ने पनपना शुरू कर
दिया। बाद में इन आर्यों का भारतीयकरण हो गया और उन्हें भारतीय आर्य की
संज्ञा प्राप्त हो गई।
आर्यो का आदि देश
सर्वप्रथम हमें
यह जान लेना आवश्यक है कि क्या आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या कहीं
दूसरे देश से प्रस्थान कर भारत में बस गए थे। इस विवाद की शुरूआत तब हुई जब कलोरेंस
के एक व्यापारी ने, जो कि गोआ में 5
वर्ष तक निवास कर (1583-88), वापिस जाते समय
यह खोज कर सका कि संस्कृत तथा यूरोप की महत्वपूर्ण भाषाओं में कोई सम्बन्ध है।
1786 ई. में सर विलियम जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
में सुझाव दिया कि संस्कृत तथा यूरोप की महत्वपूर्ण भाषाओं में
संबंध का कारण है कि इन भाषाओं को बोलने वाले कभी एक समय में इक्ट्ठे रहे होंगे।
उन्होंने ग्रीक,
लैटिन, गोथिक, सेल्टिक, संस्कृत पर्शियन आदि
भाषाओं का उद्गम केन्द्र एक ही माना तथा इन भाषाओं को इण्ड्रों यूरोपीयन
नाम दिया।
आर्यों के मूल देश के
बारे में विभिन्न के मत है। कुछ विद्वान आर्यों को भारत का मूल निवासी
मानते हैं तो कुछ इन्हें विदेशी मानते हैं जो मूलतः दूसरे देश से आकर भारत
में बस गए। अविनाश चन्द्र दास आर्यों को सप्त सैन्धव प्रदेश, महामहोप्याय गंगावाभ का
इन्हें ब्रह्मर्षि देश, राजबली पांडे के
विचारों अनुसार मध्य प्रदेश, श्री एल. डी.
कब्ला आर्यो को कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, श्री डी एस त्रिवेदी के मतानुसार देविका प्रदेश आदि का
मूलनिवासी मानते हैं।
गाइलण महोदय के मतानुसार आर्यो
का मूल निवास स्थान हंगरी, श्री बालगंगाधर तिलक आर्यो का आदि देश उत्तरी
ध्रुव मानते हैं। पेंका नामक विद्वान के विचारों से इनका मूल निवास जर्मनी
है, डॉ. मच के अनुसार पश्चिमी
बल्टिक क्षेत्र, नेहरिंग के अनुसार रूस
आर्यो का मूल निवास स्थान मानते हैं। परन्तु अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्य
मध्य एशिया से भारत आए है। क्योंकि इसी क्षेत्र से हमें आर्यो के देवताओं इन्द्र, वरूण, मित्र तथा नस्त्य इत्यादि
के प्रमाण एलअमरणा तथा बोगाजकोई नामक स्थलों से मिलते हैं। इसके
अलावा आर्यों के अधिकतर धार्मिक कर्मकाण्डों के प्रमाण भी इसी जगह से मिलते है।
जैसे मृतकों का दाहसंस्कार, अश्व केन्द्रित अल्पतंत्र, अग्नि पूजा, रथगाड़ी, छोडों का प्रथम प्रयोग
इत्यादि का प्रमाण मध्य एशिया के स्थलों पर देखने को मिलता है। गांधार
श्वाधान संस्कृति के घूसर मृदभांडों पर आर्य मृदभांडों की छाप मिलती
है।
आर्यों के आदि
देश से संबंधित विभिन्न विचार
आर्यो के आदि
देश के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। इन के आदि देश के बारे में
कई सिद्धान्त तथा मत है। इनमें प्रमुख हैं- भारतीय मूल का मत, दूसरा यूरोप मूल
तीसरा, मध्य एशिया का
सिद्धान्त। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश को आर्यो का
आदि देश माना है। तिब्बत के पामीर क्षेत्र को भी कतिपय विद्वान आर्यो का
आदि देश मानते है। इन विचारो में प्रमुख निम्नलिखित है-
आर्यो का आदि देश यूरोप-
यूरोप को आर्यो का आदि देश
मानने वाले विद्वानों के तर्क दो आधारों पर निर्भर हैं-
(1) आज भी
इन्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार के शब्द और मुहावरे जितने यूरोप की भाषाओं में विद्यमान
हैं उतनी एशिया की भाषाओं में नहीं। इनसे अनुमान यही होता है कि कदाचित् यूरोप का
ही देश आर्यो का आदि-देश था, एशिया का नहीं।
(2) यूरोप की
लिथ्यूनियन भाषा ही समस्त इन्डो-यूरोपीयन भाषा-परिवार अत्यधिक अपरिष्कृत है और
इसलिए अत्यधिक प्राचीन लगती है। अतः लिथ्यूनिया अथवा उसके समीप का कोई यूरोपीय देश
आर्यो का आदि देश रहा होगा।
1. हंगरी- गाइल्स महोदय का मत है
कि आर्यो का आदि निवास स्थान हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी था। उनका यह मत भाषा
विज्ञान के ऊपर है। उन्होंने इंडो-यूरोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक
अध्ययन करने के पश्चात् यह निश्चित किया कि प्राचीनतम आर्यो के आदि देश की भौगोलिक
अवस्था क्या थी,
वे किन किन
अन्नों, फलों, वनस्पतियों तथा
पशु-पक्षियों से परिचित थे। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीनतम
आर्य न तो किसी द्वीप पर रहते थे और न किसी समुद्रीय प्रदेश में। कदाचित् वे
समुद्र से भलीभांति परिचित थे। अनुमानतः उनका आदि निवास स्थान तो ऐसे देश में था
जो पर्वतों, नदियों अथवा झीलों से
घिरा था। आर्यो के परिचित पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, हिरन और भालू विशेष
उल्लेखनिय हैं। हाथी, बाघ, गिद्ध और बतख से वे
अपरिचित थे। गाइल्स महोदय का निष्कर्ष है ककि हंगरी ऐसे देश में था जो पर्वतों, नदियों अथवा झीलों से
घिरा था। आर्यो के परिचित पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, हिरन और भालू विशेष
उल्लेखनिय हैं। हाथी, बाघ, गिद्ध और बतख से वे
अपरिचित थे।
गाइल्स महोदय का
निष्कर्ष है कि हंगरी का देश अथवा डेन्यूब प्रदेश ही एक ऐसा भू-खण्ड है जिसमें ये
सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। अतः यही भूखण्ड आर्यो का आदि निवास स्थान रहा होगा।
कालान्तर में ये आर्य डारडेनलीज के मार्ग से एशिया माइनर में
प्रविष्ट हुए और वहां से मेसोपोटामिया तथा ईरान होते हुए भारत पहुंचे। यही
कारण है कि समस्त देशों में आर्य-इतिहास के अति प्राचीन अवशेष मिले हैं।
2. जर्मन प्रदेश- कुछ विद्वानों ने सहज
जातीय विशेषताओं के आधार पर आर्यो के आदि देश की समस्या को हल किया है। उनका मत है
कि प्राचीनतम आर्यों की सर्वप्रमुख जातीय विशेषता थी उनके भूरे बाल।
यूनानी पौराणिक परम्पराओं में उनके देवता अपोलो के बाल भूरे थे। इसी प्रकार
प्लूटार्क कैटो और सुला नामक रोमन शासकों को भी भूरे
बालों वाला बताता है। इन उदाहरणों से अनुमान होता है कि प्राचीन आर्यो के बाल भूरे
होते हैं। यह विशेषता आज भी जर्मन-जाति में पायी जाती है। अतः कदाचित् प्राचीनतम
आर्य जर्मनी के ही निवासी थे। कुछ पूर्वमिहासिक मृद्भाण्ड मध्य जर्मनी में
मिले हैं। कुछ विद्वान इन्हें प्राचीनतम आर्यो की कृतियां मानते हैं और इन्हीं के
आधार पर मध्य जर्मनी को आर्यो का आदि देश बताते हैं।
पेन्का नामक विद्वान् की धारणा
है कि भूरे बालों के अतिरिक्त प्राचीनतम आर्यो की जो अन्य शारीरिक विशेषताएं थीं
वे जर्मनी-प्रदेश के निवासी स्कैण्डिनेवियन्स में पाई जाती हैं। अतः
स्कैण्डिनेविया को ही आर्यो का आदि देश माना है, परन्तु उनके तर्क का आधार भाषा सम्बन्धी है। उनका कथन है कि
स्कैण्डिनेविया के ऊपर कभी भी विदेशी जाति का आधिपत्य नहीं रहा और तो भी उनके
निवासी इंडो-यूरोपीय भाषा बोलते हैं। अतः यह देश प्राचीनतम आर्यो का
आदि-देश रहा होगा। कुछ अन्य विद्वानों ने पुरातत्व क आधार पर पश्चिमी बाल्टिक
समुद्र-तट को आर्यो का आदि देश माना है। इनका कथन है कि इस तट पर पूर्व-पाषाणकाल
के अनुगामी काल की अति प्राचीन और सरल वस्तुएं मिली हैं। कदाचित् ये प्राचीनतम
आर्यो की होंगी। इस मत के प्रतिपादकों में विशेष उल्लेखनिय हैं मच महोदय।
3. दक्षिणी रूस- नेहरिंग महोदय ने
त्रिपोल्जे (दक्षिणी रूस) यूक्रेन में प्राप्त कुछ मद्भाण्डों का अध्ययन करने के
पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि ये 300 ई. पू. के हैं। आर्यो का आदि देश कदाचित्
रूस ही था। पोकोर्नी महोदय का अनुमान है कि प्राचीनतम आर्य स्टेप्स अथवा विस्तत
मैदानों में निवास करते थे। इस प्रकार के मैदान रूस में वेजर और विश्चुला नदियों
के बीच में और उसके आगे श्वेत रूस तक हैं। अतः यही प्रदेश आर्यो का आदि-प्रदेश रहा
होगा।
परन्तु यूरोपीय
सिद्धान्त को स्वीकार करने में निम्नलिखित कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं-
(1) केवल शारीरिक
विशेषताओं के आधार पर किसी जाति को आर्यों का वंशज कहना उचित प्रतीत नहीं होता है।
(2) जहाँ तक भूरे
बालों का प्रश्न है, प्रसिद्ध
भाष्यकार पतंजलि ने भूरे बालों को ब्राह्मणों का गुण बताया है। इस आधार पर तो
आर्यों को भारत का ही मूल निवासी क्यों नहीं कहा जा सकता।
(3) मृद्भाण्डों
को आधार मानकर आर्यों का आदि देश स्वीकार करना भी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि इस
तरह के मृदभाण्ड अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं।
मध्य एशिया का सिद्धान्त-
आर्यो के मूल
निवास स्थान के सम्बन्ध में मध्य एशिया का सिद्धान्त एक दूसरा
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। एक ईरानी अनुश्रति के आधार पर कुछ
विद्वानों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी
थे। प्राचीन ईरानियों के धर्म ग्रन्थों तथा वैदिक साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन ये
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ईरानियों की भाषा और धर्म में घनिष्ठ सम्बन्ध था। जेंदा-अवेस्ता
की भाषा वेदों की भाषा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। एक लेखक का तो यहां तक
कहना है कि “केवल एक-आधा शब्द या
वाक्य-खंड ही नहीं, वरन् एक सम्पूर्ण
पद्यांश को बिना शब्दावली परिवर्तित किये ही भारतीय से ईरानी भाषा में लाया जा
सकता है।" ईरानियों के देवता भी आर्यो के देवता के सदश थे। इन समानताओं के
आधार पर विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईरानियों और वैदिक आर्यों के पूर्वज एक
ही थे और दन दोनों जातियों का मूल निवास स्थान एक ही रहा होगा।
मध्य एशिया में आर्यों के मूल निवास
स्थान के सम्बन्ध में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के मत इस प्रकार हैं एडुअर्ट मेयर
के मतानुसार पामीर प्रदेश आर्यों का आदि-देश था। उनका कथन है कि इंडो-ईरानी लोग
पामीर प्लेटो के आसपास कहीं रहते थे। ऋग्वेद और जेंदा-अवेस्ता आर्यों
की दो पुरानी पुस्तकें हैं जिनमें भाषा सम्बन्धी अनके बातें मिलती है। इन दोनों
ग्रन्थों में कई समान वस्तुओं का उल्लेख आया है। उदाहरणार्थ, इनमें घोड़ों, प्राचीन गांवों, नाव खेने तथा कई वक्षों
का वर्णन आया है जिसमें पीपल मुख्य है। अतएव आर्यों की जन्मभूमि ऐसे स्थान में
होनी चाहिए जहां घोड़ों और गायों की अधिकता है, नाव चलाने के लिए झीलें हों, पीपल के वक्ष खूब होते हों और सर्दी भी पड़ती है। ऐसी भूमि
पामीर प्रदेश ही है, क्योंकि यहां ये
सारी चीजें पायी जाती है। रेहार्ड ने कहा है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य
एशिया ही था। उसने कहा है प्रारम्भ में आर्य वैक्ट्रिया और उसके आसपास के भूभाग पर
निवास करते थे। इस स्थान में जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण उन लोगों ने पूर्व–पश्चिम और उत्तर की ओर
प्रस्थान किया। उसके इस मत का आधार ईरानी प्राचीन अनुश्रुतियां हैं।
मध्य एशिया के
सिद्धांत के वास्तविक प्रवर्तक जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्समूलर माने जाते हैं। उनका कहना है कि आर्य
जाति और उसकी सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों और जेंदा-अवेस्ता से होता है। इन
ग्रन्थों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय तथा ईरानी आर्य
बहुत दिनों तक एक साथ निवास करते थे। अतएव इनका आदि देश भारत तथा ईरान के निकट
किसी स्थान पर रहा होगा। वहीं से एक शाखा ईरान को, दूसरी भारत को तथा तीसरी यूरोप को गयी होगी। उपर्युक्त
दोनों ग्रन्थों से यह पता लगता है कि प्राचीन आर्य पशु-पालन और कृषि
कार्य करते थे। अतएव वे एक लम्बे मैदान में रहते होंगे। इन तथ्यों के आधार पर मैक्समूलर
और अन्य विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मध्य एशिया ही आर्यों का मूल
देश था।
कुछ विद्वानों ने
रूसी और तुर्किस्तान को आर्यों का आदि-देश माना है। इस मत के प्रमुख
समर्थक हर्जफेल्ड महोदय हैं। बैंडेन्स्टीन का कहना है कि प्रारम्भिक, इण्डो-यूरोपीयों के
शब्द-कोष से यह पता चलता है कि पर्वत के निकट स्टेप्स के मैदान में रहते थे।
प्रोफेसर चाइल्ड तथा अन्य
कई यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि एशिया माइनर के बोगाजकोई (1400
ई.पू.) नामक स्थान में खुदाई होने पर कुछ ऐसे लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें ऋग्वैदिक
काल के आर्यों के देवता इन्द्र, वरुण आदि के नाम अंकित हैं। इन लेखों के अतिरिक्त बर्तन और
कोई अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां कोई
ऐसी जाति रही होगी जो बकरी, भेड़, गाय, बैल और घोड़े आदि पशु
पालती है, खेती करती और गांव बसाकर
रहती थी। ये सारी बातें आर्यों की सभ्यता यही स्थल था और यही से वे ईरान, भारत, अफगानिस्तान तथा यूरोप
में फैले थे। इन विद्वानों का यह मत है कि ऋग्वेद में वर्णित वनस्पतियों, फल फूल, पशु एवं भौगोलिक स्थिति
केवल एशिया के इसी भाग में ही सम्भव था। अतः मध्य एशिया ही आर्यों की जन्मभूमि है।
परन्तु मध्य
एशिया को आर्यों का देश स्वीकार करने में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं-
1. मध्य एशिया के
निवासियों में आर्यों के गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि आर्यों का आदि स्थान यहाँ
पर था तो यहाँ की आधुनिक जातियों में उनके वंशज आर्यों का प्रभाव क्यों नहीं पाया
जाता।
2. आर्य कृषि
कर्म करते थे परन्तु मध्य एशिया में कृषि कर्म हेतु उपजाऊ तथा उर्वरक प्रदेश नहीं
थे। अतः जल की कमी तथा अनुपजाऊ वाले प्रदेश को आर्यों का आदि देश स्वीकार करना
कठिन है।
आर्यो का आदि देश
भारत-
कुछ विद्वानों का
यह मत है कि आर्य भारतवर्ष में बाहर से नहीं आये थे, इसी देश के मूल निवासी
थे।
(1) सप्त सैन्धव- डॉ. अविनाशचन्द्र दास ने
सप्तसैन्धव-प्रदेश को आर्यो का आदि देश माना है। इस प्रदेश में
सिन्धु, वितस्ता, असिवनी, परुष्णी, बिपासा शतुद्रि और
सरस्वती नामक सात नदियां बहती थीं। इन्हीं के द्वारा सींचा गया उर्वर
प्रदेश प्राचीन काल में सप्तसैन्धव प्रदेश के नाम से प्रख्यात था और यही
प्रदेश आर्यों का आदि प्रदेश था। कालान्तर में इनके बीच धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो
गये। आर्यों का एक वर्ग देवों का उपासक रहा और दूसरा वर्ग असुरों का उपासक हो गया।
दोनों वर्गों में भंयकर युद्ध हुआ, जो वैदिक साहित्य में देवासुर-संग्राम के नाम
से उल्लिखित है। इस संग्राम में अअसुर-उपासक परास्त हुए और सप्तसैन्धव प्रदेश को
छोड़कर पश्चिम की ओर चल पड़े तथा ईरान में जाकर बस गये। पारसीकों के प्राचीनतम
ग्रन्थ जेन्दा-अवेस्ता में जिस अहुर-मज्दा का वर्णन है वह ईरान में
नवागत विरोधी 'आर्य-वर्ग' का ही देवता था। डॉ.
सम्पूर्णानन्द ने भी सप्तसैन्धव को ही आर्यों का आदि देश माना है।
(2)
ब्रह्मर्षि-देश- महामहोपाध्याय पं. गंगानाथ झा का मत है कि आर्यों का आदि-देश भारतवर्ष
का ब्रह्मर्षि-देश था।
(3) मध्यदेश- डॉ. राजबली पाण्डेव
भारतवर्ष के मध्यदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। यहीं से वे
पश्चिमी भारतवर्ष,
मध्य एशिया और
पश्चिमी एशिया पहुंचे थे। ऋग्वेद में सप्त-सैन्धव का वर्णन अवश्य है, परन्तु इसकी रचना जो उस
समय हुई थी जब आर्य अपने मूल निवास मध्य देश को छोड़कर पंजाब में आ गये थे।
(4) कश्मीर- श्री एल.डी. कल्ल ने
मतानुसार कश्मीर अथवा हिमालय-प्रदेश को आर्यों का आदि देश
समझना चाहिए।
(5) देविका
प्रदेश- मुल्तान में देविका
नामक नदी है। श्री डी. एस. त्रिदेव इसी नदी के समीपवर्ती प्रदेश को आर्यों
का आदि निवास स्थान मानते हैं।
परन्तु भारतवर्ष
को आर्यों का आदि देश मानने में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं-
यदि आर्यों का
आदि देश भारत होता तो वे अपने देश का पूर्णरूपेण आर्यीकरण करते तब
दूसरे देशों को जाते। परन्तु ऋग्वेद से स्पष्ट सूचना मिलती है कि तत्कालीन
आर्य मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत तथा दक्षिणापथ से प्रायः अपरिचित थे जबकि ईरान
और अफगानिस्तान के सन्दर्भ में उनका भौगोलिक ज्ञान अपेक्षाकृत ज्यादा था। इससे
प्रतीत होता है कि वे बाहर से आये थे और ऋग्वैदिक काल तक वे पंजाब के प्रदेष से
आगे के भारत में प्रविष्ट नहीं हुए थे।
इण्डो-यूरोपियन
परिवार की प्राचीनतम भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से हमें जिन वनस्पतियों और
पशु-पक्षियों का पता चलता है वे सब भारत में नहीं पायी जाती। इससे यह निष्कर्ष
निकालना स्वाभाविक है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे।
बलूचिस्तान में द्रविड़ भाषा के प्रचलन से यह स्पष्ट हो जाता
है कि भारत के अधिकांश भागों में आर्य भाषा का प्रचलन नहीं था। इस आधार पर भी भारत
को आर्यों का आदि देश नहीं माना जा सकता है।
उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश-
श्री बालगंगाधर
तिलक ने ऋग्वैदिक
विवरण की व्याख्या में लम्बी अवधि प्रायः 6 माह के रात और दिन का अनुमान लगाकर उत्तरी ध्रुव प्रदेश या
आर्कटिक प्रदेश को आर्यों का निवास बताया है जहाँ से हिम प्रलय के कारण वे
हटकर भारत आये थे। श्री तिलक के मतानुसार ईरानी अवेस्ता में उत्तरी ध्रुव
के संकेत मिलते हैं और भीषण तुषारापात का वर्णन भी मिलता है। आर्यों द्वारा
वर्णित वनस्पति और उनकी औषधियां उत्तरी ध्रुव में प्राप्त होती हैं। परन्तु इस
सिद्धान्त को मानने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि
सम्पूर्ण भारतीय
साहित्य में कहीं भी उत्तरी ध्रुव को आर्यों की भूमि नहीं कहा गया है और यदि आर्य उत्तरी
ध्रुव को अपना आदि देश मानते तो सप्तसैंधव को 'देवकृत योनि' न कहते।
वर्तमान विचार-
हिन्द-यूरोपीय
भाषा, आर्य संस्कृति की
सर्वप्रमुख विशेषता मानी जाती है। भाषाशास्त्रीयों ने आद्य हिन्द-यूरोपीय
भाषा का प्रारंभ सातवीं या छठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व अर्थात आज से 8-9 हजार वर्ष पूर्व बतलाया
है। हिन्द-यूरोपीय भाषा का की दो शाखाऐं थीं- एक पूर्वी शाखा और दूसरी पश्चिमी
शाखा। भाषाशास्त्रियों के अनुसार पूर्वी हिन्द-यूरोपीय भाषा शाखा के उच्चारण
संबंधी विकास में पांचवी सहस्राब्दी के मध्य में अनेक चरण देखने को मिलते हैं। ऐसी
ही एक भाषा संभवतः आद्य हिन्द-ईरानी भाषा थी।
डॉ. आर. एस.
शर्मा बतलाते हैं कि
इसमें हिन्द-आर्य भाषा भी शामिल थी और इस भाषा के प्राचीनतम प्रमाण इराक के
अगेड वंश के पाटिया पर लिखे मिलते हैं जिनका समय 2300 ईसा पूर्व है। डॉ
शर्मा आगे बताते हैं कि इस अभिलेख में अरिसेन और सोमसेन नामक
व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। इसी प्रकार हिट्टाइट अभिलेख से जो साक्ष्य
मिले हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस स्थान पर हिन्द-यूरोपीय भाषा की
पश्चिमी शाखा के बोलने वाले वहां 19वीं सदी से 17वीं सदी ईसा पूर्व में विद्यमान थे। इसी प्रकार डॉ. शर्मा
बतलाते हैं कि मेसापोटामिया में कैस्साइट और मिटानी शासकों के बोगजकोई
अभिलेखों से पता चलता है कि 16वीं से 14वीं सदी ईसा पूर्व में इस
भाषा की पूर्वी शाखा के बोलने वाले विद्यमान थे।
डॉ. शर्मा का विचार है कि
हिन्द-ईरानी भाषा का विकास पश्चिम में फिनलैण्ड और पूरब में कॉकेशस क्षेत्र के बीच
कहीं था। गॉर्डन चाइल्ड ने इण्डो-आर्यों के उद्गम पर प्रकाश डालते हुए अनातोलिया
को इण्डो यूरोपीयों का मूल निवास स्थान बतलाया। कुछ अन्य
पुराविद्-सह-भाषाशास्त्रियों ने भी इस मत का समर्थन करते हुए इण्डो-यूरोपीय भाषा
का मूल स्थान कॉकेशस के दक्षिण क्षेत्र अर्थात पूर्वी अनातोलिया और उत्तरी
मेसोपोटामिया क्षेत्र को माना है। रेनफ्रू नामक पुराविद् भी पूर्वी
अनातोलिया को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं।
 |
| वैदिक सभ्यता (Vedic Civilization) |
इस संबंध में
डॉ. आर. एस. शर्मा रोचक तथ्य रखते हुए बताते हैं कि जीवन विज्ञानियों की हाल
के शोध कार्य मध्य एशिया से मानव प्रसरण पर सम्यक पेकाश डालते हैं। मानव की रक्त
कोशिकाओं में जो उत्पत्ति संबंधी संकेत (डी.एन.ए.) होते हैं वे मानव पीढ़ियों में
सदैव रहते हैं। जीवन-वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह के कुछ विशेष संकेत मध्य एशिया
के एक छोर से दूसरी छोर तक 8000 इस्वी पूर्व के
आसपास मिलते हैं। इन विशेष संकेतों का नाम एम 17 दिया गया है और ऐसे संकेत मध्य एशिया के 40 प्रतिशत से अधिक लोगों
में मिलते हैं लेकिन ये संकेत द्रविड़ भाषाभाषियों के केवल 10 प्रतिशत जनसंख्या में
मिले हैं, इससे पता चलता है कि
इण्डो-आर्य मध्य एशिया से भारत पहुंचे थे।
भारत में आर्यों का
आगमन
प्राचीनतम आर्य
भाषाभाषी पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर
प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों तक फैले हुए थे। अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ जैसे कुभा
नदी और सिंधु नदी तथा उसकी पांच शाखाऐं ऋग्वेद में उल्लिखित हैं।
सिंधु नदी, जिसकी पहचान अंग्रेजी के 'इंडस' से की जाती है, आर्यों की विशिष्ट नदी है, और इसका बार-बार उल्लेख
होता है। दूसरी नदी 'सरस्वती' ऋग्वेद में सबसे अच्छी
नदी (नवीतम) कही गई है। इसकी पहचान हरियाणा और राजस्थान में स्थित घग्गर-हाकरा की
धार से की जाती है। लेकिन इसके ऋग्वैदिक वर्णन से पता चलता है कि यह अवेस्ता
में अंकित हरख्वती नदी है जो आजकल दक्षिण अफगानिस्तान की हेलमंद नदी
है। यहां से सरस्वती नाम भारत में स्थानांतरित किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप के
अंतर्गत जहां आर्य भाषाभाषी पहले पहल बसे वह संपूर्ण क्षेत्र सात नदियों का देश
कहलाता था।
ऋग्वेद से हम भारतीय आर्यों के
बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 363 बार उल्लेख है, और इससे सामान्यतया
हिंद-आर्य भाषा बोलने वाले सांस्कृतिक समाज का संकेत मिलता है। ऋग्वेद
हिंद-आर्य भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है
लेकिन इसमें अनेक मुंडा और द्रविड शब्द भी मिलते हैं। शायद ये शब्द हड़प्पा
लोगों की भाषाओं से ऋग्वेद में चले आए।
ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरूण आदि देवताओं की
स्तुतियों संगृहित हैं जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्रस्रष्टाओं ने
की है। इसमें दस मंडल या भाग हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दशम
मंडल सबसे बाद में जोड़े गए मालूम होते हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें जेंदा-अवेस्ता
से मिलती हैं। जेंदा-अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम गंथ हैं। दोनों में
बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी समान हैं। पर हिंद-यूरोपीय भाषा का
सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 2200 ई० पू० के एक अभिलेख
में मिला है। बाद में इस तरह के नमूने अनातोलिया (तुर्की) में उन्नीसवीं से
सत्रहवीं सदी ईसा पूर्व के हत्ती (Hittite) अभिलेखों में मिलते हैं। इराक
में मिले लगभग 1600 ई० पू० के कस्सी (Kassite) अभिलेखों में तथा सीरिया
में मितानी (Mitanni) अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। उनसे
पश्चिम एशिया में आर्य भाषाभाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। लेकिन भारत में
अभी तक इस तरह का कोई अभिलेख नहीं मिला है।
भारत में आर्य जन कई खेपों
में आए। सबसे पहले की खेप में जो आए वे हैं ऋग्वैदिक आर्य, जो इस उपमहादेश में 1500
ई. पू. के आसपास दिखाई देते हैं। उनका दास, दस्यु आदि नाम के स्थानीय
जनों से संघर्ष हुआ। चूंकि दास जनों का उल्लेख प्राचीन ईरानी साहित्य में भी मिलता
है, इसलिए प्रतीत
होता है कि वे पूर्ववर्ती आर्यों की ही एक शाखा में पड़ते थे। ऋग्वेद में
कहा गया है कि भरत वंश के राजा दिवादास ने शंबर को हराया। यहाँ दास
शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे
गए हैं वे संभवतः इस देश के मूलवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित
किया था वह त्रसदस्यु कहलाया। वह राजा दासों के प्रति तो कोमल था, पर दस्युओं का परम शत्रु
था। ऋग्वेद में दस्युहत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, पर दासहत्या का नहीं।
पश्चिमी एशिया के
बोगाजकोई (एशिया माइनर) से प्राप्त चौदहवीं शताब्दी ई० पू० के कुछ अभिलेखों
में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है, जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो सन्धियों की साक्षी तथा
रक्षा के लिए इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे देवताओं का आहवान करते थे। यह निश्चित है
कि ये अभिलेख आर्य धर्म की विकासावस्था के हैं, जबकि उनके इन्द्र, वरूण और उनसे सम्बद्ध
अन्य देवता भी अपनी प्रारम्भिक वैदिक प्रधानता कायम रखे हुए थे। इन्द्र के
ये उपासक अपने पहले के निवास स्थान सिन्धु की तराई से एशिया माइनर चले गये या इसकी
क्रिया ठीक इसके विपरीत थी। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद की एक ऋचा में एक उपासक
अपने प्रत्न ओकस् यानी प्राचीन निवास स्थान से उन्हीं इन्द्रदेव का
आहवान करता है, जिन्हें उसके पूर्वज भी पूजते थे। यह भी ज्ञात है कि यदु और
तुर्वंश ऋग्वेद के दो प्रधान जन थे, इन्द्र जिन्हें किसी दूर
देश से लाये थे। कई ऋचाओं में यदु का विशेष सम्बन्ध पशु या पर्शु से जो नाम
पर्शिया के प्राचीन निवासियों का था, स्थापित किया गया है।
तुर्वश ने एक राजा से युद्ध में भाग लिया था, जिसका नाम पार्थव
कहा गया है।
वैदिक संस्कृति
वैदिक संस्कृति को जानने के हमारे पास
मुख्यतः चार वैदिक ग्रन्थ है जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अन्य तीन उससे बाद
के हैं। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बाटा जाता है प्रथम ऋग्वैदिक
संस्कृति या पूर्व वैदिक काल (1500-1000 ई.पू.) जिसमें ऋग्वेद पर
आधारित उस काल के समाज का वर्णन है जबकि आर्य लोग छोटे-२ कबीलों में रहते
थे तथा मुख्यतः पशुपालक थे। इस समय वे हरियाणा में सरस्वती तक ही बसे थे। दूसरे
काल को उत्तर वैदिक काल (1000-600 ई.पू.) कहा जाता है जिसका मुख्य स्त्रोत
बाद के तीनों वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थ इत्यादि है। इस समय उनका प्रसार पूर्वी भारत
तथा विन्ध्य पर्वत तक के क्षेत्र में हो चुका था।
ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल (1500-1000 ई.पू.)
ऋग्वेद को भाषा विज्ञान के आधार
पर 1500-1000 ई. पूर्व माना जा सकता है। इसके 10 सर्ग या मंडल है जिनमें दूसरे और
सातवें को सबसे पहले की रचना माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग छोटे-२ बहुत
से कबीलों में बंटे हुए थे तथा हमेशा ही नए क्षेत्रों की तलाश में आए बढ़ रहे थे।
ये कबीले न केवल गैर आये लोगों से निरन्तर युद्धरत रह बल्कि आपस में भी उनका हमेशा
संघर्ष चलता रहता था।
पंचजन-
भारतीय आर्य
अनेक वर्गों में विभक्त थे। इनमें 'पंचजन' विशेष प्रसिद्ध
थे। इनके नाम हैं- अनु, द्रद्यु, यदु, तुर्वसु तथा पुरू इनके
अतिरिक्त अन्यान्य गण भी थे। इनमें भरत, क्रिवि और त्रिसु विशेष उल्लेखनीय हैं।
पारस्परिक युद्ध-
पारस्परिक
युद्धों में सर्वप्रमुख युद्ध है दश राजाओं का युद्ध। आर्यो के
भारतवर्ष का राजा सुदास था। यह अत्यन्त वीर और साम्राज्यवादी नरेश था। बहुत दिनों
से विश्वामित्र भरत-वर्ग का पुरोहित था। वह बड़ा योग्य व्यक्ति था। परन्तु कुछ समय
के पश्चात् वह पुरोहित-पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित-पद
दिया गया। विश्वामित्र इस अपमान से बड़ा क्षुब्ध हुआ। उसने निकटवर्ती दस
राजाओं का एक संघ बनाया और उसकी सहायता से भरत-नरेश सुदास के विरुद्ध युद्ध की
घोषणा कर दी। परुष्णी (रावी) के तट पर दोनों पक्षों में भंयकर युद्ध हुआ।
इसमें सुदास की विजय हुई और पंजाब में उसकी प्रतिष्ठा अभूतपूर्व हो गई।
दस राजाओं के इस
संघ के अतिरिक्त सुदाय ने शिवों, अलिनों, विषणियों और पक्थों के
संघों को भी भिन्न-भिन्न कालों में पराजित किया था। सुदास अपने काल का एक
प्रमुख वीर और साम्राज्यवादी था। अनायों से युद्ध पारस्परिक युद्धों के अतिरिक्त
आर्यों को अनार्यों के साथ भी युद्ध करने पड़े थे। ये अनार्य भारतवर्ष कि निवासी
थे। ऋग्वेद में इनकी जातियों और इनके नरेशों के नामोल्लेख मिलते हैं।
अनार्य जातियों में अज, यक्षु, किकट, पिशाच और शिग्रु आदि के
नाम आते हैं। अनार्य राजाओं में विशेष उल्लेखनीय हैं मेद। इसे सुदास ने पराजित
किया था। इन नरेशों के अतिरिक्त सम्बर, धुनि और चुमुरि आदि अन्यान्य अनार्य-नरेश भी थे।
आर्यों को अपने भूमि-विस्तार के
लिए पग-पग पर इन्हीं अनार्यों से युद्ध करना पड़ा। अपने उत्कृष्ट सैनिक संगठन और
प्रबल अश्वारोहियों के कारण इस आर्य-अनार्य युद्ध में आर्यों की विजय हुई और
उन्होंने शनैः शनैः अनार्य-प्रदेशों को अधिकृत कर लिया तथा अनार्यों को 'दास' अथवा 'दस्यु' की संज्ञा दी। ऋग्वेद के
वर्णनों से प्रकट होता है कि आर्यों और अनार्यो में मौलिक रूप से शारीरिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक
भेद थे। अनार्य काले थे और उनकी नाक चपटी होती थी। ऋग्वेद में उन्हें 'अनासा' (बिना नाक वाले) कहा गया
है। उनकी भाषा भी भिन्न थी। इसी से आर्य अनार्यो को 'मध्रबाक्' कहते थे। इन भेदों के
अतिरिक्त आर्यो और अनार्यो में प्रबल धार्मिक भेद था। इसी तथ्य को प्रदर्शित करते
हुए आर्यो के लिए 'देवपीयु' (देवताओं को अपवित्र करने
वाले), अदेवयुः (देवताहीन), अन्यव्रत (अन्य प्रकार की
क्रियायें करने वाले), अयज्वन् (यज्ञ न करने वाले) और 'अकर्मन्' (कर्महीन) आदि शब्दों का
प्रयोग किया है।
युद्ध प्रणाली-
आक्रमण अथवा उसकी सम्भावना होने
पर वे अपने धन-जन की रक्षा के हेतु विशिष्ट प्रकार से बने हुए दुर्गों में शरण
लेते थे। इन्हें 'पुर' कहते थे। ये
पाषाण-निर्मित अथवा धातु निर्मित होते थे। इनके चारों ओर प्रायः लकड़ी की
चारदिवारी बनी रहती थी। इन दुर्गों के अतिरिक्त आर्यों के ग्राम भी कभी-कभी
चारदिवारी अथवा खाइयों से संरक्षित होते थे। आग लगाकर इन चारदिवारी को नष्ट करना
आक्रमणकारियों की सर्वप्रथम योजना होती थी। युद्ध करने के लिए राजा के पास सेना
होती थी।
राजा और राजन्य (उसके
उच्चवर्गीय सहायक) रथों पर चढ़कर लड़ते थे और साधारण मनुष्य पैदल। आर्य
अश्वारोहण से परिचित थे। अतः उनकी सेना में पदाति के साथ-साथ अश्वारोही भी होते
होंगे। परन्तु ऋग्वेद में रथारोहियों का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद मे शर्ध, व्रात और गण आदि शब्दों
का प्रयोग किया गया है। बहुत सम्भव है कि ये सेना की इकाइयों के नाम हो।
सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी
स्वयं राजा होता था। युद्ध के अवसर पर वह सेना का नेतत्व करता था। सैनिक कार्यों
में राजा की सहायता करने के लिए सेनापति की नियुक्ति की जाती थी। वह राजा के
परामर्श से सेना का संगठन करता और युद्ध की योजना बनाता था। राजा और सेनापति के
अतिरिक्त सेना के साथ राजपुरोहित भी होता था। वह अपने देश और नरेश की विजय के लिए
देव-स्तुति करता था और सैनिकों को उत्साहित करता था। युद्ध प्रमुखतया धनुष-बाण से
होता था। बाणों की नोंकें प्रायः नुकीले लोहे की होती थी। कभी-कभी बाणों के सिरों
पर नुकीले और विशाक्त सींग भी लगे रहते थे। ऋग्वैदिक काल के अन्यान्य
आयुधों से बरछी,
भाला, फरसा और तलवार उल्लेखनीय
हैं।
ऋग्वेद में
कहीं-कहीं पर 'पुरचरिष्णु' का उल्लेख हुआ है।
कदाचित् दुर्गो के गिराने के लिए विशेष प्रकार के इंजिन थे। युद्धों में आत्मरक्षा
के लिए प्रधान योद्धा कवच और शिरस्त्राण धारण करते थे। कभी-कभी बाहुत्राण और
अंगुलित्राण के प्रयोग के उदाहरण भी मिलते हैं। सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए
रण-वाद्य का भी उपयोग होता था। उनके साथ पताकाएं भी रहती थीं।
ऋग्वैदिक कालीन राज्य संरचना (Rigvedic State Structure)
इस काल में हमें
राज्य की संरचना का अधिक ज्ञान, साक्ष्यों के
अभाव में नहीं है। प्रारंभिक वैदिक काल मे राज्य का पूर्ण स्वरूप सामने नहीं आया
था। इसकी जानकारी हमें प्राचीन स्त्रोतों से मिलती है। प्रसिद्ध सप्ताहंग सिद्धांत
के आधार पर यदि हम देखें तो इस काल में ये सातों अंग 1. राजा 2. मंत्री 3. क्षेत्र
4. संसाधन 5. किले 6. सेना 7. सहयोगी, में से अधिकतर अंग नहीं थे।
प्रांरभिक वैदिक
समाज अलग-अलग कबीलों में विभजित था, जिन्हें जन या विश कहते थे। इन कबीलों के
अनार्यो से परस्पर संघर्ष चलता रहता था इसके अलावा ये आपस में भी युद्ध करते रहते
थे। इस काल के प्रमुख कबील युद्ध, तुरकसु, द्रहयु, अनु और पुरू इत्यादि थे।
ये एक स्थान पर टिक कर निवास नहीं करते थे बल्कि जगह-जगह घूमते रहते थे। यानि लंबे
अरसे तक कहीं स्थायी निवास नहीं करते थे। इस प्रकार क्षेत्र, जो राज्य का एक
महत्वपूर्ण अंग होता है इस काल में नहीं था।
इस काल में ना
कोई महत्वपूर्ण शासक था बल्कि प्रत्येक कबीले (जन) का अपना अलग मुखिया होता
था जो राजन कहलाता था। यद्यपि यह पद वंशानुगत होता था जिसका प्रमाण हमें दिवोदास
तथा सुदास राजाओं से मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उदाहरण है जब
सर्वसम्मती से राजा का चुनाव किया हो तथा आवश्यकता पड़ने पर जनता ने राजा को
पदच्युत कर दिया। वंशानुगत राज्याधिकार तभी तक वैध था जब तक जनता उसको अनुमोदित
करती। इस काल ने राज्य के कोई संसाधन नहीं थे तथा लोगों की सम्पति उनके मवेशी
होते थे। जिसके पास ज्यादा गाय होती वह ज्यादा सम्पन्न माना जाता था।
राजकोष जो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है इस काल में नहीं था। इस काल में
किले और सैनिकां का महत्व था। सेना स्थायी नहीं थी, आवश्यकता पड़ने पर आम जनता सैनिक कार्य भी करती थी। सेना
में पैदल और घुड़सवार दोनों शामिल थे। राजा या राज्य के सहयोगी राज्य का अन्तिम
सांतवा अंग माना जाता है इस काल में सभी जन आपस में झगड़ते रहते थे यद्यपि दश
राजाओं के संघ का संयुक्त युद्ध करने का प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है।
उपर्युक्त
साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में राज्य सरंचना अभी नहीं हुई थी।
इस काल में राज्य का स्वरूप कबीलाई संरचना पर आधारित था। जिसमें कबीले
के लोगों के आपसी संबंध थे। इस काल के जनों का कोई स्थाई क्षेत्रीय आधार नहीं था
तथा राजन या कबीलें का मुखिया अपने कबीलें के साथ हर समय घूमता रहता था। इस
काल में अश्व केन्द्रित राजतंत्र का काफी महत्व था जिनके पास घोड़े
थे उन्हें उच्च माना जाता था। राज्य सता के सूचक संघटनों के प्रमाण हमें ऋग्वेद
से नहीं मिलते। ऋग्वेद में वर्णित व. वता, जन, विश, गण, गह, व्रजा तथा ग्राम इत्यादि
शब्दों का उल्लेख जनसमूह अथवा योद्धा समूह के लिए हुआ है। जो इस बात की पुष्टि
करता है कि ऋग्वैदिक समाज अस्थाई और घुमक्कड़ जनसमुदाय था तथा रक्त संबंधों
पर आधारित जन-जातिय समाज संगठित था।
राजनैतिक इकाइयां (Political Units)
ऋग्वैदिक काल में
सामान्यतः राजतन्त्रात्मक सरकार थी। राजन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक
बार हुआ है। ऋग्वेद की एक ऋचा मे सिन्धु प्रदेश के राजा का उल्लेख है तथा अन्य में
सरस्वती पर निवास कर रहे राजा चित्र का उल्लेख है। सुदास का दस राजाओं के संगठन से
युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। दान-स्तुतियों में भी राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये
प्रमाण राजतंत्र की ओर इशारा करते हैं। इसके अतिरिक्त गण, गणपति तथा ज्येष्ठ का
उल्लेख गणतंत्रात्मक स्वरूप होने की ओर इशारा करता है। ऋग्वैदिक काल में
राज्य जनों में विभक्त था और प्रत्येक जन में एक ही कबीले के लोग निवास करते थे
जिनका आपस में रक्त-संबंध थे। सूपास के साथ युद्ध करने वाले दस राजाओं के
संगठन का राजनैतिक स्वरूप कैसा था, इसकी जानकारी हमारे पास नही हैं इस काल में राजा की स्थिति
काफी महत्वपूर्ण थी हांलाकि वह अपने कबीलें का मुखिया ही था। लेकिन कुछ राजा कबीले
के मुखिया की स्थिति से उपर थे। सामान्यतः वंशानुगत राजतंत्र के प्रमाण मिलते हैं।
किन्तु ऐसे भी प्रमाण है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विश (जो
राष्ट्र की एक इकाई थी) राजपरिवार या राजसदस्यों में से राजा का भी चुनाव कर सकते
थे।
सभा एवम् समिति (Assembly And Committee)
ऋग्वेद में सभा और समिति
का अनेक बार उल्लेख हुआ है। सभा और समिति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हिलबॅण्ड
का कथन है कि समिति एक राजनैतिक संस्था थी तथा सभा उसका अधिवेशन
स्थल। लुडविंग सभा को उच्चतर सदन तथा समिति को निम्न सदन का
नाम देते है। परन्तु ऋग्वेद में इस बात का प्रमाणित करने के उल्लेख कहीं
नहीं मिलता। जिमर महोदय का कहना है कि सभा ग्राम संस्था थी तथा समिति
केन्द्रीय संस्था। ऋग्वेद में समय शब्द के उल्लेख (सभा के योग्य) से पता
चलता है कि सभा का कोई प्रशासनिक उद्देश्य था तथा समिति को वैदिक कबीलों की एक
संस्था के रूप में माना जा सकता है। लुडविंग के अनुसार समिति में विश के
लोग ब्राह्मण तथा अन्य उच्चवर्ग के व्यक्ति शामिल थे।
यद्यपि सभा
और समिति के कार्यों में अतंर स्पष्ट करना कठिन है लेकिन प्रतीत होता है कि
समिति एक ऐसी संस्था थी, जिसमें कबीलों के
प्रमुख कार्य सम्पन्न किए जाते थे तथा राजा उनका अध्यक्ष होता था। तथा सभा समिति
की तुलना में कम महत्व की संस्था था जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल थे। यद्यपि
हमें सभा और समिति के कार्यो एवम् अधिकारों का अधिक ब्यौरा ऋग्वेद में नहीं
मिलता। लेकिन इन दोनों संस्थाओं का समाज में काफी महत्व था तथा ये इस काल में राजा
की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। इन दोनों राजनैतिक संस्थाओं के अतिरिक्त राजा पर
पुरोहित का भी काफी प्रभाव था। यह राजा के साथ ने केवल युद्धों में जाता था। बल्कि
यज्ञ और प्रार्थनाएं भी सम्पन्न करता था। इस काल के शक्तिशाली पुरोहितों में वशिष्ठ
तथा विश्वामित्र के नाम उल्लेखनीय हैं जिनका राजा पर काफी नियंत्रण था।
प्रशासनिक संस्थाएं (Administrative Institutions)
इस काल में
सम्पूर्ण कार्य अनेक जनों में विभक्त थे। ऋग्वेद में उल्लिखित पंचजन उस काल
के पंच महत्वपूर्ण कबीले थे। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे कबीलें भी थे।
ऋग्वेदि में विश शब्द का उल्लेख अनेक बार हुआ है जिसका उस काल की राजनैतिक
संस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। सभी कबीले के सदस्य मिलकर राष्ट्र या कबीले के
मुखिया का निर्माण करते थे। विश, जन तथा गांव में
विभक्त थे। सुरक्षा के लिए पुर का निर्माण करते थे। सुरक्षा के लिए पुर का निर्माण
किया जाता था जो पत्थरों से निर्मित थे। ग्राम एक ही कुल की अलग-अलग
इकाईयों के बने थे। जिसमें कुल का प्रशासनिक संगठन में महत्व था। एक स्थान पर कुलपा
या कुल का संरक्षक का वाजपति जो शायद ग्रामणी ही था के साथ एक झण्डे तले
लड़ने का वर्णन है। यह वर्णन हमें कुलपा के ग्रामीण के साथ सिविल और सैनिक कार्यो
के महत्व को दर्शाता है। सेनानी उस समय का सैनिक अधिकारी था, तथा पुरोहित के समान ही
यह महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हमें स्पर्श का भी उल्लेख
मिलता है। दूत या संदेशवाहक का कार्य इस काल ने राजा के संदेश लोगों तक या अन्य
कबीलों तक पहुचाना था।
ऋग्वैदिक कालीन समाज (Rigvedic Society)
प्रारंभिक वैदिक
काल के समाज का आधार सगोत्रीय और मुख्यतः कबीलाई संरचना पर आधारित
था। जिसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया के चिन्ह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने नहीं आए
थे। इस काल का समाज कई अर्थो में प्रायः समानतावादी था जिसमें एक ओर पदों के आधार
पर अनेक विभिन्नताएं थी, जो विशेषकर पशुओं
की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती थी, इसके अतिरिक्त लिंग और आयु भेद के आधार पर भी सामाजिक स्तर
पर असमानताएं थी। लेकिन दूसरी ओर मनुष्यों के लिए उत्पादक संसाधनों को प्राप्त
करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। ऋग्वेद में वर्णित इकाइया विश, जन, गण-वात आदि कबीलाई संगठन
की ओर संकेत करती है। जन और विश सामूहिक उत्पादन की महत्वपूर्ण
इकाइयां थी। ऋग्वेद में जन और विश शब्दों का कई बार प्रयोग हुआ है, जन विश के रूप में विभक्त
था, उनमें से एक का संबंध
संपूर्ण कबीले से था तथा दूसरे का गोत्र से। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275
बार तथा विश का 171 बार हुआ है।
परिवारिक जीवन (Family Life)
इस काल में
परिवार का आधार पितृसतात्मक था, उसमें तीन या चार
पीढियों का समावेश था। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में वर्णित शुनहशेप
कहानी से हमें बच्चों पर पिता के पूरे नियंत्रण का पता चलता है। परिवार में
अनुशासन बहुत कठोर था तथा इसे तोडने वाले को सजा देने का अधिकार भी पिता को था।
जैसा कि उल्लेख है एक जुआरी पुत्र को उसके पिता तथा भाइयों ने दण्ड स्वरूप उसे बेच
दिया था। इस सन्दर्भ का तात्पर्य यह नहीं है कि इस काल में माता-पिता तथा संतान के
इसी प्रकार के सम्बन्ध हुआ करते थे, अपितु पिता को एक अच्छा तथा दयालु हृदय बताया गया है। एक ही
परिवार के कई पीढ़ियों के इक्ट्ठे रहने के भी प्रमाण मिले है। परिस्थितिवश परिवार
में पत्नी की मां के भी रहने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के दसवें अध्याय
में एक जुआरी यह शिकायत करता बताया गया है कि घर में उसकी सास उससे नफरत करती थी।
अतिथि सत्कार घर में एक धार्मिक कार्य माना जाता था।
प्रणय सूत्र (Courtship Formula)
ऋग्वेद में माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र और पुत्री के लिए
अलग-अलग शब्दावली थी, लेकिन भतीजों, पोत्रों और चचेरे भाइयों
के लिए मात्र एक शब्द नाप्त/नपत का प्रयोग किया जाता था। परिवार में पुत्र
प्राप्ती के लिए ऋग्वेद में विभिन्न स्तुतियों और प्रार्थनाओं का उल्लेख
मिलता है।
विवाह (Marriage)
ऋग्वेद से हमें विवाह
संबंधी जानकारियों का वर्णन मिलता है। सामान्यतः वयः सन्धि के बाद लड़की की शादी
की जाती थी और उन्हें अपने पति के चुनाव के अधिकार की भी स्वतन्त्रता थी। अविवाहित
लड़कियों का भी वर्णन मिलता हैं, घोषा इसी की तरह की एक
अविवाहित लड़की थी। इसके अतिरिक्त अपने प्रेमियों का लुभाने के लिए कन्याओं का
उत्सवों पर गहने पहनने का वर्णन तथा युवकों के अपनी प्रेमिकाओं को भेंट इत्यादि
देने के अनेक मंत्रों का वर्णन है। इनका विवाह दस्यु वर्ग या अनार्य
लोगों में नहीं हो सकता था तथा आर्यो में भाई-बहन तथा पिता-पुत्री
के विवाह पर प्रतिबन्ध था। विवाह में व्यस्कों को अपने पति और पत्नी चुनने की काफी
स्वतंत्रता थी ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नही कि माता-पिता या भाई की सहमति आवश्यक थी।
विवाह के दौरान इनकी उपस्थिति अनिवार्य थी।
विवाह में मंत्रों से पता चलता
है कि एक नवविवाहित स्त्री किस प्रकार अपने सास-ससुर, देवर और ज्येष्ठ पर अपने
प्यार और स्नेह से राज्य करती थी तथा उनका आदर भी करती थी। वधु विवाह भोज
में भी सम्मिलित रहती थी। बारातियों का स्वागत इस काल में गाय का मांस खिला कर
किया जाता था। वर-वधु का हाथ पकड़ कर अग्नि के पास-पास चक्कर लगाकर में बंधते थे।
सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी, ऋग्वेद में जो
प्रार्थनाएं की गई हैं वे पति और पत्नी दोनों की तरफ से है। परिवार में पुत्र और
पौत्र प्राप्ति की कामना के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। वधु को अपने घर में
सम्मान का दर्जा प्राप्त था, ऐसा वर्णन है कि
वह अपने पति के पिता, भाई तथा बहनों पर
राज करती थी, यह संदर्भ सभवतः उस
स्थिति का है जब बडे पुत्र की शादी हो गई हो तथा लड़के का पिता जीवन से मुक्त हो चुका
हो। परन्तु प्रतीत होता है कि यह अधिकार प्रेम के कारण ज्यादा था। यज्ञ, विवाह आदि अवसरों पर पति-पत्नी
की उपस्थिति अनिवार्य थी।
इस काल में विवाह
मुख्य रुप से सन्तानोत्पति (पुत्र की प्राप्ति) के लिए किया जाता था, पुत्री प्राप्ति की कामना
के प्रमाण ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलते। संभवत पितृसतात्मक समाज में पुत्र
की प्राप्ति ही आवश्यक थी। केवल पुत्र ही पिता का अंतिम संस्कार कर सकता था तथा
उसी से वशं आगे बढता था। यद्यपि पुत्र ना होने की स्थिति में पुत्र गोद लेने के भी
प्रमाण है परन्तु यह अधिक प्रचलित नहीं था।
महिलाओं की स्थिति (Condition of
Women)
पितृसतात्मक समाज के बावजुद
स्त्रियों की स्थिति उत्तरकालीन महिलाओं की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। ऋग्वेद
में पत्नी का यज्ञ करने और अग्नि में आहुतियाँ देने का स्पष्ट प्रमाण है। वे सभाओं
में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थी।
ऋग्वेद में ऐसी महिलाओं का
जिक्र है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचनाएँ की, जिनमें अपाला और विश्वआरा उल्लेखनीय है। इससे
स्पष्ट है कि स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतन्त्र थी। ऋग्वेद
के मंत्रों में पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएँ की गई है लेकिन पुत्री के
जन्म को कही भी दुःखद नहीं माना गया है। इस काल में सती प्रथा का
कोई सपष्ट प्रमाण नहीं है ऋग्वेद में एक स्थान पर एक विधवा को अपने पति की चिता से
नीचे उतर आने का कहे जाने के प्रमाण तो है लेकिन यह सती प्रथा का सपष्ट
प्रभाव नहीं है। यदि विधवा स्त्री को पुत्र नहीं है, तो वह अपने देवर के साथ सहवास कर पुत्र प्राप्त कर सकती थी।
यह बाद की नियोग प्रथा का ही एक प्रारूप है। इसके अतिरिक्त विधवा पुनःविवाह भी कर
सकती थी।
साधारणतः हमें एक
पत्नी विवाह के प्रमाण मिलते हैं लेकिन एक पुरूष की एक से ज्यादा पत्नियों
के भी प्रमाण है। यह शायद राजभ्य वर्ग में ज्यादा प्रचलित था, साध्य प्रमाण है। इसके
अतिरिक्त प्रजापति की कहानी में पिता-पुत्री तथा यम-यमी की कहानी में बहन-भाई के
शारीरिक संबंधों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसे मिथ्या मानते हैं। स्त्रियों को
विवाह तक अपने पिता की सुरक्षा में, विवाहोपरान्त पति की, यदि अविवाहित है तो अपने भाई की सुरक्षा में रहना पड़ता था।
इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे बाहर स्वेच्छा से घूमने, भोज, नत्य और उत्सवों से भाग
लेने के लिए स्वतंत्र ना हो। उनकी स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं था।
भोजन (Food)
प्रांरभिक वैदिक
काल में आर्य मांसाहारी दोनों प्रकार का आहार लेते थे। मुख्यतः पशुपालन पर
आधारित अर्थव्यवस्था के कारण दूध और उससे बनी वस्तुओं का वे अधिक सेवन करते
थे। घी या घृत का प्रयोग, जौ के आटे को दूध
या मक्खन में मिलाकर रोटी बनाने के प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। बैल, भेड़ और बकरी का मांस
इनके भोजन का मुख्य अंग था। अश्वमेघ सम्पन्न होने पर घोड़े का मांस सामान्य
रूप से खाया जाता था, ताकि घोड़े जैसी
तेजी प्राप्त कर सकें। यद्यपि गाय को अधन्य माना गया है दूध न देने वाली
गाय के मांस का सेवन भोजन के रूप में किया जाता था। इसके अतिरिक्त अतिथियों को
विशेष अवसरों पर गाय का मांस परोसा जाता था। ऋग्वेद में सोमरस पेय
का भी वर्णन है,
सुरा व शराब पीने
का भी उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त शहद का भी भोजन में प्रयोग करते थे।
पहनावा (Attire)
इस काल में पहनावा
साधारण था और आर्य मुख्यतः चार प्रकार के वस्त्र धारण करते थे जिनमें नीवी, वास,
अधिवास तथा अंतका प्रमुख थे, इसके अलावा भी था जो निम्न है-
नीवी- शरीर के निचले हिस्से
में पहनने वाला वस्त्र।
वास- मध्यभाग में पहनने वाला
वस्त्र।
अधिवास- ऊपरी हिस्से पर पहनने
वाला वस्त्र था।
अंतका- ऊन से बना हुआ वस्त्र।
क्षोम- धनी वर्ग के लोग एक
विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे जिसे क्षोम कहा जाता था।
उष्णीय- पुरूषों द्वारा सिर पर
पहनी जाने वाली पगड़ी।
कुम्ब- पुरूषों द्वारा पहने जाने
वाले विशेष प्रकार का आभूषण था।
निष्क- महिलाओं द्वारा गले में
पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण (कई विद्वानों ने स्वर्ण मुद्रा भी बताया है)
सोने की शुद्धता जाँच हेतु प्रयुक्त पारख पत्थर निष्क कहलाता था।
स्त्री और पुरूष
के पहनावे में ज्यादा अन्तर नही था। खाल या चमड़े का भी प्रयोग वस्त्र के रूप में
किया जाता था। मारूत को मृग छाल पहने हुए बताया गया है। इस काल में अटक भी एक
प्रकार का बुना हुआ वस्त्र था। ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। कढ़ाई किए गए
वस्त्र को पहने नृतकी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विवाह के अवसर पर वप्पु
विशेष वस्त्र धारण करती थी। सुन्दर वस्त्रों के लिए सुवासस् तथा सुवसन
शब्दों का उल्लेख मिलता है।
समाज में स्त्री और पुरूष
दोनों वर्ग आभूषण धारण करते थे। सोने का कर्णशोभन संभवतः पुरूषों के लिए
पहनने वाला आभूषण था। हिरण्यकर्ण सोने का आभूषण था जो देवताओं को पहने
दर्शाया गया है। कुरीर वधु के सिर पर पहनने वाला गहना था। हार के रूप में
सोने का आभूषण निष्क इस काल में प्रचलित था। मोती और हीरे में निर्मित
आभूषण गले में पहने जाते थे। एक ऋचा में अश्विनों को कमल के फूलों से ढ़का बताया
गया है। केश श्रंगार के भी शौकीन थे। तेल लगाकर कंघी निकाले हुए बताया गया है।
पुरूषों को दाढ़ी और मूंछ रखने का शौक था।
चिकित्सक और दवाईयां (doctors and medicines)
ऋग्वेद में इस काल में चिकित्सा
पद्धति का भी प्रमाण है। बिमारियों में दक्षम का भी यदा-कदा वर्णन मिलता है। ऋयाओ
में अनेक औषधियों तथा उनके गुणों का वर्णन है। इस काल में टूटी हुई हड्डियों को
जोड़ने की कला से ये परिचित थे। आंखों की रोशनी पुनः प्राप्त करने, अन्धेपन का इलाज, तथा अंगहीनता ठीक करने के
प्रमाण इस काल में मिलते हैं।
शिक्षा (Education)
ऋग्वेद के दसवें मण्डल में
शिक्षा प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है, कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक
शक्तियों का विकास कर सकता है। ऋग्वेद में उपनयन संस्कार को कोई प्रमाण नही
है। ऋग्वेद के मण्डूक सूक्त में हमें शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी
मिलती है, इसमें वर्णन है कि
विद्यार्थी अपने गुरू से मौखिक शिक्षा प्राप्त करते थे और विद्यार्थी उस सामूहिक
रूप से दोहराते थे। इस काल के विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचारी शब्द प्रयुक्त
किया जाता था। शिक्षा गुरूकुलों में दी जाती थी। इस काल में महिला शिक्षिकाओं का
भी उल्लेख है,
मैत्रेयी और गार्गी इस काल
की विदुषियां थी।
मनोरंजन (Amusement)
संगीत का ऋग्वैदिक काल में
विशेष महत्व था। वैदिक ऋचाओं का एक संगीतमयी लय में उच्चारण किया जाता था। इसके
अतिरिक्त वीणा और ढोला बजाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। अविवाहित कन्याओं
द्वारा किए जाने वाले नृत्य का भी वर्णन मिलता है। सामाजिक समारोह और
उत्सवों में पुरूष और स्त्री दोनों की नृत्य में भाग लेते थे। कीथ नामक
विद्वान के अनुसार इस काल में धार्मिक नाटकों का भी प्रचलन था। इसके अतिरिक्त
रथदौड़ और घुड़दौड़ मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था। चौपट तथा जुआ खेलने के
प्रमाण भी ऋग्वेद की विभिन्न ऋचाओं से मिलते है। आखेट भी मनोरंजन का एक
महत्वपूर्ण साधन था।
वर्ण व्यवस्था (Varna System)
वर्णसमाज की रूपरेखा ऋग्वैदिक काल
के अंतिम चरण मे आरम्भ हो गई थी जिसे पुरूष सूक्त 10वें मंडल में देखा जा सकता है।
ऋग्वेद के दसवें मंडल के प्रमुख पुरुष सूक्त में चार वर्णो का उल्लेख मिलता है।
इसमें उल्लेख है
कि देवताओं ने आदि पुरूष के 4 भाग किए; ब्राह्मण उसका मुख, राजन्य (क्षत्रिय) बाहु तथा जंघा वैश्य
हो और शुद्र की उत्पति उसके पैरों से हुई। प्रथम तीनों वर्णो की
उत्पति आदि पुरूष से नही हुई बल्कि वे उसके मुख, बाहु और जंघा के समान बताए गए है जबकि शुद्र की उत्पति
पैरों से होने का अर्थ यह हुआ कि उसका जन्म तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए हुआ
है।
प्रारंभ में शायद
वर्ग विभाजन मुख्यतः आर्य और अनार्यो के बीच हुआ होगा क्योंकि दोनों की
संस्कृतियां भिन्न थी। ऋग्वेद में 'दास' और 'दस्यु' वर्ग का उल्लेख भी मिलता
है जिनके साथ आर्यो के संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। दास और दस्यु
इस क्षेत्र में आदिम निवासी थे जिनसे आर्यो का संघर्ष हुआ। संभवतः युद्ध में हारे
जाने पर अनार्यो का बंदी बना कर सेवा कार्य लिया जाता होगा। संस्कृत में वर्ग लिए वर्ण
शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही वर्ण शब्द विभिन्न रूप-रंगों और विजातीय
संस्कृतियों के लोगों के साथ आर्यो के संपर्क के परिणामस्वरूप चार वर्णो के उद्भव
की ओर इशारा करता है। इस काल के अंतिम दौर में समाज चार वर्णो में बँट गया था, लेकिन जात-पात का बखेड़ा
खड़ा नहीं हुआ था इस व्यवस्था में लचीलापन था। ऋग्वेद में एक उदाहरण मिलता
है कि एक व्यक्ति कहता है, मेरे पिता पुरोहित है माता अनाज पीसती है और पुत्र
चिकित्सक है। इससे पता चलता है कि व्यवसाओं को अपनाने की स्वतंत्रता थी।
| वर्ण | उत्पत्ति | कार्य |
|---|---|---|
| 1.ब्राह्मण | मुख से | यज्ञ, हवन, कर्मकांड |
| 2.क्षत्रिय | भुजाओ से | रक्षा करना, शासन संचालन |
| 3.वैश्य | जंघाहों से | व्यापार, वाणिज्य |
| 4.शूद्र | पैरों से | निम्न वर्ग के कार्य, दास के रूप में |
ऋग्वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी यहाँ देवापि (पुरोहित) व उनके
पुत्र शांतनु का उल्लेख मिलता है।
आश्रम व्यवस्था (Ashram System)
आश्रम व्यवस्था का
उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में मिलता है।
इसमें संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसे चार बराबर भागों में
विभाजित कर दिया गया।
(1) ब्रह्माचर्याश्रम
(बाल आश्रम)- इसमें मानव जीवन
का समय 0 से 25 वर्ष तक का माना गया है। उपनयन संस्कार से प्रारंभ संत सामान्त
समावर्तन संस्कार से संयुक्त रूप से पूर्ण करना
इस आश्रम के
दौरान बालक को गुरु के पास भेजकर समस्त विधियों में निपुण बनाया जाता था विद्या
समाप्त होने के बाद वह अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने जीवन के दूसरे आश्रम गृहस्थ
आश्रम में प्रवेश करता था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय व इन तीनों
वर्णों को ही ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करना होता था अतः इन्हें द्विज कहा गया
शूद्रों के लिए केवल एक ही आश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम होता था।
(2) गृहस्थाश्रम- मानव जीवन का समय 26 से
50 वर्ष तक का माना गया है। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। इसे
संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है क्योंकि इस आश्रम के दौरान संतान
उत्पत्ति की जाती है जिससे यह संसार चलायमान रहता है।
(3)
वानप्रस्थाश्रम- इस में मानव जीवन का समय 51 से 75 वर्ष तक का माना गया है इसका शाब्दिक अर्थ वन
को गमन है। इस आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है।
इस दौरान मानव पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया से विरक्त नहीं हो पाता।
(4) संन्यासाश्रम- इस में मानव जीवन का समय
76 से 100 वर्ष तक का माना गया है इस आश्रम के दौरान मानव संन्यासी जीवन
व्यतीत करता है तथा सांसारिक माया जाल से मुक्त हो जाता है।
| आश्रम | आयु | कार्य |
|---|---|---|
| ब्रह्मचर्याश्रम | 0-25 वर्ष तक | बालक द्वारा गुरु से विद्या प्राप्त करना |
| गृहस्थाश्रम | 26-50 वर्ष तक | संतान उत्पत्ति करना |
| वानप्रस्थाश्रम | 51-75 वर्ष तक | वन को गमन करना |
| संन्यासाश्रम | 76-100 वर्ष तक | संन्यासी जीवन व्यतीत करना |
पुरुषार्थ (Effort)
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त
में 10वें मंडल में चार प्रकार के पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ से
तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्येश्य से है। पुरुषार्थ = पुरुष+अर्थ अर्थात मानव
को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। प्रायः मनुष्य के लिये वेदों में 4
पुरुषार्थों का नाम लिया गया है।
धर्म- नैतिक कर्तव्यों का
समूह। (ब्रह्मचर्य आश्रम में)
अर्थ- भौतिक आवश्यकताओं की
पूर्ति करना। (गृहस्थ आश्रम के लिए)
काम- संतानोत्पति करना (गृहस्थ
आश्रम के लिए)
मोक्ष- जन्म-मरण चक्र से मुक्ति
तथा जीवन के दुखों से मुक्ति। (संन्यास, वानप्रस्थ आश्रम के लिए)
ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था (Rig Vedic Economy)
वैदिक युग में भारतीय
समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि इस काल में लोहे के प्रयोग ने भारत के उत्तरी
मैदानों को कृषि योग्य बना दिया जिसके परिणामस्वरूप कृषि प्रणाली एवम् उससे जुड़ी
स्थायी जीवन व्यवस्था स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई जिसने अन्य पहलूओं (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक) को
भी प्रभावित किया। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वैदिक युग को
मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है; प्रथम जिसमें मुख्यतः पशुपालन पर आधारित आर्थिक व्यवस्था
पर जोर दिया गया तथा द्वितीय जिसमें कृषि की ओर झुकाव प्रदर्शित होता है।
इस काल की
अर्थव्यवस्था में पशु-पालन का सर्वाधिक महत्व था और पशु उनके स्वत्व और
संपति के सर्वाधिक मूल्यवान साधन थे। पशुधन की महता की जानकारी पशुओं के लिए की
जाने वाली प्रार्थनाओं से मिलती है। पशुओं के लिए बहुधा विभिन्न कबीलों में युद्ध
होते थे, युद्ध के लिए विशिष्ट
शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका अभिप्राय है गायों की खोज। ऋग्वेद में
कई स्थानों पर गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, यानि गाय का वध नहीं करना
चाहिए, इससे उसके आर्थिक महत्व
का बोध होता है।
गाय और बैल की इस काल
में महत्वपूर्ण पालतू पशु थे, यहीं इस काल का
धन थे तथा यज्ञ समापन के बाद दक्षिणा के रूप में इन्हें पुरोहितों का दिया जाता
था। गायों को रात के समय तथा दिन की धूप में बाड़ों में रखा जाता था। जबकि अन्य
समय में वे स्वतः चरागाहों में चरती रहती थी। शाम के समय गायों को वापिस बाड़ों
में लाया जाता था। इन कार्यो के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता
है। स्वसर का अभिप्राय सुबह चरगाहों में घास चरने जाने का है जबकि सम्गाव
का अर्थ शाम को दूध दोहने के लिए वापिस लाने के लिए प्रयुक्त होता था। लड़कियों के
लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दूध दोहने का कार्य वे ही किया करती थी।
ऋग्वेद में गायों पर आने वाले
खतरों का भी उल्लेख मिलता है जैसे गाय का खो जाना, चोरी हो जाना, पैर टूट जाना इत्यादि । इस काल में पशुओं के कानों पर निशान
दाग दिए जाते थे। जिससे उनके स्वामित्व की आसानी से पहचान की जा सकती थी। गाय को
इस काल में पवित्र नही माना गया क्योंकि भोजन के लिए गाय और बैल दोनों का वध किया
जाता था। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां तथा
घोड़े पालतू पशुओं की श्रेणियों में आते थे। पशुओं का पालन-पोषण सामूहिक रूप से
किया जाता था यानि कबीले के सभी सदस्यों का उन पर समान अधिकार था। पशुओं के महत्व
का इस बात से भी पता चलता है कि मुखिया का गोपति अर्थात् पशुओं का स्वामी
या सरंक्षक कहा जाता था।
इस काल में सीमित
कृषि का प्रमाण मिलता है और संभवतः इसका प्रचलन और महत्व अधिक नही था।
क्योंकि इस काल में यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। ऋग्वेद के प्रथम
और दशम् मण्डल से कृषि का उल्लेख मिलता है। प्रथम मण्डल में वर्णन
है कि देवताओं ने मनु को हल चलाना और जौ की खेती करना सीखाया। ऋग्वेद
के परवर्ती भाग में जुताई, बुआई, कटाई तथा ओसाई और दवाईयों
का उल्लेख मिलता है। संभवतः इस काल में यव काल में अर्थात् जौ नामक एक ही प्रकार
का अन्न पैदा किया जाता था और जमीन पर कबीले के सदस्यों का समान अधिकार नहीं था।
ऋग्वेद ये जमीन तथा उसकी माप-प्रणाली के बारे में विस्तत वर्णन है, लेकिन कही भी किसी
व्यक्ति द्वारा जमीन की ब्रिकी, हस्तातंरण, गिरवी अथवा दान का उल्लेख
नहीं मिलता। इससे स्पष्ट होता है कि जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिक प्रचलन
नही था।
कृषि सामान्यतः वर्षा पर ही
निर्भर थी परन्तु इस काल में सिंचाई व्यवस्था का विकास हो चुका था। ऋग्वेद
में कुल्या तथा खनितमा आप शधो का उल्लेख मिलता है जो इससे इस बात का संकेत मिलता
है कि कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था का ज्ञान उन्हें था। इसके अतिरिक्त कूपो
द्वारा भी सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख खेतों में हल जोतने के लिए तथा गाडियां
खींचने के लिए बैल उपर्युक्त साधन थे। ऋग्वेद में शिल्प विशेषज्ञों का
अपेक्षाकृत कम उल्लेख हुआ है जबकि चर्मकार, बढ़ई, कुम्हार, धातुकर्मियों तथा
शिल्पीयों का वर्णन मिलता है। शिल्पी कार्यों से जुड़े इन समूहों में से किसी को
भी निम्न स्तर का नही माना जाता था इसका कारण संभवतः यह था कि इनमें से कुछ जैसे:-
बढ़ई, धातुकर्मी, चर्मकार आदि की रथों के
निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो युद्ध में सफलता के लिए उतरदायी होते थे।
ऋग्वेद में वर्णित अयस, धातु विवादग्रस्त है जिसे
तांबे या कांस्य से जोड़ा गया है हांलाकि इसका अर्थ लोहे से भी
लगाया जाता है। यह स्पष्ट है कि वे धातु गलाने की कला से परिचित थे। इस काल में
बुनाई एक घरेलु शिल्प था, जो महिलाओं
द्वारा किया जाता था। इस काल में जुलाहे भी थे तथा कुम्हार के लिए 'कुलान' शब्द का प्रयोग हुआ है।
ऋग्वेद कपास का उल्लेख ना होने से संभवतः ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था।
स्पष्टतः इस काल में हस्तशिल्प छोटे स्तर का था जिसका प्रसार उत्तर वैदिक काल
में बढ़ गया था।
प्रांरभिक काल की
व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इसमें हमें व्यापारियों
द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर व्यापार कर लाभ कमाने के कई संदर्भ मिलते
हैं। व्यापार में मुनाफे के लिए अनेक प्रार्थनाएं और आहुतियां देने के प्रमाण है।
ऋग्वेद से आन्तरिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में होने वाली
समुद्री व्यापार के संदर्भ में विद्वान मानते हैं कि व्यापारी समुद्र तथा समुद्री
व्यापार से अनभिज्ञ थे जबकि मैक्समूलर, जिमर तथा लासेन का मत है कि इन्हें समुद्र का पूरा ज्ञान
था। इस काल में सरस्वती नदी को समुद्र में गिरने वाली बताया गया है।
ऋग्वेद के दसवें मंडल में
पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है तथा इसमें वर्णित भुज्यु की कहानी से हमें
समुद्री व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इस काल के लोगों को न केवल
समुद्री यातायात की जानकारी थी। अपितु उनके दूसरे देश से व्यापारिक सम्बन्ध भी थे।
इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में नाव, चप्पुओं, वाली नावों एवम् हजार
चप्पुओं वाले जहाज का भी वर्णन मिलता है। इन्हें समुद्र में आने वाले ज्वार-भाटे
की भी जानकारी थी।
ऋग्वेद में उल्लेखित बातें इनकी
समुद्री व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। प्रारंभिक वैदिक कालीन चरण में
आर्थिक व्यवस्था विस्तृत पैमाने वाली अर्थव्यवस्था नही थी। कबीलाई
अर्थप्रणाली थी जिसमें विनिमय-प्रणाली कीमती वस्तुओं के आदान-प्रदान पर आधारित थी।
गाय विनिमय की प्रमुख इकाई थी। संभवतः इसके अतिरिक्त भी कई अन्य इकाइयां रही होगी।
इस काल के निष्क का प्रचलन भी व्यापार में होने लगा था।
विद्वानों के
अनुसार प्रारंभ में निष्क उस काल में गले में पहनने वाला सोने का आभूषण
रहा होगा। कई स्थानों पर रूद्र द्वारा निष्क पहनने का संदर्भ मिलता
है। ऋग्वेद में इस बात का भी उल्लेख है कि एक कवि ने अपने राजा से 100
निष्क और 100 घोड़े दान स्वरूप प्राप्त किए। इस काल में पणि वर्ग द्वारा ऋण
लेने और देने की प्रथा का प्रचलन था, जिसकी ऋग्वेद में निन्दा की गई है। लेकिन इस काल की
आर्थिक उन्नति में इनके योगदान को नजरअंदाज नही किया जा सकता। प्रांरभिक चरण में
बलि कर शक्तिशाली वर्ग के लिए स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था हांलाकि शत्रु
समुदायों के लिए यह स्पष्टतः एक उपहार था जो बलपूर्वक वसूल किया जाता था, इसमें पशु तथा अन्न शामिल
थे।
ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक
स्थिति (Religions
Condition of Rigvedic Period)
ऋग्वेद में देव अथवा देवता
शब्द का अनेक बार उल्लेख हुआ है। इस काल के प्रारंभ में 'बहुदेववाद' के दर्शन होते हैं।
ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा की गई है, वे प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक है, जिनका मानवीकरण किया गया
है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया-
(1) पथ्वी के
देवता- पथ्वी अग्नि, सोम, हस्पति तथा नदियों के
देवता,
(2) अंतरिक्ष के
देवता- इन्द्र, रूद्र, वायु, पर्जन्य मातरिश्वन आदि,
(3) धुस्थान
(आकाश) के देवता- द्यौस, वरूण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषन, विष्णु, उषा आदि।
इस काल में
ऋषियों ने जिस देवता की प्रार्थना की है, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें सम्पूर्ण गुणों, ज्ञान और सत्य का आरोपण
कर दिया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक रचनाएं लिखी गई। विद्वान मैसमूलर ने इस
प्रकृति को ‘डीनोथीज्म' कहा है। ऋग्वेद से
प्रसिद्ध देवता निम्न थे। जैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त (250) इन्द्र को
समर्पित है। इन्द्र को पुरंदर (किले को ध्वस्त करने वाला), जितेन्द्र (विजयी), रथयोद्धा, मधवान तथा शांति का देवता
बताया गया है। यह आकाशीय देवता युद्ध, शांति और मौसम का देवता था।
इन्द्र शक्ति का स्वामी था
जिसकी उपासना शत्रुओं को नष्ट करने के लिए की जाती थी। वह बादलों का देवता था, उससे समय-2 पर वर्षा के
लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। बादल और वर्षा शक्ति से संबंधित थे जिसको पुरूष के
रूप में मानवीकरण किया गया और जिसका प्रतिनिधित्व इन्द्र करता था। युद्ध का मुखिया
के रूप में भी इसका उल्लेख है। इन्द्र की स्तुति में ऋग्वेद में लगभग 250 रचनाएं
है। जिसका अभिप्राय है कि इस वेद की सम्पूर्ण रचनाओं का एक चौथाई भाग एकमण
इन्द्र की स्तुति से ही भरा है।
इन्द्र के
पश्चात् सर्वाधिक सूक्त (220) अग्नि को समर्पित हैं यज्ञों के दौरान अग्नि
का विशेष महत्व था। जहां तक कि ऋग्वेद में उसे पुरोहित, यज्ञिय और होता भी कहां
गया है। अग्नि के द्वारा यज्ञ में समर्पित आहुति देवताओं तक पहुंचाई जाती
थी, इसलिए इसे देवताओं का मुख
भी कहां गया है। अग्नि विवाह संस्कार, यज्ञों तथा दाह संस्कार आदि के लिए अनिवार्य थी। ऋग्वेद के
मंत्रों में इसे पिता पथ-प्रदर्शक और मित्र भी कहा गया है।
मित्रावरूण ऋग्वेद में वरूण
का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। वरूण को आकाश, पथ्वी और सूर्य का
निर्माता का गया है। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, नदियां उसी के आदेश से
प्रवाहित होती है। वरूण विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था का भी रक्षक था।
सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वह अनियन्त्रित और स्वेच्छाचारी नहीं है।
सूर्य को अंधकार दूर कर रोशनी
फैलाने वाला माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देवों का अनीक, चर-अचर की आत्मक तथा उनका
मित्र और वरूण एवम् अग्नि का नेत्र था। सवित भी सूर्य का ही एक रूप है, और प्रसिद्ध गायत्री
मंत्र उसी को समर्पित है। सूर्य मनुष्यों के सत्-असत् कर्मो का दष्टा है
तथा वह विश्वकर्मा है।
रूद्र आंधी का प्रतीक है।
ऋग्वेद में रूद्र से महामारी और महाविनाश से दूर रखने के लिए अनेक
प्रार्थनाएं की गई हैं। यह अनेक जड़ी-बूटियों का भी संरक्षण कर्ता था।
ऋग्वेद में अन्य बहुत देवता
थे जैसे सोम, वायु, विष्णु घौस, मरूत। ऋग्वेद में पुरूष
देवताओं के अलावा अनेक देवियों का भी उल्लेख है जैसे: उषा, पृथ्वी, अदिति अरण्यनी, सावित्री, अप्सरा और पुरामाधि आदि।
इनको सम्बोधित करते हुए ऋग्वेद में अनेक प्रार्थनाएं और श्लोक लिखे गए।
ऋग्वैदिक धर्म में बलि और यज्ञों
का विशेष महत्व था जो प्रायः देवताओं की उपासना करने, युद्ध में विजय, पशुओं तथा पुत्र की
प्राप्ती के लिए किए जाते थे। सामान्यतः पुरोहित यज्ञों के सम्पन्न कराते थे। इस
काल में यज्ञों में बलि का विस्तृत उल्लेख है, जिस कारण पुरोहितों के महत्व में वद्धि हुई। बलिदान
अनुष्ठानों के कारण गणित और पशु शरीर संरचना ज्ञान के विकास में भी वद्धि हुई।
यज्ञों के दौरान उसमें घी, दूध चावल और
सोमरस आदि वस्तुओं की आहुति दह जाती थी। इस काल में देवताओं की उपासना किसी अर्मूत
दार्शनिक अवधारणा के कारण नही बल्कि भौतिक लाभों के लिए की जाती थी इस काल
के धर्म में बलिदान या यज्ञों के महत्व में काफी वद्धि हुई।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।
Back To - प्राचीन भारत का इतिहास






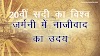







0 Comments