भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक
भारतीय संविधान में
संघवाद
भारतीय संविधान में संघवाद के आधारभूत लक्षणों को निम्न प्रकार
विवेचित किया गया है-
1. शक्तियों का
विभाजन-
संसार के अन्य संघात्मक संविधानों की भाँति भारतीय संविधान द्वारा भी केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-
(क) संघीय सूची- इसमें 97 विषय हैं (वर्तमान में इसमें 99 विषय
हैं, नये दोनों विषय अनुच्छेद 246 में भाग-2 के
अन्तर्गत नये भाग 2-क द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। जिन पर संघीय (केन्द्रीय) सरकार
को कानून बनाने का पूर्ण व एकमात्र अधिकार है। सुरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध तथा शान्ति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बीमा, बैंक, अखिल भारतीय
सेवाएँ, सर्वोच्च न्यायालय, आयकर, सीमा शुल्क आदि प्रमुख संघीय विषय हैं।
(ख) राज्य सूची- इसमें 66 विषय हैं (वर्तमान में 62 विषय हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के चार विषय समवर्ती सूची में
कर दिये गये हैं) जिन पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का पूर्ण एवं एकमात्र
अधिकार है। इस सूची के मुख्य विषय हैं—स्थानीय
स्वशासन, पुलिस, जेल, न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि।
 |
| भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक |
(ग) समवर्ती सूची– इस सूची में 47 विषय हैं
(वर्तमान में इसके विषयों की संख्या 52 है,42वें
संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के चार विषय तथा एक नया विषय समवर्ती सूची में
जोड़ दिया गया) जिन पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों को
है। जिन मुख्य विषयों को इस सूची में रखा गया है, वे हैं-दीवानी
और फौजदारी कानून, दण्ड- विधि, विवाह, तलाक, श्रमिक संघ, कारखाने, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, मूल्य
नियन्त्रण, समाचार पत्र, परिवार नियोजन
आदि।
2. लिखित एवं कठोर
संविधान-
अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान भी लिखित है, जिसमें केन्द्रों और एककों के मध्य स्पष्ट शक्ति-विभाजन किया गया है। इसमें 25
भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 3 परिशिष्ट
हैं। भारतीय संविधान यद्यपि अमरीकी संविधान जितना तो कठोर नहीं है, फिर भी इसमें संवैधानिक कानून तथा साधारण कानून में अन्तर किया गया है।
संविधान में संशोधन संविधान में वर्णित पद्धति के आधार पर ही किया जा सकता है। संविधान
द्वारा किये गये शक्ति विभाजन में संघीय सरकार या राज्य सरकारों में से किसी एक के
द्वारा ही अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वरन् इन प्रावधानों में
परिवर्तन दोनों की सहमति से ही सम्भव है।
3. संविधान की
सर्वोच्चता-
भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान समस्त देश में
बाध्यकारी है और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता
है। संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया
जा सकता और भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और
अन्य पदाधिकारियों को संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेनी पड़ती है। केन्द्र
तथा राज्य सरकारें दोनों ही सीधी संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं।
लेकिन जब कभी दोनों में से कोई एक या दोनों ही सांविधानिक उपबन्धों की उल्लंघना
करके या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कानून बनाते हैं या कार्यपालिका आदेश देती
है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर रद्द कर सकती है।
4. उच्च सदन राज्यों
का सदन' होना-
भारतीय संसद का उच्च सदन (राज्य सभा) राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान
के उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण
संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है।
5. स्वतन्त्र उच्चतम
न्यायालय-
भारतीय संविधान भी अन्य संघीय संविधानों की तरह सर्वोच्च न्यायालय
(सुप्रीम कोर्ट) के रूप में एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना करता
है। यह न केवल नागरिक अधिकारों की कार्यपालिका अथवा विधायी निरंकुशता से रक्षा
करता है, वरन् केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक विवादों
का निपटारा भी करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन
का अधिकार है। वह किसी भी कार्यपालिका के आदेश या व्यवस्थापिका के कानून को अवैध
घोषित कर सकता है यदि वे संवैधानिक उपबन्धों के विपरीत है।
न्यायालय की यह व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतः अनुकूल है। डॉ. के. वी. राव
के अनुसार, "इस दृष्टि से हमारा
संविधान सोवियत रूस या स्विट्जरलैण्ड के संविधान से अधिक संघात्मक
है।"
6. दोहरी शासन
व्यवस्था-
संघात्मक व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों में अलग-अलग सरकारें पायी जाती हैं, भारत में भी यही व्यवस्था है। केन्द्र और राज्य सरकार संविधान के आधार पर
अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करती हैं।
भारतीय संविधान के
एकात्मक तत्त्व
भारतीय संविधान के एकात्मक तत्त्व : संविधान द्वारा शक्तिशाली केन्द्र की
स्थापना
1. शक्तियों का बँटवारा
केन्द्र के पक्ष में-
भारत के संविधान में शक्तियों का बँटवारा इस प्रकार किया गया है कि
केन्द्र को राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। संघ सूची में
97 विषय रखे गये हैं तथा इन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, राज्य के विधान मण्डल नहीं। समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गये हैं, जिन पर केन्द्र और राज्यों के विधान मण्डल दोनों कानून बना सकते हैं, परन्तु यदि दोनों के बनाये गये कानूनों में कोई विरोध हो जाये, तो केन्द्र का कानून ही मान्य होगा और विरोध की स्थिति की सीमा तक राज्य का
कानून रद्द हो जायेगा। इस प्रकार राज्य के विधान मण्डल समवर्ती सूची पर
केन्द्र की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकते।
जहाँ तक राज्य सूची का सम्बन्ध है, इसमें दिये गये
विषयों पर राज्य के विधान मण्डलों को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद इन पर भी कानून बना सकती है।
इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को ही दी गई हैं। इस प्रकार भारत संघ में
केन्द्र बहुत शक्तिशाली बन गया है।
2. संघ और राज्यों
के लिए एक ही संविधान-
साधारणतः संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों के संविधान संघ
के संविधान से पृथक् होते हैं, किन्तु भारत
में संघ के संविधान के साथ-साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। भारतीय
संघ के एककों को संयुक्त राज्य अमेरिका के एककों की भाँति अपना
पृथक् संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। भारत में संघ तथा इकाइयाँ दोनों के
संविधान का निर्माण एक ही संविधान सभा द्वारा किया गया है और दोनों की संशोधन
पद्धति भी समान है।
3. इकहरी नागरिकता-
संघात्मक सरकारों में प्रायः दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अमेरिकन
अपने राज्य का नागरिक भी होता है तथा सम्पूर्ण देश का नागरिक भी। भारतीय संविधान
में सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है।
प्रत्येक भारतीय को सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वह किसी भी राज्य का नागरिक क्यों न हो। इकहरी नागरिकता की यह व्यवस्था
संघात्मक शासन के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है।
4. संसद को राज्यों
के पुनर्गठन आदि का अधिकार-
अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, उनके क्षेत्र को कम या अधिक कर सकती है, उनके नाम बदल
सकती है, दो राज्यों को मिला सकती है और एक राज्य को दो
राज्यों में परिवर्तित कर सकती है। किसी संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा बढ़ाकर उसे
राज्य का दर्जा दे सकती है। उदाहरणार्थ, 1 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवम्बर, 2000 को
झारखण्ड और 15 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड एवं 1 जून, 2014 को तेलंगाना चार नये राज्यों का निर्माण हुआ। इस तरह 2019 तक भारत संघ
में कुल 29 राज्य और 7 संघ-राज्य क्षेत्र हैं।
5. एकीकृत न्याय
व्यवस्था-
अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में संघीय तथा राज्यों के न्यायालय पृथक्-पृथक् होते
हैं, परन्तु भारत में इकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था
की गई है, यह सारे देश में एक जैसी है। सर्वोच्च न्यायालय
सबसे ऊपर है। वह राज्यों के उच्च न्यायालयों की अपील सुनता है।
6. राज्यों का राज्य
सभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं-
यद्यपि भारतीय संघ के उच्च सदन, राज्य सभा में
इकाइयों (राज्यों) को प्रतिनिधित्व दिया गया है और राज्य के विधान मण्डलों द्वारा
ही उसके सदस्यों का निर्वाचन होता है, फिर भी अमेरिका
या स्विट्जरलैण्ड की भाँति उनको समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। भारत का
प्रत्येक राज्य जनसंख्या के आधार पर राज्य सभा में प्रतिनिधि भेजता है। चौथी
अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या 1 से
34 के बीच है।
7. मौलिक बातों में
एकरूपता-
सारे देश के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की एक जैसी व्यवस्था, इकहरी न्यायपालिका, सभी राज्यों के लिए प्रशासनिक एकरूपता, एक ही नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की व्यवस्था, एकल निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिससे राज्यों
की स्वायत्तता प्रभावित होती है।
8. राज्यों की
दुर्बल आर्थिक स्थिति-
वित्तीय क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हें संविधान
के आधार पर केन्द्र पर निर्भर बनाया गया है अर्थात् आर्थिक संकट के समय वे हमेशा
केन्द्र के सामने हाथ फैलाते नजर आते हैं। बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के राज्यों की
स्वायत्तता नाममात्र की रह जाती है।
9. राष्ट्रपति
द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति-
भारतीय संघ में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति
द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की कृपा बने रहने तक ही अपने पद पर
विद्यमान रहता है और उसी के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। राज्यपाल
केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से राज्यपालों के माध्यम
से केन्द्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियन्त्रण रहता है।
राज्यपाल की नियुक्ति किये जाने की यह विधि संघात्मक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।
10. केन्द्र की
संकटकालीन शक्तियाँ-
भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई
हैं-
(i) अनुच्छेद 352 के अनुसार
विदेशी आक्रमण एवं आन्तरिक विद्रोह की आशंका पर
(ii) अनुच्छेद 356 के अनुसार, राज्य में संवैधानिक विफलता के समय
(iii), अनुच्छेद 360 के अनुसार
वित्तीय संकट के समय।
इन तीनों आपातकालीन घोषणाओं के परिणामस्वरूप संघीय व्यवस्था एकात्मक
रूप ग्रहण कर लेती है।
11. अखिल भारतीय
सेवाएँ-
अखिल भारतीय सेवाएँ (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.सी.एस. आदि) केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। राज्य के उच्च पदों, जैसे जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, सचिवालयों के सचिव आदि पर इन्हीं अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। यद्यपि ये उच्च पदाधिकारी राज्य सेवाओं में रहते हैं तथा राज्य के राजस्व से ही अपने वेतन, भत्ते आदि प्राप्त करते हैं, फिर भी नियन्त्रण उन पर केन्द्रीय सरकार का होता है। उन पर यदि राज्य सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही करना चाहे, तो केन्द्रीय सरकार और संघीय लोक सेवा आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रकार इन उच्च पदाधिकारियों के माध्यम से केन्द्र राज्यों पर नियन्त्रण रखता है।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।
Back To - भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था




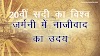










0 Comments