भारतीय संसद की शक्तियाँ
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-79 में उल्लेख किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों को मिलाकर बनेगी। ये दो सदन हैं- राज्य सभा एवं लोकसभा।
संसद भारतीय प्रशासन की धुरी
है जिस पर सरकार का सारा यन्त्र जाल घूमता है। भारतीय संसद की शक्तियों का
विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है-
1. व्यवस्थापन
सम्बन्धी शक्तियाँ-
संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती
सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह संकटकाल के
उद्घोषणा के समय में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है तथा जब कभी
दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी विषय
के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकती है। इसी
प्रकार जब राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित
में संसद को राज्य-सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद
कानून बना सकती है।
 |
| भारतीय संसद की शक्तियाँ व सीमाएँ |
2. कार्यपालिका
शक्तियाँ-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के
अनुसार मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल
केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है।
संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य 'अविश्वास
के प्रस्ताव',
निन्दा प्रस्ताव' एवं 'काम
रोको' द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाये रखते हैं। संसद के
सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के सम्बन्ध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ
सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार
करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं।
3. वित्तीय शक्तियाँ-
संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त
पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। सभी कर सम्बन्धी प्रस्ताव तथा अनुदानों की माँगें
संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं। क्योंकि संविधान के
अनुसार 'विधि के अधिकार' के
बिना न तो कर लगाया जाएगा और न एकत्रित किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और
लोक-लेखा समिति को नियुक्त करती है तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन पर
विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को
राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है।
4. संविधान संशोधन
से सम्बन्धित शक्तियाँ-
संविधान के अनुच्छेद 368(1) के
अनुसार संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है।
संशोधन सम्बन्धी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। परन्तु कुछ
विषयों पर आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति भी आवश्यक है।
5. राज्यों से
सम्बन्धित शक्तियाँ-
संसद को संविधान द्वारा यह अधिकार
प्राप्त है कि वह राज्यों की इच्छा के बिना भी उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन
कर सकती है, नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती
है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है।
6. संविधान की
न्यायिक शक्तियाँ-
भारतीय संसद को न्यायिक शक्तियाँ
भी प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति
पर महाभियोग लगाने के समय एक न्याय-संस्था के रूप में कार्य करती है। इसके
अतिरिक्त संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण
तथा प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त है।
7. निर्वाचन
सम्बन्धी शक्तियाँ-
संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार
संसद को कुछ निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मण्डल के अंश
हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार, संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का
निर्वाचन करते हैं।
8. जनता की शिकायतों
का निवारण-
लोक सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि
हैं। उनका कर्त्तव्य है- जनता की शिकायत को सरकार तक पहुँचाना। विरोधी दल इस कार्य
को पूरा करते हैं। वार्षिक बजट, राष्ट्रपति का भाषण तथा अन्य मामलों में
विरोधी दल के सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं। संसद को व्यय के आकलनों, विनियोजन
तथा राजस्व विधेयकों पर विचार-विमर्श के समय राज्य के विभिन्न विभागों के कार्य की
समीक्षा और आलोचना करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार की अलोचना तथा समीक्षा
द्वारा सदन के सदस्य अपनी शिकायतों को दूर करवा सकते हैं।
9. अनुमोदन सम्बन्धी
शक्तियाँ-
संसद को अनुमोदन की शक्तियाँ भी
प्राप्त हैं। सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न संवैधानिक प्रस्तवों पर संसद का अनुमोदन
आवश्यक होता है। उदाहरण- अनुच्छेद 356 तथा 360 के अधीन की गई आपातकाल की घोषणा
जारी होने की तिथि के 2 मास के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया
जाना आवश्यक है अन्यथा ये घोषणाएँ निरस्त मानी जायेंगी।
भारतीय संसद की सीमाएँ
भारतीय संसद की सम्प्रभुता को
मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्त्व सीमित करते हैं-
1. संविधान का
संघात्मक स्वरूप-
भारतीय संविधान का संघीय ढाँचा भी
संसद की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान के भाग-II एवं
7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
किया गया है,
जिसमें मुख्यतः राज्य सूची के विषयों के सम्बन्ध में संसद
की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो जाती है। प्रो. टी. के. टोपे ने लिखा है कि
"भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अन्तर्गत विधायिका है। ब्रिटिश संसद
के समान इसकी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं।"
2. लिखित एवं कठोर
संविधान-
भारतीय संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है।
संविधान के अनुसार संसद संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारत
के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
केशवानन्द भारती के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर कि भारतीय
संसद संविधान के उन अंशों में परिवर्तन नहीं कर सकती, जो
संविधान के मूलभूत ढाँचे से सम्बन्धित हैं, संसद की सर्वोच्चता को सीमित
कर दिया है।
3. मूल अधिकार-
संविधान के अध्याय 3 में उल्लिखित मूल
अधिकार भी कानून निर्माण की शक्ति पर मर्यादायें लगाते हैं। अनुच्छेद 13(2) के
अनुसार, यदि संसद का कोई कानून नागरिकों के मूल अधिकारों की उल्लंघना करता है, तो
वह उस सीमा तक अवैध है जिस सीमा तक वह उसका उल्लंघन करता है। यह सत्य है कि संसद
संवैधानिक संशोधनों द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, परन्तु
इसकी प्रक्रिया कठोर व जटिल है विशेषकर उन परिस्थितियों में जब संसद
में किसी एक दल का पूर्ण बहुमत न हो क्योंकि तब संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत को
प्राप्त करना कठिन होगा।
4. न्यायिक पुनरावलोकन
की व्यवस्था-
न्यायिक पुनरावलोकन का
तात्पर्य संविधान की सर्वोच्चता और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी सर्वोच्चता की
रक्षा करने की व्यवस्था से है। भारतीय संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के
लिए उनकी शक्तियों के सम्बन्ध में कुछ सीमायें निश्चित कर दी हैं और न्यायालय को
उन संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा
के लिए न्यायालय सतर्क पहरेदार की तरह विद्यमान है।
न्यायिक पुनरावलोकन की
व्यवस्था के तहत संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायपालिका द्वारा जाँच की जाती है
और यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी कानून से संविधान
का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है।
5. राष्ट्रपति का
निषेधाधिकार-
संसद द्वारा पारित विधेयक तभी लागू
हो सकते हैं,
जब राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर दे। राष्ट्रपति
चाहे तो कानूनों को अस्वीकार कर सकते हैं या चाहे तो उन्हें पुनर्विचार के लिए
वापस लौटा सकते हैं । यद्यपि भारतीय राष्ट्रपति के पास अमरीकी राष्ट्रपति
की तरह 'जेबी निषेधाधिकार'
नहीं है, फिर भी भारतीय संवधिान में इस बात का कोई
उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय तक किसी विधेयक को अपने पास रोककर रख सकता
है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक पर अनावश्यक देरी कर सकता है।
6. जनमत-
जनमत भी संसद की शक्तियों पर एक महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्ध है।
संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती, जिसे जनता पसन्द न करे। संसद को अन्तर्राष्ट्रीय
कानून का समुचित सम्मान करना पड़ता है।
7. दलीय अनुशासन और
नियन्त्रण-
वर्तमान समय में दलीय अनुशासन और नियन्त्रण
इतना कठोर हो गया है कि कोई सदस्य दलीय आदेशों और निर्देशों की अवहेलना कर अपने
राजनीतिक जीवन को खतरे में नहीं डालता । मन्त्रिमण्डल ही गृह व विदेश नीतियों तथा
सामाजिक और आर्थिक नीतियों को निर्धारित करता है और उसकी इच्छा के बिना न कोई
कानून पास हो सकता है न किसी कानून में संशोधन।
यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत या पुनर्विचार के लिए भेजे गये विधेयकों को यदि संसद उन्हें दुबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजे, तो पुन: वीटों के प्रयोग का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, फिर भी यह तथ्य ही संसदात्मक सर्वोच्चता की मर्यादा है कि राष्ट्रपति के पास एक बार वीटो का अधिकार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का निषेधाधिकार संसद की सर्वोच्चता पर अंकुश लगाता है।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।
Back To - भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था





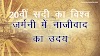









0 Comments