राज्यपाल
राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए की जाती है लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है।
राज्यपाल की शक्तियाँ
राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता
है-
1. कार्यपालिका
शक्तियाँ-
राज्य की कार्यपालिका
शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा
सम्पादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर
अन्य मंत्रियों की। वह महाधिवक्ता, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा
इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
नियुक्ति के सम्बन्ध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की
कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित हैं। समवर्ती
सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अन्तर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग
करता है। राज्य सरकार के कार्य के सम्बन्ध में वह नियमों का निर्माण करता है । वह मंत्रियों
के बीच कार्यों का वितरण भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की
सूचना माँगने का अधिकार है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्यपाल
को मंत्रिमण्डल के सभी निर्णयों से अवगत कराये। वह मुख्यमंत्री को
किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के समक्ष विचार के लिए
रख सकता है।
 |
| राज्यपाल की शक्तियाँ, भूमिका एवं स्थिति |
2. विधायी शक्तियाँ-
राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक
अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित
करता है और स्थगित करता है और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन
को विघटित भी कर सकता है। महानिर्वाचन के बाद विधानमण्डल की पहली
बैठक में वह एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के सम्बन्ध में सन्देश भेज सकता है।
राज्य विधान मण्डल
द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर
सकता या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमण्डल को लौटा सकता है। अगर विधानमण्डल
दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी।
वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है।
उदाहरण के लिए,
वे विधेयक जो सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से हस्तगत
करने या उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी से सम्बन्धित हों, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित किये जा
सकते हैं।
वह राज्य विधान परिषद् के सदस्यों को ऐसे
लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता
आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यावहारिक ज्ञान हो। अगर वह ऐसा
समझे कि विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय को उचित
प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के कुछ सदस्यों की मनोनीत कर सकता
है। इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त
हैं।
3. वित्तीय
शक्तियाँ-
राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ
भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना
कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह व्यवस्थापिका
के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है तथा उसकी सिफारिश के बिना कोई भी
अनुदान की माँग नहीं कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही
अधिकार में रहती है तथा विधानमण्डल स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से
किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है।
4. न्यायिक
शक्तियाँ-
संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, "जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन
विषयों से सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाल
कम कर सकता है,
स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर
सकता है।"
5. विविध शक्तियाँ-
राज्यपाल को विधिक शक्तियाँ भी प्राप्त
हैं-
(1) वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य
की आय व्यय के सम्बन्ध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और
उन्हें विधानमण्डल के समक्ष रखता है।
(2) अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार
चलना सम्भव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की
विफलता के सम्बन्ध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के
अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केन्द्रीय मंत्रिमण्डल
द्वारा की जा सकती है। उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता
है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अन्दर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप
में कार्य करता है।
(3) अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल राज्य विधानमण्डल
द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखने से सम्बन्धित कार्य
को अपने विवेकानुसार कर सकता है।
(4) राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते
केन्द्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों
की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा भी सकता है।
राज्यपाल की भूमिका एवं स्थिति
राज्यपाल की स्थिति तथा
भूमिका के बारे में सामान्य तौर पर दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित रहे
हैं। इनमें से प्रथम में राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना
गया है और दूसरे में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्यपाल की भूमिका एवं
संवैधानिक अध्यक्ष से कहीं अधिक है, यथा-
1. राज्यपाल
संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में-
हमारे संविधान में कहा गया है कि सरकार की समस्त
शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं और मन्त्रिपरिषद् का कार्य इसको
शासन में सहायता तथा परामर्श देना है। इस प्रकार राज्यपाल एक संवैधानिक
शासक है और राज्य का सम्पूर्ण शासन उसके नाम पर चलाया जाता है। संवैधानिक
रूप से राज्यपाल को जितनी भी शक्तियाँ प्राप्त हैं; वह उनका प्रयोग राज्य
की मन्त्रिपरिषद् के माध्यम से करता है। संविधान राज्यपाल की
स्वविवेक की शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। केवल असम तथा नागालैण्ड
के राज्यपाल को ही इस प्रकार की स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस प्रकार कहा
जा सकता है कि साधारणतया राज्यपाल राज्य का वैधानिक या नाममात्र का अध्यक्ष ही है।
डॉ. अम्बेडकर, ए.के. अय्यर आदि विद्वानों ने भी इस विचार का समर्थन किया है कि राज्यपाल केवल एक
संवैधानिक अध्यक्ष ही है। राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके विभिन्न
व्यक्तियों, जैसे-सरोजनी नायडू,
श्री प्रकाश, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
आदि ने भी राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष कहा है जिसे
अपने सभी कार्य मन्त्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार करने होते है।
2. राज्यपाल
संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक अर्थात् संविधान के रक्षक की भूमिका-
कुछ विचारकों का मानना है कि राज्यपाल मात्र
संवैधानिक अध्यक्ष ही नहीं है, वरन् इससे अधिक भी कुछ है। इस विचार को
निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत व्यक्त किया जा सकता है-
(1)
राज्यपाल का राज्य शासन में स्थान- राज्य शासन में राज्यपाल
की शक्तियाँ वास्तविक नहीं हैं, लेकिन उसका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और
प्रतिष्ठित होता है। वह दलगत राजनीति के ऊपर होने के कारण सत्तारूढ़ और विरोधी
दोनों दलों का विश्वासपात्र होता है। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल
राज्य के शासन की ढुलमुल और अस्थायी राजनीति में स्थायित्व और स्थिरता लाने की
स्थिति में होता है। वह विरोधी पक्ष और मन्त्रिमण्डल के मध्य अनेक मतभेदों को दूर
करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। राज्य शासन को सुगम, सुचारू
और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल का बहुत अधिक महत्त्व होता है।
(2)
संविधान सभा का दृष्टिकोण- संविधान सभा के वाद-विवाद के
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का यह दृष्टिकोण था
कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में
कार्य करेगा,
परन्तु विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका संवैधानिक
अध्यक्ष से अधिक की हो सकती है।
(3)
राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य- राज्यपाल के निम्नलिखित
स्वविवेकी कार्यों के कारण वह संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक है।
(अ) मुख्यमन्त्री की नियुक्ति- भारतीय संविधान की
धारा 164 (1) के अनुसार राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद
164 (2) के अनुसार मन्त्रिमण्डल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता
है। यदि राज्य विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं होती या बहुमत दल के नेता पद
के लिए एक से अधिक दावेदार होते हैं तो इस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से कार्य
कर सकता है। समय-समय पर 1967 के पश्चात् से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती रही हैं और
राज्यपालों ने ऐसी स्थितियों में अपने स्व-विवेक की शक्ति का उपयोग किया है जिसका
कई बार दुरुपयोग भी हुआ है और विवाद उत्पन्न होते रहे हैं।
(ब) मन्त्रिमण्डल को भंग करना- राज्यपाल को यह
अधिकार प्राप्त है कि वह मन्त्रिपरिषद् को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि
वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये। इस बारे में निम्न विभिन्न परिस्थितियों
में राज्यपाल ने अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर
राष्ट्रपति से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। ये सभी निर्णय
राज्यपाल की आलोचना के कारण भी बने हैं।
(स) विधानसभा का अधिवेशन बुलाना- असाधारण परिस्थितियों
में राज्यपाल बिना मुख्यमन्त्री के परामर्श के विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है।
डॉ. एल. एम. सिंघवी के शब्दों में, "मन्त्रिमण्डल के बहुमत
की जाँच करना वह (राज्यपाल) अपना ऐसा स्वविवेक अधिकार समझ सकता है जिसके लिए वह
मन्त्रिमण्डल के परामर्श के विरुद्ध अपनी इच्छानुसार विधानसभा का अधिवेशन बुला
सकता है।" इस सम्बन्ध में सिवाच महोदय का मत है कि "जब तक मुख्यमन्त्री को
विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राज्यपाल को मुख्यमन्त्री के परामर्श पर ही
विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिए। लेकिन ज्यों ही उसके बहुमत पर सन्देह होता है
और वह विधानसभा का सामना करने से कतराता है और किसी बहाने अधिवेशन बुलाने के लिए
टालमटोल करता है या अनावश्यक देरी करता है तो राज्यपाल को विधानसभा के अधिवेशन
बुलाने और सदन के पटल पर शक्ति परीक्षण का अधिकार है।"
(द) विधानसभा को भंग करना- विशेष परिस्थितियों में
राज्यपाल विधान सभा को भंग करने के मुख्यमन्त्री के परामर्श को मानने से इन्कार कर
सकता है, अथवा मुख्यमन्त्री के परामर्श के बिना ही विधान सभा को भंग करने की सिफारिश
केन्द्र सरकार को कर सकता है। राज्यपालों ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग अनेक बार
केन्द्र सरकार के इशारों पर कर इसका दुरुपयोग किया तथा केन्द्र सरकार ने इसके आधार
पर विपक्षी दलों की सरकारों को अपदस्थ कर राष्ट्रपति शासन लगाया और विधानसभाओं को
भंग कर दिया।
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि चाहे हमारे संविधान
निर्माताओं का मुख्य प्रयोजन राज्यपाल को एक सांविधानिक प्रमुख ही बनाने का
था तथापि उसे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वास्तविक शासक के रूप में भी कार्य करना
पड़ता है।
3. राज्यपाल
केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में-
राज्यपाल राज्य में केन्द्र सरकार के
प्रतिनिधि के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल की नियुक्ति
तथा विमुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, जिसका वास्तविक अर्थ है कि राज्यपाल
की नियुक्ति तथा विमुक्ति प्रधानमन्त्री व मन्त्रिपरिषद् के हाथ में है।
केन्द्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति चाहे तो समय से पूर्व राज्यपाल
को पद से विमुख कर सकता है आदि। परन्तु राज्यपाल को राज्य विधान मण्डल महाभियोग
द्वारा अपदस्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर राष्ट्रपति के
माध्यम से केन्द्र सरकार का नियन्त्रण रहता है।
केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल अग्रलिखित
भूमिकाएँ निभाता है-
(1)
भारतीय संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य
सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
(2)
केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल
का यह कर्त्तव्य है कि यदि राज्य में कोई सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर
रही है तो राज्यपाल द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के
लिए राष्ट्रपति को पोर्ट भेजना। राष्ट्रपति इस प्रकार की रिपोर्ट स्वविवेक से
भेजता है।
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति
राज्यपाल को जो भी प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय कार्य सौंपे, राज्यपाल
उन सबको पूरा करता है और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन
का संचालन करता है।
(3)
केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक
अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य है कि राज्य के कार्य के सम्बन्ध में समय-समय पर
राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। इसमें उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिये जाते
हैं।
(4)
राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत
राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किये गये किसी विधेयक को राष्ट्रपति की
स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरणार्थ, सम्पत्ति के अनिवार्य
अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने सम्बन्धी विधेयकों को राज्यपाल
राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
(5)
अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी
करने का अधिकार दिया गया है, किन्तु उसे कुछ विषयों के सम्बन्ध में
अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है।
राज्यपाल पद के संस्थाकरण के लिए सुझाव
राज्यपाल पद के संस्थाकरण के सम्बन्ध
में सहाय समिति,
सरकारिया आयोग व अन्य विद्वानों ने जो सुझाव दिये हैं, उनमें
प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं-
1. राज्यपाल की
नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव-
राज्यपाल की नियुक्ति
के समय मुख्यमन्त्री से परामर्श लेने की परम्परा को विकसित किया जाये। दूसरे, ऐसे
व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाये जो दलगत राजनीति से परे हो और जिसे
सार्वजनिक सेवा का काफी अनुभव हो। दल से सम्बन्धित राजनीतिज्ञों, हारे
हुए नेताओं आदि को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाये। दूसरे, राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमन्त्री नहीं बनाना चाहिए, जिसे
चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया हो। राज्यपाल पद पर केवल
उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये जो राजनीतिज्ञ तो हों, लेकिन
दलगत राजनीति से न्यूनतम 5 वर्षों से उनका कोई सम्बन्ध न हो।
2. विधानसभा भंग
करने सम्बन्धी सुझाव–
यदि विधानसभा में मुख्यमन्त्री की हार हो जाए तथा
स्पष्ट वैकल्पिक सरकार बनाने की सम्भावना न हो तथा हारा हुआ मुख्यमन्त्री
विधानसभा को भंग करने का परामर्श दे तो उसे मान लेना चाहिए।
3. राज्यपाल द्वारा
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव-
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करते समय
विवादास्पद या सन्देहास्पद बहुमत का प्रश्न सामान्य रूप से विधानसभा के पटल पर ही
निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकानुसार जिस
व्यक्ति के पक्ष में बहुमत समझता है, उसको मुख्यमन्त्री इस
शर्त के साथ बनाना चाहिए कि वह एक निर्धारित छोटी अवधि में विधानसभा में अपने
बहुमत को स्पष्ट करे। यदि विधानसभा का विश्वास प्राप्त करने के विषय में कोई मुख्यमन्त्री
विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के उत्तरदायित्व को नहीं निभाता तो राज्यपाल द्वारा
उसे पदच्युत कर देना चाहिए।
4. गठबन्धन सरकार
में किसी सहयोगी दल के असहयोग की स्थिति-
यदि गठबन्धन सरकार का कोई भागीदार दल का मन्त्री
मुख्यमन्त्री से मतभेद हो जाने के कारण मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे देता
है तो मुख्यमन्त्री के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, परन्तु
यदि इससे विधानसभा में उसके बहुमत पर सन्देह होता है तो राज्यपाल को यह
चाहिए कि वह मुख्यमन्त्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अतिशीघ्र अपने बहुमत को
स्पष्ट करने को कहे।
5. अन्य-
(1) किसी सरकार के विधायिका में विश्वास मत हासिल कर
लेने के बाद ही राज्यपाल को भाषण देना चाहिए। संविदा में संविद के मुख्यमन्त्री
को सम्बद्ध दलों तथा गुटों के द्वारा औपचारिक रूप से चुना जाना चाहिए।
(2)
राज्यपाल पद धारण करने वाले व्यक्ति
पर संविधान संशोधन द्वारा इस तरह के प्रतिबन्ध अधिरोपित किये जाएँ जिनके तहत वह राज्यपाल
से निवृत्त होने के बाद पुनः प्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन के द्वारा राजनीतिक रूप
से सक्रिय न हो सके और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद को छोड़कर
अन्य कोई पद धारण न कर सके।
(3)
केन्द्र में सरकार बदलने के साथ ही अधिकांश राज्यपाल
बदले जाने की परम्परा प्रतिबन्धित हो।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई
होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।
Back To - भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था












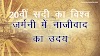


0 Comments