आहड़ सभ्यता की खोज
उदयपुर नगर से दो-तीन मील दूर आहड़ एक कस्बा है जिसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। यह संस्कृति आज खण्डहरों के ढेर में दबी पड़ी है। यह ढेर लगभग 1600 फुट लम्बा व 550 फुट चौड़ा है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है जिससे यहाँ ताँबे के औजारों के बनने का केन्द्र प्रभावित होता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं।
आहड़ सभ्यता के मुख्य उत्खननकर्ता एच. डी. सांकलिया थे, जिन्होंने 1956 में
उत्खनन कार्य का नेतृत्व किया था। इससे पहले, 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास ने इस स्थल की खोज की थी, और 1954 में रतनचन्द्र
अग्रवाल ने उत्खनन कार्य शुरू किया था।
अभी तक की गयी खुदाई से यह प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उत्खनन में यहाँ की
बस्तियों के कई स्तर मिले हैं।
पहले स्तर में कई मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के
टुकड़े तथा पत्थर के ढेर मिले हैं।
दूसरे स्तर की बस्ती जो कि प्रथम स्तर पर ही बसी थी।
कुछ फूटकर तैयार की गयो दीवारें और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले
हैं।
तीसरी बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रभावित होता है।
चौथी बस्ती के स्तर से एक बर्तन से दो ताँबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं जो कि बड़े महत्त्व की हैं।
इन चार स्तर पर चार और स्तर मिलते हैं। जिनमें मकान बनाने की पद्धति, बर्तन की विधि आदि में
अन्तर देखने को मिलता है। ये सभी स्तर एक-दूसरे पर बनते-बिगड़ते चले गये। डॉ. दशरथ शर्मा का मानना है कि आहड़ का जटिल और समन्वित
नागरिक जीवन निस्सन्देह शताब्दियों के विकास का परिणाम है। सभ्यता के
विध्वंस के सम्बन्ध में डॉ. गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि भूकम्प
आहड़ नदी के प्रवाह या बाढ़ आक्रमण आदि कोई भी नगर के विनाश का कारण हो सकता
है।
 |
| आहड़ सभ्यता की खोज तथा प्रमुख विशेषताएँ |
आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ
(1) निवास स्थान-
यहाँ के टीलों को देखने से लगता है कि यहाँ पहले काफी बड़ा समृद्ध नगर रहा होगा। यह नगर पास को आहड़ नदी के तट पर बसा था। आहड़ वासी पत्थर व
धूप में सुखाई गई ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे। मुलायम काले
पत्थरों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। मकान छोटे व
बड़े दोनों ही प्रकार के थे, बड़े कमरों की लम्बाई-चौड़ाई 33x20 फीट तक देखी गयी है। कमरों में बांस की परदी बनाकर उन्हें छोटा किया गया था।
दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था। फर्श को भी मिट्टी से लीपा जाता
था।
फर्श बनाने के लिये ये लोग काली मिट्टी के साथ-साथ
नदी की बजरी को भी मिला देते थे। छत बाँस की बनायी जाती थी जिन्हें बल्लियों पर
रखा जाता था और बल्लियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। मकानों से गन्दा पानी
निकालने की वैज्ञानिक विधि से भी ये लोग परिचित थे। 15-20 फुट तक गड्ढे खोद
दिये जाते थे जिनमें गन्दा पानी गिरता रहता था। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और
कुछ मकानों में तो 6 चूल्हे तक मिलते हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि आहड़
में बड़े परिवारों के लिये भोजन व्यवस्था थो अथवा सामूहिक भोजन भी बनाया जाता था।
(2) मृदभाण्ड व बर्तन-
उत्खनन में प्राप्त सामग्री में सर्वाधिक संख्या मृदभाण्डों की है। लाल
काले रंग के मृदभाण्डों से यह पता चलता है कि लगभग तीन या चार हजार वर्ष
पहले आहर सभ्यता के अन्तिम चरण में सिन्धु सभ्यता का मेवाड़ में प्रवेश
हुआ। लाल-काले धरातल वाले चमकोले पात्र अन्दर से सम्पूर्ण काले रंग के व बाहर से
ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे सम्पूर्ण लाल रंग के हैं। ऐसे पात्र तीन
प्रकार के हैं। प्रथम सादे, जिन पर किसी प्रकार की डिजाइन नहीं है, दूसरे जिन पर अन्दर व बाहर की ओर हल्की डिजाइन बनी हुयी है
और तीसरे प्रकार में बाहर की ओर गर्दन पर सफेद रंग में कई प्रकार की लाइनें व
बिन्दु बने हुये हैं।
साधारणतः मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाये जाते थे लेकिन इन्हें चाक से भी बनाया
जाता था। इस सम्बन्ध में डॉ. गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि यह सामग्री अपनी
विविधता व प्रचुरता के विचार से बड़े महत्त्व की है। खुदाई में अनाज रखने के लिये
बड़े मृद भाण्ड भी पाये गये हैं जिन्हें यहाँ कोयोलचाल की भाषा में गोरे व कोठ भी
कहा जाता था। यहाँ प्राप्त बर्तनों के विभिन्न प्रकारों से इस बात का संकेत मिलता
है कि 2000-1000 ई.पू. तक आहड़वासियों का ईरान से भी सम्बन्ध था।
(3) मुद्राएँ, मुहरें व उपकरण-
आहड़ की खुदाई में छ: ताम्बे की मुद्रायें व तीन मुहरें प्राप्त हुयी है। एक
मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है, दूसरी में अपोलो खड़ा है व तीसरी पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। लिपि के
आधार पर इसका काल दूसरी शताब्दी ई.पू. माना गया है।
अनुमान लगाया जातात है कि वे पत्थरों से अपने औजार बनाया करते थे जिनका प्रयोग
काटने, छीलने या छेद करने में
किया जाता था क्योंकि इनके किनारे काफी धारदार दिखाई देते हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं
के अनुसार उस काल में यह स्थान ताँबे की वस्तुओं को बनाने का केन्द्र रहा होगा और
ताम्र उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग रहा होगा। इनके अतिरिक्त यहाँ से 79 लोहे के उपकरण
भी मिले हैं जिनका उपयोग चाकू, कुल्हाड़ी व कोल की तरह होता था अर्थात् यहाँ लौह संस्कृति का भी प्रवेश हो
चुका था।
(4) मणियाँ व आभूषण-
आहड़वासी कीमती पत्थरों से गोल मणिएँ भी बनाते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा
ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिये भी किया जाता था तथा इनके ऊपर सजावट व अलंकरण
का कार्य भी किया जाता था। इनका आकार गोल, चपटे, चतुष्कोणीय व षट्कोणीय होता था। खुदाई में दो प्रकार की मणियाँ प्राप्त हुयी
हैं। एक कीमती पत्थर की और दूसरी पकी हुई मिट्टी की। इनमें से कुछ के बीच में छेद
है और कुछ पर रेखाओं द्वारा डिजाइन भी बनाई गयी है।
डॉ. सांकलिया को मान्यता है कि रेखाओं द्वारा मणियाँ मध्य एशिया को
सभ्यता के प्रभाव को स्पष्ट करती हैं । सम्भवत: कीमती पत्थर के मणियों का प्रयोग यहाँ
के सम्पन्न नागरिकों द्वारा ही किया जाता होगा तथा मिट्टी के मणियों का प्रयोग
मध्यम व निम्न वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता होगा। मानव आकृति में नाक लम्बी
बनायी जाती थी।
(5) कृषि व्यवसाय व रहन-सहन-
इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने व नदी पास होने के कारण कृषि का उत्पादन
पर्याप्त मात्रा में किया जाता था। लेकिन यह बताना कठिन है कि ये कौनसा आनाज पैदा
किया करते थे। वे अन्न को पकाकर खाते थे। बड़ी-बड़ी भट्टियों के मिलने से ऐसा प्रतीत
होता है कि यहाँ सामूहिक भोज का आयोजन होता था। खुदाई में कपड़ों आदि पर छपाई के ठप्पे
भी प्राप्त हुए हैं। शरीर पर लगे मैल को छुड़ाने के भावों से ऐसा लगता है ये लोग
अपने शरीर की सफाई का भी ध्यान रखते थे। खुदाई में तौल के बाट व माप भी मिले हैं।
ऊपरी सतह पर मिले मानव के अस्थि पंजर से प्रतीत होता है कि ये शवों को गाड़ते
थे। शव का मस्तक उत्तर व पाँव दक्षिण की तरफ रखे जाते थे। शवों के साथ पहनने के
आभूषण भी गाड़ देते थे।
इस सभ्यता के सम्बन्ध में यह कहना अभी सम्भव नहीं है कि इसका उद्भव व विकास कैसे
हुआ, इस पर शोध अभी जारी है। श्री रतन चन्द्र अग्रवाल के शब्दों में आहड़ इस
युग की ताम्र-पाषाण संस्कृति विशेष का मुख्य केन्द्र था और नदियों के
किनारे-किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे बेड़च, बनास व चम्बल के काठे में
हो गया। डॉ. गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि सम्भवतः आहड़ सभ्यता का
समृद्ध काल 1900 ई.पू.से 1200 ई.पू. तक रहा होगा।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गई
जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आई हो तो इसे अपने
दोस्तों से जरूर शेयर करें।



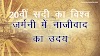











0 Comments