राजस्थान में
सामन्त व्यवस्था (सामन्तवाद)
राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था में सामन्त पद्धति अपना विशेष स्थान रखती है। राजस्थान के राज्यों में आरम्भ से ही राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित रही है और सामन्त व्यवस्था इस राजतंत्र प्रणाली का ही एक प्रतिफल है। सामन्त पद्धति एक प्रकार की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था का रूप थी जिसमें नेता के रूप में एक राजा रहता था और उसके साथ उसके अपने कुल के वंशज या अन्य राजपूत कुल के वंशज उसके साथी और सहयोगी के रूप में रहते थे।
राजा अपने भाइयों व अन्य समीप के सम्बन्धियों को उनकी
जीविका के लिए अपने राज्य में से कुछ भूमि जागीर के रूप में देता था। उस
भूमि पर जागीर प्राप्ति का जन्मजात अधिकार हो जाता था और वे अपने को राजा के
समकक्ष ही समझते थे। जागीरों के माध्यम से अपना भरण-पोषण करने वाले ये राजपूत
ही सामन्त कहलाते थे।
राजस्थान में
आरम्भ में सामन्त व्यवस्था का स्वरूप
प्रारम्भिक काल में शासन का स्वरूप कुलीन व्यवस्था
होने के कारण राजस्थान में सामन्त बहुत शक्तिशाली थे। अपनी जागीर को
व्यवस्था करने के अलावा वे राजा को प्रशासन, शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने में भी सहायता करते थे। राजा
सामन्तों के प्रभाव में इतना था कि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता
था। उत्तराधिकार के प्रश्न में सामन्त प्रमुख भूमिका निभाते थे।
उदाहरण के लिए मारवाड़ के राव सूजा ने अपने पौत्र वीरम
को मारवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया परन्तु सामन्तों ने उसे अयोग्य करार देते हुए
उसके भ्राता राव गंगा को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया। इस प्रकार सामन्त उत्तराधिकार
में भी हस्तक्षेप करते थे।
 |
| राजस्थान में सामन्त व्यवस्था |
राजस्थान में सामन्त व्यवस्था प्रबल ही नहीं वरन् व्यापक भी थी। डॉ. आर. पी. व्यास के अनुसार, "राजस्थान के राज्यों के कुल क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत भू-भाग सामन्तों के अधिकार में था।" इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक कालीन सामन्त प्रभावशाली और शक्तिशाली थे।
राजस्थान में
सामन्त व्यवस्था के विकसित होने के कारण
(1) हिन्दू उत्तराधिकार नियम-
हिन्दू उत्तराधिकार नियम के अन्तर्गत राजा
के मरने के उपरान्त उसकी गद्दी उसके ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी। अत: जब ज्येष्ठ
पुत्र पिता की गद्दी पर आसीन हो जाता था तो उसे अपने कनिष्ठ भ्राताओं के जीवन-यापन
के लिए जागीर देना आवश्यक था। इस प्रकार राजाओं के छोटे पुत्र सामन्त बनते
ही चले गये।
(2) राजपूत नरेशों की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा-
राजस्थान के राजपूत नरेश पृथ्वीराज चौहान व महाराणा
सांगा की भांति महत्त्वाकांक्षी होते थे। वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी
बनकर राज्य करना चाहते थे। विशाल साम्राज्य की स्थापना के उपरान्त राजपूत नरेशों
को अपनी राजधानी से दूरस्थ प्रदेशों पर अपने प्रशासक नियुक्त करने पड़ते थे।
राजपूत नरेशों ने अपने छोटे भाइयों और रक्त सम्बन्धियों को प्रशासन नियुक्त
किया तथा उन्हें जागीर प्रदान की। इस प्रकार राजपूत नरेशों की साम्राज्यवादी
महत्त्वाकांक्षा ने सामन्ती व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया।
(3) राजपूत नरेशों का सदैव संघर्षरत रहना-
राजपूत राजा स्वाभिमानी होते थे। वे किसी के पराधीन
रहना पसन्द नहीं करते थे। इस कारण राजस्थान के नरेश सदैव आपस में ही संघर्ष करते
रहते थे। संघर्षों में विजयी होने की अभिलाषा में राजपूत नरेश अपने लघु भ्राताओं तथा
सम्बन्धियों को भूमि देकर बदले में सैनिक सहायता माँगना प्रारम्भ किया। इस प्रकार
सैनिक सहयोग प्राप्त करने के लिए राजपूत राजाओं को सामन्ती व्यवस्था को
पल्लवित करना पड़ा।
(4) पुरस्कार वितरण के लिए भूमि ही एक मात्र साधन-
कई बार राजा युद्ध में अपूर्व वीरता एवं स्वामी भक्ति
प्रदर्शित करने के उपलक्ष्य में भी लोगों को पुरस्कृत करना चाहते थे। मध्यकाल
से आधुनिक काल तक तो पुरस्कार में भूमि देना ही सर्वोत्तम समझते। इस
प्रणाली के कारण भी सामन्ती व्यवस्था का उदय हुआ।
(5) सामन्तों का विश्वसनीय एवं स्वामी-भक्त होना-
एक रक्त से सम्बन्धित होने के कारण सामन्त अपने
स्वामी मरेशों के परम स्वामी भक्त होते थे। अत: राजाओं ने संकट के समय सहयोग को
लालसा के कारण सामन्ती व्यवस्था को जन्म दिया।
राजस्थान की
सामन्त व्यवस्था की विशेषताएँ
(1) सामन्तों का राजा से रक्त सम्बन्ध-
राजस्थान के अधिकांश सामन्तों का सम्बन्ध उनके राजा से रक्त
का होता था। उन्हें जागीर इसलिए दी जाती थी कि वे राजा के भाई-बन्धु या सम्बन्धी
ही होते थे। इनके अलावा कुछ ही सामन्त ऐसे होते थे जिन्हें राजा उनकी वीरता तथा धार्मिक
निष्ठा के कारण जागीर प्रदान करता था। इसलिए वे अपने राजा की सुरक्षा के लिए
मर-मिटना अपना कर्तव्य समझते थे। अन्य सामन्त राजा को अपने ही कुल का एक सदस्य
मानते थे।
(2) समानता पर आधारित-
राजस्थान की सामन्ती व्यवस्था समानता के सिद्धान्त
पर आधारित थी। यहाँ राजा व सामन्तों के सम्बन्ध दास व स्वामी के सिद्धान्त पर
आधारित न होकर समानता के आधार पर आधारित थे। सामन्त अपने को राजा के दास न समझकर
उसके समकक्ष समझते थे। जागीर मिलना राजा की अनुकम्पा का प्रतिफल न मानकर सामन्त
अपने अधिकार का प्रतिफल मानते थे।
(3) सामन्ती व्यवस्था का उत्थान व पतन उनके
राजाओं के साथ होना-
राजस्थान के नरेशों के उत्थान का इतिहास वहाँ के
सामन्तों के उत्कर्ष का इतिहास है। इसी प्रकार उनका पतन भी राजाओं के साथ
ही हुआ।
(4) स्वामी भक्ति-
सामन्त व राजाओं के सम्बन्धों में निःसन्देह
उतार-चढ़ाव आते रहे परन्तु सामन्त सदा अपने राजा के परम भक्त बने रहे।
सामन्तों के शक्तिशाली होने के कारण कई बार इन्होंने राजाओं की आज्ञा का उल्लंघन
किया परन्तु फिर भी संकट के समय सामन्तों ने एकजुट होकर अपने स्वामी का साथ दिया।
सामन्तों की
श्रेणियाँ, पद और प्रतिष्ठा
मुगल सम्राटों का आश्रय पाकर राजपूत नरेश अपने सामन्तों को
निर्बल बनाने का प्रयास करने लगे। मुगल प्रशासन से प्रभावित होने के कारण राजपूत
नरेशों ने मनसबदारी प्रथा के आधार पर अपने सामन्तों का वर्गीकरण
करना आरम्भ किया। परिणामस्वरूप कुलीय भावना पर आधारित भाई-बिरादरी, स्वामी-सेवक सम्बन्धों में परिवर्तित होने लग
गई।
(1) मेवाड़ के सामन्त-
मेवाड़ में महाराणा अमरसिंह द्वितीय (1698-1710) ने अपने सामन्तों को
तीन श्रेणियों में विभाजित किया जो आगे चलकर क्रमशः सौलह, बत्तीस व गोल के सरदार कहलाये। महाराणा
अमरसिंह द्वितीय के काल में प्रथम श्रेणी के सामन्तों की संख्या 16 थी। इन्हें प्राय: उमराव कहा जाता था।
द्वितीय श्रेणी के सामन्तों की संख्या 32 थी, अत: वे बत्तीस कहलाये। तृतीय श्रेणी के सरदारों की
संख्या कई सौ थी अत: उन्हें गोल का सरदार कहा जाता था। उमराव अपने आपको राज्य
की सम्पत्ति का हिस्सेदार, राज्य का संरक्षक
तथा महाराणा का सलाहकार मानते थे। महाराणा का खास रुका मिलने पर ही वे दरबार में
उपस्थित होते थे।
(2) मारवाड़ के सामन्त-
मारवाड़ के सामन्तों की कई श्रेणियाँ थीं। इनमें चार प्रमुख
श्रेणियाँ थीं- (1) राजवी (2) सरदार (3)
मुत्सदी और (4) गनायत। राजा के छोटे भाई व निकट
के सम्बन्धी जिन्हें अपनी उदरपूर्ति के लिए जागीर दी जाती थी, वे राजवी कहलाते थे। उन्हें तीन पीढ़ी तक रेख, चाकरी, हुक्मनामा आदि शुल्कों से छूट होती थी। तीन
पीढ़ी के बाद ये राजवी भी सामान्य जागीरदारों की श्रेणी में आ जाते थे। राजपरिवार
के अतिरिक्त अन्य राठौड़ सामन्तों को सरदार कहा जाता था। जिन अधिकारियों को
जागीरें मिली हुई थीं वे "मुस्तदी" कहलाते थे और राठौड़ों के
अलावा अन्य शाखाओं के सामन्तों को “गनायत" कहा जाता था।
(3) ग्रासिये और भौमिये-
राजस्थान की सामन्त व्यवस्था में ग्रासियों और भौमियों
का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था। ग्रासिये वे सामन्त थे जो सैनिक सेवा के उपलक्ष में
राजा द्वारा भूमि की उपज का, जो 'ग्रास'
कहलाती थी, उपभोग करते थे। ऐसी भूमि सेवा में
ढिलाई करने या आज्ञा का उल्लंघन करने पर छीनी जा सकती थी या फिर दी जा सकती थी। भौमिए
वे सामन्त थे, जिन्होंने राज्य की रक्षा में अथवा राजकीय
सेवाओं के लिए अपना बलिदान किया था। ऐसे लोगों को जो राज्य की भूमि दी जाती थी,
उस पर उन्हें नाममात्र का कर देना पड़ता था। ऐसे सामन्तों को उनकी
भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मध्यकालीन राजस्थान में
सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में सामन्तीय व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्थान था।
ये सामन्त शासक के सहयोगी होते थे। शासक इनके बीच बराबर वालों में प्रथम की हैसियत
रखता था। परन्तु मुगल शासन के प्रभाव से धीरे-धीरे इन सामन्तों की स्थिति में
परिवर्तन आता गया और इनकी हैसियत कमजोर होती गयी। 18वीं सदी के आरम्भ तक
उत्तरी-पूर्वी राजस्थान के सामन्त तो अत्यन्त निर्बल हो गये क्योंकि इस क्षेत्र
में मुगल प्रभाव अधिक था।
18वीं शताब्दी में सामन्तों की स्थिति में
परिवर्तन
(1) पुनः शासकों की सामन्तों पर निर्भरता-
औरंगजेब को मृत्यु ने भारतीय इतिहास में एक संक्रमण काल
प्रस्तुत कर दिया। निर्बल मुगल शहजादे गद्दी के लिए निरन्तर संघर्ष करने लगे और वे
मुगल गद्दी से जल्दी-जल्दी हाथ धोने लगे। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय शासन कमजोर हो गया।
इसका प्रभाव यह हुआ कि राजपूत शासकों के परम्परागत कुलीन झगड़े पुनः उठ खड़े हुए। सभी
ने अपने-अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में राजपूत शासकों को
पुनःअपने सामन्तों की सहायता पर निर्भर हो जाना पड़ा।
ऐसी स्थिति में सामन्तों ने भी अपने पुराने अधिकारों को
पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया जिसमें उत्तराधिकार के चयन में निर्णायक भाग ले
सकना महत्त्वपूर्ण था।
(2) मराठों से सैनिक सहयोग-
सामन्तों की बढ़ती हुई शक्ति से राजपूत शासक भयभीत
हो गये अतः उन्होंने सामन्तों के आन्तरिक दवाव से मुक्त होने तथा आपसी संघर्षों को
सफलतापूर्वक हल करने और अपनी निरंकुशता एवं अधिकारों को दृढ़ बनाये रखने के लिए राजपूत
शासकों ने मराठों का सैनिक सहयोग प्राप्त किया। परिणामस्वरूप राजपूत राज्यों को मराठों
और पठानों को लूट-खसोट का शिकार होना पड़ा।
(3) सामन्तों की शक्ति में वृद्धि-
18वीं सदी में प्रत्येक राज्य में सामन्तों
की शक्ति में काफी वृद्धि हो गयी थी। सामन्त लोग अपनी जागीरों में लगभग
स्वतन्त्र शासक की भाँति शासन करते थे। सामन्तों के अपने दरबार थे। उनके अपने
अधिकारी, कर्मचारी तथा सैनिक दस्ते थे। अपनी जागीरों में
शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने तथा आन्तरिक उपद्रवों को दबाने की जिम्मेदारी भी
उन्हीं की थी।
उनके न्यायिक अधिकार भी काफी थे। बडे सामन्तों को
मृत्युदण्ड के अलावा सभी प्रकार को सजायें देने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें किसी
भी व्यक्ति को अपनी गढी में शरण देने का अधिकार था। व्यापारिक तथा दुकानदारों की
सुरक्षा के बदले में उन्हें उनसे कई प्रकार के वसूल करने का अधिकार प्राप्त था। इस
प्रकार 18वीं सदी तक सामन्तों को अपने-अपने क्षेत्र में पर्याप्त
अधिकार प्राप्त हो गये थे।
(4) पारस्परिक कलह और शक्ति क्षीणता-
उत्तराधिकार के नियम के अन्तर्गत भूमि का विभाजन होता गया
और धीरे-धीरे भूमि के कई छोटे-छोटे विभाग होते गये। ऐसी स्थिति में बड़े जागीरदार
की भूमि भी कई भागों में बँटकर छिन्न-भिन्न हो गयी। मेके के शब्दों में, "सूर्य और चन्द्र के लाल तथा अग्नि पुत्र अपनी परम्परा को भूलकर शौर्य की
बजाय शराब और व्यभिचार के व्यसन सेवी बन गये। वे कर्ज में डूब गये।"
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 18वीं
सदी के अन्त तक शासकों और सामन्तों की आपसी कलह जारी रही। संयोगवश, सामन्तों में परस्पर विरोधी गुट बनते गये और उनकी आपसी स्पर्द्धा के कारण
लगभग सभी राज्यों में अव्यवस्था फैल गयी। जोधपुर, बीकानेर
आदि राज्यों में तो शासकों और सामन्तों के मध्य तथा सामन्तों का एक-दूसरे के विरुद्ध
संघर्ष चरम सीमा पर पहुँच चुका था। ऐसी स्थिति में राजपूत शासकों ने ब्रिटिश
संरक्षण स्वीकार कर लिया जिसका सामन्तों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश
संरक्षण स्वीकार कर लेने के कारण राजपूत शासकों को सामन्तों के सहयोग की आवश्यकता
नहीं रही परन्तु फिर भी खालसा भूमि, सैनिक सेवा, उत्तराधिकार शुल्क और सामन्तों के अधिकारों को लेकर राजाओं का अपने
सामन्तों के साथ लम्बे समय तक विवाद बना रहा।
निष्कर्ष
सामन्त व्यवस्था के इन सभी पहलुओं पर विश्लेषणात्मक ढंग से
विचार करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजस्थानी सामन्त व्यवस्था
आपसी भाई-चारे की व्यवस्था थी। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी व प्रशासनिक
अध्यक्ष अवश्य होता था, परन्तु सामन्त रूपी तारों में लगभग उसको
अवस्था चाँद जैसी होती थी। सामन्त व शासक सम्बन्ध पूर्ण रूप से आश्रितों का न होकर
समकक्ष आज्ञाकारी सहयोगियों का था। निःसन्देह यह व्यवस्था एक प्रकार से सामाजिक,
आर्थिक व राजनीतिक विशेषताओं से युक्त थी परन्तु 18वीं शताब्दी में बाहर प्रभाव के कारण सामन्त व शासक के बीच मतभेद उत्पन्न
हो गये।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी पसंद आई
होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें।




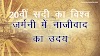









0 Comments