स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की प्रमुख भूमिका
परिचय- स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका, विशेष रूप से जयपुर, मेवाड़, मारवाड़ और भरतपुर के प्रजामंडल आंदोलनों ने भारतीय राजनीति को नया दिशा दी। इस ब्लॉग पोस्ट में हम इन प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इन आंदोलनों ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में किस प्रकार योगदान दिया।
राजस्थान की
राजनीतिक चेतना में प्रजामण्डलों की भूमिका-
1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रारम्भ में कांग्रेस का लक्ष्य केवल ब्रिटिश प्रान्तों को ही स्वतन्त्रता दिलाना था। इसने भारत के देशी राज्यों के राजनीतिक जागरण की ओर ध्यान नहीं दिया। 1936 के कराँची अधिवेशन के बाद कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में हुआ।
इस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया
था तथा उन देशी राज्यों में भी उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव पास किया
गया। इस अधिवेशन के पश्चात् कांग्रेस और देशी राज्य लोक परिषद् का सम्पर्क घनिष्ठ होता
चला गया। तब से कांग्रेस देशी राज्यों के मामलों में अधिकाधिक रुचि लेने लगी। अब कांग्रेस
ने रियासती जनता को अपने-अपने राज्य में राजनीतिक संगठन स्थापित करने की अनुमति दे
दी। अत: राजस्थान के अनेक राज्यों में प्रजामण्डलों की स्थापना हुई।
मारवाड़ प्रजामंडल का संघर्ष: राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय
(1) मारवाड़ सेवा
संघ की स्थापना-
मारवाड़ सेवा संघ की
स्थापना 1920 ई. में की गई थी। इसे राजस्थान सेवा संघ से सम्बन्धित किया गया। जानवरों की निकासी को लेकर 1926 में इस संस्था ने
आन्दोलन चलाया। सरकार ने कई लोगों को सजाएँ दी। अन्त में आन्दोलन सफल रहा।
 |
| स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की प्रमुख भूमिका |
(2) मारवाड़
हितकारिणी सभा और सरकार की दमन नीति-
इसकी स्थापना 1917 में हो चुकी थी और
यह जन-आन्दोलन कर रही थी। 1922 में जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा
ने इस संस्था में सम्मिलित होकर नई चेतना उत्पन्न की। 1927 में देशी राज्य लोक
परिषद् के बम्बई अधिवेशन में जयनारायण व्यास ने भी भाग लिया। वहाँ से वापस लौटकर व्यासजी
ने जोधपुर में अखिल भारतीय देशी
राज्य लोक परिषद् की शाखा स्थापित करने का
प्रयास किया किन्तु राज्य के प्रधानमन्त्री डोनाल्ड फील्ड की दमनात्मक नीति
के कारण सम्मेलन का आयोजन नहीं करवा सके। 11-12 अक्टूबर, 1929 को व्यासजी ने जोधपुर में 'मारवाड़ राज्य लोक परिषद्' का अधिवेशन करने की तैयारियाँ की लेकिन सरकार की दमन नीति
के कारण सफल न हो सके। 23 सितम्बर, 1930 को उन्हें राज्य विरोधी
कार्यवाहियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार राज्य सरकार की दमनकारी
गतिविधियों ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को लगभग समाप्त कर दिया।
(3) यूथ लीग की
स्थापना-
1931 ई. में जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने 'यूथ लीग' की स्थापना की। इसकी शाखाएँ
दूसरे नगरों में भी स्थापित की गई। व्यासजी को मारवाड़ राज्य लोक परिषद् का अधिवेशन आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया। इस सम्मेलन
में मारवाड़ में उत्तरदायी शासन को आवश्यकता पर जोर दिया व नागरिक अधिकारों व
मारवाड़ में शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। 1932 में मारवाड़ की शान्ति एवं
व्यवस्था में विघ्न डालने वाली गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
लेकिन चौपासनी वाला ने स्वतन्त्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो वे पकड़े गये
और बुरी तरह पीटे गये और बाद में रिहा कर दिया गया। चौपासनी वाला जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के अधिवेशन में भाग लेने
गये तो उन्हें गिरफ्तार कर 6 माह के लिए नजरबन्द कर
दिया।
(4) मारवाड़
प्रजामण्डल-
1934 में मानमल जैन, अभय जैन और छगनराज चौपासनीवाला
ने मारवाड़ प्रजामण्डल स्थापित कर लिया। 10 मार्च, 1936 को इस संस्था ने पं. जवाहर लाल नेहरू का उत्साह से स्वागत किया। इस
अवसर पर नेहरू ने जोधपुरवासियों से कहा कि वे अपने आपको ब्रिटिश साम्राज्य के
विरुद्ध भारतीय संघर्ष का अभिन्न हिस्सा समझे। किन्तु नेहरू की वापसी के बाद
जोधपुर सरकार ने मारवाड़ प्रजामण्डल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया।
(5) मारवाड़ अधिकार
रक्षक सभा-
मारवाड़ प्रजामण्डल
के समाप्त होने के बाद 1936 में मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा की स्थापना की लेकिन उसे भी सरकार ने गैर-कानूनी घोषित कर
दिया।
(6) सलाहकार परिषद्
का पुनर्गठन-
1938 में मारवाड़ लोक परिषद् की स्थापना की
गई जिसका उद्देश्य मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। परन्तु राज्य
सरकार ने इसे भी गैर-कानूनी घोषित कर दिया।
(7) 1939 में
द्वितीय महायुद्ध और स्वतन्त्रता प्राप्ति तक आन्दोलन की निरन्तरता-
1939 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया और
अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे ही भारत को युद्ध में धकेल दिया।
परिणामतः ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देशी रियासतों में भी असन्तोष फैल गया। ऐसी
स्थिति में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में प्रशासन में अधिक अधिकारों की
माँग के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना की माँग की। इस पर कई नेताओं को जेलों में ठूंस
दिया। 29 मार्च, 1940 को मारवाड़ लोक परिषद्
को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। 1942 में लोक परिषद् और राज्य
सरकार के मध्य पुनः टकराव शुरू हो गया।
चन्द्रावल ठाकुर तथा
नीमाज के सिपाहियों ने लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं पर लाठियों तथा भालों से हमला
किया। वहाँ धारा 144 लगा दी गई। जयनारायण व्यास ने
महाराजा से मिलकर सारी स्थिति को साफ करने की कोशिश की लेकिन सरकार शान्त रही। अत:
इस स्थिति ने आन्दोलन का रूप ले लिया। सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू की। 12 जून, 1942 ई. को जेल अधिकारियों की यातनाओं के कारण बालमुकुन्द विस्सा का
जेल में ही देहान्त हो गया।
1944 में गर्मियों में सभी नेताओं को रिहा कर दिया
गया। 1944 में सरकार ने शासन व्यवस्था में सुधार हेतु जोधपुर
राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की, लेकिन इसको कोई विशेष
अधिकार प्रदान नहीं किये। वास्तविक अधिकार एक कौंसिल के हाथों में रखे गये। अत: मारवाड़
लोकपरिषद् ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपना आन्दोलन जारी रखा।
उन्हीं दिनों राज्य
के कई ठिकानों में परिषद् के कार्यकर्ताओं तथा किसानों पर जुल्म ढाया जाता रहा।
अत: अक्टूबर 1946 में परिषद् को जागीरदारों के विरुद्ध संघर्ष
छेड़ना पड़ा। 1947 के प्रारम्भ में डीडवाना तहसील के डाबला
गाँव में 700 पुष्करण ब्राह्मण परिवारों को बिना किसी कारण
गाँव से बाहर कर दिया तो परिषद् के कार्यकर्ता डाबला पहुँचे तो सभी नेताओं
को राजद्रोह के नाम पर गिरफ्तार कर लिया।
स्वतन्त्रता के बाद जयनारायण व्यास का मन्त्रिमण्डल बनने के बाद इन
नेताओं को रिहा किया गया।
3 जून, 1947 ई. को जब ब्रिटिश सरकार ने
भारत की स्वतन्त्रता तथा देश के विभाजन की घोषणा की तो राजनीतिक वातावरण फिर गर्म
हो गया। इस घोषणा में देशी राजाओं को भारत अथवा पाकिस्तान के साथ मिलने की खुली
छूट दी गयी। जोधपुर में हनुवंत सिंह महाराजा बना। जिन्ना उसे
पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए प्रलोभन दे रहा था। भारत सरकार जोधपुर राज्य का
विलय भारत में चाहती थी। ऐसी स्थिति में जयनारायण व्यास के नेतृत्व
में मारवाड़ लोक परिषद् ने पूरा प्रयत्न किया कि
महाराजा पाकिस्तान के साथ न मिलने पाये अन्ततः प्रयास सफल रहा और महाराणा ने
जोधपुर राज्य का भारत के साथ विलय स्वीकार कर लिया।
जयपुर प्रजामंडल की भूमिका और इसका जनसंचार
जयपुर राज्य में
राजनीतिक चेतना का अलख जगाने वाले अर्जुनलाल सेठी थे। 1907 में उन्होंने अजमेर
में जैन शिक्षा समिति की स्थापना की। 1908 में इस संस्था को
जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया और जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से एक स्कूल भी चलाया गया। इस विद्यालय में
क्रान्तिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्रान्तिकारी आन्दोलन के संचालन के लिए
क्रान्तिकारियों को धन की बहुत आवश्यकता थी। अत: सेठी ने मुगलसराय में रहने वाले एक
धनी महन्त की हत्या की योजना बनाई। 20 मार्च, 1913 को महन्त की हत्या कर दी गई परन्तु क्रान्तिकारियों के धन हाथ नहीं लगा। सबूत
के अभाव में अर्जुनलाल सेठी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका।
23 दिसम्बर, 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लार्ड
हार्डिंग का जुलूस दिल्ली में जब चाँदनी चौक में से गुजर रहा था तब उन पर एक
बम फेंका गया। सेठी को भी इस षड्यन्त्र में सम्मिलित होने के लिए बन्दी बना लिया
गया। उन्हें मद्रास के वेलूर जेल में 7 वर्ष को सजा काटनी पड़ी
तथा 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1920-21के असहयोग आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया और जेल गये। उन्हें 11/2 वर्ष के बाद सागर
जेल से रिहा किया गया। उनका शेष जीवन हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने में बीता। 1945 में उनकी मृत्यु हो
गई।
1931 में जयपुर में प्रजामण्डल की स्थापना की
गई। 1938 में जमनालाल बजाज प्रजामण्डल के
अध्यक्ष और पं. हीरालाल शास्त्री इसके मन्त्री बने। 1938 में जमनालाल
बजाज की अध्यक्षता में प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में किया गया।
शीघ्र ही जयपुर सरकार ने सेठ जमनालाल बजाज के जयपुर राज्य में
प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी। इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रजामण्डल को भी गैर-कानूनी
घोषित कर दिया। 11 फरवरी, 1939 को बजाज बैराठ के निकट वन्दी
बना लिए गए। हीरालाल शास्त्री भी बन्दी बनाए गए। जयपुर की जनता ने
अपने लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। जयपुर शहर में जबरदस्त हड़ताल
हुई। लगभग 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्त में 5 अगस्त, 1939 को प्रजामण्डल तथा जयपुर सरकार के बीच समझौता हो गया। इसके फलस्वरूप सभी
सत्याग्रही रिहा कर दिए गए। 8 अगस्त को बजाज को भी रिहा
कर दिया गया। प्रजामण्डल को वैध मान लिया गया।
1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामण्डल
के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपनी लगन तथा संगठन शक्ति के बल पर प्रजामण्डल को सुदृढ़
आधार प्रदान किया। जब 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हुआ तो
जयपुर प्रजामण्डल में फूट पड़ गई। हीरालाल शास्त्री इस आन्दोलन में सक्रिय
भाग लेने के विरुद्ध थे। परन्तु प्रजामण्डल के बाबा हरिश्चन्द्र वाले गुट ने आजाद
मोर्चा स्थापित कर आन्दोलन छेड़ दिया। आन्दोलन में भाग लेने के कारण बाबा
हरिश्चन्द्र, दौलतमल भण्डारी गुलाब चन्द कासलीवाल आदि अनेक कार्यकर्ता
बन्दी बनाये गये। सिद्धराज ढड्ढ़ा भी भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में बन्दी
बनाए गए और 2 वर्ष तक वाराणसी जेल में रहे।
1945 में जब पं. जवाहर लाल नेहरू जयपुर आये
तो आजाद मोर्चे के नेता बाबा हरिश्चन्द्र ने नेहरूजी की प्रेरणा से आजाद मोर्चे को
प्राजमण्डल में विलीन कर दिया। 1946 में जयपुर में विधानसभा
तथा विधान परिषद् की स्थापना हुई। प्रजामण्डल के अध्यक्ष देवीशंकर तिवाड़ी
15 मई, 1946 को राज्य के मन्त्रिमण्डल में लिए गए। 27 मार्च, 1948 को मन्त्रिमण्डल का विस्तार किया गया जिसमें दीवान के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। जयपुर
महाराज ने भारतीय संघ में मिलने की घोषणा करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया।
मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन: भारतीय राजनीति में राजस्थान का योगदान
(1) मेवाड़
प्रजामण्डल की स्थापना तथा सरकार का दमन चक्र-
बिजोलिया-सत्याग्रह और बेगूं किसान आन्दोलन
की आंशिक सफलता से प्रेरित होकर माणिक्य लाल वर्मा ने अप्रेल, 1938 में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना की। इसका प्रमुख
उद्देश्य जनता के अधिकारों और संवैधानिक सुधारों की माँग करना तथा प्रजा के आर्थिक
कष्टों को दूर करने का प्रयास करना था।
इस संस्था के प्रथम
सभापति बलवन्तसिंह मेहता और उपाध्यक्ष भूरेलाल बया बनाये
गये। माणिक्य लाल वर्मा मंत्री बने। किन्तु उदयपुर राज्य के
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री धर्म नारायण ने इस संस्था को गैर-कानूनी घोषित
कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को शहर छोड़ देने की आज्ञा दे दी। माणिक्य
लाल वर्मा अजमेर चले गये व प्रेस के माध्यम से प्रचार कार्य किया।
4 अक्टूबर, 1938 को विजयादशमी के
दिन प्रजामण्डल ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया और यह मांग की कि प्रजामण्डल को
कानूनी संस्था माना जाये तथा माणिक्य लाल वर्मा को पुनः उदयपुर प्रवेश दिया
जाये। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ से बाहर सत्याग्रह का संचालन किया। अब
सरकार ने अपना दमन-चक्र और भी तेज कर दिया। भूरेलाल बया को तो सराड़ा किले
में नजरबंद कर दिया गया। आंदोलन का सबसे अधिक जोर नाथद्वारा में रहा जब पुलिस ने
नरेन्द्रपालसिंह और प्रो. नारायण दास को गिरफ्तार कर लिया और भीड़ पर लाठी चार्ज
किया।
मेवाड़ में इस दौरान
238 गिरफ्तारियाँ हुई। लेकिन मेवाड़ सरकार को चैन कहाँ था। 12 फरवरी, 1939 को देवली
में मेवाड़ की सीमा में वर्माजी को घसीट कर बन्दी बनाया गया। गाँधीजी ने हरिजन पत्र में इस अमानुष व्यवहार को बड़ी भर्त्सना की। 3 मार्च, 1939 को महात्मा गाँधी ने मेवाड़ प्रजामण्डल का सत्याग्रह स्थगित कर
रचनात्मक कार्य करने का सलाह दी। फरवरी, 1941 ई. में राज्य सरकार
ने प्रजामण्डल पर से प्रतिबन्ध हटा दिया। इसके बाद प्रजामण्डल का खूब प्रचार हुआ।
(2) मेवाड़
प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन तथा मेवाड़ हरिजन सेवक संघ' की स्थापना-
नवम्बर, 1941 में मेवाड़ प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के
सभापरित्व में उदयपुर में हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जे.बी. कृपलानी
ने किया और इस अवसर पर खाद और ग्रामोद्योग की वृहत् प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती
विजय लक्ष्मी पंडित ने किया। इस अधिवेशन के समय मेवाड़ में हरिजनों की सेवा के
लिए मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई और इसका
कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा।
(3) भारत छोड़ो
आंदोलन तथा मेवाड़ राज्य मण्डल-
अगस्त, 1942 में महात्मा गाँधी का भारत छोड़ो आन्दोलन सारे देश में व्याप्त
था। मेवाड़-राज्य प्रजामण्डल भी इस आंदोलन में कूद पड़ा। महात्मा गाँधी
के सुझावानुसार मेवाड़-प्रजामण्डल की ओर से महाराणा को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत
किया गया जिसमें ब्रिटिश सरकार से सरकार विच्छेद करने तथा राज्य में उत्तरदायी
शासन की स्थापना करने का अनुरोध था। 21 अगस्त, 1942 को एक सार्वजनिक सभा करने का निश्चय किया। फलत: सरकार ने भावी आशंका मानकर
गिरफ्तारियाँ की व सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया। प्रजामण्डल को गैर कानूनी घोषित
कर दिया गया।
भारत छोड़ो आन्दोलन में मेवाड़ की महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इनमें माणिक्य
लाल वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी, वर्माजी की पुत्री
सुशीला आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया।
लगभग 600 विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये। यह आन्दोलन उदयपुर
के अतिरिक्त नाथद्वारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, छोटी सादड़ी आदि
अन्य नगरों में भी फैल गया। यह आन्दोलन जनवरी, 1944 तक चला रहा। अंत में फरवरी, 1944 को सभी लोगों को रिहा किया गया।
(4) उदयपुर सम्मेलन-
अप्रैल, 1944 में उदयपुर में एक सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें विविध राज्यों के 250 कार्यकर्ताओं ने
भाग लिया। इसमें एक कमेटी का निर्माण किया गया और उसे राजपूताना तथा मध्य भारत के
लिये एक समान कार्यक्रम निर्धारित करने को कहा। लेकिन सरकार ने पुनः सभाओं पर
प्रतिबन्ध लगा दिया। 6 अप्रैल, 1945 को गाँधीजी रिहा कर
दिये गये और सितम्बर, 1945 में राज्य सरकार ने प्रजामण्डल पर लगे
प्रतिबन्ध को उठा लिया। इससे उत्साहित होकर प्रजामण्डल ने राज्य में रचनात्मक
कार्यों की ओर ध्यान दिया।
(5) अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् का अधिवेशन-
मेवाड़ प्रेजामण्डल के अनुरोध पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् ने 31 दिसम्बर, 1945 को उदयपुर में एक सम्मेलन पं. नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया इसमे
देशी राज्यों के 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें देशी राज्यों
में उत्तरदायी शासन की स्थापना को पुनः दोहराया गया।
1946 में प्रजामण्डल ने राज्य में अनेक समस्याओं
यथा-गैर मेवाड़ियों को सरकारी नौकरियाँ देने को कड़ी आलोचना की, कर्मचारियों के
वेतनमानी, महँगाई भत्ते में वृद्धि न करने आदि को लेकर सरकार से
मोर्चा लिया। प्रजामण्डलों के कार्यालयों के बाहर बोर्डो पर तथा राष्ट्रीय
गतिविधियों का विवरण लिखकर जनता को प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी देते रहने का
सफल प्रयास किया गया। देश में राजनीतिक वातावरण में तेजी से बदलाव आया। 23 मई, 1947 को राज्य का नया
संविधान प्रदान किया। परिणामतः प्रजामण्डल के एक नेता मोहनलाल सुखाड़िया
को 23 मई, 1947 को मंत्रीपद पर नियुक्त कर दिया गया।
भरतपुर प्रजामंडल: सत्याग्रह से स्वतंत्रता संग्राम तक
हरिपुरा कांग्रेस के बाद भरतपुर के
प्रमुख नेताओं ने राज्य से बाहर रेवाड़ी में दिसम्बर, 1928 में भरतपुर
राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की। गोपीलाल
यादव इसके अध्यक्ष बने तथा मास्टर आदित्येन्द्र को कोषाध्यक्ष बनाया गया। राज्य
सरकार ने संगठन का पंजीकरण नहीं किया तथा उसे गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया।
फलस्वरूप प्रजा मण्डल ने 21 अप्रैल, 1938 को सत्याग्रह आरम्भ कर
दिया तथा जनता का ध्यान राज्य सरकार के अत्याचारों पर केन्द्रित करने का प्रयास
किया गया। अन्त में 23 दिसम्बर, 1940 को प्रजामण्डल व राज्य
सरकार के बीच समझौता हो गया। प्रजामण्डल का प्रजा परिषद् के नाम से पंजीकरण हो गया तथा सभी नेताओं को रिहा कर दिया
गया। प्रजा परिषद् के उद्देश्य सार्वजनिक समस्याओं को प्रस्तुत करना, प्रशासनिक सुधारों
पर बल देना तथा जनमत को शिक्षित करना रखे गये।
प्रजा परिषद् ने 27 अगस्त से 2 सितम्बर, 1940 तक एक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। इसने अनेक प्रस्ताव पास किये गए जिसमें
उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रस्ताव भी सम्मिलित था। इन सभी प्रस्तावों को, माँगों के रूप में, राज्य के दीवान के
समक्ष रखा गया, किन्तु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 30 दिसम्बर, 1940 को परिषद् का पहला राजनैतिक सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में
हुआ, जिसमें पुन: उत्तरदायी शासन की स्थापना पर जोर दिया गया।
सरकार इन गतिविधियों को कब सहन करने वाली थी। सरकार ने परिषद् के मन्त्री को बन्दी
बना दिया। भारत छोड़ो आन्दोलन आरम्भ होने तक प्रजा परिषद्
काफी सक्रिय हो गयो थी तथा सार्वजनिक समस्याओं पर चर्चा तीव्र हो गई।
अगस्त, 1942 में इसने सत्याग्रह आरम्भ कर दिया जो दिनों-दिन उग्रतर हो गया। सरकार ने अनेक
नेताओं को बन्दी बनाया, फिर भी आन्दोलन की उग्रता में कमी नहीं आयी। जनता को
सन्तुष्ट करने के लिए अक्टूबर, 1942 में सरकार ने केन्द्रीय
सलाहकार परिषद् के स्थान पर बृज-जय प्रतिनिधि सभा का गठन किया। जिसमें
कुल 50 सदस्यों में से 37 निर्वाचित सदस्य रखे गये।
अगस्त, 1943 में चुनाव हुए जिसमें 27 सदस्य प्रजा परिषद्
के चुने गये। युगल किशोर चतुर्वेदी को नेता तथा मास्टर आदित्यनेन्द्र को उपनेता
चुना गया। लेकिन शीघ्र ही प्रतिनिधि सभा का खोखलापन स्पष्ट हो गया तथा राजनीतिक जागृति
भी बढ़ती गयी। अत: अप्रैल, 1945 में परिषद् ने प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार कर
राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की माँग की।
23 मई, 1945 को प्रजा परिषद् का दूसरा अधिवेशन बयाना
में हुआ, जिसमें उत्तरदायी शासन की माँग पुनः दोहरायी गयी। अखिल
भारतीय स्तर पर भी राज्य सरकार की अनुत्तरदायी नीति की आलोचना की गयी। 25 नवम्बर, 1945 को प्रजा परिषद् ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि राज्य में उत्तरदायी
शासन स्थापित नहीं हुआ तो 12 दिसम्बर से सत्याग्रह आरम्भ कर दिया जायेगा। सरकार ने
प्रजा परिषद् के नेताओं को 12 दिसम्बर से पहले ही गिरफ्तार
कर लिया। कुछ दिनों बाद उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् का सातवाँ अधिवेशन हुआ, जिसमें पूरे क्षेत्र में
उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की गयी। राज्य सरकार ने संवैधानिक सुधारों के
लिए एक समिति नियुक्त की, जिसमें प्रजा परिषद् के सदस्यों का बहुमत दिसम्बर, 1946 को प्रजा परिषद्ने कामां में एक सम्मेलन किया जिसमें बेगार समाप्त
करने तथा उत्तरदायी शासन की माँग दोहरायी गयी।
14 जनवरी, 1947 को भारत के वायसराय लार्ड
वैवल और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह शिकार के लिए भरतपुर पहुंचे तो राज्य
प्रशासन के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्वर
अत्याचार किये। पुलिस की बर्बरता के विरुद्ध भरतपुर में 17 दिन तक हड़ताल रही।
आन्दोलन दिन-प्रतिदिन तेज होता गया। प्रजा परिषद् के नेता जेल में ठूंस दिये गये।
किन्तु युगल किशोर चतुर्वेदी व मास्टर आदित्येन्द्र भूमिगत होकर आन्दोलन संचालित
करते रहे विभिन्न स्थानों पर उपद्रव हुए जो कुछ ही दिनों में साम्प्रदायिक झगड़ों
में बदल गये। जाट और मेवों के पारस्परिक संघर्षों को राज्य सरकार नियन्त्रित न कर सकी।
अत: विवश होकर जनवरी, 1948 में चार लोकप्रिय मन्त्रियों को नियुक्त किया
गया। फिर भी महाराजा का व्यवहार राष्ट्र-विरोध रहा। लोकप्रिय मन्त्री भी केवल तीन
महीने कार्य कर सके। 18 मार्च, 1948 को मत्स्य संघ
के बन जाने से भरतपुर राज्य का पृथक् अस्तित्व समाप्त हो गया।
क्या आप राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? कृपया इस पोस्ट को शेयर
करें और हमें अपने विचार कमेंट में बताएं!




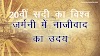









0 Comments