शिक्षा का समाज पर प्रभाव
जिस प्रकार समाज शिक्षा के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है तो ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी समाज को प्रत्येक पक्ष पर प्रभावित करती है, चाहे आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्वरूप हो। इस पर हम बिन्दुवार आगे कुछ विस्तार से देखेंगे-
शिक्षा व समाज का स्वरूप-
शिक्षा का प्रारूप समाज के
स्वरूप् को बदल देती है क्योंकि शिक्षा परिवर्तन का साधन है। समाज प्राचीनकाल से
आत तक निरन्तर विकसित एवं परिवर्तित होता चला आ रहा है क्येांकि जैसे-जैसे शिक्षा
का प्रचार-प्रसार होता गया इसने समाज में व्यक्तियों के प्रस्थिति, दृष्टिकोण , रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाजों पर असर डाला
और इससे सम्पूर्ण समाज का स्वरूप बदला।
शिक्षा व सामाजिक सुधार एवं प्रगति-
शिक्षा समाज के व्यक्तियों को इस योग्य बनाती है कि वह समाज में व्याप्त समस्याओं, कुरीतियों गलत परम्पराओं के प्रति सचेत होकर उसकी आलोचना करते है, और धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन हेाता जाता है। शिक्षा समाज के प्रति लेागों को जागरूक बनाते हुये उसमें प्रगति का आधार बनाती है। जैसे शिक्षा पूर्व में वर्ग विशेष का अधिकार थी जिससे कि समाज का रूप व स्तर अलग तरीके का या अत्यधिक धार्मिक कट्टरता, रूढिवादिता एवं भेदभाव या कालान्तर में शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिये अनिवार्य बनी जिससे कि स्वतंत्रता के पश्चात् सामाजिक प्रगति एवं सुधार स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है।
डयूवी ने लिखा है कि- शिक्षा
में अनिश्चितता और अल्पतम साधनों द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्यों के
साथ-साथ, समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रूचि
का दूषित होना पाया जाता है।
शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण-
शिक्षा समाज का स्वरूप बदलकर उस
पर नियंत्रण भी करती है अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण एवं उसके
क्रियाकलाप समाज को गतिशील रखते हैं। शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर
उसके क्रियाकलापों में परिवर्तन कर समूह मन का निर्माण करती है और इससे
अत्यव्यवस्था दूर कर उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है।
शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन-
समाज की रचना मनुष्य ने की है, और समाज का आधार मानव
क्रिया है ये अन्त: क्रिया सदैव चलती रहेगी और शिक्षा की क्रिया के अन्तर्गत होती
है इसीलिये शिक्षा व्यवस्था जहां समाज से प्रभावित हेाती है वहीं समाज को
परिवर्तित भी करती है जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात् सबके लिये शिक्षा एवं समानता
के लिये शिक्षा हमारे मुख्य लक्ष्य रहे हैं इससे शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ और
समाज का पुराना ढांचा परिवर्तन होने लगा। आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर भौतिक
मूल्य अधिक लोकप्रिय हुआ। सादा जीवन उच्च विचार से अब हर वर्ग अपनी इच्छाओं के
अनुरूप जीना चाहता है। शिक्षा ने जातिगत व लैंगिक असमानता को काफी हद तक दूर करने
का प्रयास किया और ग्रामीण समाज अब शहरी समाजों में बदलने लगे और सामूहिक परिवारों
का चलन कम हो रहा है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन और इसके द्वारा शिक्षा पर
प्रभाव दोनों ही तथ्य अपने स्थान पर स्पष्ट है।
सैयदेन ने इस बात को और स्पष्ट
करते हुये लिखा है कि- इस समय भारत में शिक्षा बहुत नाजुक पर रोचक अवस्था में से
होकर गुजर रही है,
यह स्वाभाविक है
क्योंकि समग्र रूप में राष्ट्रीय जीवन भी जिसका शिक्षा भी अनिवार्य अंग है, ऐसी ही अवस्था में से
होकर गुजर रहा है।
 |
| शिक्षा का समाज पर प्रभाव एवं स्थान |
शिक्षा का समाज में स्थान
वैंकटरायप्पा ने शिक्षा व समाज के
सम्बंध को स्पष्ट करते हुये लिखा है- ‘‘शिक्षा समाज के बालकों का समाजीकरण करके उसकी सेवा करती है।
इसका उद्द्देश्य युवकों को सामाजिक मूल्यों विश्वासों और समाज के प्रतिमानो को
आत्मासात करने के लिये तैयार करना और उनको समाज की क्रियाओं में भाग लेने के योग्य
बनाना है।’’ शिक्षा व्यक्ति व समाज के
लिये यह कार्य करती है।
1. शिक्षा व्यक्ति
व समाज की प्रक्रिया का आधार- शिक्षा को चाहे व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया कहें या
सामाजिक प्रक्रिया इन दोनों में वह व्यक्ति व समाज से सम्बंध स्थापित करती है।
शिक्षा समाज को गतिशील बनाती है, और विकास का आधार
प्रदान करती है।
2. समाज के व्यक्तियों
का व्यक्तित्व विकास- शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के
विकास से तात्पर्य शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक और बौद्धिक गुणों
के विकास के साथ सामाजिक गुणों का विकास होना। विकसित व्यक्तित्व का बाहुल्य समाज
की प्रगति का आधार बनता है। व्यक्ति को निर्जीव मानकर समाज उसका उपयोग नहीं कर
सकता।
3. संस्कृति व
सभ्यता के हस्तांतरण की प्रक्रिया- शिक्षा समाज की संस्कृति एवं सभ्यता के हस्तांतरण का आधार
बनती है। शिक्षा के इस कार्य के विषय में ओटवे महोदय ने लिखा है कि - ‘‘शिक्षा का कार्य समाज के
सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरूण और शक्तिशाली सदस्यों
को प्रदान करना है। पर असल में यह उसके साधारण कार्यो में से एक है।’’
शिक्षा के इस कार्य पर टायलर
ने लिखा है कि ‘‘संस्कृति वह जटिल समग्रता
है, जिसमें ज्ञान विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य
योग्यतायें और आदतें सम्मिलित होती है, जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप शिक्षा से प्राप्त करता
है।’’ महात्मा गांधी ने शिक्षा
के इस कार्य की आवश्यकता एवं प्रशंसा करते हुये लिखा है - ‘‘संस्कृति ही मानव जीवन की
आधार शिला और मुख्य वस्तु है यह आपके आचरण और व्यक्तिगत व्यवहार की छोटी सी छोटी
बातों में व्यक्त होनी चाहिये।’’
4. शिक्षा सामाजिक
प्रक्रिया के अंग के रूप में- रासे के के अनुसार- ‘‘शिक्षा एक आधारभूत सामाजिक कार्य और सामाजिक प्रक्रिया का
अंग है।’’ ओटवे ने शिक्षा को सामाजिक
विज्ञान का रूप देते हुये स्पष्ट किया है- ‘‘शिक्षा समाज में होने वाली क्रिया है और इसके उद्देश्य एवं
विधियां उस समाज के स्वरूप के रूप के अनुरूप होती है, जिनमें इसकी क्रिया होती
है।’’
5. शिक्षा के
द्वारा समाज की स्थिरता- शिक्षा समाज के मानव संसाधन को सुसंस्कृत बनाकर अपने व
समाज के लिये उपयोग बनाती है। ओर्शिया ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुये कहा है कि ‘‘समाज की शिक्षा व्यवस्था
व्यक्तियों का मानसिक, व्यावसायिक, राजनीतिक और कलात्मक
विकास करके न केवल समाज के अधोपतन की रक्षा करती है, वरन उसको स्थिरता भी प्रदान करती है।’’
6. भावी पीढ़ी के
प्रशिक्षण- शिक्षा समाज को
प्रशिक्षित भावी पीढी़ प्रदान करती है, जो कि समाज का भविष्य हेाते हैं। ब्राउन लिखते है कि- ‘‘शिक्षा व्यक्ति व समूह के
व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यह चैतन्य रूप
में एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा
व्यक्ति के व्यवहार में और व्यक्ति द्वारा समूह में परिवर्तन किये जाते हैं।
शिक्षा समाज को सभ्य एवं सुसंस्कृत पीढ़ी प्रदान करती है।’’
7. शिक्षा समाज
की प्रगति का आधार- शिक्षा समाज के लिये वह साधन है, जिसके द्वारा समाज के मनुष्यों के विचारों, आदर्शों, आदतों और दृष्टिकोण में
परिवर्तन कर समाज की प्रगति की जाती है। एलवुड ने स्पष्ट किया है- ‘‘शिक्षा वह साधन है जिसमें
समाज सब प्रकार की महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति की आशा कर सकता है।’’
8. समाज में
परिर्वतन का आधार- समाज का स्वरूप एवं प्रस्थिति में निरन्तर बदलाव की ओर अग्रसर होता है, और यह आवश्यक भी नही है, कि यह व्यक्ति और समाज के
लिये हितकर हेा इसमें शिक्षा इस बदलाव एवं व्यक्ति व समाज के मध्य सम्बधं स्थापित
करते हुये सामंजस्य बैठाती है। एलवुड ने स्पष्ट किया है- ‘‘समाज का सर्वोत्तम
परिवर्तन मानव के स्वभाव में परिवर्तन कर किया जा सकता है और ऐसा करने की सर्वोत्तम
विधि शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।’’
9. सामाजिक दोषो
के सुधार का आधार- शिक्षा में नैतिकता चारित्रिक एवं दार्शनिक पक्ष की प्रधानता हेाती है और
शिक्षा अपनी व्यवस्था में भावी पीढ़ी को समाज में व्याप्त दोषों को इंगित कर उनमें
सुधार हेतु समझ एवं मार्ग प्रदान करती है।
10. समाज की
सदस्यता की तैयारी का आधार- शिक्षा व्यक्ति को अपने व समाज के लिये उपयोगी बनाती है, प्रारम्भ में बालक परिवार
का सदस्य होता है और उन्हें सामाजिक कर्तव्यों एवं नागरिकता के गुणों को विकसित कर
उन्हें समाज के भावी सदस्य के रूप में तैयार करती है।
शिक्षा पर समाज का
प्रभाव
शिक्षा पर समाज
के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि समाज शिक्षा की व्यवस्था करता है।
समाज के स्वरूप का प्रभाव-
समाज के स्वरूप का शिक्षा की
पकृति पर प्रभाव पड़ता है, जैसा समाज का
स्वरूप होगा वह शिक्षा को वैसे ही व्यवस्थित करता है। भारत लोकतांत्रिक देश है तो
शिक्षा की प्रकृति उद्देश्यों उसके संगठन एवं वातावरण में लोकतांत्रिक आदर्श
प्रतीत होते हैं। तानाशाही समाज की शिक्षा में अनुशासन व आज्ञाकारिता, आदि पर बल दिया जाता है।
समाजवादी देशों की शिक्षा में समाजवादी तत्व एवं स्वरूप दिखयी देता है।
सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव-
समाज की प्रस्थिति एवं स्वरूप
जैसे तैसे बदलता जाता है वैसे वैसे शिक्षा का रूप भी बदलता जाता है। भारत में
आदिकाल से धार्मिक शिक्षा दी जाती थी उसके पश्चात् समय के साथ आधुनिक युग आया और
देश ने राजतंत्र से प्रजातंत्र में प्रवेश किया और शिक्षा में लोकतंत्रीय आदर्श
एवं मूल्य समावेशित हुये सामाजिक असमानता, कुरीतियों एवं आर्थिक असमानता को दूर कर वर्ग विशेष के लिये
शिक्षा व्यवस्था से सबके लिये शिक्षा को मुख्य लक्ष्य माना गया और सभी को शिक्षा
प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कराया गया।
राजनैतिक दशाओं का प्रभाव-
किसी भी समाज की
राजनैतिक दशा का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राजनीति को मजबूत आधार शिक्षा प्रदान करती है।
अंग्रेज जब भारत आये तो उन्होनें अपने शासन को मजबूत आधार देने के लिय शिक्षा
व्यवस्था को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया और इसके लिये निष्पन्दन का
सिद्धान्त का अनुसरण कर आवश्यकतानुसार शिक्षा देने का प्रयास किया कम्पनी के
संचालकों का विश्वास था कि ‘‘प्रगति उस समय हो
सकती है, जब उच्च वर्ग के उन
व्यक्तियों को शिक्षा दी जाये जिसके पास अवकाश है।’’ वैदिक युग में राजतंत्र था तो
शिक्षा वर्ग विशेष के लिये थी परन्तु प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी आयु
वर्ग, लिंग, जाति एवं धर्म के लोगों
को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
आर्थिक दशाओं का प्रभाव-
जिस समाज की
आर्थिक दशा अच्छी हो ती है वहां की शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है।
अमेरिका जैसे देश विकसित हें तो वहां पर शिक्षा का प्रचार-प्रसार जल्दी हुआ और
भारत जैसे देश में हमें शिक्षा की सुविधा देने में वर्षों लग रहे हैं। आर्थिक रूप
से सम्पन्न समाज अच्छे विद्यालय खोलने में सक्षम रहता है, इसके फलस्वरूप व्यावसायिक, प्राविर्थिाक, प्रौद्योगिक, वैज्ञानिक आदि पक्षों का
अधिक से अधिक विकास हेतु संसाधन उपलब्ध रहता है। आर्थिक रूप से विपन्न देशों व
समाजों की शिक्षा में भी यह विपन्नता स्पष्ट दिखायी देती है।
सामाजिक आदर्शो, मूल्यो व आवश्यकताओ का प्रभाव-
शिक्षा पर सामाजिक आदर्शों का
प्रभाव पड़ता है जैसे भारत में शिक्षा का स्वरूप पर डा0 राधाकृष्णन ने लिखा कि- ‘‘शिक्षा को व्यक्ति और
समाज दोनों का उत्थान करना चाहिये। तब हमारी शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों, शिक्षण विधियों पाठ्यक्रम
एवं शिक्षार्थी,
शिक्षक के गुणों
की संकल्पना पर इसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।’’ इस प्रकार भारतीय समाज की
आवश्यकता है, गरीबी, बेरोजगारी, को दूर करना असमानता की
भावना दूर करना,
और लोकतांत्रिक
मूल्यों का समावेश किया जाये तब इन तथ्यों को शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पक्षों
उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम में स्पष्ट समावेशित किया गया।
समाज के दृष्टिकोण का प्रभाव-
शिक्षा व्यवस्था में समाज के दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है, जैसे यदि समाज रूढ़िवादी दृष्टिकोण का है तो शैक्षिक प्रशासन एवं अनुशासन व पाठ्यक्रम में इसका स्पष्ट छाप दिखायी देती है।समाज के उदार दृष्टिकोण का प्रभाव वहॉ की शिक्षा व्यवस्था में देखी जा सकती है। जैसे वैदिक युगीन समाज का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था तब उस समय शिक्षा व्यवस्था धार्मिक थी। इसी प्रकार से जनतांत्रिक दृष्टिकोण एंव उदार शिक्षा का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था में स्पष्ट दिखायी देता है। एच0ओड का कथन है- ‘‘समाज और शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का सम्बंध है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।
è यह भी देखें ¦ शिक्षा के घटक, प्रकार एवं महत्व
è यह भी देखें ¦ शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं सम्प्रत्यय
è यह भी देखें ¦ शिक्षा के साधन व शिक्षा के कार्य




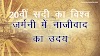










0 Comments