ऐतिहासिक अनुसन्धान विधि
ऐतिहासिक
अनुसन्धान का सम्बन्ध भूतकाल से हैं। यह भविष्य को समझने के लिये भूत का विष्लेशण
करता है।
जॉन डब्ल्यू
बेस्ट के अनुसार ‘‘ऐतिहासिक अनुसन्धान का
सम्बन्ध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विष्लेशण से है। इसके विभिन्न पद भूत के
सम्बन्ध में एक नयी सूझ पैदा करते है, जिसका सम्बन्ध वर्तमान और भविष्य से हेाता है।’’
करलिंगर के अनुसार, ‘‘ ऐतिहासिक अनुसन्धान का तर्क संगत अन्वेषण है। इसके द्वारा अतीत की सूचनाओं एवं सूचना सूत्रों के सम्बन्ध में प्रमाणों की वैधता का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है और परीक्षा किये गये प्रमाणों की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जाती है।’’
ऐतिहासिक अनुसन्धान के उद्देश्य
1. ऐतिहासिक अनुसन्धान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान
को समझना एवं भविष्य के लिये सतर्क होना है।
2. ऐतिहासिक अनुसन्धान का उद्देश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के
सम्बन्ध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शान्त करना है।
3. ऐतिहासिक अनुसन्धान का उद्देश्य अतीत के परिपेक्ष्य में
वर्तमान घटनाक्रमों का अध्ययन कर भविष्य में इनकी सार्थकता को ज्ञात करना है।
ऐतिहासिक अनुसन्धान के पद-
ऐतिहासिक
अनुसन्धान जब वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है तो उसमें पद सम्मिलित होते हैं -
1. समस्या का चुनाव और समस्या का सीमा निर्धारण।
2. परिकल्पना या परिकल्पनाओं का निर्माण।
3. तथ्यों का संग्रह और संग्रहित तथ्यों की प्रामाणिकता की जाँच।
4. तथ्य विष्लेशण के आधार पर परिकल्पनाओं की जाँच।
5. परिणामों की व्याख्या और विवेचना।
 |
| ऐतिहासिक अनुसंधान विधि |
ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत-
ऐतिहासिक
साक्ष्यों के स्रेात मुख्यत: देा श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाते है- 1. प्राथमिक स्रोत 2. गौण स्रोत।
प्राथमिक स्रोत-
जब कोई
अनुसन्धानकर्ता अध्ययन क्षेत्र मे जाकर अध्ययन इकाईयों से स्वयं या अपने सहयोगी
अनुसन्धानकर्ताओं के द्वारा सम्पर्क करके तथ्यों का संकलन करता है तो यह तथ्य
संकलन का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। मौलिक अभिलेख जो किसी घटना या तथ्य के प्रथम
साक्षी हेाते हैं ‘प्राथमिक स्रोत’ कहलाते हैं। ये किसी भी
ऐतिहासिक अनुसन्धान के ठोस आधार होते हैं।प्राथमिक स्रोत किसी एक महत्वपूर्ण अवसर
का मौलिक अभिलेख होता है, या एक प्रत्यक्षदर्शी
द्वारा एक घटना का विवरण होता है या फिर किसी किसी संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण
होता है।
प्राथमिक स्रेात
के उदाहरण - न्यायालयों के निर्णय, अधिकार पत्र, अनुमति पत्र, घोशणा पत्र, आत्म चरित्र वर्णन, कार्यालय सम्बन्धी अभिलेख, इश्तिहार, विज्ञापन पत्र, रसीदें, समाचार पत्र एवं
पत्रिकायें आदि।
गौण स्रोत-
जब साक्ष्यो के प्रमुख
स्रोत
उपलब्ध नहीं होते
है तब कछु ऐतिहासिक अनुसन्धान अध्ययनों को आरम्भ करने एवं विधिवत ढ़ंग से कार्य
करने के लिये इन साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। गौण स्रोत का लेखक घटना के समय
उपस्थित नहीं होता है बल्कि वह केवल जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे, उन्होनें क्या कहा? या क्या लिखा ? इसका उल्लेख व विवेचन
करता है।
एक व्यक्ति जो
ऐतिहासिक तथ्य के विशय में तात्कालिक घटना से सम्बन्धित व्यक्ति के मुँह से
सुने-सुनाये वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है ऐसे वर्णन को गौण स्रोत कहा
जायेगा। अधिकांश ऐतिहासिक पुस्तकें और विधाचक्र कोष गौण स्रोतों का उदाहरण है।
ये गौण होने से
महत्त्वहीन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सच तो यह है कि गौण स्रोतों की पूरी तरह से
जानकारी के बाद ही एक अनुसंधानकर्ता प्रधान स्रोतों का उचित उपयोग कर सकता है, सामयिक दस्तावेजों को
उचित स्थानों पर रख सकता है और गौण विवरणों में सुधार ला सकता है।
ऐतिहासिक साक्ष्यों की आलोचना
ऐतिहासिक विधि
में हम निरीक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हो चुका
उसे दोहराया नही जा सकता है। अत: हमें साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ता है।
ऐतिहासिक अनुसन्धान में साक्ष्यों के संग्रह के साथ उसकी आलोचना या मूल्यांकन भी
आवश्यक होता है जिससे यह पता चले कि किसे तथ्य माना जाये, किसे सम्भावित माना जाये
और किस साक्ष्य को भ्रमपूर्ण माना जाये इस दृष्टि से हमें ऐतिहासिक विधि में
साक्ष्यों की आलोचना या मूल्यांकन की आवश्यकता हेाती है। अत: साक्ष्यों की आलोचना
का मूल्यांकन स्रेात की सत्यता की पुष्टि तथा इसके तथ्यों की प्रामाणिकता की दोहरी
विधि से सम्बन्धित है। ये क्रमश: 1. बाह्य आलोचना और 2. आन्तरिक आलोचना
कहलाती है।
बाह्य आलोचना-
बाह्य आलोचना का
उद्देश्य साक्ष्यों के स्रोत की सत्यता की परख करना होता है कि आँकड़ों का स्रोत
विश्वसनीय है या नहीं। इसका सम्बन्ध साक्ष्यों की मौलिकता निश्चित करने से है।
वाह्य आलोचना के अंतर्गत साक्ष्यों के रूप, रंग, समय, स्थान तथा परिणाम की
दृष्टि से यथार्थता की जाँच करते हैं। हम इसके अन्तर्गत यह देखते हैं कि जब
साक्ष्य लिखा गया,
जिस स्याही से
लिखा गया, लिखने में जिस शैली का
प्रयोग किया गया या जिस प्रकार की भाषा, लिपि, हस्ताक्षर आदि
प्रयुक्त हुए है,
वे सभी तथ्य
मौलिक घटना के समय उपस्थित थे या नहींं। यदि उपस्थित नही थे, तो साक्ष्य नकली माना
जायेगा।उपरोक्त बातों के परीक्षण के लिये हम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का
प्रयास करते हैं -
1. लेखक कौन था तथा उसका
चरित्र व व्यक्तित्व कैसा था?
2. लेखक की सामान्य रिपोर्टर
के रूप में योग्यता क्या पर्याप्त थी?
3. सम्बन्धित घटना में उसकी
रूचि कैसी थी?
4. घटना का निरीक्षण उसने
किस मनस्थिति से किया?
5. घटना के कितने समय बाद
प्रमाण लिखा गया?
6. प्रमाण किस प्रकार लिखा
गया - स्मरण द्वारा, परामर्श द्वारा, देखकर या पूर्व-ड्राफ्टों
को मिलाकर?
7. लिखित प्रमाण अन्य
प्रमाणों से कहाँ तक मिलता है?
आन्तरिक आलोचना -
आन्तरिक आलोचना
के अन्तगर्त हम सा्र ते में निहित तथ्य या सूचना का मूल्यॉकन करते हैं। आन्तरिक
आलोचना का उद्देश्य साक्ष्य ऑकड़ों की सत्यता या महत्व को सुनिश्चित करना होता है।
अत: आन्तरिक आलोचना के अन्तर्गत हम विषय वस्तु की प्रमाणिकता व सत्यता की परख करते
हैं। इसके लिये हम निम्न प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
1. क्या लेखक ने वर्णित घटना
स्वयं देखी थी?
2. क्या लेखक घटना के विश्वसनीय
निरीक्षण हेतु सक्षम था?
3. घटना के कितने दिन बाद
लेखक ने उसे लिखा?
4. क्या लेखक ऐसी स्थिति में
तो नहीं था जिसमें उसे सत्य को छिपाना पड़ा हो?
5. क्या लेखक धर्मिक, राजनैतिक, व जातीय पूर्व-धारणा से
तो प्रभावित नहीं था?
6. क्या लेखक को तथ्य की जानकारी
हेतु पर्याप्त अवसर मिला था?
7. उसके लेख व अन्य लेखों
में कितनी समानता है?
8. इन प्रश्नों के उत्तरों
के आधार पर ऐतिहासिक ऑकड़ो की आन्तरिक आलोचना के पश्चात ही अनुसन्धानकर्ता किसी
निश्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करता है।
ऐतिहासिक अनुसन्धान का क्षेत्र
वैसे तो ऐतिहासिक
अनुसन्धान का क्षेत्र बहुत व्यापक है किन्तु संक्षेप में इसके क्षेत्र में
निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं -
1. बड़े शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार ।
2. संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य।
3. विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के
विकास की स्थिति।
4. एक विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव एव उसके स्रोत का
अध्ययन।
5. शिक्षा के लिये संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन।
ऐतिहासिक अनुसन्धान का महत्व
जब कोई
अनुसन्धानकर्ता अपनी अनुसन्धान समस्या का अध्ययन अतीत की घटनाओं के आधार पर करके
यह जानना चाहता है कि समस्या का विकास किस प्रकार और क्यों हुआ है? तब ऐतिहासिक अनुसन्धान
विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसन्धान के महत्व को
बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं -
1. अतीत के आधार पर वर्तमान
का ज्ञान- ऐतिहासिक
अनुसन्धान के आधार पर सामाजिक मूल्यों, अभिवृत्तियों और व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करके यह
ज्ञात किया जा सकता है कि इनसे सम्बन्धित समस्यों अतीत से किस प्रकार जुड़ी है तथा
यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि इनसे सम्बन्धित समस्याओं का विकास कैसे-कैसे और
क्येां हुआ था ?
2. परिवर्तन की प्रकृति के
समझने में सहायक- समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान में अनेक ऐसी समस्यायें हैं जिनमें परिवर्तन
की प्रकृति को समझना आवश्यक होता है। जैसे सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, औद्योगीकरण, नगरीकरण से सम्बन्धित
समस्याओं की प्रकृति की विशेष रूप से परिवर्तन की प्रकृति को ऐतिहासिक अनुसन्धान
के प्रयोग द्वारा ही समझा जा सकता है।
3. अतीत के प्रभाव का
मूल्यांकन- व्यवहारपरक
विज्ञानों में व्यवहार से सम्बन्धित अनेक ऐसी समस्यायें हैं जिनका क्रमिक विकास
हुआ है। इन समस्याओं के वर्तमान स्वरूप पर अतीत का क्या प्रभाव पड़ा है? इसका अध्ययन ऐतिहासिक
अनुसन्धान विधि द्वारा ही किया जा सकता है।
4. व्यवहारिक उपयोगिता- यदि कोई अनुसन्धानकर्ता
सामाजिक जीवन में सुधार से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम या योजना लागू करना चाहता है
तो वह ऐसी समस्याओं का ऐतिहासिक अनुसन्धान के आधार पर अध्ययन कर अतीत में की गयी
गलतियों को सुधारा जा सकता है और वर्तमान में सुधार कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी
ढ़ंग से लागू करने का प्रयास कर सकता है।
ऐतिहासिक अनुसन्धान की सीमायें और समस्यायें
वर्तमान
वैज्ञानिक युग में ऐतिहासिक अनसुन्धान का महत्व सीमित ही है। आधुनिक युग में किसी
समस्या के अध्ययन में कार्यकारण सम्बन्ध पर अधिक जोर दिया जाता है जिसका अध्ययन
ऐतिहासिक अनुसन्धान विधि द्वारा अधिक सशक्त ढ़ंग से नहीं किया जा सकता है केवल
इसके द्वारा समस्या के संदर्भ में तथ्य एकत्रित करके कुछ विवेचना ही की जा सकती
है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसन्धान की सीमाओं को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट
कर सकते हैं-
1. बिखरे तथ्य- यह ऐतिहासिक अनसुन्धान
की एक बड़ी समस्या है कि समस्या से सम्बन्धित साक्ष्य या तथ्य एक स्थान पर प्राप्त
नहीं होते हैं इसके लिये अनुसन्धानकर्ता केा दर्जनों संस्थाओं और पुस्तकालयों में
जाना पड़ता है। कभी-कभी समस्या से सम्बन्धित पुस्तकें, लेख, शोधपत्र-पत्रिकायें, बहुत पुरानी होने पर इसके
कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण ये सभी आंशिक रूप से ही उपलब्ध हो पाते हैं ।
2. प्रलेखो का त्रुटिपूर्ण
रखरखाव- पुस्तकालयों तथा
अनेक सस्ंथाओं में कभी प्रलेख क्रम में नही हेाते है तो कभी प्रलेख दीमक व चूहो के
कारण कटे-फटे मिलते हैं ऐसे में ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता को बहुत कठिनाई होती है।
3. वस्तुनिष्ठता की समस्या- ऐतिहासिक अनुसन्धान में
तथ्यों और साक्ष्यों, का संग्रह
अध्ययनकर्ता के पक्षपातों, अभिवृत्तियों, मतों और व्यक्तिगत
विचारधाराओं से प्रभावित हो जाता है जिससे परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता संदेह
के घेरे में रहती है।
4. सीमित उपयोग- ऐतिहासिक अनुसन्धान का
पय्रोग उन्हीं समस्याओं के अध्ययन मे हो सकता है जिनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से
सम्बन्धित प्रलेख,
पाण्डुलिपियाँ
अथवा ऑकड़ो, या तथ्यों से सम्बन्धित
सामग्री उपलब्ध हो। अन्यथा की स्थिति में ऐतिहासिक अनुसन्धान विधि का प्रयोग सम्भव
नहीं हो पाता है।












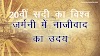


0 Comments