इतिहास-दर्शन का स्वरूप
इतिहास-दर्शन का स्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। यदि हम उसके प्राचीन स्वरूप को देखें तो पायेंगे कि पहले उसका स्वरूप धर्मशास्त्रीय था, बाद में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक हो गया।
प्रारम्भ में
इतिहासकारों ने संस्मरणों के आधार पर अपने पूर्वजों के कार्यों को
स्थायित्व प्रदान करने के इतिहास लिखा। उन लोगों ने अतीत की प्रत्येक घटना को इतिहास
मान लिया। बाद में 'प्रमुख घटनाओं' को ही लिया गया। इस तरह
चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और तब चिन्तन और विवेक' से काम लिया जाने लगा। तब
इतिहास के स्वरूप में और भी परिवर्तन आया। वह धार्मिकता और पौराणिकता से बदलते हुए
राजतन्त्रीय जीवन-प्रशस्तियों के युग में प्रविष्ट होकर साहित्यिक परिकल्पनाओं के
दौर से गुजरते हुए पाश्चात्य संस्कृतियों के प्रभाव में आने के बाद में प्रविष्ट
हुआ, जिसके फलस्वरूप इतिहास
में दर्शन और विज्ञान की अन्विति हुई और वर्तमान परिस्थितियों में वह सामंजस्य
स्थापित करने का प्रयास करता हुआ 'विश्व-इतिहास' के रूप में समग्र एवं सम्पूर्ण इतिहास बन गया।
 |
| इतिहास-दर्शन का वर्गीकरण व स्वरूप |
ऐतिहासिक
अनुसन्धान में यदि हम ज्ञान मीमांसा के वर्चस्व को स्वीकार करें, तो वह सम्पूर्ण मानवीय
क्रियाओं का अध्ययन कहा जायेगा। इतिहास-दर्शन इस सन्दर्भ में उन क्रियाओं के
अन्तर्गत पाये जाने वाले विचारों का प्राकट्य-रूप कहा जायेगा। ऐसी स्थिति में उसके
दो स्वरूप सामने आयेंगे- (1) सम्पूर्ण मानवीय क्रियाकल्पना, (2) वर्तमान में उसकी
पुनर्रचना।
इसमें प्रथम भाग
का सम्बन्ध घटना की वास्तविकता से होगा, जबकि दूसरे का सम्बन्ध उस घटना के विषय में वैज्ञानिक
चिन्तन से होगा। प्रो. बाड ने प्रथम को परिकल्पनात्मक तथा दूसरे को
विश्लेषणात्मक कहा है। दोनों साधनों का लक्ष्य इतिहास-दर्शन के माध्यम से सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् का प्रस्तुतीकरण है, जिसे हम इतिहास-दर्शन कह
सकते हैं। इस प्रकार इतिहास-दर्शन का स्वरूप जहाँ धर्मशास्त्रीय प्राप्त होता है, वहीं आलोचनात्मक और
वैज्ञानिक भी प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रीय स्वरूप ही दूसरी तरह से
परिकल्पनात्मक कहा गया है जबकि आलोचनात्मक और वैज्ञानिक स्वरूप ही दूसरी तरह से
परिकल्पनात्मक कहा गया है जबकि आलोचनात्मक और वैज्ञानिक स्वरूप को हम
विश्लेषणात्मक कह सकते हैं।
इस तरह मुख्य रूप
से इतिहास-दर्शन के इन्हीं दो स्वरूपों को मान्यता दी गई है। इतिहास-दार्शनिकों ने
इन्हीं दो स्वरूपों के विषय में अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।
विश्लेषणात्मक इतिहास-दर्शन
प्रो. शेक अली के इतिहास-दर्शन का
अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांशयुक्त प्रस्तुतीकरण है। इस अनुसार
विश्लेषणात्मक प्रकार की अवधारणा वैज्ञानिक युग की देन है। प्रारम्भ में इतिहास को
दर्शन तथा साहित्य का अंग स्वीकार किया जाता था। अरस्तू ने इतिहास को कविता
से तुच्छ तथा वाल्तेयर ने इतिहास को मृत अतीत के प्रति एक चाल कहा है।
परन्तु 19वीं शताब्दी में नेबूर तथा रांके ने इतिहास को वैज्ञानिक
विधाओं से अलंकृत किया।
रूसो, कारलायल, हीगेल, काम्टे, मिल, मार्क्स तथा बकल ने इतिहास
में सामान्यीकरण के सिद्धान्तों को प्रतिरोपित कर उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान
करने का प्रयास किया है। इसमें अनुभव किया गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन
कठिन है क्योंकि अतीतकालिक मानवीय कार्यों का प्रत्यक्षीकरण तथा अवलोकन सम्भव नहीं
है। इसमें मनुष्य के अध्ययन का विषय मनुष्य माना गया है।
इतिहास का
विश्लेषणात्मक दर्शन ऐतिहासिक ज्ञान के सामान्य रूप पर केन्द्रित हो गया है।
इतिहास को तार्किक विश्लेषण के उपकरणों से प्रयुक्त करने का प्रयास किया जा रहा
है। विश्लेषणात्मक इतिहास-दर्शन का मूल उद्देश्य इतिहास-चिन्तन की मूलभूत समस्याओं
पर विचार करना तथा उसे वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत करना है। इतिहास की प्रमुख
समस्याएँ हैं- इतिहास का अविच्छिन्न ज्ञान, रूप, ऐतिहासिक
यथार्थता, तथ्य, वस्तुनिष्ठा, व्याख्या तथा मूल्य।
1. इतिहास
अविच्छिन्न ज्ञान के रूप में-
इतिहास-दर्शन
उदाहरणों द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। ई.एच. कार के अनुसार इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के
बीच क्रिया को अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद
है। अतीत एवं वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद का अभिप्राय ज्ञान की अविच्छिन्नता
है। इतिहासकार इस ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करता है। इस प्रकार ऐतिहासिक ज्ञान
समाज के लिए उपयोगी होता है। इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों से सन्तुष्ट न होकर
सामाजित प्रश्नों का उत्तर देता रहता है। वाल्श के अनुसार इतिहासकार के द्वारा
सामाजिक प्रश्नों का उत्तर अविच्छिन्न ज्ञान है।
2. ऐतिहासिक
यथार्थता का तथ्य-
विश्लेषणात्मक
इतिहास-दर्शन का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यान्वेषण है। इतिहास का सम्बन्ध
सम्पूर्ण मानवता से न होकर व्यक्ति विशेष, समाज विशेष तथा काल विशेष से होता है । इतिहास का सम्बन्ध
अतीत से है, अतीत के तथ्यों का
प्रत्यक्षीकरण अथवा अवलोकन सम्भव नहीं है। वर्तमान की अपेक्षा अतीत के तथ्यों का
निर्धारण कठिन है। इतिहासकार मनोनुकूल तथ्यों का ही चयन करता है। इस प्रकार
इतिहास- अध्ययन में विषयनिष्ठा की समस्या है।
प्रो. वाल्श के अनुसार यद्यपि अतीत
का यथावत् प्रत्यक्षीकरण कठिन है, फिर भी वर्तमान
में उससे सम्बन्धित साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इतिहासकार इन साक्ष्यों
के यथार्थान्वेषण द्वारा अतीत को पुनजीवित कर प्रत्यक्षीकरण कराने में समर्थ होता
है। विश्लेषणवादी दार्शनिक इतिहासकार तथ्यों को यथावत् स्वीकार न करके उनकी
यथार्थता का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। इस प्रकार वह इतिहासको विषयनिष्ठता के
दोषों से अलग करने का प्रयास करता है।
3. ऐतिहासिक
वस्तुनिष्ठा-
वस्तुनिष्ठा
वैज्ञानिक विधा की विशेषता है। वैज्ञानिक के वस्तुनिष्ठात्मक निष्कर्ष को सभी एक
स्वर से स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक विधाओं में आस्थावान इतिहासकार भी इतिहास को
वस्तुनिष्ठात्मक विशेषताओं से अलंकृत कर उसे विज्ञान के समक्ष लाना चाहता है। यदि
इतिहास को पूर्णरूपेण विज्ञान स्वीकार कर लिया जाए, तो इसमें भी वस्तुनिष्ठा अपेक्षित है।
डाडेल ने लिखा है कि स्वयमेव
कोई भी तथ्य वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तथ्य को विषय से अलग कर वस्तुनिष्ठा प्रतिरोपित
की जाती है। वियर्ड के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों का चयन इतिहासकार व्यक्तिगत द्वेष, श्रान्ति, व्यक्तिगत झुकाव, सामाजिक तथा आर्थिक
प्रभावों से प्रभावित होकर करता है। इतिहास की पुनर्रचना सामाजिक आवश्यकता के
अनुसार होती है। इस प्रकार ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की कुछ समस्याएँ होती हैं जिन्हें
मान्यता प्रदान करने का तात्पर्य इतिहास में वस्तुनिष्ठा के समावेश को जटिल
स्वीकारना होता है। परन्तु अधिकांश वैज्ञानिक इतिहासकारों ने इतिहास में
वस्तुनिष्ठा की आवश्यकता को स्वीकार किया है। पी. गार्डिनर ने लिखा है कि
इतिहासकार को व्यक्तिगत रुचि के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों को अतिरंजित नहीं करना
चाहिए।
डिल्थे के अनुसार मानव-स्वभाव
का वस्तुनिष्ठ अध्ययन वस्तुनिष्ठ इतिहास का आधार होना चाहिए। रेनियर के अनुसार
इतिहास-अनुशासन में आस्थावान इतिहासकार को ही इतिहास लिखना चाहिए। इस प्रकार
वर्तमान समाज इतिहासकारों से वस्तुनिष्ठ रचना की अपेक्षा करता है।
4. ऐतिहासिक
व्याख्या-
इतिहासकार के
ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय किसी घटना के यथार्थ स्वरूप का प्रस्तुतीकरण होता
है। इतिहासकार अपनी व्याख्या में क्या घटित हुआ है, इसी से सन्तुष्ट नहीं होता, वह इस तथ्य की भी व्याख्या करता है कि घटना क्यों घटी। इसके
अतिरिक्त आकस्मिकता तथा व्यक्ति विशेष की समस्या ऐतिहासिक व्याख्या को जटिल बना
देती है।
कार्लजी हेम्पेल ने यह सिद्ध करने का
प्रयास किया है कि इतिहास में मानवीय घटनाओं की व्याख्या भौतिक जगत की भाँति
वैज्ञानिक विधाओं द्वारा की जा सकती है। वैज्ञानिक विधि से उनका तात्पर्य उपयुक्त
साक्ष्यों से है जो ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणित कर सकें और सन्तोषजनक निष्कर्ष
में सहायक हो सकें। वैज्ञानिक विधा में आस्था रखने वाले इतिहासकारों ने इतिहास की
व्याख्या में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है।
वैज्ञानिक की
भाँति इतिहासकार भी व्याख्या में सामान्यीकरण सिद्धान्तों का सहारा लेता है।
परन्तु विलियम ड्रे ने हेम्पेल की ऐतिहासिक व्याख्या में वैज्ञानिक
विधा के प्रयोग की कटु आलोचना की है। उसने लिखा है कि इतिहासकार केवल घटित घटनाओं
का वर्णन करता है। उसका कार्य भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि घटना मात्र को
स्पष्ट करना है। ऐतिहासिक व्याख्या में इतिहासकार का कार्य क्या और क्यों के साथ
यह भी स्पष्ट करना है कि घटना क्या थी।
विलियम ड़े के अनुसार इतिहासकार की
व्याख्या का यही लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारत की स्वतन्त्रता को
सम्भव बना दिया। विलियम ड्रे के अनुसार भारत की स्वतन्त्रता एक प्रकार की ऐतिहासिक
व्याख्या है। ऐतिहासिक व्याख्या नियमों के अधीन नहीं हो सकती। इतिहास में मानवीय
घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या सम्भव नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऐतिहासिक
व्याख्या इतिहासकार की मानसिक पुनर्रचना होती है।
5. मूल्य सम्पृक्त
व्याख्या-
मनुष्य स्वीकृत
मूल्यों के सन्दर्भ में कार्य करता है। प्रत्येक युग के समाज का अपना मूल्य होता
है। इतिहास की पुनर्रचना प्रत्येक युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है।
कार्ल बेकर के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकतानुसार
इतिहास लिखता है। प्रत्येक युग में इतिहास-स्वरूप में परिवर्तन अवश्यम्भावी है। इस
प्रकार ऐतिहासिक व्याख्या का मूल्य सम्पृक्त होना स्वाभाविक है। परन्तु
विश्लेषणात्मक दार्शनिक इतिहासकार अपने को मूल्यों के प्रश्नों से दूर रखने का
प्रयास करता है। वह प्रश्नों को तर्क और सूक्ष्मता में रूपान्तरित करता है।
इतिहासकार का कार्य है इतिहास को बोधगम्य बनाना और यह एक प्रकार का अर्थ है।
6. ऐतिहासिक
साम्यवाद-
विश्लेषणवादी
इतिहास-दर्शन में इतिहासकारों ने इतिहास की मूलभूत समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक
साम्यवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक साम्यवाद एक
विचारधारा है जिसके माध्यम से मानवीय कार्यों का विश्लेषण सम्भब है। इसके तीन
प्रमुख तत्त्व हैं-(1) आकस्मिकता, (2) आवश्यकता तथा
(3) तर्क।
आकस्मिकता इतिहास का वह तत्त्व है
जो इतिहास की गति को आशा के विपरीत अकस्मात् प्रवाहित करता है। आवश्यकता
अनुसन्धान की जननी है। इतिहास की गति को आवश्यकताओं ने समय-समय पर नवीन मोड़ दिया
है। तीसरा तत्त्व तर्क है। मानवीय कार्यों के पीछे दीर्घकालीन परम्पराएँ
क्रियाशील रहती हैं। इस प्रकार विश्लेषणवादी दार्शनिक इतिहासकार ऐतिहासिक व्याख्या
में ऐतिहासिक साम्यवाद का प्रयोग करते हैं । इस प्रकार के तर्क दार्शनिकों को कुछ
नियमों के प्रतिपादन में सहायक होते हैं। आदर्शवादी दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिक तथा
ऐतिहासिक साम्यवाद इतिहास की व्याख्या का एक आधुनिकतम प्रयास है।
परिकल्पनात्मक इतिहास-दर्शन
दर्शन-परिकल्पनात्मक
इतिहास-दर्शन का जन्म प्लेटो तथा अरस्तू से माना जाता है।
परिकल्पनात्मक इतिहास से दार्शनिकों का अभिप्राय ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य
में इतिहास का विशेष अर्थ तथा लक्ष्य को ढूँढना है। यदि इतिहास की अपनी कोई गति, स्वर एवं लक्ष्य है, तो उसे प्रकाश में लाना
है। इन दार्शनिकों ने इतिहास की परियोजना को मानव-समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है।
इसका अभिप्राय यह है कि इतिहास में अन्तर्निहित परियोजना, लक्ष्य तथा विशेष अर्थ
होता है। ऐतिहासिक घटनाएँ इन्हीं के द्वारा नियन्त्रित होती रही हैं। इसलिए इन
परियोजनाओं तथा लक्ष्यों को मानवीय प्रयास भी नहीं रोक सकता है।
इतिहास की
धार्मिक अवधारणाएँ इन विचारों की पुष्टि करती हैं। यूनानी इतिहास की अवधारणा
चक्रात्मक है। इसके अनुसार मानवीय दु:ख तथा सुख चक्रात्मक परियोजना के अनुसार
नियन्त्रित होते रहते हैं। भारतीय अवधारणा के अनुसार समय-समय पर ईश्वर का अवतार
मनुष्य के दु:खों का अन्त करने के लिए और सुख की स्थापना के लिए होता है। अतः
इतिहास में ईश्वर का हस्तक्षेप अपरिहार्य है। ईसाई अवधारणा के अनुसार ऐतिहासिक
घटनाओं में ईश्वरीय इच्छा प्रधान होती है। इस्लामी अवधारणा ने भी ईश्वरीय इच्छा को
ही ऐतिहासिक घटनाओं में मान्यता प्रदान की है।
1. इब्नखल्दून-
इब्नखल्दून इस्लामी जगत के एक
निराले इतिहासकार थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही राजवंशों, साम्राज्यों तथा समाजों
की अवयवी व्याख्या की थी। उनके अनुसार इतिहास समाजों का जीवविज्ञान है। इसका कार्य
मृत समाज के शवों का वर्गीकरण, विश्लेषण, परीक्षण, उनके शारीरिक विधान का
निर्माण और वृद्धि की प्रक्रिया का अन्वेषण तथा अनुसन्धान और उनके विकास एवं विजय
की प्रवृत्तियों और नियमों का निर्धारण है। उनका मानवीय दृष्टिकोण बड़ा विशाल था।
वे दास-प्रथा,
परम्परागत शासन
पद्धति तथा व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध थे। सर्वप्रथम इब्नखल्दून ही एक ऐसे
इतिहासकार, विचारक तथा दार्शनिक थे
जिन्होंने किसी भी राष्ट्र के इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का
विश्लेषण किया था।
2. विको-
इटली के दार्शनिक
विको के अनुसार इतिहास का ज्ञान प्रकृति के ज्ञान से भिन्न है। प्रकृति
ईश्वर की रचना है,
अत: उसका ज्ञान
केवल ईश्वर को ही हो सकता है। इतिहास का रचयिता मनुष्य है, क्योंकि उसकी रचना उसने
स्वयं की है। अतएव मनुष्य प्रकृति की अपेक्षा इतिहास को अधिक स्पष्ट रूप से जान
सकता है। इतिहास आत्मप्रकाशकीय है। इतिहास मानव चेष्टा तथा चिन्तन का फल है।
इतिहास का अपना विशिष्ट अर्थ होता है जिसे बहिर्भूत प्रतिमानों की सहायता के बिना
प्रत्यक्ष अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। इतिहास वह प्रक्रिया है जो मानव द्वारा
भाषा, रूढ़ि, नियम, शासन आदि के सर्जन और
विकास में सन्निहित है। इतिहास का स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से निष्पन्न
है। मनुष्य स्वयं इतिहास का निर्माता है एवं उसकी प्रकृति में सर्वत्र मौलिक
समानता मिलती है। इतिहास में अक्षुण्णता और क्रम बना रहता है। बुद्ध प्रकाश
के अनुसार इतिहास-गति के दो पक्ष होते हैं-(1) कोर्स तथा (2) रिकोर्स। विको
के अनुसार प्राचीन काल कोर्स का युग था तथा मध्यकाल रिकोर्स का।
3. कांट-
जर्मनी के
दार्शनिक कांट के अनुसार इतिहास केवल तथ्यों का परिगणन अथवा घटना की तालिका
मात्र नहीं है। वह इससे अधिक विकास प्रक्रिया है। इतिहास दृश्य जगत से अन्तर्जगत
की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। मनुष्य का आन्तरिक तत्त्व बुद्धि है। अत:
इतिहास बुद्धिमत्ता की प्रगति भी है और उन्नति भी। इतिहास का मुख्य लक्ष्य मानव का
आत्मिक विकास और बौद्धिकता की उन्नति है। कांट नैतिकता के प्रति सचेत थे। नैतिकता
पर आधारित न होने के कारण सभी कुछ कृत्रिमता के आवरण में ढंका हुआ है।
4. हर्डर-
हर्डर ने मानवीय इतिहास की
व्याख्या मनुष्य तथा सौरमण्डल के परिप्रेक्ष्य में की है। हर्डर ने कहा है कि
मनुष्य ईश्वर की महत्त्वपूर्ण कृति है। वह बुद्धि में प्रखर होने के कारण सभी
जीवों में श्रेष्ठ है। मनुष्य केवल तर्कशील प्राणी ही नहीं है, बल्कि यह निश्चय करने
वाला तथा अनुभव करने वाला प्राणी भी है। इतिहासकार को मानव-अतीत के अन्दर जाकर
उसकी वास्तविकता का अनुभव करना चाहिए। हर्डर के अनुसार अनुभव को तर्क के ऊपर रखा
जाना चाहिए और इतिहास को समझने के लिए अन्तर्दृष्टि होनी चाहिए।
5. हीगेल-
प्रो. वाल्श के अनुसार हीगेल
को परिकल्पनात्मक दर्शन का संस्थापक कहा जा सकता है। उसका इतिहास-दर्शन मौलिक, गम्भीर एवं युगान्तकारी
है। हीगेल के अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु घटनाओं के भीतर
छिपी हुई कार्य- कारण प्रक्रिया की गवेषणा है। इतिहासकार केवल घटनाओं को निश्चित
नहीं करता, बल्कि आन्तरिक
प्रवृत्तियों को हृदयंगम करता है। कार्य-कारण की सूक्ष्म प्रक्रिया का जाल
सार्वभौम तथा विश्वव्यापी है । अत: इतिहास मानवता की सम्पूर्ण प्रगति का वृत्तान्त
है, बर्बरता से सभ्यता तक
समस्त विकास का कथानक है।
विश्व-इतिहास की
मुख्य प्रवृत्ति मानव स्वतन्त्रता का विकास है। मानव स्वतन्त्रता का अर्थ नैतिक
बुद्धि का प्रसार है। राष्ट्र नैतिक बुद्धि की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। चरम सत्य
विश्वात्मा है जिसके विशेष गुण विवेक और स्वातन्त्र्य होते हैं। विश्वात्मा की
अनुभूति ऐतिहासिक प्रक्रिया में होती है। इस प्रकार दर्शन का ऐतिहासिकरण करने का
श्रेय हीगेल को है। हीगेल के अनुसार प्रकृति की प्रक्रिया चक्रात्मक
है। इसमें तथ्यों की पुनरावृत्ति होती है। इसका स्वरूप एक-सा बना रहता है। प्रकृति
विकासशील नहीं है और न इसका इतिहास ही होता है। किन्तु इतिहास चक्रवत् नहीं, बल्कि रेखावत् होता है।
इसकी प्रवृत्तियों में नवीनता होती है। इतिहास-प्रक्रिया ईश्वरीय परियोजना है।
ऐतिहासिक विकास आकस्मिक नहीं, अपितु आवश्यकता
है।
हीगेल के इतिहास-दर्शन को
द्वन्द्वात्मक आदर्शवाद कहा जा सकता है। तार्किक प्रक्रिया के द्वन्द्वात्मक और
विरोधात्मक होने के कारण वाद, प्रतिवाद तथा
साम्यवाद का उद्भव होता है। इसमें एक विरोध स्थिति को जन्म देती है और उन दोनों के
संघर्ष से एक नवीन समन्वित स्थिति का जन्म होता है। हीगेल का इतिहास-दर्शन
तार्किक विचारों का एक सुन्दर समन्वय है।
6. सापेक्षवादी
आन्दोलन-
प्रकृति विज्ञान
के क्षेत्र में सापेक्षवाद एक दर्शन है, जिसका अभिप्राय प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को वैज्ञानिक विधा
द्वारा प्रकाश में लाना है। सापेक्षवाद दो बातों पर विशेष जोर देते हैं-तथ्यों का
संकलन तथा सामान्यीकरण सिद्धान्त के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन।
काम्टे इतिहास के क्षेत्र में
वैज्ञानिक विधा के प्रयोग के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार इतिहास एक सामाजिक
भौतिकशास्त्र है और वैज्ञानिक विधा के द्वारा ऐतिहासिक ज्ञान में अभिवृद्धि की जा
सकती है। सापेक्षवादियों के अनुसार ऐतिहासिक प्रक्रिया तथा प्राकृतिक प्रक्रिया
में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए इतिहास में सत्यान्वेषण के लिए वैज्ञानिक विधा का
प्रयोग अपेक्षित है।
7. कार्ल मार्क्स-
कार्ल मार्क्स का विचार केवल
परिकल्पनात्मक ही नहीं, अपितु
सापेक्षवादी सिद्धान्तों पर आधारित वैज्ञानिक भी था। कार्ल मार्क्स के
अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना आर्थिक कारणों के परिणामस्वरूप होती है। सामाजिक
परिवर्तन तथा राजनीतिक क्रान्तियाँ मनुष्य के मस्तिष्क की उपज न होकर उत्पादन तथा
वितरण की प्रक्रिया के बदलने से होती हैं।
मार्क्स के अनुसार प्रत्येक
अवस्था में एक अन्तर्द्वन्द्व रहता है। एक वर्ग उत्पादन में परिश्रम करता है तथा
दूसरा साधन सम्पन्नता के कारण अतिरिक्त धन का उपभोग करता है। मार्क्स के
अनुसार अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। उत्पीड़क तथा
उत्पीड़ित सदा एक विरोध की स्थिति में रहे हैं और निरन्तर संघर्ष करते रहे हैं
जिसका अन्त कभी समाज के क्रान्तिकारी पुनर्गठन से हुआ है, कभी दोनों वर्गों के समान
विनाश से। इस प्रकार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का निरूपण वर्ग-संघर्ष के इतिहास में
परिणत होता है।
8. स्पेंगलर-
स्पेंगलर के अनुसार इतिहास
संस्कृतियों की जीवन-लीला है। यह एक प्रकार का जीवनशास्त्र है जिसके नियम अटल तथा
अलंघ्य हैं। मानव समाज इन्हीं नियमों के अधीन है और मनुष्य उसमें परिवर्तन नहीं कर
सकता। स्पेंगलर का कहना है कि वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच
चुकी है। हम इसके भविष्य पर शोक प्रकट कर सकते हैं, परन्तु इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता
का भविष्य निराशापूर्ण है। इतिहास की गतिप्रधान प्रक्रिया और विश्व की परिवर्तनशील
चर्या के विषय में उनके विचार अत्यन्त मार्मिक और तलस्पर्शी हैं । स्पेंगलर के इस
स्वरूप-विवेचन में कुछ त्रुटियाँ भी हैं, तो भी उनकी कृति विचारवर्धक और भावोत्तेजक है।
9. टायनबी-
टायनबी ने विश्व संस्कृतियों का
अध्ययन करके इतिहास के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला है। उनके इतिहास-दर्शन का
मुख्य विषय संस्कृति और धर्म रहा है। उनके अनुसार विश्व-इतिहास का ढाँचा सभ्यताओं
और समाजों के सम्पर्क से निर्मित हुआ है। उनकी यह अवधारणा है कि समस्त विश्व का
एकीकरण धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमताओं का निराकरण इतिहास की प्रमुख
प्रवृत्तियाँ हैं। सर्जन ही सांस्कृतिक इतिहास की मूल प्रक्रिया है। समाज के
प्रवाहात्मक स्तर पर संस्कृति का सृजनात्मक स्तर पर आरोपित रहता है। इन दोनों के
संश्लेषण से ऐतिहासिक प्रक्रिया निष्पन्न होती है। ऐतिहासिक प्रक्रिया का अधिष्ठान
एक विशिष्ट संस्कृति से अनुप्राणित समाज होता है जिसे 'सभ्यता' कहते हैं। इतिहास
सभ्यताओं का होता है- यह कहकर टायनबी ने इतिहास में एक नवीन स्तर का
अन्वेषण कर इतिहास-दर्शन को नवीन प्रारूप दिया है।
आशा हैं कि हमारे
द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो
इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।



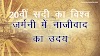











0 Comments