ऐतिहासिक लेखों के लिए दत्त संकलन के मुख्य
स्रोत
एक उत्तम शोध, जिसे पाण्डित्यपूर्ण अभिलेख कहा जा सकता है, को तैयार करना सरल कार्य नहीं है। इसको न केवल शोधार्थी की विद्वत्ता की तथा उसके द्वारा संगृहीत किये गये अधिकृत आँकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है अपितु विभिन्न स्रोतों को, शोध के द्वारा शोध-कार्य को उत्तम नमूना बनाने हेतु स्पष्ट करना आवश्यक होता है। कभी-कभी अधूरे प्रमाणों को बड़ी संख्या का उपयोग करना होता है जो कि एक किताब से प्राप्त नहीं होते। सम्पूर्ण सामग्री, जो एक विशेष काल के इतिहास के निर्माण में सहायक होती है, को स्रोत कहते हैं।
जी. आर. एल्टन उचित रूप से टिप्पणी
करते हैं, “ऐतिहासिक शोध कभी भी, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, विशिष्ट
प्रश्नों, विविध साक्ष्यों के माध्यम से समाधान नहीं होता। वरन् यह किन्हीं विशिष्ट खोज में
सम्पूर्णता के साथ सभी परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है। वास्तव में यह सिद्धान्त
उन विशिष्ट खतरों के लिए सावधानी का सूचक है जो इतिहास में व्यक्तिगत साक्ष्यों के
चुनाव पर जोर देते है।“
ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-
(i)
प्राथमिक या प्रधान, एवं (ii) द्वितीयक या गौण या सहायक।
आँकड़ों का एक प्राथमिक स्रोत वह होता है
जिसे शोधार्थी या विद्वान स्वयं अपने प्रयासों से सृजित करता है। हम यह भी कह सकते
हैं कि प्राथमिक स्रोत मौलिक होते हैं। किसी भी शोधार्थी को योग्य
और विश्वसनीय इतिहासकार नहीं कहा जा सकता जब तक वह अपना कार्य प्राथमिक
स्रोत सामग्री की सहायता से नहीं करता। द्वितीयक स्रोतों के बारे में, हम
कह सकते हैं कि यह ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य हैं जो घटना घटित होने के समय उपस्थित
नहीं था। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा लिखे ग्रन्थ द्वितीयक स्रोत में रखे
जाते हैं। वस्तुतः द्वितीयक स्रोत का महत्त्व प्राथमिक स्रोत के
महत्त्व से कम नहीं होता।
प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों
के मध्य के अन्तर को स्पष्ट करते हुए विद्वान ए. मार्विक कहते हैं, "प्राथमिक स्रोत कच्चे माल की
तरह होता है जिसका उपयोग एक कुशल इतिहासकार, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना
में अधिक कर सकता है। सहायक अथवा द्वितीयक स्रोत की सम्बद्धता होती
है जो कि इतिहास की कृति,
अभिलेखों, लघु-शोधों या ग्रन्थों में व्यक्त होती
हैं जिसमें कि दोनों बुद्धिमान एवं सामान्य व्यक्ति आते हैं तथा इतिहासकार जो कि
एक नवीन विषय पर शोध करने का साहस कर रहे हैं अथवा अपने चुने हुए क्षेत्र में नवीन
खोजों से सम्पर्क बनाये रखे हुए हैं अथवा अपने सामान्य ऐतिहासिक ज्ञान को विस्तृत
करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कुछ चाहते हैं, सोच-समझकर
विचार करेंगे।"
 |
| ऐतिहासिक अनुसन्धान के स्रोत |
यह शोध के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि संगृहीत आँकड़ें प्राथमिक
हैं या द्वितीयक। कभी-कभी एक संगृहीत आँकड़ों को प्राथमिक और द्वितीयक
स्रोत के रूप में भी मान लिया जा सकता है। एक प्राथमिक सोत एक द्वितीयक स्रोत की
तरह उपयोग में लाया जा सकता है। सामान्यतया एक समाचार-पत्र को प्राथमिक स्रोत की
तरह मानते हैं लेकिन पत्र में दी गयी सूचना पूर्णतया प्राथमिक स्रोतों पर
आधारित नहीं होती हैं,
अत: व द्वितीयक स्रोत से सम्बन्धित होते हैं।
दत्त संकलन के
प्राथमिक स्रोत-
शोध या नधीन सिद्धान्त की
स्थापना की दृष्टि से,
प्राथमिक सोत द्वितीयक स्रोत
से अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह मौलिक विचार और तथ्य को
समावेशित करते हैं। सामान्यतः एक हस्तलिखित दस्तावेज, एक टंकित
दस्तावेज से अधिक विश्वसनीय माना जाता है जैसा कि यह शोधार्थी तथा घटना के
मध्य अन्तरंग सम्बन्धों को इंगित करते हैं अथवा दर्शाते हैं। लेकिन प्रो. मार्विक
इससे सहमत नहीं है वह लिखता है कि, कभी-कभी टंकित
दस्तावेज ज्यादा मूल्यवान होता है।
एक व्यक्ति द्वारा हस्तलिखित दस्तावेज प्रकाशित विवरण का
वास्तविक अभिलेख हो सकता है जो कि वास्तव में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है या एक
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखित कथन के विश्वास में एक अभिलेख है अथवा एक
सामूहिक निर्णय का अभिलेख है अथवा यह लेखक का पूर्ण खोज का अंश हो सकता है। ऐसी
दशा में, यह केवल कुछ निश्चित प्रश्नों का उत्तर देगा। यदि किसी को आवश्यकता है, तो
यह सरकारी योजना या व्यक्तिगत वाद-विवाद का निर्णयात्मक कथन है, तब
मुद्रित दस्तावेज,
प्राथमिक स्रोत से कहीं ज्यादा मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं।
वस्तुतः प्राथमिक स्रोत तथा द्वितीयक स्रोत
सामग्री के मध्य सीमा निर्धारित करने के लिए रेखा खींचना अत्यन्त कठिन है। कभी-कभी
यह इतनी धुंधली दिखायी देती है कि एक शोधार्थी को यह घोषणा करना मुश्किल हो
जाता है कि यह प्राथमिक है या द्वितीयक, लेकिन यह निश्चित है कि दोनों
स्रोत विशेष काल के इतिहास को स्थापित करने में एक विद्वान के लिए सहायक होते हैं।
एक जीवनी प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों ही हो सकती है जब इसे क्रमश: लेखक
के दर्शन के दृष्टिकोण से तथा काल की महत्त्वपूर्ण घटना के दृष्टिकोण से देखा
जाये। प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में निम्नलिखित स्रोत आते हैं-
1. समकालीन अभिलेख-
प्रो. गौसचाक लिखते हैं, "समकालीन अभिलेख ऐसा दस्तावेज है जिससे सम्बद्ध व्यक्ति को अपने कार्य-सम्पादन
के लिए अनुदेश दिये जाते हैं अथवा व्यक्तियों को, जो सम्पादन में
सम्मिलित हैं,
स्मृति को सहायता प्राप्त होती है।" एक नियुक्ति पत्र, युद्ध-क्षेत्र
पर दिया गया एक आदेश,
विदेश कार्यालय से एक राजदूत के लिए निर्देश आदि एक शोधार्थी
के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं । सामान्यतया ये दस्तावेज निस्सन्देह
काफी विश्वसनीय होते हैं और इनमें त्रुटि की सम्भावना भी कम रहती है।
आशुलिपिक तथा ध्वनि सम्बन्धित अभिलेख
भी एक शोधार्थी के लिए महत्त्वपूर्ण शोध सामग्री होते हैं। यह अभिलेख बहुत महत्त्वपूर्ण
और बहुमूल्य हैं चूँकि वे हमें भावनात्मक तनावों की तह तक पहुंचाते हैं।
कानूनी तथा व्यापारिक कागज अथवा
दस्तावेज; जैसे जर्नल्स,
बिल्स् (bills), आदेश,कर-आदेश
आदि न केवल व्यवसाय-संघ की कार्य-प्रणाली की तह तक पहुँचने की योग्यता प्रदान करते
हैं बल्कि उन व्यक्तियों से भी परिचित कराते हैं जो इन कार्यों में संलग्नित रहे
हैं। सामान्य तौर से,
कुछ विशेषज्ञों द्वारा ये दस्तावेज तैयार किये गये हैं अतः
वे अत्यधिक विश्वसनीय हैं और उनमें धोखे की सम्भावना अत्यन्त कम होती है।
कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत डायरी अथवा नोट-बुक को
लिखने की आदत को नियमित रूप से बनाये रखते हैं और ये उनमें रोजाना, अपनी
गतिविधियों को लिख लिया करते हैं। ये नोटबुक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी
विश्वसनीय अभिलेख होते हैं। इन व्यक्तिगत स्मरण-लेखों में पूर्व धारणा के कोई अवसर
नहीं हैं। अत: वे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं।
2. गोपनीय प्रतिवेदन-
गोपनीय प्रतिवेदन आम लोगों
के लिए कोई महत्त्व नहीं रखता। वे समकालीन अभिलेखों की तुलना में कम विश्वसनीय
होते हैं, क्योंकि वह घटना घटित हो जाने के उपरान्त लिखे गये हैं। व्यक्तिगत पत्र भी
इतिहास के भरोसेमन्द स्रोत होते हैं। ऐसे पत्र अत्यन्त नम्र तरीके से लिखे गये
होते हैं और वे पूर्णत: सम्मानित करने योग्य होते हैं। ये नये व्यक्ति को गुमराह
कर सकते हैं, जो पत्र-लेखन की कला से पूरी तरह अनभिज्ञ है। कभी-कभी पत्र सही सूचना नहीं देते, अत:
एक शोधार्थी को पत्र-लेखक के छिपे हुए अर्थ का पता लगाने के लिए गूढ़ता को
स्पष्ट करना पड़ता है। गोपनीय प्रतिवेदनों का प्रयोग ऐतिहासिक स्रोतों के
रूप में किये जाने से पूर्व इनकी विश्वसनीयता को परख लेना चाहिए।
3. सार्वजनिक प्रतिवेदन-
सार्वजनिक प्रतिवेदन गोपनीय
प्रतिवेदनों की तरह महत्त्वपूर्ण तथा विश्वसनीय नहीं होते। सार्वजनिक प्रतिवेदन
को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक में विश्वसनीयता
की भिन्न-भिन्न मात्रा होती है।
(क) समाचार-पत्र
एवं विज्ञप्ति- एक समाचार-पत्र अथवा विज्ञप्ति की विश्वसनीयता उस स्रोत पर आधारित होती है
जहाँ से वह प्रकाशित हुआ है। यदि एक समाचार-पत्र या जर्नल में कोई विशेष व्यक्तिगत
सूचना प्रकाशित हो जाती है तो यह विश्वसनीय नहीं होती और न ही महत्त्वपूर्ण
किन्तु आज इस क्षेत्र में विशेष संवाददाताओं के साथ-साथ कतिपय एजेन्सियाँ एवं
सिण्डीकेट कार्यरत हैं किन्तु यह भी सत्य है कि किसी प्रलोभन या दबाव के कारण
असत्य समाचार भी प्रकाशित कर दिये जाते हैं।
विज्ञप्ति की विश्वसनीयता समाचार
देने वाली एजेन्सी एवं प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र दोनों ही पर निर्भर करती
है। उन्नीसवीं शताब्दी तक,
विशेष संवाददाताओं को नियुक्तियाँ प्रारम्भ नहीं हुई थी, तब
ऐसी स्थिति में समाचार-पत्रों की विश्वसनीयता संदिग्ध रहती थी। अत: वर्तमान में
समाचार-पत्र तथा विज्ञप्तियाँ शोध-कार्य में महत्त्वपूर्ण हिस्सा लेती हैं।
(ख) संस्मरण तथा
आत्मकथाएँ- संस्मरण तथा आत्मकथाएँ भी
एक शोधार्थी के लिए स्रोत-सामग्री हैं। यद्यपि वे बहुत से व्यक्तियों द्वारा पढ़ी गयी
और प्रशंसित हुईं फिर भी वे बहुत विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। प्रायः संस्मरण तथा आत्मकथाएँ
प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने जीवनकाल के अन्तिम समय में लिखे जाते हैं। ऐसी अवस्था
में, लेखक की याददाश्त उतनी तीक्ष्ण नहीं होती जितनी उसकी पूर्व दिनों में होती थी।
अत: एक लेखक अपने जीवन की घटनाओं को कम होती हुई याददाश्त
के आधार पर लिखता है,
इसलिए उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है। कुछ आत्मकथाएँ तथा
संस्मरणों की,
उनको इन्हीं कमजोरियों के कारण दूसरे विद्वानों द्वारा
आलोचना तथा भर्त्सना की जाती है।
(ग) अधिकृत इतिहास- यह इतिहास पूर्णतया आधिकारिक रिकार्डो पर आधारित होता है। यह एक सार्वजनिक
प्रतिवेदन है जिसमें किसी सरकार या व्यावसायिक घराने से सम्बन्धित
महत्त्वपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन यह पूर्णतया विश्वसनीय
नहीं होते जैसा कि वे विद्वानों तथा इतिहासकारों द्वारा लिखे गये हैं। ऐसे विद्वान
सरकारी विभागों में कार्यरत होते हैं, अत: उनके लेखन का बड़ी
सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए।
अधिकृत विद्वानों द्वारा जो कुछ द्वितीय विश्व-युद्ध
अथवा भारत के राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में लिखा गया था, इन
स्रोतों के कोई परिणाम या निष्कर्ष निकालने से पूर्व इन्हें अच्छी तरह परखने की
जरूरत है क्योंकि ऐसे इतिहास लेखन के विद्वान किसी सिद्धान्त विशेष की स्थापना के
उद्देश्य से कुछ प्रतिकूल सूचनाओं को अपने तरीके से तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने
में संकोच नहीं करते।
4. प्रश्नावली विधि-
यह दत्त संकलन की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधि है। इस
विधि में, शोधार्थी विशेष विषय पर, सूचना तथा विचार या मत
प्राप्त करने हेतु शोध या योजना के विषय को दर्शाते हुए कुछ प्रश्न तैयार करता है।
प्रश्नावली शोधार्थी को सूचनाओं को संचित कोष प्रदान करते हैं। वह विश्लेषण करता
है और पाठकों के समक्ष अन्तिम कृति रखता है। निस्सन्देह दत्त संकलन के वास्ते यह
विधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन यह उन विद्वानों के लिए ही उपयोगी है जिसकी
पहुंच आलोचनात्मक है वरना शोधार्थी का सारा श्रम व्यर्थ जायेगा।
5. साक्षात्कार
व्यवस्था-
प्रश्नावली विधि के अलावा, शोधार्थी
तत्कालीन अथवा प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के साक्षात्कार द्वारा कुछ निश्चित
निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए साक्षात्कार व्यवस्था का सहारा लेता है। इस व्यवस्था
के द्वारा वह उपस्थित ज्ञान में कुछ नया जोड़ने की इच्छा रखता है। निस्संदेह, ऐसे
व्यक्तियों के साथ भेंट कर विचार-विमर्श करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसके लिए
अधिक धन तथा समय की आवश्यकता होती है। लेकिन
गम्भीर विद्वान कुछ नया खोजने के लिए कोई भी कसर न उठा रखने की कोशिश करता
है।
6. सरकारी दस्तावेज-
सरकारी दस्तावेज एक शोधार्थी
की योजना के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना देने में सहायक होते हैं। वे प्रायः अति
सम्मानित विद्वानों तथा इतिहासकारों द्वारा तैयार किये जाते हैं। इस श्रेणी में, जनगणना
प्रतिवेदन, वित्तीय अंकडे तथा राष्टीय एवं प्रादेशिक वार्षिकी को सम्मिलित करते हैं। इसकी
एकत्रित वर्तमान सूचना आने वाले कल के इतिहासकारों के लिए उपयोगी स्रोत सामग्री
होती है। वस्तुतः सरकार स्वयं को बदनाम नहीं करना चाहती और केवल उन सूचनाओं को
प्रदान करती है जोकि उनकी योजनाओं को प्रकाशित करते हैं और सारी सूचनाओं की जो कि
असफलताओं और कानूनी तौर से अधिकार छिन जाने अथवा गिरावट की ओर संकेत करते हैं, उपेक्षा
करते हैं। अत: शोधार्थी से तथ्य तथा आँकड़े छिपाने की पूरी सम्भावनाएँ रहती हैं।
7. जनमत अथवा लोकमत-
समाचार-पत्र भी दत्त संकलन के महत्त्वपूर्ण
स्रोत में से एक है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के इतिहासकार तथा विद्वान
अपने विचारों को सम्पादकीय,
भाषणों,पत्रों जो कि सम्पाक को लिखे जाते हैं तथा
पर्चे जो कि विद्वानों द्वारा पढ़े व समझे जाते हैं, लिखे जाते हैं। इसके
अतिरिक्त लोकमत चुनाव दत्त संग्रहण के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है लेकिन एक इतिहासकार
को सूचना की विश्वसनीयता के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह प्रायः
छल-कपट से भरी होती है। इन स्रोतों का सहारा लेने से पूर्व उसे कुछ दूसरे प्रमाणों
को जानकारी हेतु देखना चाहिए।
8. साहित्य-
तत्कालीन साहित्य भी शोधार्थी के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्रोत
सामग्री है। यह ठीक ही कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अत: एक
इतिहासकार साहित्य के द्वारा तत्कालीन समाज की सामाजिक दशा, रीति-रिवाज
और संस्कृति के बारे में जानने योग्य होते हैं लेकिन कुद इतिहासकार इस तथ्य से
सहमत नहीं हैं। वे विश्वास करते हैं कि इतिहास और साहित्य दोनों ही अलग-अलग
केन्द्र-बिन्दु होते हैं। इतिहास तथ्यों पर आधारित है, जबकि
साहित्य पूर्णतया उपन्यास या अवास्तविकता तथा कल्पना से भरा होता है।
अतः एक शोधार्थी यदि कोई साहित्यिक कृति तैयार कर
रहा है तो उसे बड़ी सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। इतिहासकार जिस युग विशेष का
अध्ययन कर रहा है वह उस युग के साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। फिर भी पूर्णतया
साहित्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रो. मार्विक कहते हैं, "इतिहासकारों को साहित्यिक कृतियों में उपलब्ध सूचनाओं का तब तक प्रयोग नहीं
करना चाहिए, जब तक अन्य स्रोतों से उसकी पुष्टि न हो जाये।"
9. लोकोक्तियाँ तथा
लोकगीत-
लोकोक्तियाँ तथा लोकगीत, कभी-कभी
एक महत्त्वपूर्ण स्रोत-सामग्री सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि वे कहानी के हीरो या
नायक की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं। उनका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन भी किया जाता
है। तथ्य तथा अवास्तविकता परस्पर इतनी घुल-मिल जाती है कि उन्हें एक-दूसरे से अलग
नहीं किया जा सकता है तथा एक तथा सही तस्वीर से पाठक अनभिज्ञ रहता है अतः इसका
उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिऐ पाठक को तथ्य तथा परिकलपना के बीच अन्तर
अवश्य ही कर लेना चाहिए;
जैसे- भारत में राजपूताना के नायक आल्हा-ऊदल की कथा।
दत्त संकलन के द्वितीयक स्रोत-
इन्हें सहायक अथवा गौण स्रोत भी कहते
हैं। ये भी एक शोधार्थी के लिए उसके शोध-कार्य को आगे बढ़ाने में मदद देते
हैं। वास्तव में द्वितीयक स्रोतों के अध्ययन के पश्चात् ही प्राथमिक
स्रोतों का उचित उपयोग कर सकते हैं। प्रो. गौसचाक के अनुसार द्वितीयक स्रोत
के निम्नांकित उपयोग है-
(अ) इनकी सहायता से अन्य सन्दर्भ ग्रन्थों का अध्ययन सुगम हो जाता है।
(ब) सहायक विवरणों में आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं।
(स) इसकी मदद से समस्याएँ सुलझायी जा सकती है।
(द) इनसे उद्धरणों को प्राप्त किया जा सकता है।
एक शोधार्थी को प्रत्येक उपलब्ध स्रोत का उपयोग करने
की आवश्यकता होती है। उसे उनके महत्त्व को समझे बिना उन्हें दौड़ना नहीं चाहिए।
वास्तव में शोध-कार्य घटनाओं की विस्तृत समालोचना चाहता है। अतः निर्णयात्मक
निष्कर्ष निकालने के लिए,
प्रत्येक स्रोत को भली-भाँति समझना और उसका विश्लेषण करना
चाहिए। इन स्रोतों के द्वारा ही आवश्यक साक्ष्यों तथा सन्दर्भो की प्राप्ति होती
है।
द्वितीयक स्रोतों की अपेक्षा
प्राथमिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं किन्तु कहीं-कहीं प्राथमिक स्रोतों
की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। अतः सम्बन्धित दस्तावेजों का अध्ययन बड़ी
सूक्ष्मता और बुद्धिमत्ता के साथ किया जाना चाहिए। चूँकि द्वितीयक स्रोत का
उद्गम प्राथमिक स्रोतों से हो है अतः द्वितीयक स्रोतों के आधार पर प्राथमिक
स्रोतों की पुष्टि की जाती है। उपरोक्त दोनों प्रकार की श्रेणियों के स्रोत
शोधकर्ता के लिए आवश्यक हैं और दोनों की पुष्टि अत्यन्त आवश्यक है ताकि प्रामाणिक
इतिहास की रचना हो सके।
ऐतिहासिक शोध का महत्त्व
ऐतिहासिक शोध एक अत्यन्त कठिन
कार्य है। इस उद्यम में समय का उपदी ही गर्ग होता बल्कि इसमें धैर्य और मेहनत की
आवश्यकता होती है। इसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता भी होती है और इस बात की सम्भावना
भी होती है कि अच्छे प्रयासों के बावजूद भी शोध में लगा श्रम व्यर्थ नहीं जाये। इस
बात में भी सन्देह नहीं होना चाहिए कि शोधार्थी नये परिणाम या नये विचार या
ज्ञान जोड़ने में सफल हो सकता है। प्रायः ये सभी समस्याएँ शोध-कार्य के मध्य में
ही शोधार्थी को उसके कार्य से अलग होने के लिए प्रेरित करती हैं। फिर भी
बहुत से उत्साही शोध विद्वान, संगठन तथा संस्थाएँ हैं जो इतिहास में शोध
पर अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं।
वस्तुतः इतिहास में शोध-कार्य को न तो कभी
हतोत्साहित किया गया और न ही उनके कार्य की गति में कमी आयी है। इतिहास में
विद्वानों की संख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और विद्वान, दिनों-दिन, ऐतिहासिक
शोध-कार्य में स्वयं को समर्पित करते जा रहे हैं। वे शोध-क्षेत्र में नयी तकनीक का
उपयोग कर रहे हैं। उनके विचार दिनों-दिन विश्लेषणात्मक तथा समालोचनात्मक
होते जा रहे हैं।
ऐतिहासिक शोध-कार्य की उपयोगिता तथा महत्ता को ध्यान में
रखते हुए, विद्वान इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐतिहासिक शोध-कार्य के कुछ महत्त्वपूर्ण
लाभ निम्नांकित हैं-
व्यक्तिगत उपयोग-
ऐतिहासिक शोध का बड़ा लाभ उनके
लिए है जिन्होंने अपनी वृत्ति अभी तक शुरू नहीं की है। अपना शोध-कार्य समाप्त करने
के पश्चात् और ऐतिहासिक शोध का कुछ अनुभव प्राप्त करने के उपरान्त, वे
किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वे अभिलेखागार
अथवा पुरातत्त्व विभाग आदि में नियुक्त हो सकते हैं। एक शोध डिग्री व्यक्ति को
प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ाती है। एक अच्छा शोध-कार्य एक अच्छे तथा योग्य शोधार्थी
को मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक सन्तुष्टि प्रदान करता है
प्रायः व्यक्तियों को तीन श्रेणियाँ होती हैं जो कि ऐतिहासिक
शोध-कार्य के लिए समर्पित हैं। पहली श्रेणी सीखने वालों की होती है।
निस्सन्देह, वे इतिहास लेखन में सकारात्मक योगदान नहीं बना पाते। उनका मुख्य उद्देश्य
डिग्री प्राप्त करना तथा कहीं भी रोजगार प्राप्त करना होता है।
विद्वानों की दूसरी श्रेणी उनकी होती है जो
घटनाओं तथा ऐतिहासिक शोध की प्रचुर जानकारी रखते हैं। वे कुछ इतिहास की अच्छी
किताबें भी लिख चुके हैं और शोध लेख भी लेकिन उन अभी भी अपने विचारों में आगे के
विकास की आवश्यकता है ताकि वे कुछ अधिक उच्च श्रेणी का योगदान दे सकें।
तीसरी श्रेणी उन विद्वानों
की है जो पूरी तरह से प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त हैं। उनके योगदान राष्ट्रीय
तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। उनकी धारणाएँ स्पष्ट हैं और उनको
पहुँच विश्लेषणात्मक तथा समालोचनात्मक है। उन्होंने विद्यमान ज्ञान में कुछ नया
जोड़ने तथा अपना नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने हेतु नवीन ग्रन्थ लिखे हैं।
राष्ट्र के लिए
लाभदायक-
विभिन्न ढंगों से ऐतिहासिक शोध के द्वारा
वास्तव में, समाज व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लाभ उठाता है। प्राचीन राष्ट्रों के इतिहास में
कई कड़ियाँ खो चुकी हैं। इन खाली स्थानों को केवल ऐतिहासिक शोधों से दूर किया जा
सकता है। राष्ट्र ऐतिहासिक शोध-कार्यों से लाभ प्राप्त करते हैं क्योंकि यह घटनाओं
के कालानुक्रम,वंशों तथा सभ्यताओं के उत्थान-पतन के बारे में सन्देहों को दूर करते हैं। इस
प्रकार एक राष्ट्र अपने उत्थान और पतन को स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है।
कुछ नयी खोजें ऐतिहासिक शोध के माध्यम से भी
होती हैं। इनमें से कुछ खोजें न केवल व्यक्तियों के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं
बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी होती हैं। सिन्धु घाटी सभ्यता (Indus Valley
Civilization) की खोज लोगों के पुराने विचारों को बदल चुकी है। अब
उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि भारतीय सभ्यता काफी पुरानी है, अभी
तक कुछ लोग सोचते थे कि भारतीय इतिहास में वैदिक युग सबसे प्राचीन था।
ऐतिहासिक शोध लोगों में फैली
हुई मिथ्या धारणाओं को भी दूर करता है। राज्यशाही राष्ट्रों, जिन्होंने
विभिन्न स्थानों पर औपनिवेशों तथा स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना की, उन
विशेष राष्ट्रों के सही इतिहास को वर्णित नहीं किया गया। उन्होंने यह धारणा
स्थापित की कि गुलाम राष्ट्रों की कोई अपनी संस्कृति या सभ्यता नहीं होती और उनकी
सांस्कृतिक विरासत का कोई मूल्य नहीं है। अतः उन्हें पढ़ाने-लिखाने तथा सभ्य बनाने
का उत्तरदायित्व श्वेत जाति के लोगों का है। शोधार्थी का कर्तव्य है कि वह
इन पुराने मतों को एक किनारे कर, वास्तव में क्या हुआ, एक स्पष्ट
तस्वीर प्रस्तुत करे।
सम्पूर्ण विश्व के
लिए उपयोगी-
ऐतिहासिक शोध विश्व के लिए
लाभप्रद है। ये शोध हमें पूर्व की संस्कृति तथा सभ्यता का ज्ञान करती हैं।
वे उनकी संस्कृति के सामान्य लक्षणों पर भी प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक शोध
राष्ट्रों के मध्य आपसी समझ विकसित करने में मदद देते हैं। संघर्ष के बहुत से कारण
होते हैं, जो कि विभिन्न बिन्दुओं पर राष्ट्रों को विभकत करते हैं, इन्हें
शोध के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
अत: केवल व्यक्ति या राष्ट्र बल्कि विश्व ऐतिहासिक
शोधों से लाभ उठाते हैं। ऐतिहासिक शोध दूसरे देश के साथ अपने सम्बन्धों की जानकारी
का लाभ भी प्रदान करते हैं और ऐतिहासिक शोधों से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय
सम्बन्ध प्रगाढ़ हो जाते हैं।
आशा है कि हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आई
होगी। यदि जानकारी आपको पसन्द आयी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करे।












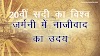


0 Comments